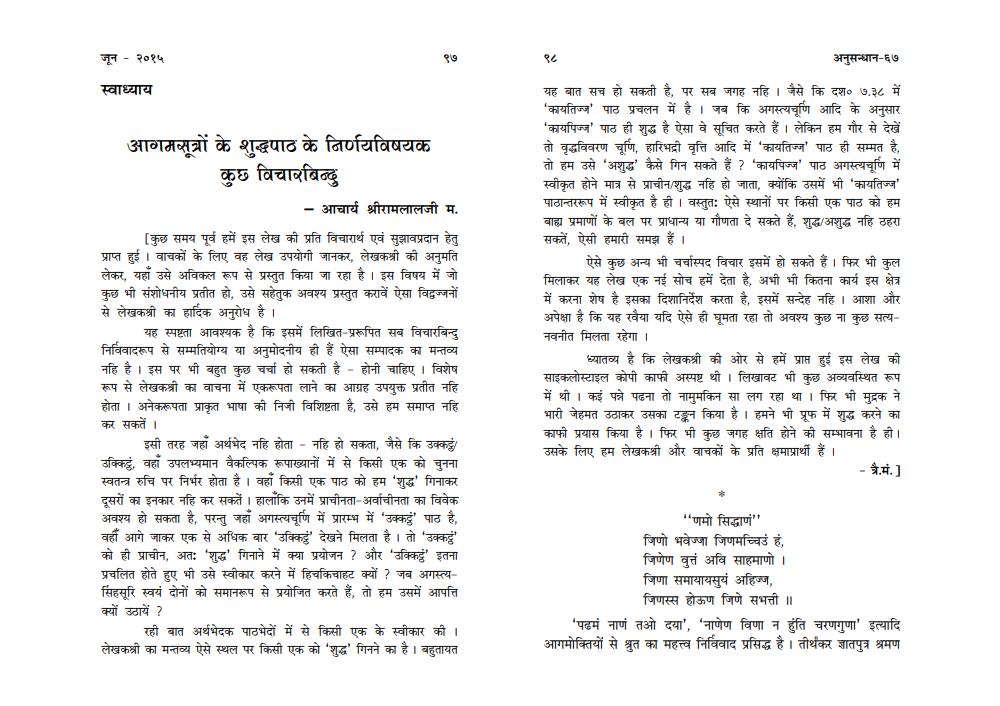________________
जून - २०१५
अनुसन्धान-६७
स्वाध्याय
आगमसूत्रों के शुद्धपाठ के निर्णयविषयक कुछ विचारबिन्दु
- आचार्य श्रीरामलालजी म. [कुछ समय पूर्व हमें इस लेख की प्रति विचारार्थ एवं सुझावप्रदान हेतु प्राप्त हुई । वाचकों के लिए वह लेख उपयोगी जानकर, लेखकश्री की अनुमति लेकर, यहाँ उसे अविकल रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है । इस विषय में जो कुछ भी संशोधनीय प्रतीत हो, उसे सहेतुक अवश्य प्रस्तुत करावें ऐसा विद्वज्जनों से लेखकश्री का हार्दिक अनुरोध है ।
यह स्पष्टता आवश्यक है कि इसमें लिखित प्ररूपित सब विचारबिन्दु निर्विवादरूप से सम्मतियोग्य या अनुमोदनीय ही हैं ऐसा सम्पादक का मन्तव्य नहि है । इस पर भी बहुत कुछ चर्चा हो सकती है - होनी चाहिए । विशेष रूप से लेखकत्री का वाचना में एकरूपता लाने का आग्रह उपयुक्त प्रतीत नहि होता । अनेकरूपता प्राकृत भाषा की निजी विशिष्टता है, उसे हम समाप्त नहि कर सकतें ।
इसी तरह जहाँ अर्थभेद नहि होता - नहि हो सकता, जैसे कि उक्कटुं उक्किटुं, वहाँ उपलभ्यमान वैकल्पिक रूपाख्यानों में से किसी एक को चुनना स्वतन्त्र रुचि पर निर्भर होता है। वहाँ किसी एक पाठ को हम 'शुद्ध' गिनाकर दूसरों का इनकार नहि कर सकतें । हालांकि उनमें प्राचीनता-अर्वाचीनता का विवेक अवश्य हो सकता है, परन्तु जहाँ अगस्त्यचूर्णि में प्रारम्भ में 'उक्कट्ठ' पाठ है, वहीं आगे जाकर एक से अधिक बार 'उक्किट्ठ' देखने मिलता है। तो 'उक्कट्ठ' को ही प्राचीन, अत: 'शुद्ध' गिनाने में क्या प्रयोजन ? और 'उक्किट्ठ' इतना प्रचलित होते हुए भी उसे स्वीकार करने में हिचकिचाहट क्यों ? जब अगस्त्यसिंहसूरि स्वयं दोनों को समानरूप से प्रयोजित करते हैं, तो हम उसमें आपत्ति क्यों उठायें ?
रही बात अर्थभेदक पाठभेदों में से किसी एक के स्वीकार की । लेखकत्री का मन्तव्य ऐसे स्थल पर किसी एक को 'शुद्ध' गिनने का है। बहुतायत
यह बात सच हो सकती है, पर सब जगह नहि । जैसे कि दश० ७.३८ में 'कायतिज्ज' पाठ प्रचलन में है । जब कि अगस्त्यचूणि आदि के अनुसार 'कायपिज्ज' पाठ ही शुद्ध है ऐसा वे सूचित करते हैं। लेकिन हम गौर से देखें तो वृद्धविवरण चूणि, हारिभद्री वृत्ति आदि में 'कायतिज्ज' पाठ ही सम्मत है, तो हम उसे 'अशुद्ध' कैसे गिन सकते हैं ? 'कायपिज्ज' पाठ अगस्त्यचूणि में स्वीकृत होने मात्र से प्राचीन/शुद्ध नहि हो जाता, क्योंकि उसमें भी 'कायतिज्ज' पाठान्तररूप में स्वीकृत है ही । वस्तुत: ऐसे स्थानों पर किसी एक पाठ को हम बाह्य प्रमाणों के बल पर प्राधान्य या गौणता दे सकते हैं, शुद्ध/अशुद्ध नहि ठहरा सकतें, ऐसी हमारी समझ हैं ।
ऐसे कुछ अन्य भी चर्चास्पद विचार इसमें हो सकते हैं। फिर भी कुल मिलाकर यह लेख एक नई सोच हमें देता है, अभी भी कितना कार्य इस क्षेत्र में करना शेष है इसका दिशानिर्देश करता है. इसमें सन्देह नहि । आशा और अपेक्षा है कि यह रवैया यदि ऐसे ही घूमता रहा तो अवश्य कुछ ना कुछ सत्यनवनीत मिलता रहेगा।
ध्यातव्य है कि लेखकश्री की ओर से हमें प्राप्त हुई इस लेख की साइकलोस्टाइल कोपी काफी अस्पष्ट थी । लिखावट भी कुछ अव्यवस्थित रूप में थी। कई पन्ने पढना तो नामुमकिन सा लग रहा था । फिर भी मुद्रक ने भारी जहमत उठाकर उसका टङ्कन किया है। हमने भी प्रूफ में शुद्ध करने का काफी प्रयास किया है। फिर भी कुछ जगह क्षति होने की सम्भावना है ही। उसके लिए हम लेखकत्री और वाचकों के प्रति क्षमाप्रार्थी हैं।
- त्रै.मं.]
"णमो सिद्धाणं" जिणो भवेज्जा जिणमच्चिउं हं, जिणेण वुत्तं अवि साहमाणो । जिणा समायायसुयं अहिज्ज,
जिणस्स होऊण जिणे सभत्ती ॥ 'पढमं नाणं तओ दया', 'नाणेण विणा न हंति चरणगणा' इत्यादि आगमोक्तियों से श्रुत का महत्त्व निर्विवाद प्रसिद्ध है। तीर्थकर ज्ञातपुत्र श्रमण