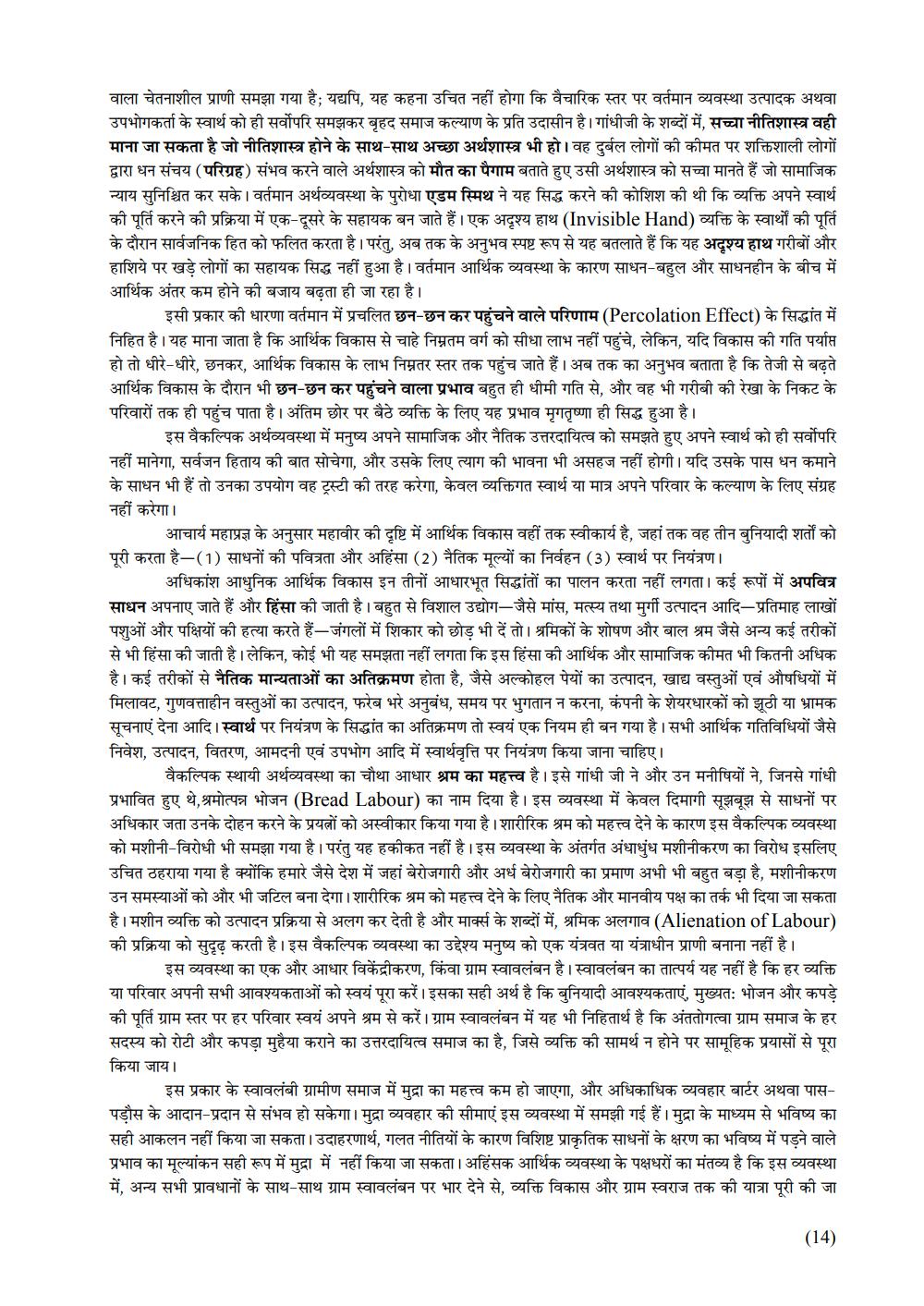________________
माहा
वाला चेतनाशील प्राणी समझा गया है। यद्यपि, यह कहना उचित नहीं होगा कि वैचारिक स्तर पर वर्तमान व्यवस्था उत्पादक अथवा उपभोगकर्ता के स्वार्थ को ही सर्वोपरि समझकर बृहद समाज कल्याण के प्रति उदासीन है। गांधीजी के शब्दों में, सच्चा नीतिशास्त्र वही माना जा सकता है जो नीतिशास्त्र होने के साथ-साथ अच्छा अर्थशास्त्र भी हो। वह दुर्बल लोगों की कीमत पर शक्तिशाली लोगों द्वारा धन संचय (परिग्रह) संभव करने वाले अर्थशास्त्र को मौत का पैगाम बताते हुए उसी अर्थशास्त्र को सच्चा मानते हैं जो सामाजिक न्याय सुनिश्चित कर सके। वर्तमान अर्थव्यवस्था के पुरोधा एडम स्मिथ ने यह सिद्ध करने की कोशिश की थी कि व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति करने की प्रक्रिया में एक-दूसरे के सहायक बन जाते हैं। एक अदृश्य हाथ (Invisible Hand) व्यक्ति के स्वार्थों की पूर्ति के दौरान सार्वजनिक हित को फलित करता है। परंतु, अब तक के अनुभव स्पष्ट रूप से यह बतलाते हैं कि यह अदृश्य हाथ गरीबों और हाशिये पर खड़े लोगों का सहायक सिद्ध नहीं हुआ है। वर्तमान आर्थिक व्यवस्था के कारण साधन-बहुल और साधनहीन के बीच में आर्थिक अंतर कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है।
इसी प्रकार की धारणा वर्तमान में प्रचलित छन-छन कर पहुंचने वाले परिणाम (Percolation Effect) के सिद्धांत में निहित है। यह माना जाता है कि आर्थिक विकास से चाहे निम्नतम वर्ग को सीधा लाभ नहीं पहुंचे, लेकिन, यदि विकास की गति पर्याप्त हो तो धीरे-धीरे, छनकर, आर्थिक विकास के लाभ निम्नतर स्तर तक पहुंच जाते हैं। अब तक का अनुभव बताता है कि तेजी से बढ़ते आर्थिक विकास के दौरान भी छन-छन कर पहुंचने वाला प्रभाव बहुत ही धीमी गति से, और वह भी गरीबी की रेखा के निकट के परिवारों तक ही पहुंच पाता है। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए यह प्रभाव मृगतृष्णा ही सिद्ध हुआ है।
इस वैकल्पिक अर्थव्यवस्था में मनुष्य अपने सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व को समझते हुए अपने स्वार्थ को ही सर्वोपरि नहीं मानेगा, सर्वजन हिताय की बात सोचेगा, और उसके लिए त्याग की भावना भी असहज नहीं होगी। यदि उसके पास धन कमाने के साधन भी हैं तो उनका उपयोग वह ट्रस्टी की तरह करेगा, केवल व्यक्तिगत स्वार्थ या मात्र अपने परिवार के कल्याण के लिए संग्रह नहीं करेगा।
आचार्य महाप्रज्ञ के अनुसार महावीर की दृष्टि में आर्थिक विकास वहीं तक स्वीकार्य है, जहां तक वह तीन बुनियादी शर्तों को पूरी करता है-(1) साधनों की पवित्रता और अहिंसा (2) नैतिक मूल्यों का निर्वहन (3) स्वार्थ पर नियंत्रण।
अधिकांश आधुनिक आर्थिक विकास इन तीनों आधारभूत सिद्धांतों का पालन करता नहीं लगता। कई रूपों में अपवित्र साधन अपनाए जाते हैं और हिंसा की जाती है। बहुत से विशाल उद्योग-जैसे मांस, मत्स्य तथा मुर्गी उत्पादन आदि-प्रतिमाह लाखों पशुओं और पक्षियों की हत्या करते हैं-जंगलों में शिकार को छोड़ भी दें तो। श्रमिकों के शोषण और बाल श्रम जैसे अन्य कई तरीकों से भी हिंसा की जाती है। लेकिन, कोई भी यह समझता नहीं लगता कि इस हिंसा की आर्थिक और सामाजिक कीमत भी कितनी अधिक है। कई तरीकों से नैतिक मान्यताओं का अतिक्रमण होता है, जैसे अल्कोहल पेयों का उत्पादन, खाद्य वस्तुओं एवं औषधियों में मिलावट, गुणवत्ताहीन वस्तुओं का उत्पादन, फरेब भरे अनुबंध, समय पर भुगतान न करना, कंपनी के शेयरधारकों को झूठी या भ्रामक सूचनाएं देना आदि। स्वार्थ पर नियंत्रण के सिद्धांत का अतिक्रमण तो स्वयं एक नियम ही बन गया है। सभी आर्थिक गतिविधियों जैसे निवेश, उत्पादन, वितरण, आमदनी एवं उपभोग आदि में स्वार्थवृत्ति पर नियंत्रण किया जाना चाहिए।
वैकल्पिक स्थायी अर्थव्यवस्था का चौथा आधार श्रम का महत्त्व है। इसे गांधी जी ने और उन मनीषियों ने, जिनसे गांधी प्रभावित हुए थे,श्रमोत्पन्न भोजन (Bread Labour) का नाम दिया है। इस व्यवस्था में केवल दिमागी सूझबूझ से साधनों पर अधिकार जता उनके दोहन करने के प्रयत्नों को अस्वीकार किया गया है। शारीरिक श्रम को महत्त्व देने के कारण इस वैकल्पिक व्यवस्था को मशीनी-विरोधी भी समझा गया है। परंतु यह हकीकत नहीं है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अंधाधुंध मशीनीकरण का विरोध इसलिए उचित ठहराया गया है क्योंकि हमारे जैसे देश में जहां बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी का प्रमाण अभी भी बहुत बड़ा है, मशीनीकरण उन समस्याओं को और भी जटिल बना देगा। शारीरिक श्रम को महत्त्व देने के लिए नैतिक और मानवीय पक्ष का तर्क भी दिया जा सकता है। मशीन व्यक्ति को उत्पादन प्रक्रिया से अलग कर देती है और मार्क्स के शब्दों में, श्रमिक अलगाव (Alienation of Labour) की प्रक्रिया को सुदृढ़ करती है। इस वैकल्पिक व्यवस्था का उद्देश्य मनुष्य को एक यंत्रवत या यंत्राधीन प्राणी बनाना नहीं है।
इस व्यवस्था का एक और आधार विकेंद्रीकरण, किंवा ग्राम स्वावलंबन है। स्वावलंबन का तात्पर्य यह नहीं है कि हर व्यक्ति या परिवार अपनी सभी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करें। इसका सही अर्थ है कि बुनियादी आवश्यकताएं, मुख्यतः भोजन और कपड़े की पूर्ति ग्राम स्तर पर हर परिवार स्वयं अपने श्रम से करें। ग्राम स्वावलंबन में यह भी निहितार्थ है कि अंततोगत्वा ग्राम समाज के हर सदस्य को रोटी और कपड़ा मुहैया कराने का उत्तरदायित्व समाज का है, जिसे व्यक्ति की सामर्थ न होने पर सामूहिक प्रयासों से पूरा किया जाय।
इस प्रकार के स्वावलंबी ग्रामीण समाज में मुद्रा का महत्त्व कम हो जाएगा, और अधिकाधिक व्यवहार बार्टर अथवा पासपड़ौस के आदान-प्रदान से संभव हो सकेगा। मुद्रा व्यवहार की सीमाएं इस व्यवस्था में समझी गई हैं। मुद्रा के माध्यम से भविष्य का सही आकलन नहीं किया जा सकता। उदाहरणार्थ, गलत नीतियों के कारण विशिष्ट प्राकृतिक साधनों के क्षरण का भविष्य में पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन सही रूप में मुद्रा में नहीं किया जा सकता। अहिंसक आर्थिक व्यवस्था के पक्षधरों का मंतव्य है कि इस व्यवस्था में, अन्य सभी प्रावधानों के साथ-साथ ग्राम स्वावलंबन पर भार देने से, व्यक्ति विकास और ग्राम स्वराज तक की यात्रा पूरी की जा
(14)