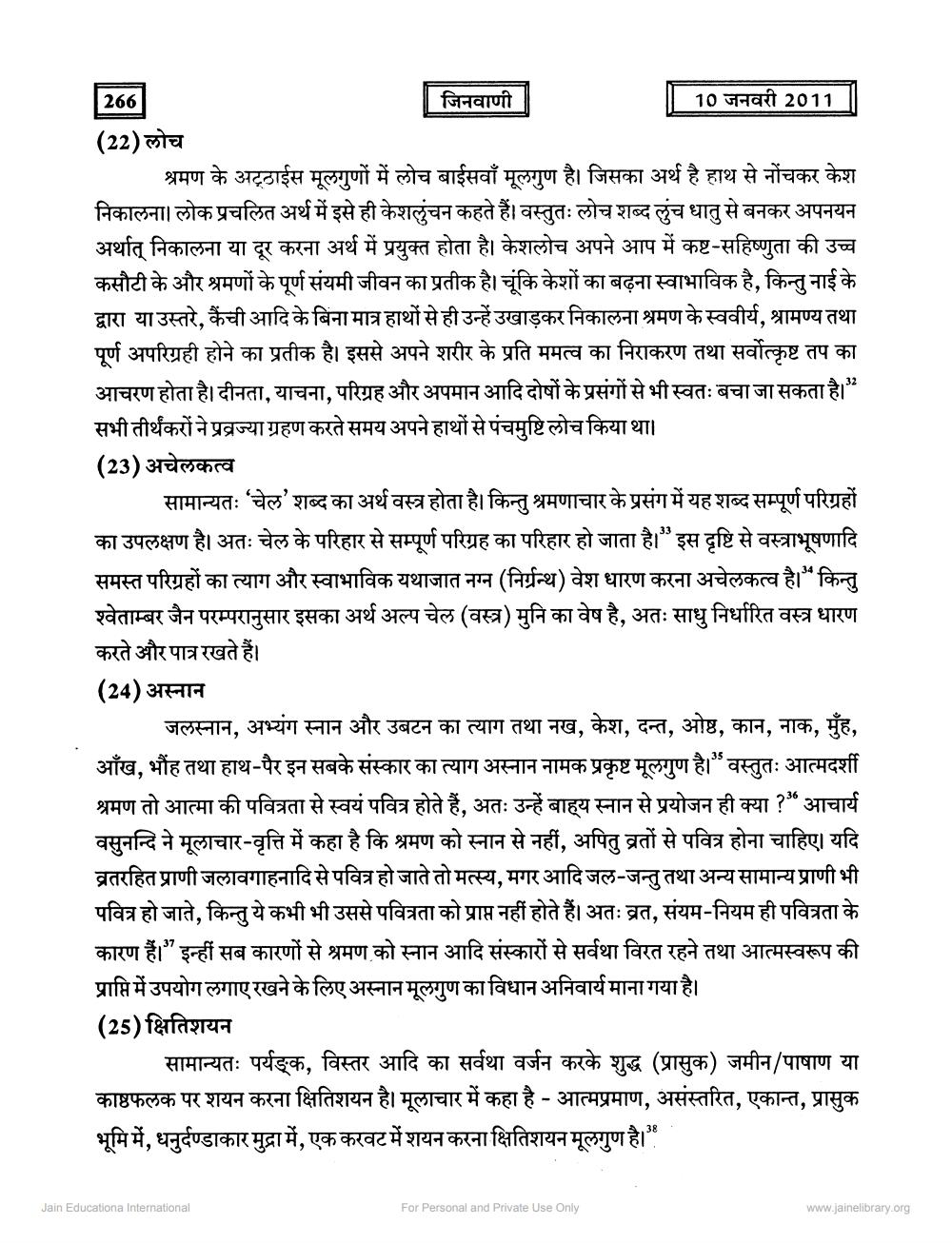________________
1266
| जिनवाणी
| 10 जनवरी 2011 (22) लोच
श्रमण के अट्ठाईस मूलगुणों में लोच बाईसवाँ मूलगुण है। जिसका अर्थ है हाथ से नोंचकर केश निकालना। लोक प्रचलित अर्थ में इसे ही केशलुंचन कहते हैं। वस्तुतः लोच शब्द लुंच धातु से बनकर अपनयन अर्थात् निकालना या दूर करना अर्थ में प्रयुक्त होता है। केशलोच अपने आप में कष्ट-सहिष्णुता की उच्च कसौटी के और श्रमणों के पूर्ण संयमी जीवन का प्रतीक है। चूंकि केशों का बढ़ना स्वाभाविक है, किन्तु नाई के द्वारा या उस्तरे, कैंची आदि के बिना मात्र हाथों से ही उन्हें उखाड़कर निकालना श्रमण के स्ववीर्य, श्रामण्य तथा पूर्ण अपरिग्रही होने का प्रतीक है। इससे अपने शरीर के प्रति ममत्व का निराकरण तथा सर्वोत्कृष्ट तप का आचरण होता है। दीनता, याचना, परिग्रह और अपमान आदि दोषों के प्रसंगों से भी स्वतः बचा जा सकता है।" सभी तीर्थंकरों ने प्रव्रज्या ग्रहण करते समय अपने हाथों से पंचमुष्टि लोच किया था। (23) अचेलकत्व
सामान्यतः 'चेल' शब्द का अर्थ वस्त्र होता है। किन्तु श्रमणाचार के प्रसंग में यह शब्द सम्पूर्ण परिग्रहों का उपलक्षण है। अतः चेल के परिहार से सम्पूर्ण परिग्रह का परिहार हो जाता है।" इस दृष्टि से वस्त्राभूषणादि समस्त परिग्रहों का त्याग और स्वाभाविक यथाजात नग्न (निर्ग्रन्थ) वेश धारण करना अचेलकत्व है। किन्तु श्वेताम्बर जैन परम्परानुसार इसका अर्थ अल्प चेल (वस्त्र) मुनि का वेष है, अतः साधु निर्धारित वस्त्र धारण करते और पात्र रखते हैं। (24) अस्नान
जलस्नान, अभ्यंग स्नान और उबटन का त्याग तथा नख, केश, दन्त, ओष्ठ, कान, नाक, मुँह, आँख, भौंह तथा हाथ-पैर इन सबके संस्कार का त्याग अस्नान नामक प्रकृष्ट मूलगुण है। वस्तुतः आत्मदर्शी श्रमण तो आत्मा की पवित्रता से स्वयं पवित्र होते हैं, अतः उन्हें बाह्य स्नान से प्रयोजन ही क्या ?" आचार्य वसुनन्दि ने मूलाचार-वृत्ति में कहा है कि श्रमण को स्नान से नहीं, अपितु व्रतों से पवित्र होना चाहिए। यदि व्रतरहित प्राणी जलावगाहनादिसे पवित्र हो जाते तो मत्स्य.मगर आदि जल-जन्त तथा अन्य सामान्य प्राणी भी पवित्र हो जाते, किन्तु ये कभी भी उससे पवित्रता को प्राप्त नहीं होते हैं। अतः व्रत, संयम-नियम ही पवित्रता के कारण हैं।” इन्हीं सब कारणों से श्रमण को स्नान आदि संस्कारों से सर्वथा विरत रहने तथा आत्मस्वरूप की प्राप्ति में उपयोग लगाए रखने के लिए अस्नान मूलगुण का विधान अनिवार्य माना गया है। (25) क्षितिशयन
सामान्यतः पर्यङ्क, विस्तर आदि का सर्वथा वर्जन करके शुद्ध (प्रासुक) जमीन/पाषाण या काष्ठफलक पर शयन करना क्षितिशयन है। मूलाचार में कहा है - आत्मप्रमाण, असंस्तरित, एकान्त, प्रासुक भूमि में, धनुर्दण्डाकार मुद्रा में, एक करवट में शयन करना क्षितिशयन मूलगुण है।"
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org