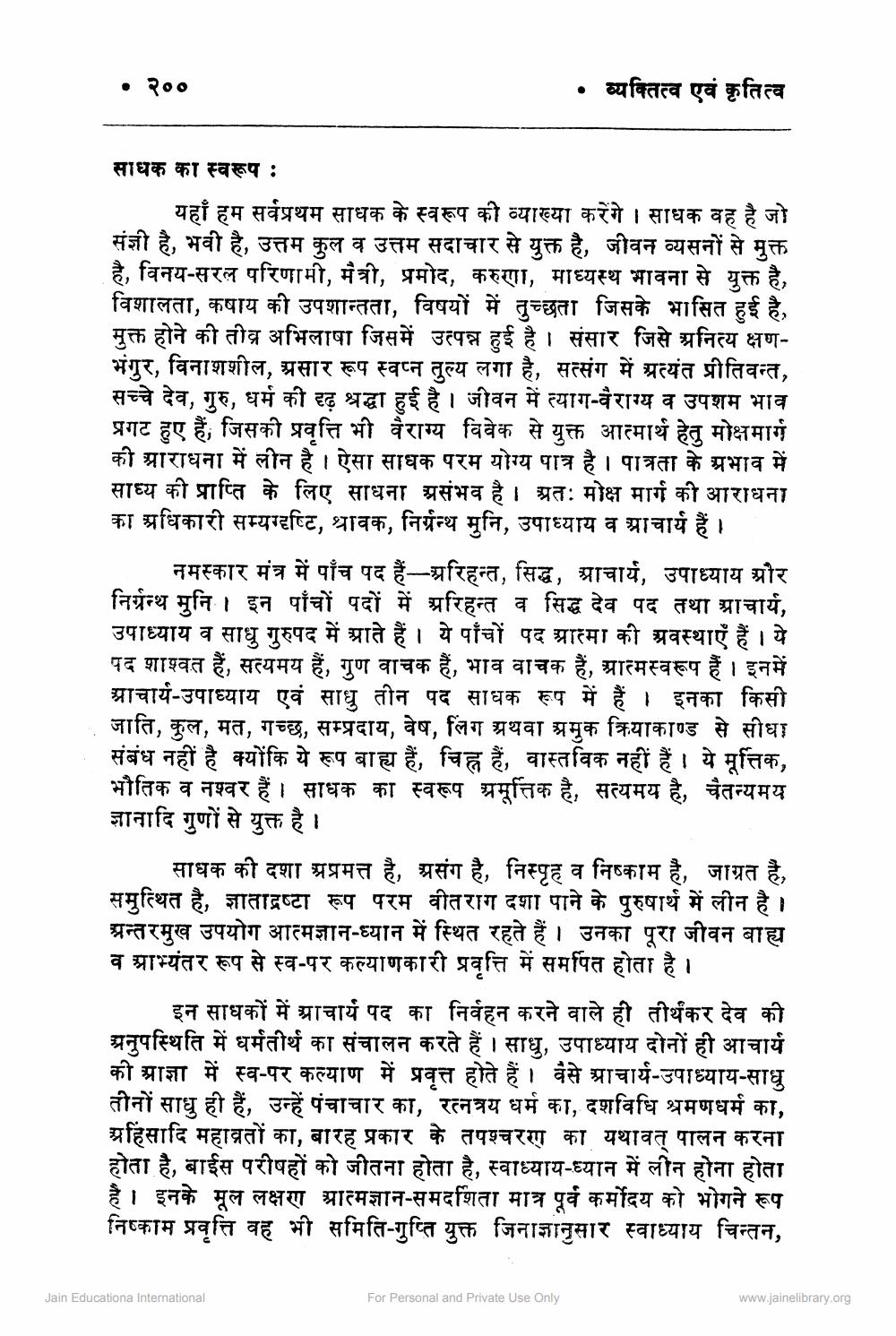________________
• २००
•
साधक का स्वरूप :
यहाँ हम सर्वप्रथम साधक के स्वरूप की व्याख्या करेंगे । साधक वह है जो संज्ञी है, भवी है, उत्तम कुल व उत्तम सदाचार से युक्त है, जीवन व्यसनों से मुक्त है, विनय सरल परिणामी, मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ भावना से युक्त है, विशालता, कषाय की उपशान्तता, विषयों में तुच्छता जिसके भासित हुई है, मुक्त होने की तीव्र अभिलाषा जिसमें उत्पन्न हुई है । संसार जिसे अनित्य क्षणभंगुर, विनाशशील, असार रूप स्वप्न तुल्य लगा है, सत्संग में अत्यंत प्रीतिवन्त, सच्चे देव, गुरु, धर्म की दृढ़ श्रद्धा हुई है। जीवन में त्याग वैराग्य व उपशम भाव प्रगट हुए हैं, जिसकी प्रवृत्ति भी वैराग्य विवेक से युक्त आत्मार्थ हेतु मोक्षमार्ग की आराधना में लीन है। ऐसा साधक परम योग्य पात्र है । पात्रता के अभाव में साध्य की प्राप्ति के लिए साधना असंभव है । अतः मोक्ष मार्ग की आराधना का अधिकारी सम्यग्दष्टि, श्रावक, निर्ग्रन्थ मुनि, उपाध्याय व प्राचार्य हैं ।
व्यक्तित्व एवं कृतित्व
नमस्कार मंत्र में पाँच पद हैं- अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और निर्ग्रन्थ मुनि । इन पाँचों पदों में अरिहन्त व सिद्ध देव पद तथा प्राचार्य, उपाध्याय व साधु गुरुपद में आते हैं । ये पाँचों पद प्रात्मा की अवस्थाएँ हैं । ये पद शाश्वत हैं, सत्यमय हैं, गुण वाचक हैं, भाव वाचक हैं, आत्मस्वरूप हैं । इनमें आचार्य - उपाध्याय एवं साधु तीन पद साधक रूप में हैं । इनका किसी जाति, कुल, मत, गच्छ, सम्प्रदाय, वेष, लिंग अथवा अमुक क्रियाकाण्ड से सीधा संबंध नहीं है क्योंकि ये रूप बाह्य हैं, चिह्न हैं, वास्तविक नहीं हैं । ये मूर्त्तिक, भौतिक व नश्वर हैं। साधक का स्वरूप श्रमूत्र्तिक है, सत्यमय है, चैतन्यमय ज्ञानादि गुणों से युक्त है ।
साधक की दशा अप्रमत्त है, असंग है, निस्पृह व निष्काम है, जाग्रत है, समुत्थित है, ज्ञाताद्रष्टा रूप परम वीतराग दशा पाने के पुरुषार्थ में लीन है । अन्तरमुख उपयोग आत्मज्ञान-ध्यान में स्थित रहते हैं । उनका पूरा जीवन बाह्य व आभ्यंतर रूप से स्व-पर कल्याणकारी प्रवृत्ति में समर्पित होता है ।
Jain Educationa International
इन साधकों में प्राचार्य पद का निर्वहन करने वाले ही तीर्थंकर देव की अनुपस्थिति में धर्मतीर्थ का संचालन करते हैं । साधु, उपाध्याय दोनों ही आचार्य की आज्ञा में स्व-पर कल्याण में प्रवृत्त होते हैं । वैसे प्राचार्य - उपाध्याय-साधु तीनों साधु ही हैं, उन्हें पंचाचार का, रत्नत्रय धर्म का, दशविधि श्रमणधर्म का,
हिंसादि महाव्रतों का, बारह प्रकार के तपश्चरण का यथावत् पालन करना होता है, बाईस परीषहों को जीतना होता है, स्वाध्याय-ध्यान में लीन होना होता है । इनके मूल लक्षण आत्मज्ञान-समदर्शिता मात्र पूर्व कर्मोदय को भोगने रूप निष्काम प्रवृत्ति वह भी समिति गुप्ति युक्त जिनाज्ञानुसार स्वाध्याय चिन्तन,
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org