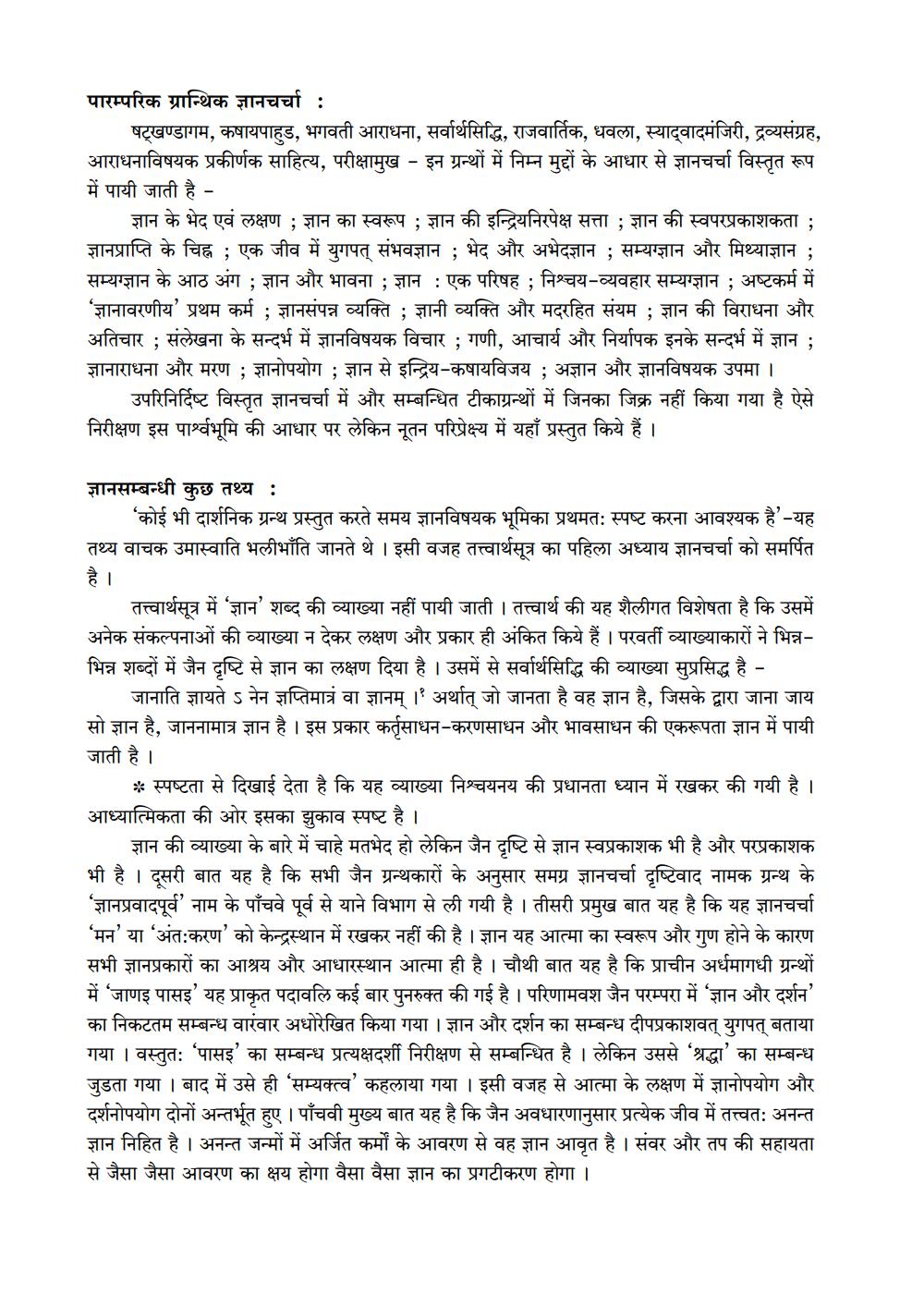________________
पारम्परिक ग्रान्थिक ज्ञानचर्चा :
षट्खण्डागम, कषायपाहुड, भगवती आराधना, सर्वार्थसिद्धि, राजवार्तिक, धवला, स्याद्वादमंजिरी, द्रव्यसंग्रह, आराधनाविषयक प्रकीर्णक साहित्य, परीक्षामुख इन ग्रन्थों में निम्न मुद्दों के आधार से ज्ञानचर्चा विस्तृत रूप में पायी जाती है
-
;
;
ज्ञान के भेद एवं लक्षण ज्ञान का स्वरूप; ज्ञान की इन्द्रियनिरपेक्ष सत्ता; ज्ञान की स्वपरप्रकाशकता; ज्ञानप्राप्ति के चिह्न ; एक जीव में युगपत् संभवज्ञान; भेद और अभेदज्ञान; सम्यग्ज्ञान और मिथ्याज्ञान; सम्यग्ज्ञान के आठ अंग ज्ञान और भावना; ज्ञान एक परिषह निश्चय व्यवहार सम्यग्ज्ञान अष्टकर्म में 'ज्ञानावरणीय' प्रथम कर्म ; ज्ञानसंपन्न व्यक्ति ; ज्ञानी व्यक्ति और मदरहित संयम ; ज्ञान की विराधना और अतिचार ; संलेखना के सन्दर्भ में ज्ञानविषयक विचार ; गणी, आचार्य और निर्यापक इनके सन्दर्भ में ज्ञान ; ज्ञानाराधना और मरण ; ज्ञानोपयोग ; ज्ञान से इन्द्रिय-कषायविजय ; अज्ञान और ज्ञानविषयक उपमा ।
;
;
उपरिनिर्दिष्ट विस्तृत ज्ञानचर्चा में और सम्बन्धित टीकाग्रन्थों में जिनका जिक्र नहीं किया गया है ऐसे निरीक्षण इस पार्श्वभूमि की आधार पर लेकिन नूतन परिप्रेक्ष्य में यहाँ प्रस्तुत किये हैं ।
ज्ञानसम्बन्धी कुछ तथ्य :
‘कोई भी दार्शनिक ग्रन्थ प्रस्तुत करते समय ज्ञानविषयक भूमिका प्रथमतः स्पष्ट करना आवश्यक है'-यह तथ्य वाचक उमास्वाति भलीभाँति जानते थे । इसी वजह तत्त्वार्थसूत्र का पहिला अध्याय ज्ञानचर्चा को समर्पित है ।
तत्त्वार्थसूत्र में 'ज्ञान' शब्द की व्याख्या नहीं पायी जाती । तत्त्वार्थ की यह शैलीगत विशेषता है कि उसमें अनेक संकल्पनाओं की व्याख्या न देकर लक्षण और प्रकार ही अंकित किये हैं । परवर्ती व्याख्याकारों ने भिन्नभिन्न शब्दों में जैन दृष्टि से ज्ञान का लक्षण दिया है । उसमें से सर्वार्थसिद्धि की व्याख्या सुप्रसिद्ध है
जानाति ज्ञायतेऽनेन ज्ञप्तिमात्रं वा ज्ञानम् ।' अर्थात् जो जानता है वह ज्ञान है, जिसके द्वारा जाना जाय सो ज्ञान है, जाननामात्र ज्ञान है । इस प्रकार कर्तृसाधन-करणसाधन और भावसाधन की एकरूपता ज्ञान में पाय जाती है ।
* स्पष्टता से दिखाई देता है कि यह व्याख्या निश्चयनय की प्रधानता ध्यान में रखकर की गयी है। आध्यात्मिकता की ओर इसका झुकाव स्पष्ट है।
T
ज्ञान की व्याख्या के बारे में चाहे मतभेद हो लेकिन जैन दृष्टि से ज्ञान स्वप्रकाशक भी है और परप्रकाशक भी है। दूसरी बात यह है कि सभी जैन ग्रन्थकारों के अनुसार समग्र ज्ञानचर्चा दृष्टिवाद नामक ग्रन्थ के 'ज्ञानप्रवादपूर्व' नाम के पाँचवे पूर्व से याने विभाग से ली गयी है । तीसरी प्रमुख बात यह है कि यह ज्ञानचर्चा 'मन' या 'अंत:करण' को केन्द्रस्थान में रखकर नहीं की है। ज्ञान यह आत्मा का स्वरूप और गुण होने के कारण सभी ज्ञानप्रकारों का आश्रय और आधारस्थान आत्मा ही है । चौथी बात यह है कि प्राचीन अर्धमागधी ग्रन्थ में 'जाणइ पासइ' यह प्राकृत पदावलि कई बार पुनरुक्त की गई है। परिणामवश जैन परम्परा में 'ज्ञान और दर्शन' का निकटतम सम्बन्ध वारंवार अधोरेखित किया गया । ज्ञान और दर्शन का सम्बन्ध दीपप्रकाशवत् युगपत् बताया गया । वस्तुतः 'पासइ' का सम्बन्ध प्रत्यक्षदर्शी निरीक्षण से सम्बन्धित है । लेकिन उससे 'श्रद्धा' का सम्बन्ध जुड़ता गया । बाद में उसे ही 'सम्यक्त्व' कहलाया गया । इसी वजह से आत्मा के लक्षण में ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग दोनों अन्तर्भूत हुए। पाँचवी मुख्य बात यह है कि जैन अवधारणानुसार प्रत्येक जीव में तत्त्वतः अनन्त ज्ञान निहित है । अनन्त जन्मों में अर्जित कर्मों के आवरण से वह ज्ञान आवृत है । संवर और तप की सहायता से जैसा जैसा आवरण का क्षय होगा वैसा वैसा ज्ञान का प्रगटीकरण होगा ।
1