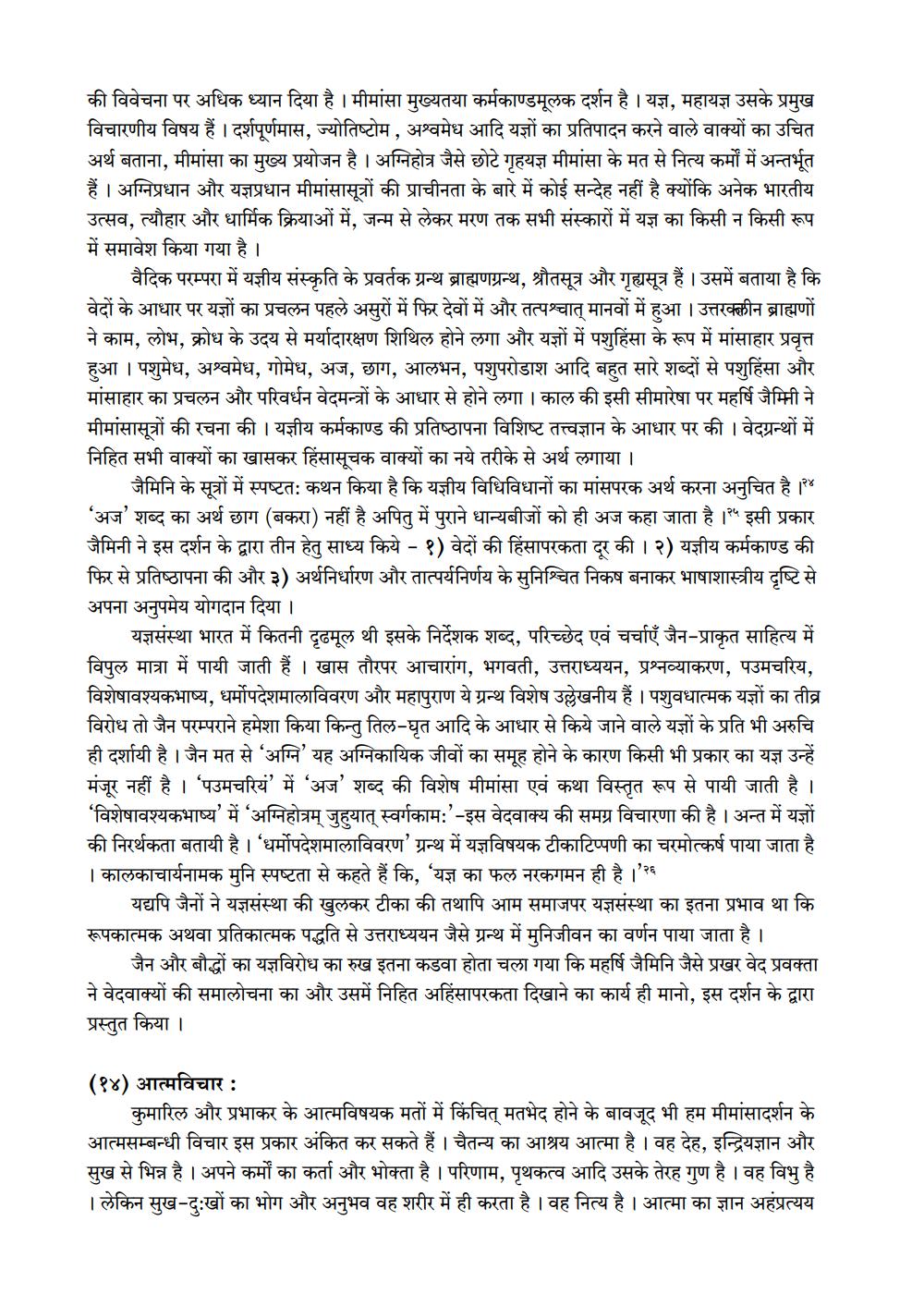________________
की विवेचना पर अधिक ध्यान दिया है । मीमांसा मुख्यतया कर्मकाण्डमूलक दर्शन है । यज्ञ, महायज्ञ उसके प्रमुख विचारणीय विषय हैं । दर्शपूर्णमास, ज्योतिष्टोम , अश्वमेध आदि यज्ञों का प्रतिपादन करने वाले वाक्यों का उचित अर्थ बताना, मीमांसा का मुख्य प्रयोजन है । अग्निहोत्र जैसे छोटे गृहयज्ञ मीमांसा के मत से नित्य कर्मों में अन्तर्भूत हैं । अग्निप्रधान और यज्ञप्रधान मीमांसासूत्रों की प्राचीनता के बारे में कोई सन्देह नहीं है क्योंकि अनेक भारतीय उत्सव, त्यौहार और धार्मिक क्रियाओं में, जन्म से लेकर मरण तक सभी संस्कारों में यज्ञ का किसी न किसी रूप में समावेश किया गया है।
__ वैदिक परम्परा में यज्ञीय संस्कृति के प्रवर्तक ग्रन्थ ब्राह्मणग्रन्थ, श्रौतसूत्र और गृह्यसूत्र हैं । उसमें बताया है कि वेदों के आधार पर यज्ञों का प्रचलन पहले असुरों में फिर देवों में और तत्पश्चात् मानवों में हुआ । उत्तरक्लीन ब्राह्मणों ने काम, लोभ, क्रोध के उदय से मर्यादारक्षण शिथिल होने लगा और यज्ञों में पशुहिंसा के रूप में मांसाहार प्रवृत्त हुआ । पशुमेध, अश्वमेध, गोमेध, अज, छाग, आलभन, पशुपरोडाश आदि बहुत सारे शब्दों से पशुहिंसा और मांसाहार का प्रचलन और परिवर्धन वेदमन्त्रों के आधार से होने लगा । काल की इसी सीमारेषा पर महर्षि जैमिमी ने मीमांसासूत्रों की रचना की । यज्ञीय कर्मकाण्ड की प्रतिष्ठापना विशिष्ट तत्त्वज्ञान के आधार पर की । वेदग्रन्थों में निहित सभी वाक्यों का खासकर हिंसासूचक वाक्यों का नये तरीके से अर्थ लगाया।
जैमिनि के सूत्रों में स्पष्टत: कथन किया है कि यज्ञीय विधिविधानों का मांसपरक अर्थ करना अनुचित है ।२४ 'अज' शब्द का अर्थ छाग (बकरा) नहीं है अपितु में पुराने धान्यबीजों को ही अज कहा जाता है ।२५ इसी प्रकार जैमिनी ने इस दर्शन के द्वारा तीन हेतु साध्य किये - १) वेदों की हिंसापरकता दूर की । २) यज्ञीय कर्मकाण्ड की फिर से प्रतिष्ठापना की और ३) अर्थनिर्धारण और तात्पर्यनिर्णय के सुनिश्चित निकष बनाकर भाषाशास्त्रीय दृष्टि से अपना अनुपमेय योगदान दिया।
यज्ञसंस्था भारत में कितनी दृढमूल थी इसके निर्देशक शब्द, परिच्छेद एवं चर्चाएँ जैन-प्राकृत साहित्य में विपुल मात्रा में पायी जाती हैं । खास तौरपर आचारांग, भगवती, उत्तराध्ययन, प्रश्नव्याकरण, पउमचरिय, विशेषावश्यकभाष्य, धर्मोपदेशमालाविवरण और महापुराण ये ग्रन्थ विशेष उल्लेखनीय हैं । पशुवधात्मक यज्ञों का तीव्र विरोध तो जैन परम्पराने हमेशा किया किन्तु तिल-घृत आदि के आधार से किये जाने वाले यज्ञों के प्रति भी अरुचि ही दर्शायी है । जैन मत से 'अग्नि' यह अग्निकायिक जीवों का समूह होने के कारण किसी भी प्रकार का यज्ञ उन्हें मंजूर नहीं है । ‘पउमचरियं' में 'अज' शब्द की विशेष मीमांसा एवं कथा विस्तृत रूप से पायी जाती है । 'विशेषावश्यकभाष्य' में अग्निहोत्रम् जुहुयात् स्वर्गकाम:'-इस वेदवाक्य की समग्र विचारणा की है । अन्त में यज्ञों की निरर्थकता बतायी है। 'धर्मोपदेशमालाविवरण' ग्रन्थ में यज्ञविषयक टीकाटिप्पणी का चरमोत्कर्ष पाया जाता है । कालकाचार्यनामक मुनि स्पष्टता से कहते हैं कि, 'यज्ञ का फल नरकगमन ही है ।'२६
यद्यपि जैनों ने यज्ञसंस्था की खुलकर टीका की तथापि आम समाजपर यज्ञसंस्था का इतना प्रभाव था कि रूपकात्मक अथवा प्रतिकात्मक पद्धति से उत्तराध्ययन जैसे ग्रन्थ में मुनिजीवन का वर्णन पाया जाता है।
जैन और बौद्धों का यज्ञविरोध का रुख इतना कडवा होता चला गया कि महर्षि जैमिनि जैसे प्रखर वेद प्रवक्ता ने वेदवाक्यों की समालोचना का और उसमें निहित अहिंसापरकता दिखाने का कार्य ही मानो, इस दर्शन के द्वारा प्रस्तुत किया ।
(१४) आत्मविचार :
कुमारिल और प्रभाकर के आत्मविषयक मतों में किंचित् मतभेद होने के बावजूद भी हम मीमांसादर्शन के आत्मसम्बन्धी विचार इस प्रकार अंकित कर सकते हैं । चैतन्य का आश्रय आत्मा है । वह देह, इन्द्रियज्ञान और सुख से भिन्न है। अपने कर्मों का कर्ता और भोक्ता है । परिणाम, पृथकत्व आदि उसके तेरह गुण है । वह विभु है । लेकिन सुख-दुःखों का भोग और अनुभव वह शरीर में ही करता है । वह नित्य है । आत्मा का ज्ञान अहंप्रत्यय