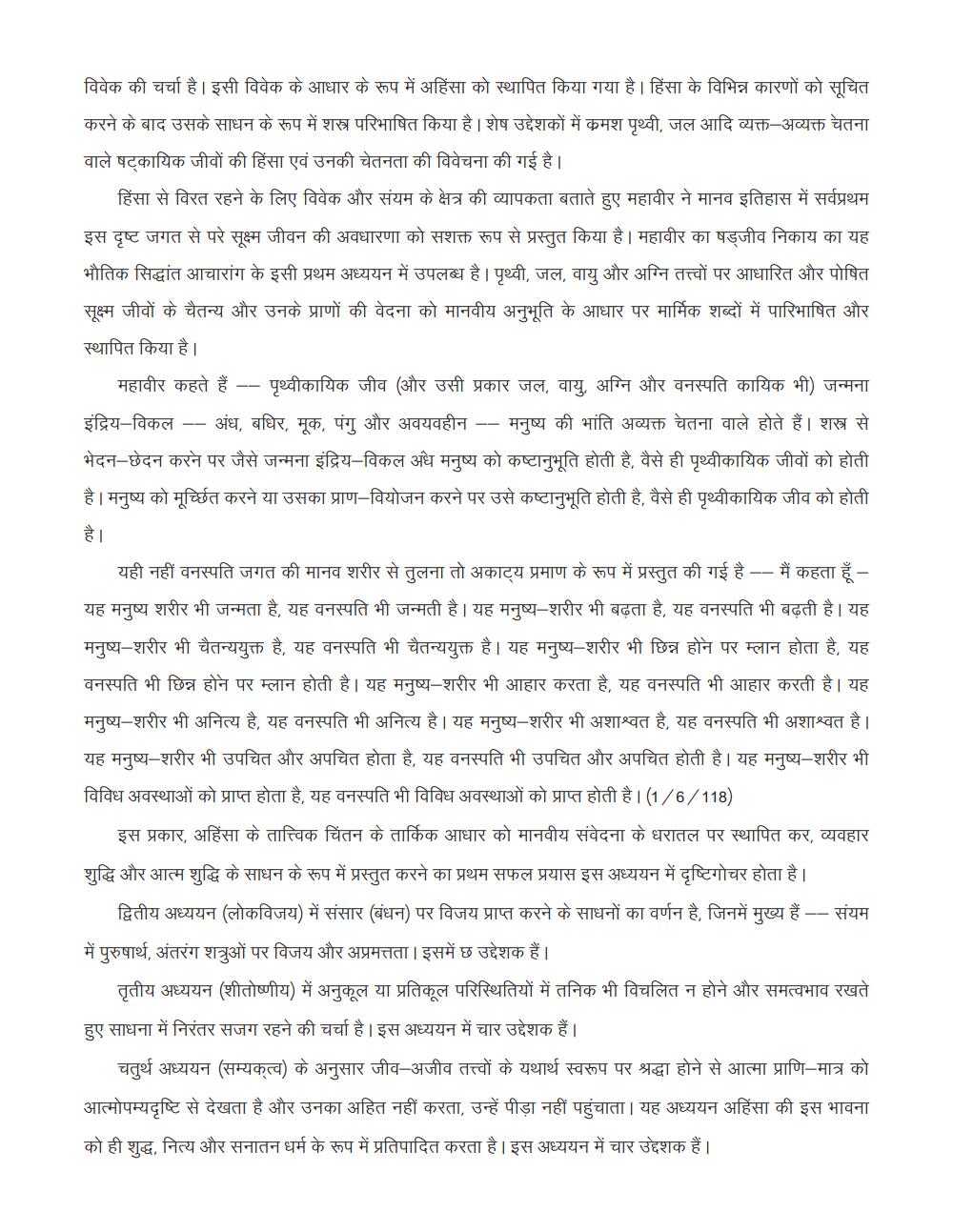________________
विवेक की चर्चा है। इसी विवेक के आधार के रूप में अहिंसा को स्थापित किया गया है। हिंसा के विभिन्न कारणों को सूचित करने के बाद उसके साधन के रूप में शस्त्र परिभाषित किया है। शेष उद्देशकों में क्रमश पृथ्वी, जल आदि व्यक्त-अव्यक्त चेतना वाले षट्कायिक जीवों की हिंसा एवं उनकी चेतनता की विवेचना की गई है।
हिंसा से विरत रहने के लिए विवेक और संयम के क्षेत्र की व्यापकता बताते हुए महावीर ने मानव इतिहास में सर्वप्रथम इस दृष्ट जगत से परे सूक्ष्म जीवन की अवधारणा को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया है। महावीर का षड्जीव निकाय का यह भौतिक सिद्धांत आचारांग के इसी प्रथम अध्ययन में उपलब्ध है। पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि तत्त्वों पर आधारित और पोषित सूक्ष्म जीवों के चैतन्य और उनके प्राणों की वेदना को मानवीय अनुभूति के आधार पर मार्मिक शब्दों में पारिभाषित और स्थापित किया है।
महावीर कहते हैं।
पृथ्वीकायिक जीव (और उसी प्रकार जल, वायु, अग्नि और वनस्पति कायिक भी) जन्मना अंध, बधिर, मूक, पंगु और अवयवहीन मनुष्य की भांति अव्यक्त चेतना वाले होते हैं। शस्त्र से भेदन-छेदन करने पर जैसे जन्मना इंद्रिय विकल अंध मनुष्य को कष्टानुभूति होती है, वैसे ही पृथ्वीकायिक जीवों को होती है। मनुष्य को मूर्च्छित करने या उसका प्राण- वियोजन करने पर उसे कष्टानुभूति होती है, वैसे ही पृथ्वीकायिक जीव को होती
है ।
इंद्रिय विकल
--
यही नहीं वनस्पति जगत की मानव शरीर से तुलना तो अकाट्य प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की गई है. मैं कहता हूँयह मनुष्य शरीर भी जन्मता है, यह वनस्पति भी जन्मती है । यह मनुष्य - शरीर भी बढ़ता है, यह वनस्पति भी बढ़ती है। यह मनुष्य-शरीर भी चैतन्ययुक्त है, यह वनस्पति भी चैतन्ययुक्त है । यह मनुष्य - शरीर भी छिन्न होने पर म्लान होता है, यह वनस्पति भी छिन्न होने पर म्लान होती है यह मनुष्य शरीर भी आहार करता है, यह वनस्पति भी आहार करती है। यह मनुष्य शरीर भी अनित्य है, यह वनस्पति भी अनित्य है यह मनुष्य शरीर भी अशाश्वत है, यह वनस्पति भी अशाश्वत है। यह मनुष्य - शरीर भी उपचित और अपचित होता है, यह वनस्पति भी उपचित और अपचित होती है। यह मनुष्य - शरीर भी विविध अवस्थाओं को प्राप्त होता है, यह वनस्पति भी विविध अवस्थाओं को प्राप्त होती है। (1/6/118)
इस प्रकार, अहिंसा के तात्त्विक चिंतन के तार्किक आधार को मानवीय संवेदना के धरातल पर स्थापित कर, व्यवहार शुद्धि और आत्म शुद्धि के साधन के रूप में प्रस्तुत करने का प्रथम सफल प्रयास इस अध्ययन में दृष्टिगोचर होता है।
द्वितीय अध्ययन (लोकविजय) में संसार (बंधन) पर विजय प्राप्त करने के साधनों का वर्णन है, जिनमें मुख्य हैं- संयम
-
――
में पुरुषार्थ, अंतरंग शत्रुओं पर विजय और अप्रमत्तता । इसमें छ उद्देशक हैं।
तृतीय अध्ययन (शीतोष्णीय) में अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में तनिक भी विचलित न होने और समत्वभाव रखते हुए साधना में निरंतर सजग रहने की चर्चा है । इस अध्ययन में चार उद्देशक हैं।
चतुर्थ अध्ययन (सम्यकृत्व) के अनुसार जीव अजीव तत्त्वों के यथार्थ स्वरूप पर श्रद्धा होने से आत्मा प्राणिमात्र को
आत्मोपम्यदृष्टि से देखता है और उनका अहित नहीं करता, उन्हें पीड़ा नहीं पहुंचाता। यह अध्ययन अहिंसा की इस भावना को ही शुद्ध, नित्य और सनातन धर्म के रूप में प्रतिपादित करता है। इस अध्ययन में चार उद्देशक हैं ।
-