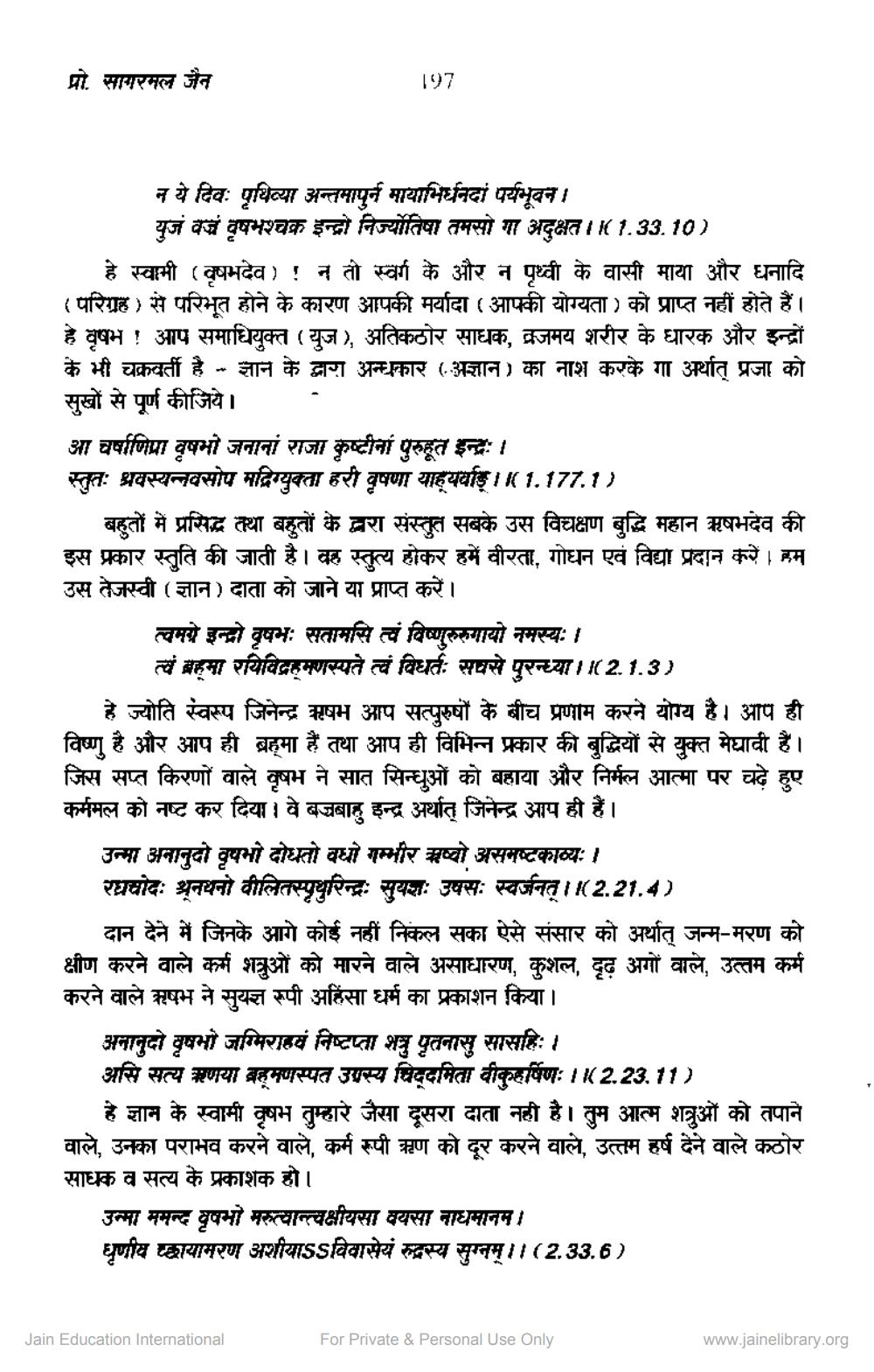________________ प्रो. सागरमल जैन 197 न ये दिवः पृथिव्या अन्तमापर्न मायाभिधनदां पर्यभूवन / युजं वजं वृषभश्चक्र इन्द्रो निज्योतिषा तमसो गा अदुक्षत / / 1.33. 10) हे स्वामी (वृषभदेव ) ! न तो स्वर्ग के और न पृथ्वी के वासी माया और धनादि ( परिग्रह ) से परिभूत होने के कारण आपकी मर्यादा ( आपकी योग्यता) को प्राप्त नहीं होते हैं। हे वृषभ ! आप समाधियुक्त (युज ), अतिकठोर साधक, व्रजमय शरीर के धारक और इन्द्रों के भी चक्रवर्ती है - ज्ञान के द्वारा अन्धकार (अज्ञान) का नाश करके गा अर्थात् प्रजा को सुखों से पूर्ण कीजिये। आ वर्षाणिग्रा वृषभो जनानां राजा कृष्टीनां पुरुहूत इन्द्रः / स्तुतः अवस्यन्नवसोप मद्रिग्युक्ता हरी वृषणा याहयाङ्।। 1.177.1) बहुतों में प्रसिद्ध तथा बहुतों के द्वरा संस्तुत सबके उस विचक्षण बुद्धि महान ऋषभदेव की इस प्रकार स्तुति की जाती है। वह स्तुत्य होकर हमें वीरता, गोधन एवं विद्या प्रदान करें। हम उस तेजस्वी (ज्ञान) दाता को जाने या प्राप्त करें। त्वमग्रे इन्द्रो वृषभः सतामसि त्वं विष्णुललगायो नमस्यः / त्वं ब्रहमा रयिविद्रह्मणस्यते त्वं विधर्तः सघसे पुरन्ध्या। 2.1.3) हे ज्योति स्वरूप जिनेन्द्र ऋषभ आप सत्पुरुषों के बीच प्रणाम करने योग्य है। आप ही विष्णु है और आप ही ब्रह्मा हैं तथा आप ही विभिन्न प्रकार की बुद्धियों से युक्त मेघावी है। जिस सप्त किरणों वाले वृषभ ने सात सिन्धुओं को बहाया और निर्मल आत्मा पर चढ़े हुए कर्ममल को नष्ट कर दिया। वे बजबाहु इन्द्र अर्थात् जिनेन्द्र आय ही हैं। उन्मा अनानुदो वृषभो दोयतो वधो गम्भीर अष्वो असमष्टकाव्यः / रघचोदः श्रूनथनो वीलितस्पृथुरिन्द्रः सुयशः उपसः स्वर्जनत् / / 2.21.4) दान देने में जिनके आगे कोई नहीं निकल सका ऐसे संसार को अर्थात् जन्म-मरण को क्षीण करने वाले कर्म शत्रुओं को मारने वाले असाधारण, कुशल, दृढ़ अगों वाले, उत्तम कर्म करने वाले ऋषभ ने सुयज्ञ स्पी अहिंसा धर्म का प्रकाशन किया। अनानुदो वृषभो जग्मिराहवं निष्टप्ता शत्रु प्रतनासु सासहिः / असि सत्य ऋणया ब्रह्मणस्पत उपस्य चिदमिता वीकुहर्षिणः / / 2.23.11) हे ज्ञान के स्वामी कृषभ तुम्हारे जैसा दूसरा दाता नही है। तुम आत्म शत्रओं को तपाने वाले, उनका पराभव करने वाले, कर्म रूपी ऋण को दूर करने वाले, उत्तम हर्ष देने वाले कठोर साधक व सत्य के प्रकाशक हो। उन्मा ममन्द वृषभो मरुत्वान्त्वक्षीयसा वयसा नाधमानम। धृणीय छायामरण अशीयाsविवासेयं रुद्रस्य सुग्नम्।। (2.33.6) Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org