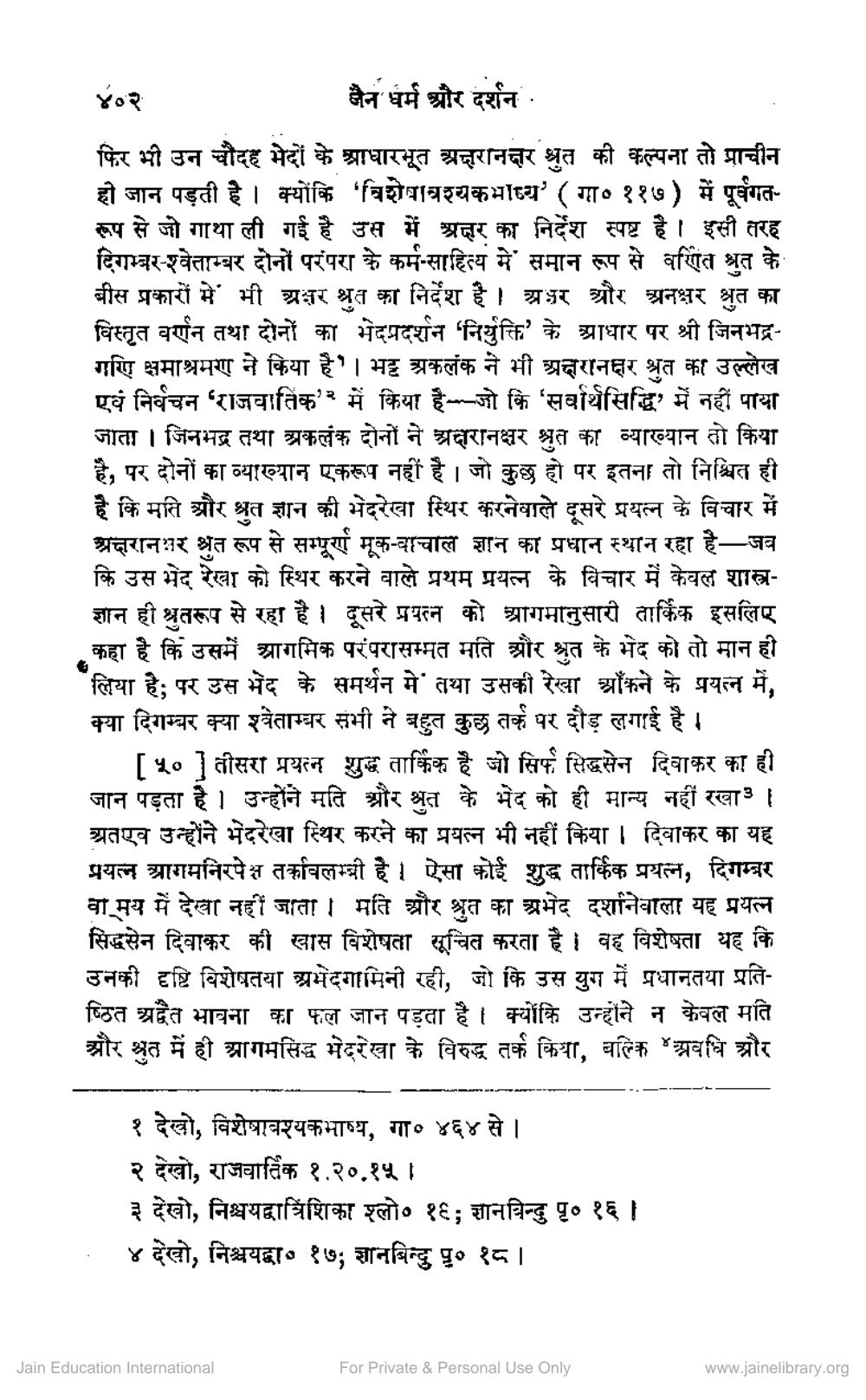________________
४०२
जैन धर्म और दर्शन
२
फिर भी उन चौदह भेदों के आधारभूत अक्षरानक्षर श्रुत की कल्पना तो प्राचीन हो जान पड़ती है । क्योंकि 'विशेषावश्यक माध्य' ( गा० ११७ ) में पूर्वगतरूप से जो गाथा ली गई है उस में अक्षर का निर्देश स्पष्ट है । इसी तरह दिगम्बर-श्वेताम्बर दोनों परंपरा के कर्म - साहित्य में समान रूप से वर्णित श्रुत के बीस प्रकारों में भी अक्षर श्रुत का निर्देश है । अर और अनक्षर श्रुत का विस्तृत वर्णन तथा दोनों का भेदप्रदर्शन 'नियुक्ति' के आधार पर श्री जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ने किया है' । भट्ट अकलंक ने भी अक्षरानक्षर श्रुत का उल्लेख एवं निर्वचन 'राजवातिक' में किया है - जो कि 'सर्वार्थसिद्धि' में नहीं पाया जाता । जिनभद्र तथा कलंक दोनों ने अक्षरानक्षर श्रुत का व्याख्यान तो किया है, पर दोनों का व्याख्यान एकरूप नहीं हैं । जो कुछ हो पर इतना तो निश्चित ही है कि मति और श्रुत ज्ञान की भेदरेखा स्थिर करनेवाले दूसरे प्रयत्न के विचार में अक्षरान र श्रुत रूप से सम्पूर्ण मूक - वाचाल ज्ञान का प्रधान स्थान रहा हैकि उस भेद रेखा को स्थिर करने वाले प्रथम प्रयत्न के विचार में केवल शास्त्रज्ञान ही श्रुतरूप से रहा है। दूसरे प्रयत्न को श्रागमानुसारी तार्किक इसलिए कहा है कि उसमें आगमिक परंपरासम्मत मति और श्रुत के भेद को तो मान ही लिया है; पर उस भेद के समर्थन में तथा उसकी रेखा आँकने के प्रयत्न में, क्या दिगम्बर क्या श्वेताम्बर सभी ने बहुत कुछ तर्क पर दौड़ लगाई है ।
I
—जब
6
[५० ] तीसरा प्रयत्न शुद्ध तार्किक है जो सिर्फ सिद्धसेन दिवाकर का ही जान पड़ता है । उन्होंने मति और श्रुत के भेद को ही मान्य नहीं रखा श्रतएव उन्होंने भेदरेखा स्थिर करने का प्रयत्न भी नहीं किया । दिवाकर का यह प्रयत्न श्रागमनिरपेक्ष तर्कावलम्बी है । ऐसा कोई शुद्ध तार्किक प्रयत्न, दिगम्बर वामय में देखा नहीं जाता। मति और श्रुत का भेद दर्शानेवाला यह प्रयत्न सिद्धसेन दिवाकर की खास विशेषता सूचित करता है । वह विशेषता यह कि उनकी दृष्टि विशेषतया श्रभेदगामिनी रही, जो कि उस युग में प्रधानतया प्रतिष्ठित द्वैत भावना का फल जान पड़ता है । क्योंकि उन्होंने न केवल मति और श्रुत में ही आगमसिद्ध भेदरेखा के विरुद्ध तर्क किया, बल्कि अवधि और
१ देखो, विशेषावश्यकभाष्य, गा० ४६४ से ।
२ देखो, राजवार्तिक १.२०.१५ ।
३] देखो, निश्चयद्वात्रिंशिका श्लो० १६; ज्ञानविन्दु पृ० १६ ।
४ देखो, निश्चयद्वा० १७; ज्ञानबिन्दु पृ० १८ |
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org