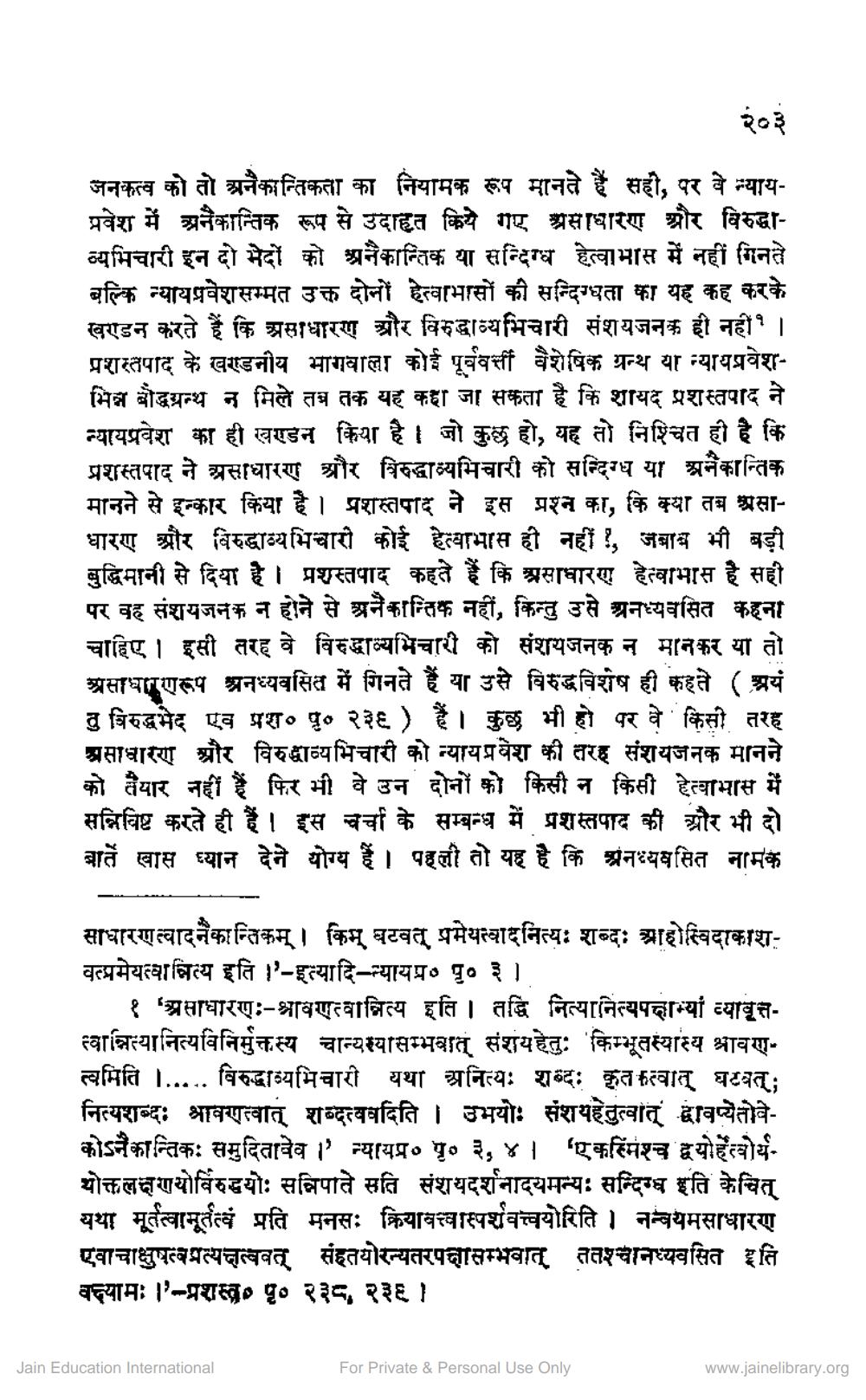________________
२०३
जनकत्व को तो नैकान्तिकता का नियामक रूप मानते हैं सही, पर वे न्यायप्रवेश में अनैकान्तिक रूप से उदाहृत किये गए असाधारण और विरुद्धाव्यभिचारी इन दो भेदों को श्रनैकान्तिक या सन्दिग्ध हेत्वाभास में नहीं गिनते बल्कि न्यायप्रवेशसम्मत उक्त दोनों हेत्वाभासों की सन्दिग्धता का यह कह कर के खण्डन करते हैं कि असाधारण और विरुद्धाव्यभिचारी संशयजनक ही नहीं ? | प्रशस्तपाद के खण्डनीय भागवाला कोई पूर्ववर्ती वैशेषिक ग्रन्थ या न्यायप्रवेशभिन्न बौद्धग्रन्थ न मिले तब तक यह कहा जा सकता है कि शायद प्रशस्तपाद ने न्यायप्रवेश का ही खण्डन किया है। जो कुछ हो, यह तो निश्चित ही है कि प्रशस्तपाद ने असाधारण और विरुद्धाव्यभिचारी को सन्दिग्ध या अनैकान्तिक मानने से इन्कार किया है । प्रशस्तपाद ने इस प्रश्न का, कि क्या तब असाधारण और विरुद्धाव्यभिचारी कोई हेत्वाभास ही नहीं ?, जबाब भी बड़ी बुद्धिमानी से दिया है । प्रशस्तपाद कहते हैं कि असाधारण हेत्वाभास है सही पर वह संशयजनक न होने से अनैकान्तिक नहीं, किन्तु उसे श्रनध्यवसित कहना चाहिए । इसी तरह वे विरुद्धाव्यभिचारी को संशयजनक न मानकर या तो श्रसाधातुरूप श्रनध्यवसित में गिनते हैं या उसे विरुद्धविशेष ही कहते ( श्रयं तु विरुद्धभेद एव प्रश० पृ० २३६ ) हैं । कुछ भी हो पर वे किसी तरह असाधारण और विरुद्धाव्यभिचारी को न्यायप्रवेश की तरह संशयजनक मानने को तैयार नहीं हैं फिर भी वे उन दोनों को किसी न किसी हेत्वाभास में सन्निविष्ट करते ही हैं । इस चर्चा के सम्बन्ध में प्रशस्तपाद की और भी दो बातें खास ध्यान देने योग्य हैं। पहली तो यह है कि श्रनध्यवसित नामक
साधारणत्वादनैकान्तिकम् । किम् बटवत् प्रमेयत्वादनित्यः शब्दः श्राहोस्विदाकाशवत्प्रमेयत्वानित्य इति । - इत्यादि-न्यायप्र० पृ० ३ ।
१ 'असाधारणः - श्रावणत्वान्नित्य इति । तद्धि नित्यानित्यपक्षाभ्यां व्यावृत्तत्वान्नित्यानित्यविनिर्मुक्तस्य चान्यस्यासम्भवात् संशयहेतुः किम्भूतस्यास्य श्रावणत्वमिति । ..... विरुद्धाव्यभिचारी यथा अनित्यः शब्दः कृतकत्वात् घटवत्; नित्यशब्दः श्रावणत्वात् शब्दत्ववदिति । उभयोः संशयहेतुत्वात् द्वावप्येतोवेकोकान्तिकः समुदितावेव । न्यायप्र० पृ० ३,४ । 'एकस्मिंश्च द्वयोर्हेोर्यथोक्तलक्षणयोर्विरुद्धयोः सन्निपाते सति संशयदर्शनादयमन्यः सन्दिग्ध इति केचित् यथा मूर्तत्वामूर्तत्वं प्रति मनसः क्रियावत्त्वास्पर्शवत्त्वयोरिति । नन्वयमसाधारण एवाचाक्षुषत्व प्रत्यक्षत्ववत् संहतयोरन्यतरपक्षासम्भवात् ततश्चानध्यवसित इति वक्ष्यामः ।'- प्रशस्त्र० पृ० २३८, २३६ ॥
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org