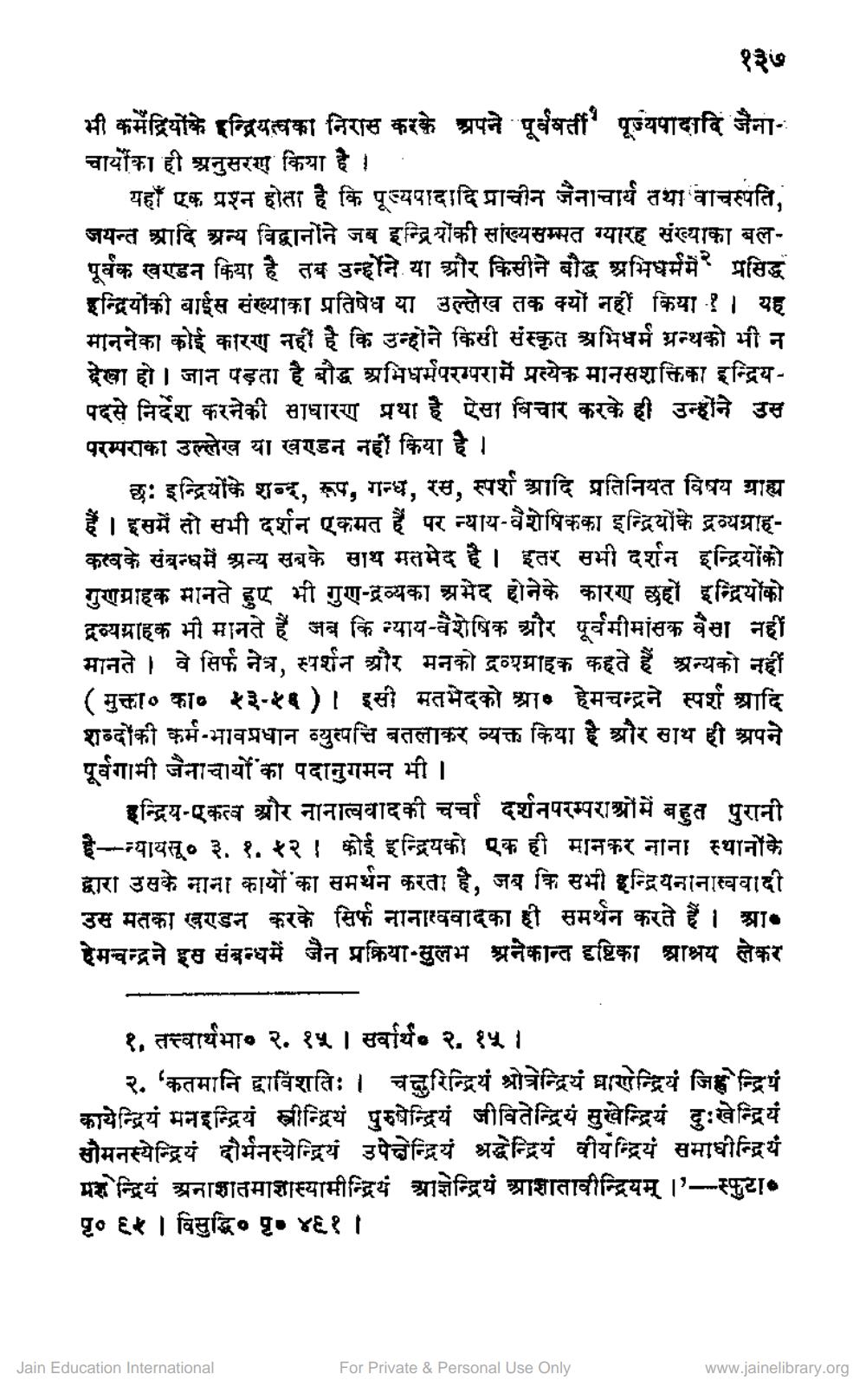________________
१३७ भी कर्मेंद्रियोंके इन्द्रियत्वका निरास करके अपने पूर्ववर्ती' पूज्यपादादि जैनाचार्योंका ही अनुसरण किया है ।
यहाँ एक प्रश्न होता है कि पूज्यपादादि प्राचीन जैनाचार्य तथा वाचस्पति, जयन्त प्रादि अन्य विद्वानोंने जब इन्द्रियोंकी सांख्यसम्मत ग्यारह संख्याका बलपूर्वक खण्डन किया है तब उन्होंने या और किसीने बौद्ध श्रभिधर्म में प्रसिद्ध इन्द्रियोंकी बाईस संख्याका प्रतिषेध या उल्लेख तक क्यों नहीं किया - १ | यह मानने का कोई कारण नहीं है कि उन्होंने किसी संस्कृत अभिधर्म ग्रन्थको भी न देखा हो । जान पड़ता है बौद्ध श्रभिधर्मपरम्परा में प्रत्येक मानसशक्तिका इन्द्रियपदसे निर्देश करनेकी साधारण प्रथा है ऐसा विचार करके ही उन्होंने उस परम्पराका उल्लेख या खण्डन नहीं किया है ।
छः इन्द्रियोंके शब्द, रूप, गन्ध, रस, स्पर्श आदि प्रतिनियत विषय ग्राह्य हैं। इसमें तो सभी दर्शन एकमत हैं पर न्याय-वैशेषिकका इन्द्रियोंके द्रव्यग्राहकरव के संबन्ध में अन्य सबके साथ मतभेद है । इतर सभी दर्शन इन्द्रियोंको गुणग्राहक मानते हुए भी गुण-द्रव्यका अभेद होनेके कारण छहों इन्द्रियोंको द्रव्यग्राहक भी मानते हैं जब कि न्याय-वैशेषिक और पूर्वमीमांसक वैसा नहीं मानते । वे सिर्फ नेत्र, स्पर्शन और मनको द्रव्यग्राहक कहते हैं अन्यको नहीं ( मुक्ता० का० २३-१६ ) । इसी मतभेदको श्रा० हेमचन्द्रने स्पर्श श्रादि शब्दों की कर्म - भावप्रधान व्युत्पत्ति बतलाकर व्यक्त किया है और साथ ही अपने पूर्वगामी जैनाचार्यों का पदानुगमन भी ।
इन्द्रिय- एकत्व और नानात्ववाद की चर्चा दर्शनपरम्पराओं में बहुत पुरानी - न्यायसू० ३ १.५२ । कोई इन्द्रियको एक ही मानकर नाना स्थानोंके द्वारा उसके नाना कार्यों का समर्थन करता है, जब कि सभी इन्द्रियनानास्ववादी उस मतका खण्डन करके सिर्फ नानाश्ववादका ही समर्थन करते हैं । श्र● हेमचन्द्र ने इस संबन्ध में जैन प्रक्रिया सुलभ श्रनेकान्त दृष्टिका श्राश्रय लेकर
१, तत्त्वार्थभा० २. १५ । सर्वार्थ २. १५ ।
२. ' कतमानि द्वाविंशतिः । चक्षुरिन्द्रियं श्रोत्रेन्द्रियं घ्राणेन्द्रियं जिह्न ेन्द्रियं कायेन्द्रियं मनइन्द्रियं स्त्रीन्द्रियं पुरुषेन्द्रियं जीवितेन्द्रियं सुखेन्द्रियं दुःखेन्द्रियं सौमनस्येन्द्रियं दौर्मनस्येन्द्रियं उपेक्षेन्द्रियं श्रद्धेन्द्रियं वीर्यन्द्रियं समाधीन्द्रियं मश ेन्द्रियं अनाशातमाज्ञास्यामीन्द्रियं श्रज्ञेन्द्रियं श्रज्ञातावीन्द्रियम् । 'स्फुटा पृ० ६५ । विसुद्धि० पृ० ४६१ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org