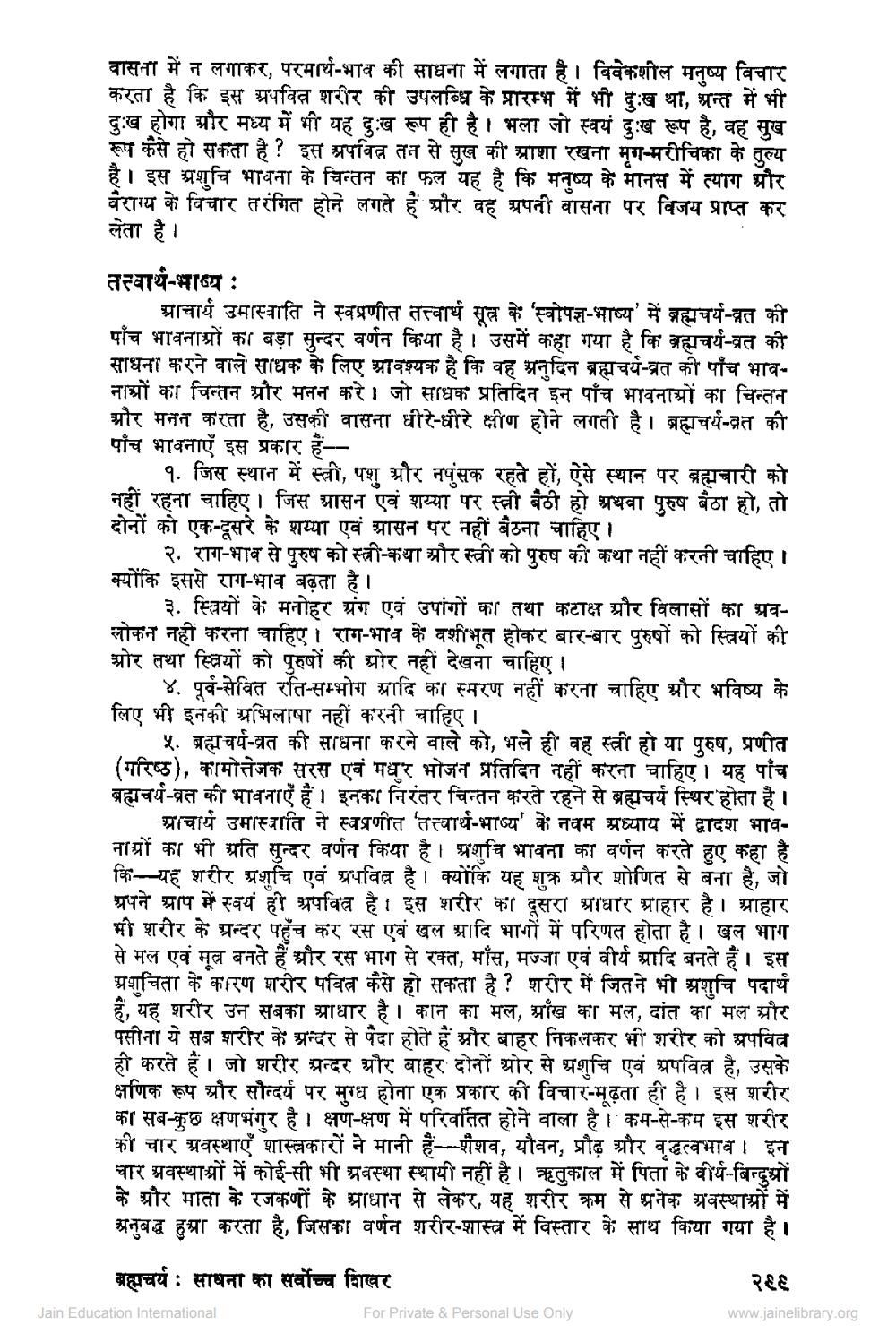________________
वासना में न लगाकर, परमार्थ-भाव की साधना में लगाता है। विवेकशील मनुष्य विचार करता है कि इस अपवित्र शरीर की उपलब्धि के प्रारम्भ में भी दुःख था, अन्त में भी दुःख होगा और मध्य में भी यह दुःख रूप ही है। भला जो स्वयं दुःख रूप है, वह सुख रूप कैसे हो सकता है ? इस अपवित्र तन से सुख की प्राशा रखना मृग-मरीचिका के तुल्य है। इस अशुचि भावना के चिन्तन का फल यह है कि मनुष्य के मानस में त्याग और वैराग्य के विचार तरंगित होने लगते हैं और वह अपनी वासना पर विजय प्राप्त कर लेता है।
तत्वार्थ-भाष्य: . प्राचार्य उमास्वाति ने स्वप्रणीत तत्त्वार्थ सूत्र के 'स्वोपज्ञ-भाष्य' में ब्रह्मचर्य-व्रत की पाँच भावनाओं का बड़ा सुन्दर वर्णन किया है। उसमें कहा गया है कि ब्रह्मचर्य-व्रत की साधना करने वाले साधक के लिए आवश्यक है कि वह अनुदिन ब्रह्मचर्य-व्रत की पाँच भावनाओं का चिन्तन और मनन करे। जो साधक प्रतिदिन इन पाँच भावनाओं का चिन्तन
और मनन करता है, उसकी वासना धीरे-धीरे क्षीण होने लगती है। ब्रह्मचर्य-व्रत की पाँच भावनाएँ इस प्रकार है
१. जिस स्थान में स्त्री, पशु और नपुंसक रहते हों, ऐसे स्थान पर ब्रह्मचारी को नहीं रहना चाहिए। जिस आसन एवं शय्या पर स्त्री बैठी हो अथवा पुरुष बैठा हो, तो दोनों को एक-दूसरे के शय्या एवं आसन पर नहीं बैठना चाहिए।
२. राग-भाव से पुरुष को स्त्री-कया और स्त्री को पुरुष की कथा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इससे राग-भाव बढ़ता है।
३. स्त्रियों के मनोहर अंग एवं उपांगों का तथा कटाक्ष और विलासों का अवलोकन नहीं करना चाहिए। राग-भाव के वशीभूत होकर बार-बार पुरुषों को स्त्रियों की ओर तथा स्त्रियों को पुरुषों की अोर नहीं देखना चाहिए।
४. पूर्व-सेवित रति-सम्भोग आदि का स्मरण नहीं करना चाहिए और भविष्य के लिए भी इनकी अभिलाषा नहीं करनी चाहिए।
५. ब्रह्मचर्य-व्रत की साधना करने वाले को, भले ही वह स्त्री हो या पुरुष, प्रणीत (गरिष्ठ), कामोत्तेजक सरस एवं मधुर भोजन प्रतिदिन नहीं करना चाहिए। यह पाँच ब्रह्मचर्य-व्रत की भावनाएं हैं। इनका निरंतर चिन्तन करते रहने से ब्रह्मचर्य स्थिर होता है।
प्राचार्य उमास्वाति ने स्वप्रणीत 'तत्त्वार्थ-भाष्य' के नवम अध्याय में द्वादश भावनाओं का भी अति सुन्दर वर्णन किया है। अशुचि भावना का वर्णन करते हुए कहा है कि यह शरीर अशुचि एवं अपवित्र है। क्योंकि यह शुक्र और शोणित से बना है, जो अपने आप में स्वयं ही अपवित्र है। इस शरीर का दूसरा प्राधार आहार है। आहार भी शरीर के अन्दर पहुँच कर रस एवं खल आदि भागों में परिणत होता है। खल भाग से मल एवं मूत्र बनते हैं और रस भाग से रक्त, मांस, मज्जा एवं वीर्य आदि बनते हैं। इस अशुचिता के कारण शरीर पवित्र कैसे हो सकता है? शरीर में जितने भी अशुचि पदार्थ है, यह शरीर उन सबका आधार है। कान का मल, आँख का मल, दांत का मल और पसीना ये सब शरीर के अन्दर से पैदा होते हैं और बाहर निकलकर भी शरीर को अपवित्र ही करते है। जो शरीर अन्दर और बाहर दोनों ओर से अशुचि एवं अपवित्र है, उसके क्षणिक रूप और सौन्दर्य पर मुग्ध होना एक प्रकार की विचार-मूढ़ता ही है। इस शरीर का सब-कुछ क्षणभंगुर है। क्षण-क्षण में परिवर्तित होने वाला है। कम-से-कम इस शरीर की चार अवस्थाएँ शास्त्रकारों ने मानी हैं-शैशव, यौवन, प्रौढ़ और वृद्धत्वभाव। इन चार अवस्थाओं में कोई-सी भी अवस्था स्थायी नहीं है। ऋतुकाल में पिता के वीर्य-बिन्दुओं के और माता के रजकणों के प्राधान से लेकर, यह शरीर क्रम से अनेक अवस्थाओं में अनुबद्ध हुआ करता है, जिसका वर्णन शरीर-शास्त्र में विस्तार के साथ किया गया है।
ब्रह्मचर्य : साधना का सर्वोच्च शिखर
२६६ www.jainelibrary.org
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only