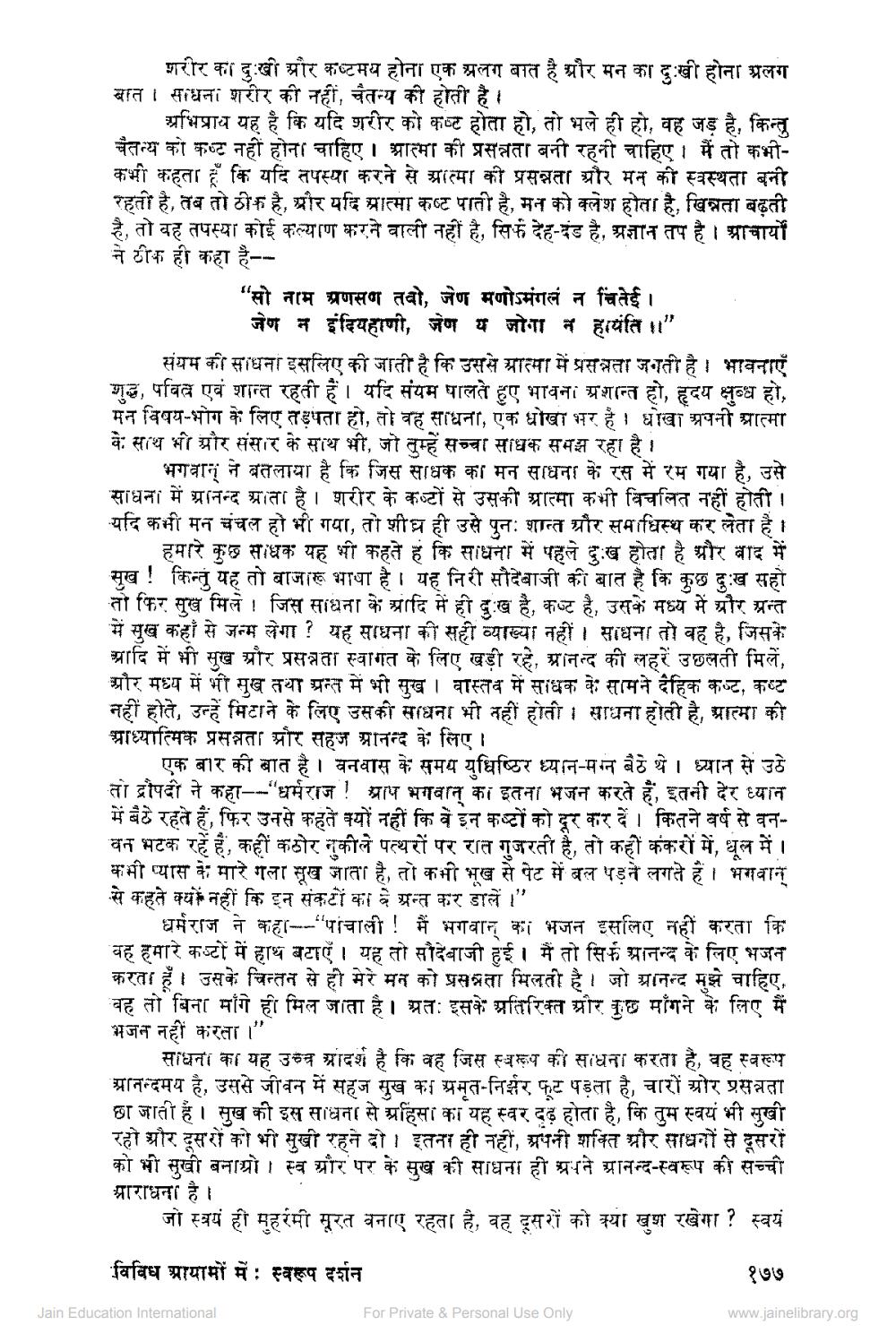________________
शरीर का दुःख और कष्टमय होना एक अलग बात है और मन का दुःखी होना अलग बात । साधना शरीर की नहीं, चैतन्य की होती है।
अभिप्राय यह है कि यदि शरीर को कष्ट होता हो, तो भले ही हो, वह जड़ है, किन्तु चैतन्य को कष्ट नहीं होना चाहिए। आत्मा की प्रसन्नता बनी रहनी चाहिए। मैं तो कभीकभी कहता हूँ कि यदि तपस्या करने से आत्मा की प्रसन्नता और मन की स्वस्थता बनी रहती है, तब तो ठीक है, और यदि श्रात्मा कष्ट पाती है, मन को क्लेश होता है, खिन्नता बढ़ती है, तो वह तपस्या कोई कल्याण करने वाली नहीं है, सिर्फ देह-दंड है, अज्ञान तप है। आचार्यो ने ठीक ही कहा है-
" सो नाम प्रणसण तवो, जेण मणोऽमंगलं न चितेई । जेण न इंदियहाणी, जेण य जोगा न हायंति ।। "
संयम की साधना इसलिए की जाती है कि उससे ग्रात्मा में प्रसन्नता जगती है । भावनाएँ शुद्ध, पवित्र एवं शान्त रहती हैं। यदि संयम पालते हुए भावना प्रशान्त हो, हृदय क्षुब्ध हो, मन विषय भोग के लिए तड़पता हो, तो वह साधना, एक धोखा भर हैं। धोखा अपनी आत्मा के साथ भी और संसार के साथ भी, जो तुम्हें सच्चा साधक समझ रहा है ।
भगवान् ने बतलाया है कि जिस साधक का मन साधना के रस में रम गया है, उसे साधना में प्रानन्द आता है। शरीर के कष्टों से उसकी आत्मा कभी विचलित नहीं होती । -यदि कभी मन चंचल हो भी गया, तो शीघ्र ही उसे पुनः शान्त और समाधिस्थ कर लेता है । हमारे कुछ साधक यह भी कहते हैं कि साधना में पहले दुःख होता है और बाद में सुख ! किन्तु यह तो बाजारू भाषा है। यह निरी सौदेबाजी की बात है कि कुछ दुःख सहो तो फिर सुख मिले। जिस साधना के आदि में ही दुःख है, कष्ट है, उसके मध्य में और अन्त में सुख कहाँ से जन्म लेगा ? यह साधना की सही व्याख्या नहीं । साधना तो वह है, जिसके आदि में भी सुख और प्रसन्नता स्वागत के लिए खड़ी रहे, प्रानन्द की लहरें उछलती मिलें, और मध्य में भी सुख तथा अन्त में भी सुख । वास्तव में साधक के सामने दैहिक कष्ट, कष्ट नहीं होते, उन्हें मिटाने के लिए उसकी साधना भी नहीं होती । साधना होती है, आत्मा की आध्यात्मिक प्रसन्नता और सहज श्रानन्द के लिए ।
एक बार की बात है । वनवास के समय युधिष्ठिर ध्यान-मग्न बैठे थे । ध्यान से उठे तो द्रौपदी ने कहा--"धर्मराज ! आप भगवान् का इतना भजन करते हैं, इतनी देर ध्यान बैठे रहते हैं, फिर उनसे कहते क्यों नहीं कि वे इन कष्टों को दूर कर दें । कितने वर्ष से वनवन भटक रहे हैं, कहीं कठोर नुकीले पत्थरों पर रात गुजरती है, तो कहीं कंकरों में धूल में । कभी प्यास के मारे गला सूख जाता है, तो कभी भूख से पेट में बल पड़ने लगते हैं । भगवान् से कहते क्यों नहीं कि इन संकटों का के अन्त कर डालें ।"
धर्मराज ने कहा--"पांचाली ! मैं भगवान् का भजन इसलिए नहीं करता कि वह हमारे कष्टों में हाथ बटाएँ । यह तो सौदेबाजी हुई। मैं तो सिर्फ श्रानन्द के लिए भजन करता हूँ। उसके चिन्तन से ही मेरे मन को प्रसन्नता मिलती है। जो प्रानन्द मुझे चाहिए, तो बिना माँगे ही मिल जाता है । अतः इसके अतिरिक्त और कुछ माँगने के लिए मैं भजन नहीं करता ।"
साधना का यह उच्च आदर्श है कि वह जिस स्वरूप की साधना करता है, वह स्वरूप आनन्दमय है, उससे जीवन में सहज सुख का प्रमृत-निर्झर फूट पड़ता है, चारों ओर प्रसन्नता छा जाती हैं । सुख की इस साधना से अहिंसा का यह स्वर दढ़ होता है, कि तुम स्वयं भी सुखी रहो और दूसरों को भी सुखी रहने दो। इतना ही नहीं, अपनी शक्ति और साधनों से दूसरों को भी सुखी बनायो । स्व और पर के सुख की साधना ही अपने ग्रानन्द-स्वरूप की सच्ची आराधना है।
जो स्वयं ही मुहर्रमी सूरत बनाए रहता है, वह दूसरों को क्या खुश रखेगा ? स्वयं
विविध आयामों में : स्वरूप दर्शन
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
१७७ www.jainelibrary.org.