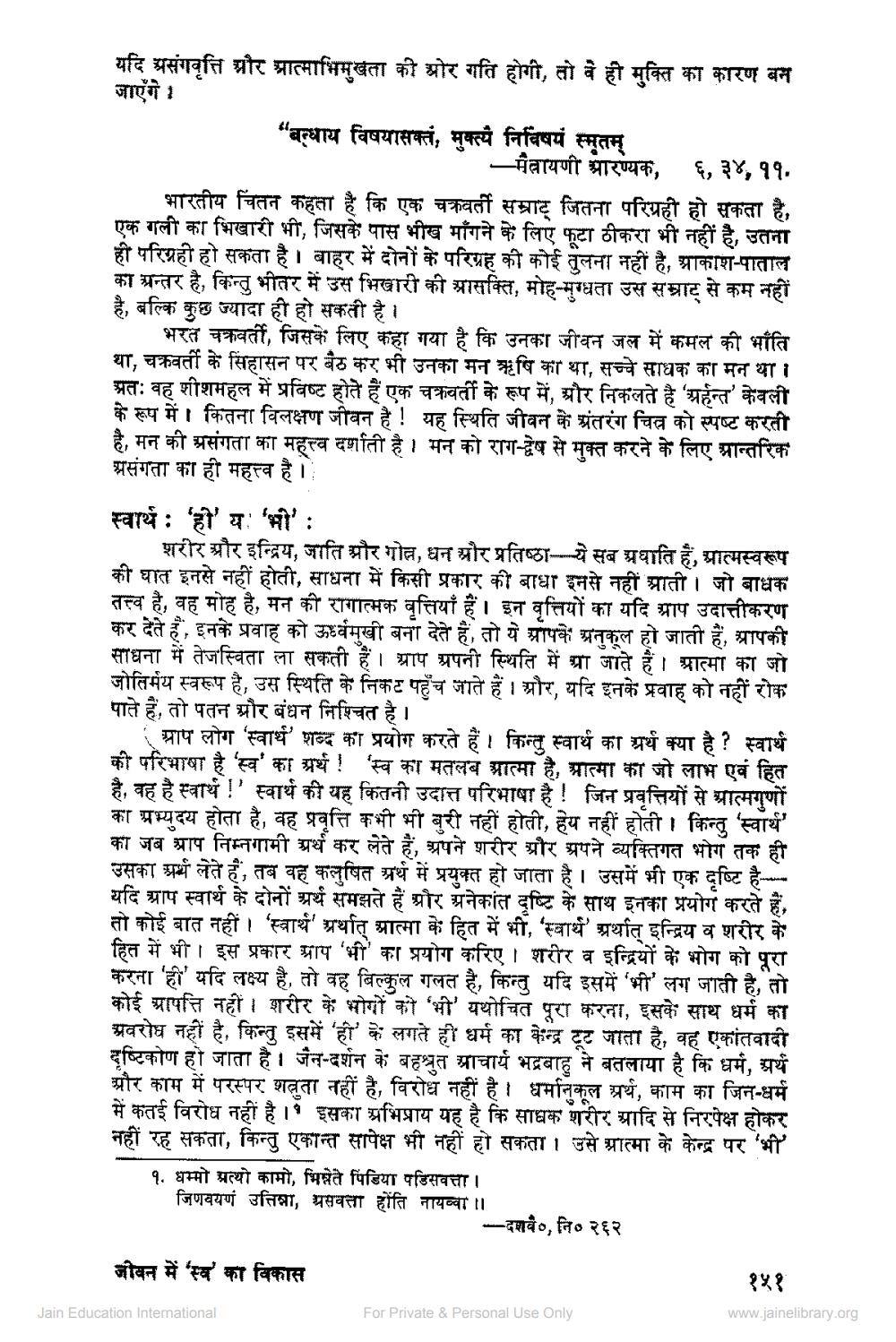________________
यदि असंगवृत्ति और आत्माभिमुखता की ओर गति होगी, तो वे ही मुक्ति का कारण बन जाएँगे 1
"बाय विषयासक्तं, मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम् — मैत्रायणी आरण्यक,
६, ३४, ११.
भारतीय चिंतन कहता है कि एक चक्रवर्ती सम्राट् जितना परिग्रही हो सकता है, एक गली का भिखारी भी, जिसके पास भीख माँगने के लिए फूटा ठीकरा भी नहीं है, उतना ही परिग्रही हो सकता है। बाहर में दोनों के परिग्रह की कोई तुलना नहीं है, आकाश-पाताल का अन्तर है, किन्तु भीतर में उस भिखारी की आसक्ति, मोह-मुग्धता उस सम्राट् से कम नहीं है, बल्कि कुछ ज्यादा ही हो सकती है।
भरत चक्रवर्ती, जिसके लिए कहा गया है कि उनका जीवन जल में कमल की भाँति था, चक्रवर्ती के सिंहासन पर बैठ कर भी उनका मन ऋषि का था, सच्चे साधक का मन था । अतः वह शीशमहल में प्रविष्ट होते हैं एक चक्रवर्ती के रूप में, और निकलते है 'अर्हन्त' केवली के रूप में । कितना विलक्षण जीवन है ! यह स्थिति जीवन के अंतरंग चित्र को स्पष्ट करती है, मन की असंगता का महत्त्व दर्शाती है। मन को राग-द्वेष से मुक्त करने के लिए आन्तरिक असंगता का ही महत्त्व है ।
स्वार्थ : 'हो' य: 'भी' :
शरीर और इन्द्रिय, जाति और गोत्र, धन और प्रतिष्ठा ये सब प्रधाति है, आत्मस्वरूप की घात इनसे नहीं होती, साधना में किसी प्रकार की बाधा इनसे नहीं आती। जो बाधक तत्त्व है, वह मोह है, मन की रागात्मक वृत्तियाँ हैं। इन वृत्तियों का यदि आप उदात्तीकरण कर देते हैं, इनके प्रवाह को ऊर्ध्वमुखी बना देते हैं, तो ये आपके अनुकूल हो जाती हैं, आपकी साधना में तेजस्विता ला सकती हैं। ग्राप अपनी स्थिति में श्रा जाते हैं । श्रात्मा का जो जोतिर्मय स्वरूप है, उस स्थिति के निकट पहुँच जाते हैं। और यदि इनके प्रवाह को नहीं रोक पाते हैं, तो पतन और बंधन निश्चित है ।
आप लोग 'स्वार्थ' शब्द का प्रयोग करते हैं । किन्तु स्वार्थ का अर्थ क्या है ? स्वार्थ की परिभाषा है 'स्व' का अर्थ ! 'स्व का मतलब आत्मा है, आत्मा का जो लाभ एवं हित है, वह है स्वार्थ !' स्वार्थ की यह कितनी उदात्त परिभाषा है ! जिन प्रवृत्तियों से आत्मगुणों का अभ्युदय होता है, वह प्रवृत्ति कभी भी बुरी नहीं होती, हेय नहीं होती । किन्तु 'स्वार्थ' का जब आप निम्नगामी अर्थ कर लेते हैं, अपने शरीर और अपने व्यक्तिगत भोग तक ही उसका अर्थ लेते हैं, तब वह कलुषित अर्थ में प्रयुक्त हो जाता है । उसमें भी एक दृष्टि है--- यदि आप स्वार्थ के दोनों अर्थ समझते हैं और अनेकांत दृष्टि के साथ इनका प्रयोग करते हैं, तो कोई बात नहीं । 'स्वार्थ' अर्थात् आत्मा के हित में भी, 'स्वार्थ' अर्थात् इन्द्रिय व शरीर के हित में भी। इस प्रकार आप 'भी' का प्रयोग करिए। शरीर व इन्द्रियों के भोग को पूरा करना 'ही' यदि लक्ष्य है, तो वह बिल्कुल गलत है, किन्तु यदि इसमें 'भी' लग जाती है, तो कोई आपत्ति नहीं। शरीर के भोगों को 'भी' यथोचित पूरा करना, इसके साथ धर्म का अवरोध नहीं है, किन्तु इसमें 'ही' के लगते ही धर्म का केन्द्र टूट जाता है, वह एकांतवादी दृष्टिकोण हो जाता है। जैन दर्शन के बहश्रुत आचार्य भद्रबाहु ने बतलाया है कि धर्म, अर्थ और काम में परस्पर शत्रुता नहीं है, विरोध नहीं है । धर्मानुकूल अर्थ, काम का जिन-धर्म में कतई विरोध नहीं है । इसका अभिप्राय यह है कि साधक शरीर आदि से निरपेक्ष होकर नहीं रह सकता, किन्तु एकान्त सापेक्ष भी नहीं हो सकता । उसे आत्मा के केन्द्र पर 'भी'
१. धम्मो त्यो कामो, भिनेते पिंडिया पडिसवत्ता । जिणवयणं उत्तिष्ठा, प्रसवत्ता होंति नायव्वा ॥
जीवन में 'स्व' का विकास
Jain Education International
- दशवे०, नि० २६२
For Private & Personal Use Only
१५१ www.jainelibrary.org.