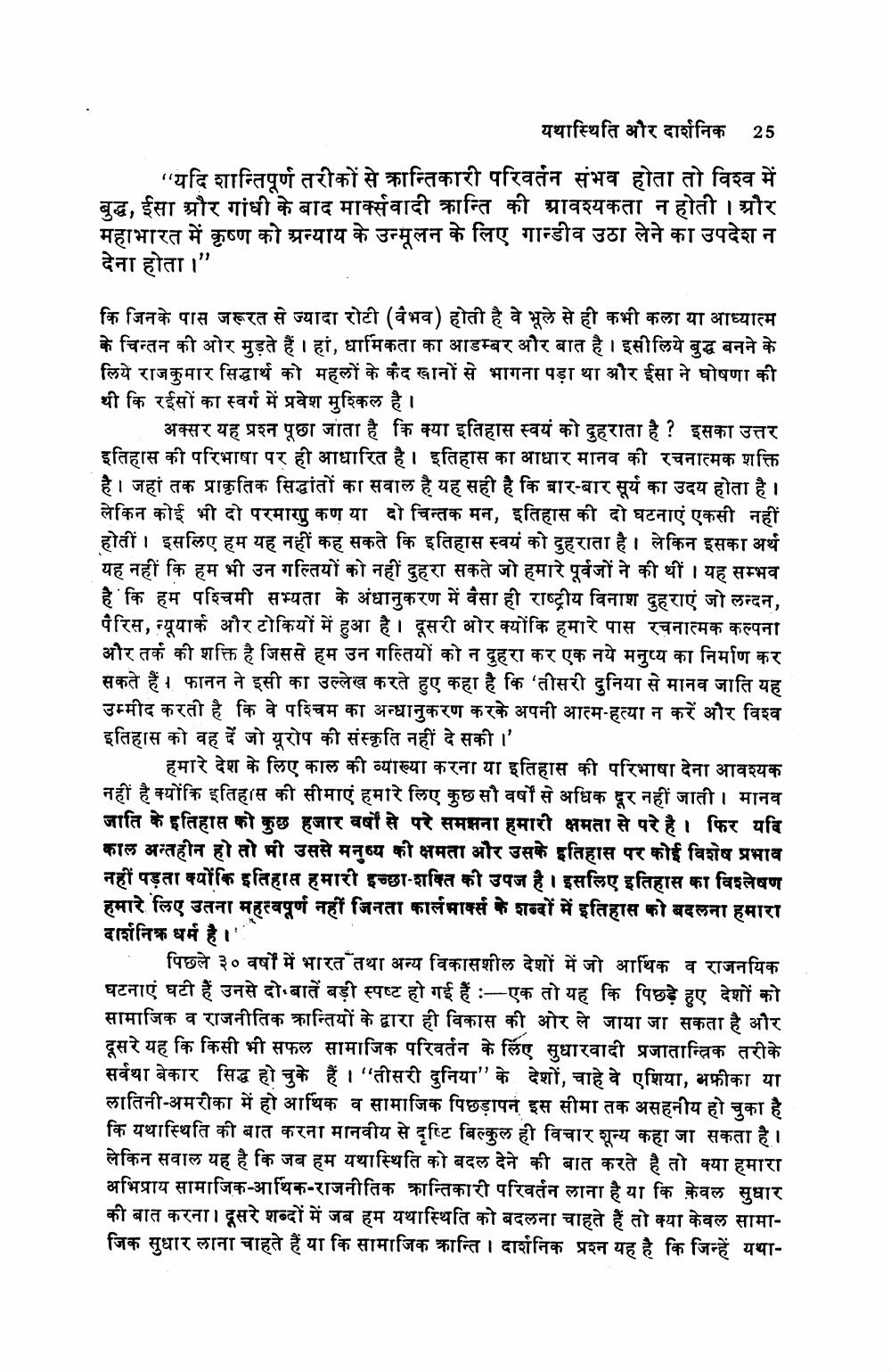________________
यथास्थिति और दार्शनिक 25 "यदि शान्तिपूर्ण तरीकों से क्रान्तिकारी परिवर्तन संभव होता तो विश्व में बुद्ध, ईसा और गांधी के बाद मार्क्सवादी क्रान्ति की आवश्यकता न होती। और महाभारत में कृष्ण को अन्याय के उन्मूलन के लिए गान्डीव उठा लेने का उपदेश न देना होता।"
कि जिनके पास जरूरत से ज्यादा रोटी (वैभव) होती है वे भूले से ही कभी कला या आध्यात्म के चिन्तन की ओर मुड़ते हैं। हां, धार्मिकता का आडम्बर और बात है। इसीलिये बुद्ध बनने के लिये राजकुमार सिद्धार्थ को महलों के कैद खानों से भागना पड़ा था और ईसा ने घोषणा की थी कि रईसों का स्वर्ग में प्रवेश मुश्किल है।
___ अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या इतिहास स्वयं को दुहराता है ? इसका उत्तर इतिहास की परिभाषा पर ही आधारित है। इतिहास का आधार मानव की रचनात्मक शक्ति है। जहां तक प्राकृतिक सिद्धांतों का सवाल है यह सही है कि बार-बार सूर्य का उदय होता है। लेकिन कोई भी दो परमाणु कण या दो चिन्तक मन, इतिहास की दो घटनाएं एकसी नहीं होती। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि इतिहास स्वयं को दुहराता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम भी उन गल्तियों को नहीं दुहरा सकते जो हमारे पूर्वजों ने की थीं । यह सम्भव है कि हम पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण में वैसा ही राष्ट्रीय विनाश दुहराएं जो लन्दन, पैरिस, न्यूयार्क और टोकियों में हुआ है। दूसरी ओर क्योंकि हमारे पास रचनात्मक कल्पना
और तर्क की शक्ति है जिससे हम उन गल्तियों को न दुहरा कर एक नये मनुष्य का निर्माण कर सकते हैं। फानन ने इसी का उल्लेख करते हुए कहा है कि 'तीसरी दुनिया से मानव जाति यह उम्मीद करती है कि वे पश्चिम का अन्धानुकरण करके अपनी आत्म-हत्या न करें और विश्व इतिहास को वह दें जो यूरोप की संस्कृति नहीं दे सकी।'
हमारे देश के लिए काल की व्याख्या करना या इतिहास की परिभाषा देना आवश्यक नहीं है क्योंकि इतिहास की सीमाएं हमारे लिए कुछ सौ वर्षों से अधिक दूर नहीं जाती। मानव जाति के इतिहास को कुछ हजार वर्षों से परे समझना हमारी क्षमता से परे है। फिर यदि काल अन्तहीन हो तो भी उससे मनुष्य की क्षमता और उसके इतिहास पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि इतिहास हमारी इच्छा-शक्ति की उपज है। इसलिए इतिहास का विश्लेषण हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं जिनता कार्लमार्क्स के शब्दों में इतिहास को बदलना हमारा दार्शनिक धर्म है।
- पिछले ३० वर्षों में भारत तथा अन्य विकासशील देशों में जो आर्थिक व राजनयिक घटनाएं घटी हैं उनसे दो बातें बड़ी स्पष्ट हो गई हैं :-एक तो यह कि पिछड़े हए देशों को सामाजिक व राजनीतिक क्रान्तियों के द्वारा ही विकास की ओर ले जाया जा सकता है और दूसरे यह कि किसी भी सफल सामाजिक परिवर्तन के लिए सुधारवादी प्रजातान्त्रिक तरीके सर्वथा बेकार सिद्ध हो चुके हैं । "तीसरी दुनिया के देशों, चाहे वे एशिया, अफ्रीका या लातिनी-अमरीका में हो आर्थिक व सामाजिक पिछड़ापन इस सीमा तक असहनीय हो चूका है कि यथास्थिति की बात करना मानवीय से दष्टि बिल्कूल ही विचार शन्य कहा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जब हम यथास्थिति को बदल देने की बात करते है तो क्या हमारा अभिप्राय सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना है या कि केवल सुधार की बात करना। दूसरे शब्दों में जब हम यथास्थिति को बदलना चाहते हैं तो क्या केवल सामाजिक सुधार लाना चाहते हैं या कि सामाजिक क्रान्ति । दार्शनिक प्रश्न यह है कि जिन्हें यथा