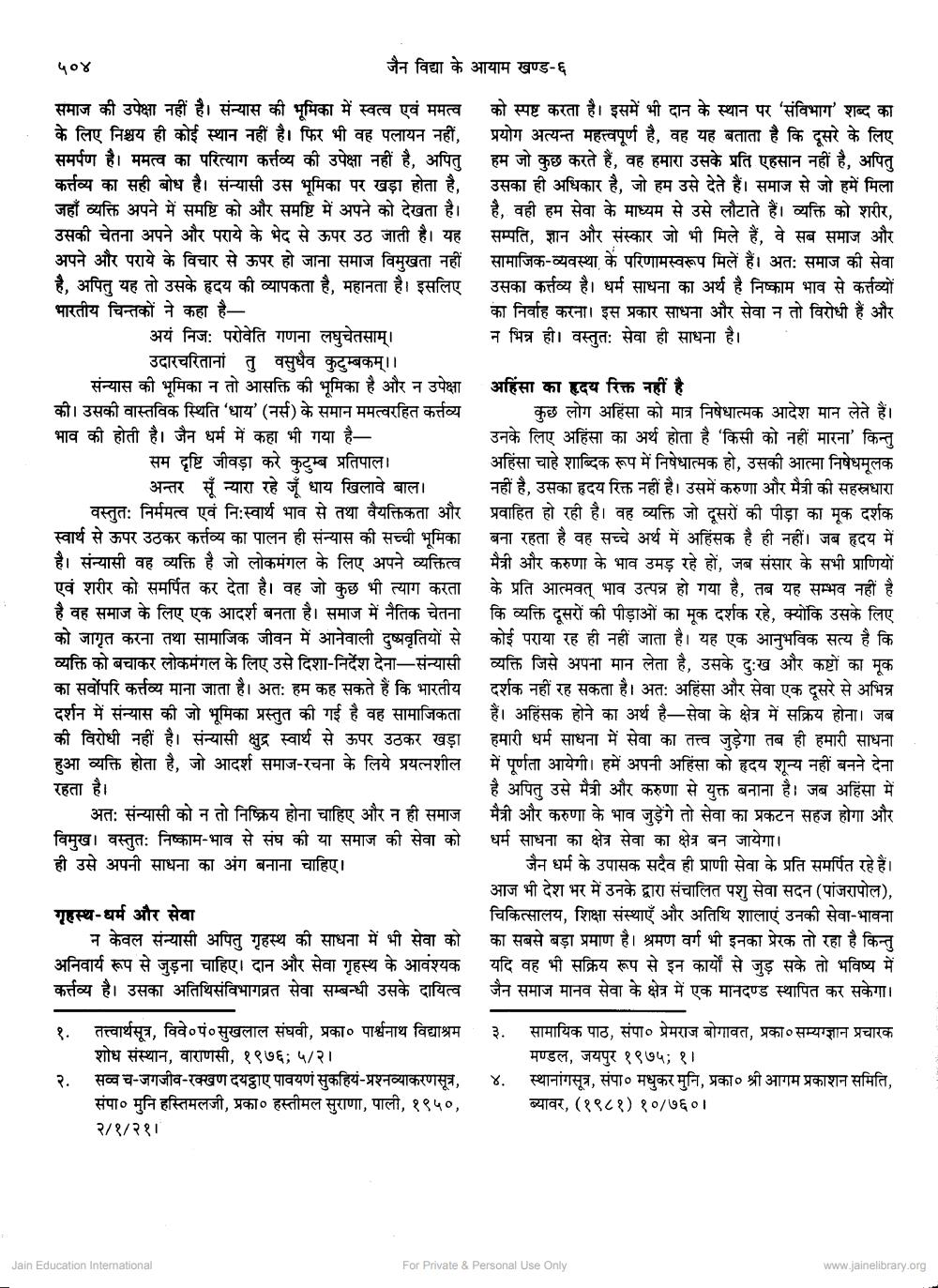________________ 504 जैन विद्या के आयाम खण्ड-६ ह समाज की उपेक्षा नहीं है। संन्यास की भूमिका में स्वत्व एवं ममत्व को स्पष्ट करता है। इसमें भी दान के स्थान पर 'संविभाग' शब्द का के लिए निश्चय ही कोई स्थान नहीं है। फिर भी वह पलायन नहीं, प्रयोग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, वह यह बताता है कि दूसरे के लिए समर्पण है। ममत्व का परित्याग कर्तव्य की उपेक्षा नहीं है, अपित् हम जो कुछ करते हैं, वह हमारा उसके प्रति एहसान नहीं है, अपितु कर्तव्य का सही बोध है। संन्यासी उस भूमिका पर खड़ा होता है, उसका ही अधिकार है, जो हम उसे देते हैं। समाज से जो हमें मिला जहाँ व्यक्ति अपने में समष्टि को और समष्टि में अपने को देखता है। है, वही हम सेवा के माध्यम से उसे लौटाते हैं। व्यक्ति को शरीर, उसकी चेतना अपने और पराये के भेद से ऊपर उठ जाती है। यह सम्पति, ज्ञान और संस्कार जो भी मिले हैं, वे सब समाज और अपने और पराये के विचार से ऊपर हो जाना समाज विमुखता नहीं सामाजिक-व्यवस्था के परिणामस्वरूप मिले हैं। अत: समाज की सेवा है, अपितु यह तो उसके हृदय की व्यापकता है, महानता है। इसलिए उसका कर्तव्य है। धर्म साधना का अर्थ है निष्काम भाव से कर्तव्यों भारतीय चिन्तकों ने कहा है का निर्वाह करना। इस प्रकार साधना और सेवा न तो विरोधी हैं और अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम्। न भिन्न ही। वस्तुत: सेवा ही साधना है। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।। संन्यास की भूमिका न तो आसक्ति की भूमिका है और न उपेक्षा अहिंसा का हृदय रिक्त नहीं है की। उसकी वास्तविक स्थिति 'धाय' (नर्स) के समान ममत्वरहित कर्त्तव्य कुछ लोग अहिंसा को मात्र निषेधात्मक आदेश मान लेते हैं। भाव की होती है। जैन धर्म में कहा भी गया है उनके लिए अहिंसा का अर्थ होता है 'किसी को नहीं मारना' किन्तु सम दृष्टि जीवड़ा करे कुटुम्ब प्रतिपाल। अहिंसा चाहे शाब्दिक रूप में निषेधात्मक हो, उसकी आत्मा निषेधमूलक अन्तर सूं न्यारा रहे जूं धाय खिलावे बाल। नहीं है, उसका हृदय रिक्त नहीं है। उसमें करुणा और मैत्री की सहस्रधारा वस्तुतः निर्ममत्व एवं निःस्वार्थ भाव से तथा वैयक्तिकता और प्रवाहित हो रही है। वह व्यक्ति जो दूसरों की पीड़ा का मूक दर्शक स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्त्तव्य का पालन ही संन्यास की सच्ची भूमिका बना रहता है वह सच्चे अर्थ में अहिंसक है ही नहीं। जब हृदय में है। संन्यासी वह व्यक्ति है जो लोकमंगल के लिए अपने व्यक्तित्व मैत्री और करुणा के भाव उमड़ रहे हों, जब संसार के सभी प्राणियों एवं शरीर को समर्पित कर देता है। वह जो कुछ भी त्याग करता के प्रति आत्मवत् भाव उत्पन्न हो गया है, तब यह सम्भव नहीं है है वह समाज के लिए एक आदर्श बनता है। समाज में नैतिक चेतना कि व्यक्ति दूसरों की पीड़ाओं का मूक दर्शक रहे, क्योंकि उसके लिए को जागृत करना तथा सामाजिक जीवन में आनेवाली दुष्प्रवृतियों से कोई पराया रह ही नहीं जाता है। यह एक आनुभविक सत्य है कि व्यक्ति को बचाकर लोकमंगल के लिए उसे दिशा-निर्देश देना-संन्यासी व्यक्ति जिसे अपना मान लेता है, उसके दुःख और कष्टों का मूक का सर्वोपरि कर्त्तव्य माना जाता है। अत: हम कह सकते हैं कि भारतीय दर्शक नहीं रह सकता है। अत: अहिंसा और सेवा एक दूसरे से अभिन्न दर्शन में संन्यास की जो भूमिका प्रस्तुत की गई है वह सामाजिकता हैं। अहिंसक होने का अर्थ है-सेवा के क्षेत्र में सक्रिय होना। जब की विरोधी नहीं है। संन्यासी क्षुद्र स्वार्थ से ऊपर उठकर खड़ा हमारी धर्म साधना में सेवा का तत्त्व जुड़ेगा तब ही हमारी साधना हआ व्यक्ति होता है, जो आदर्श समाज-रचना के लिये प्रयत्नशील में पूर्णता आयेगी। हमें अपनी अहिंसा को हृदय शून्य नहीं बनने देना रहता है। है अपितु उसे मैत्री और करुणा से युक्त बनाना है। जब अहिंसा में अत: संन्यासी को न तो निष्क्रिय होना चाहिए और न ही समाज मैत्री और करुणा के भाव जुड़ेंगे तो सेवा का प्रकटन सहज होगा और विमुख। वस्तुत: निष्काम-भाव से संघ की या समाज की सेवा को धर्म साधना का क्षेत्र सेवा का क्षेत्र बन जायेगा। ही उसे अपनी साधना का अंग बनाना चाहिए। जैन धर्म के उपासक सदैव ही प्राणी सेवा के प्रति समर्पित रहे हैं। आज भी देश भर में उनके द्वारा संचालित पशु सेवा सदन (पांजरापोल), गृहस्थ-धर्म और सेवा चिकित्सालय, शिक्षा संस्थाएँ और अतिथि शालाएं उनकी सेवा-भावना न केवल संन्यासी अपितु गृहस्थ की साधना में भी सेवा को का सबसे बड़ा प्रमाण है। श्रमण वर्ग भी इनका प्रेरक तो रहा है किन्तु अनिवार्य रूप से जुड़ना चाहिए। दान और सेवा गृहस्थ के आवश्यक यदि वह भी सक्रिय रूप से इन कार्यों से जुड़ सके तो भविष्य में कर्तव्य है। उसका अतिथिसंविभागवत सेवा सम्बन्धी उसके दायित्व जैन समाज मानव सेवा के क्षेत्र में एक मानदण्ड स्थापित कर सकेगा। 1. 2. तत्त्वार्थसूत्र, विवे०पं० सुखलाल संघवी, प्रका० पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान, वाराणसी, 1976; 5/2 / सव्व च-जगजीव-रक्खण दयट्ठाए पावयणं सुकहियं-प्रश्नव्याकरणसूत्र, संपा० मुनि हस्तिमलजी, प्रका० हस्तीमल सुराणा, पाली, 1950, 2/1/21 / 3. सामायिक पाठ, संपा० प्रेमराज बोगावत, प्रका० सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल, जयपुर 1975; 1 / 4. स्थानांगसूत्र, संपा० मधुकर मुनि, प्रका० श्री आगम प्रकाशन समिति, ब्यावर, (1981) 10/760 / Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org