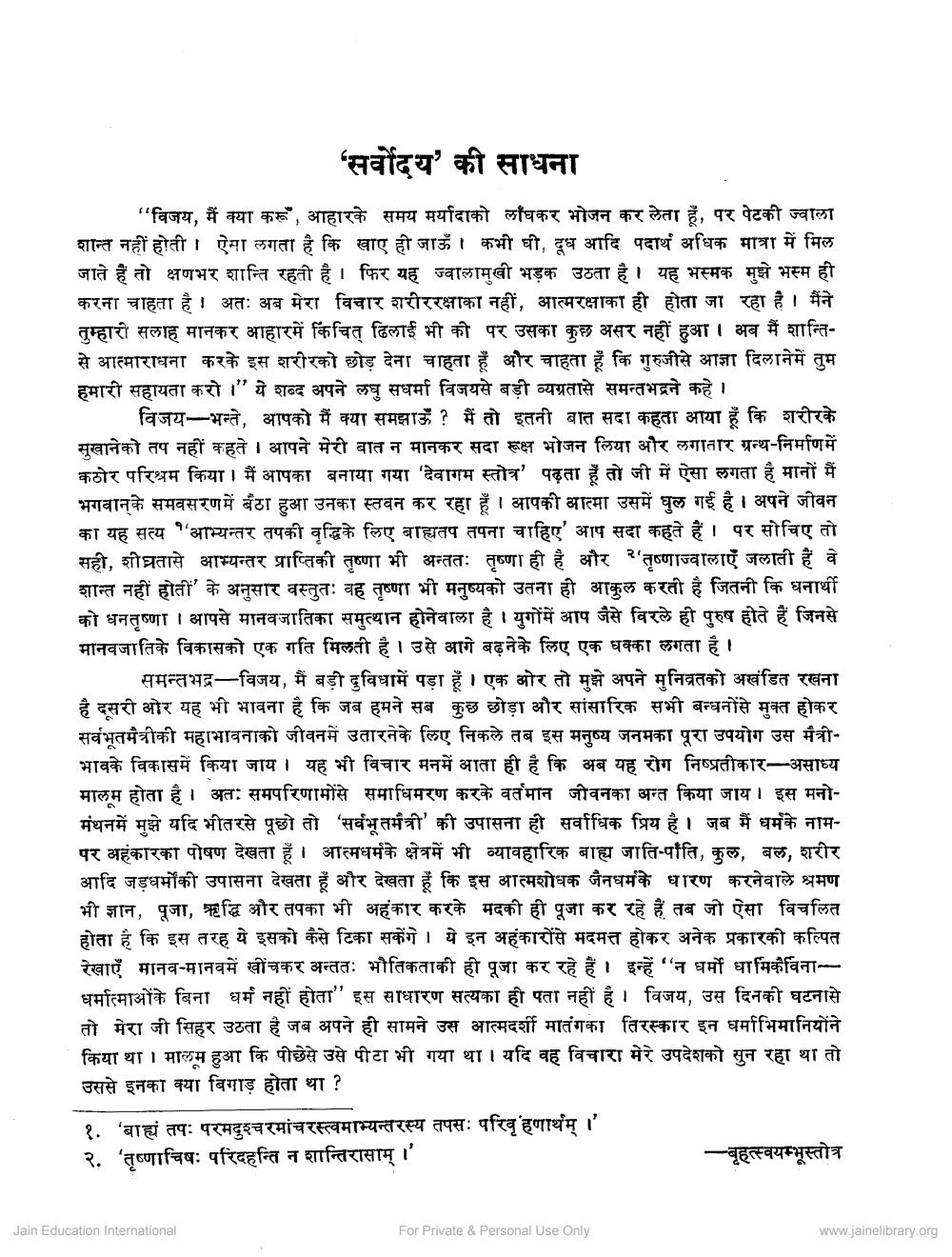________________
'सर्वोदय' की साधना
"विजय, मैं क्या करूं, आहारके समय मर्यादाको लाँधकर भोजन कर लेता हूँ, पर पेटकी ज्वाला शान्त नहीं होती। ऐमा लगता है कि खाए ही जाऊँ। कभी घी, दूध आदि पदार्थ अधिक मात्रा में मिल जाते हैं तो क्षणभर शान्ति रहती है। फिर यह ज्वालामुखी भड़क उठता है। यह भस्मक मुझे भस्म ही करना चाहता है। अतः अब मेरा विचार शरीररक्षाका नहीं, आत्मरक्षाका ही होता जा रहा है। मैंने तुम्हारी सलाह मानकर आहारमें किंचित् ढिलाई भी की पर उसका कुछ असर नहीं हुआ। अब मैं शान्तिसे आत्माराधना करके इस शरीरको छोड़ देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि गुरुजीसे आज्ञा दिलाने में तुम हमारी सहायता करो।" ये शब्द अपने लघु सधर्मा विजयसे बड़ी व्यग्रतासे समन्तभद्रने कहे।
विजय-भन्ते, आपको मैं क्या समझाऊँ? मैं तो इतनी बात सदा कहता आया हूँ कि शरीरके सुखानेको तप नहीं कहते । आपने मेरी बात न मानकर सदा रूक्ष भोजन लिया और लगातार ग्रन्थ-निर्माणमें कठोर परिश्रम किया। मैं आपका बनाया गया 'देवागम स्तोत्र' पढ़ता हूँ तो जी में ऐसा लगता है मानों मैं भगवान्के समवसरण में बैठा हुआ उनका स्तवन कर रहा हूँ। आपकी आत्मा उसमें घुल गई है। अपने जीवन का यह सत्य 'आभ्यन्तर तपकी वृद्धिके लिए बाह्यतप तपना चाहिए' आप सदा कहते हैं। पर सोचिए तो सही, शीघ्रतासे आभ्यन्तर प्राप्तिकी तृष्णा भी अन्ततः तृष्णा ही है और २'तृष्णाज्वालाएँ जलाती हैं वे शान्त नहीं होतीं' के अनुसार वस्तुतः वह तृष्णा भी मनुष्यको उतना ही आकुल करती है जितनी कि धनार्थी
। आपसे मानवजातिका समत्थान होनेवाला है। यगोंमें आप जैसे विरले ही पुरुष होते हैं जिनसे मानवजातिके विकासको एक गति मिलती है । उसे आगे बढ़नेके लिए एक धक्का लगता है ।
समन्तभद्र-विजय, मैं बड़ी दुविधामें पड़ा हूँ। एक ओर तो मुझे अपने मुनिव्रतको अखंडित रखना है दसरी ओर यह भी भावना है कि जब हमने सब कुछ छोड़ा और सांसारिक सभी बन्धनोंसे मक्त होकर सर्वभूतमैत्रीकी महाभावनाको जीवन में उतारनेके लिए निकले तब इस मनुष्य जनमका पूरा उपयोग उस मैत्रीभावके विकासमें किया जाय। यह भी विचार मनमें आता ही है कि अब यह रोग निष्प्रतीकार-असाध्य मालम होता है। अतः समपरिणामोंसे समाधिमरण करके वर्तमान जीवनका अन्त किया जाय। इस मनोमंथनमें मुझे यदि भीतरसे पूछो तो 'सर्वभूतमैत्री' की उपासना ही सर्वाधिक प्रिय है। जब मैं धर्मके नामपर अहंकारका पोषण देखता हूँ। आत्मधर्मके क्षेत्रमें भी व्यावहारिक बाह्य जाति-पाँति, कुल, बल, शरीर आदि जड़धर्मोंकी उपासना देखता हूँ और देखता हूँ कि इस आत्मशोधक जैनधर्मके धारण करनेवाले श्रमण भी ज्ञान, पूजा, ऋद्धि और तपका भी अहंकार करके मदकी ही पूजा कर रहे हैं तब जो ऐसा विचलित होता है कि इस तरह ये इसको कैसे टिका सकेंगे। ये इन अहंकारोंसे मदमत्त होकर अनेक प्रकारकी कल्पित रेखाएँ मानव-मानवमें खींचकर अन्ततः भौतिकताकी ही पूजा कर रहे हैं। इन्हें "न धर्मो धार्मिकैविनाधर्मात्माओंके बिना धर्म नहीं होता" इस साधारण सत्यका ही पता नहीं है। विजय, उस दिनकी घटनासे तो मेरा जी सिहर उठता है जब अपने ही सामने उस आत्मदर्शी मातंगका तिरस्कार इन धर्माभिमानियोंने किया था। मालम हुआ कि पीछेसे उसे पीटा भी गया था। यदि वह विचारा मेरे उपदेशको सुन रहा था तो उससे इनका क्या बिगाड़ होता था ?
१. 'बाह्यं तपः परमदुश्चरमांचरस्त्वमाभ्यन्तरस्य तपसः परिवृहणार्थम् ।' २. 'तृष्णाचिषः परिदहन्ति न शान्तिरासाम् ।'
-बृहत्स्वयम्भूस्तोत्र
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org