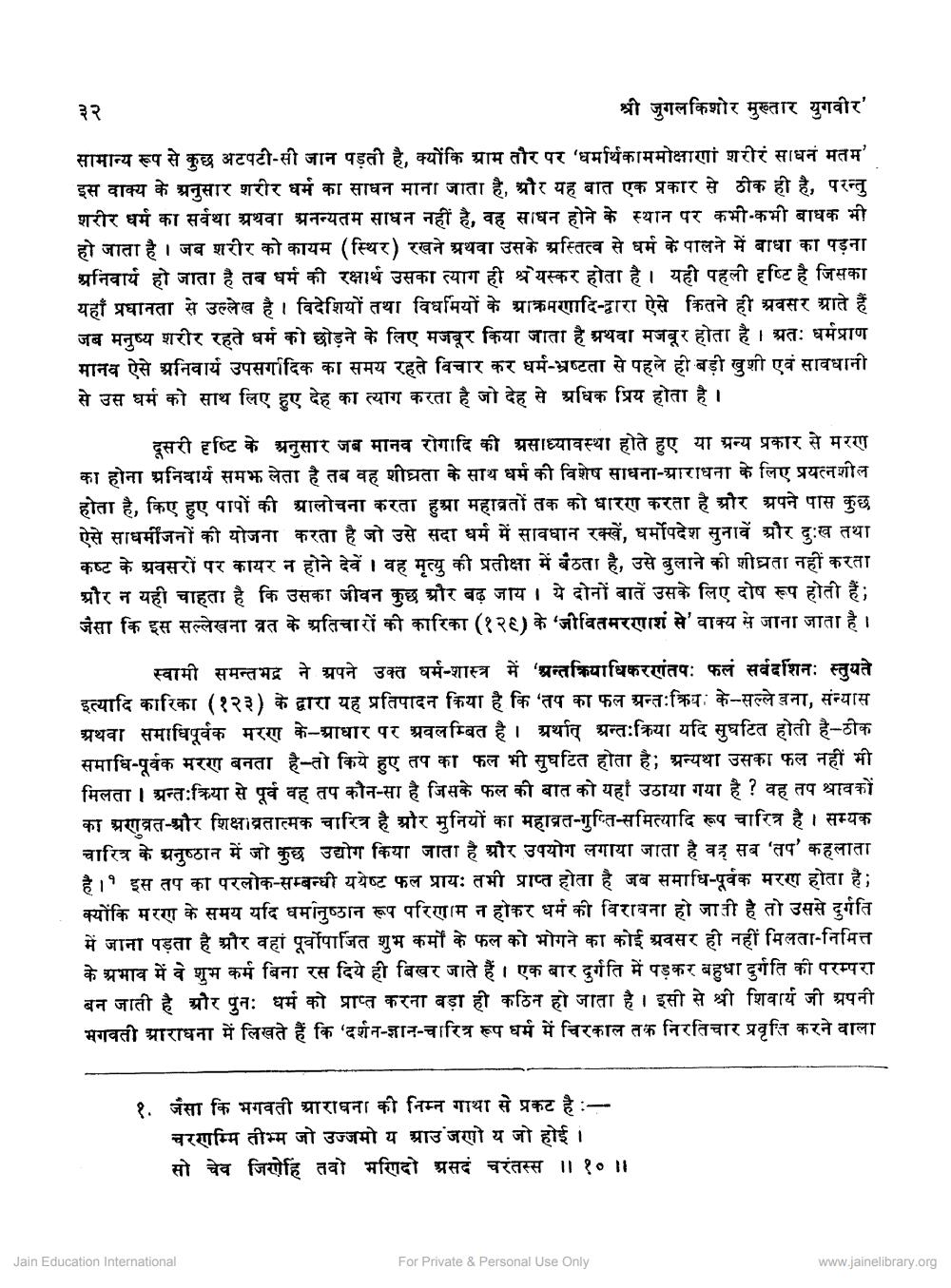________________
३२
श्री जुगलकिशोर मुख्तार युगवीर'
सामान्य रूप से कुछ अटपटी-सी जान पड़ती है, क्योंकि आम तौर पर 'धर्मार्थकाममोक्षाणां शरीरं साधनं मतम' इस वाक्य के अनुसार शरीर धर्म का साधन माना जाता है, और यह बात एक प्रकार से ठीक ही है, परन्तु शरीर धर्म का सर्वथा अथवा अनन्यतम साधन नहीं है, वह साधन होने के स्थान पर कभी-कभी बाधक भी हो जाता है । जब शरीर को कायम (स्थिर) रखने अथवा उसके अस्तित्व से धर्म के पालने में बाधा का पड़ना अनिवार्य हो जाता है तब धर्म की रक्षार्थ उसका त्याग ही श्रेयस्कर होता है। यही पहली दृष्टि है जिसका यहाँ प्रधानता से उल्लेख है। विदेशियों तथा विर्मियों के आक्रमणादि-द्वारा ऐसे कितने ही अवसर पाते हैं जब मनुष्य शरीर रहते धर्म को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है अथवा मजबूर होता है। अतः धर्मप्राण मानव ऐसे अनिवार्य उपसर्गादिक का समय रहते विचार कर धर्म-भ्रष्टता से पहले ही बड़ी खुशी एवं सावधानी से उस धर्म को साथ लिए हुए देह का त्याग करता है जो देह से अधिक प्रिय होता है।
दूसरी दृष्टि के अनुसार जब मानव रोगादि की असाध्यावस्था होते हुए या अन्य प्रकार से मरण का होना अनिवार्य समझ लेता है तब वह शीघ्रता के साथ धर्म की विशेष साधना-पाराधना के लिए प्रयत्नशील होता है, किए हुए पापों की आलोचना करता हुआ महाव्रतों तक को धारण करता है और अपने पास कुछ ऐसे साधर्मीजनों की योजना करता है जो उसे सदा धर्म में सावधान रखें, धर्मोपदेश सुनावें और दुःख तथा कष्ट के अवसरों पर कायर न होने देवें । वह मृत्यु की प्रतीक्षा में बैठता है, उसे बुलाने की शीघ्रता नहीं करता
और न यही चाहता है कि उसका जीवन कुछ और बढ़ जाय । ये दोनों बातें उसके लिए दोष रूप होती हैं; जैसा कि इस सल्लेखना व्रत के अतिचारों की कारिका (१२६) के 'जीवितमरणाशं से' वाक्य से जाना जाता है।
स्वामी समन्तभद्र ने अपने उक्त धर्म-शास्त्र में 'अन्तक्रियाधिकरणंतपः फलं सर्वशिनः स्तुयते इत्यादि कारिका (१२३) के द्वारा यह प्रतिपादन किया है कि 'तप का फल अन्तःक्रियः के-सल्ले बना, संन्यास अथवा समाधिपूर्वक मरण के आधार पर अवलम्बित है। अर्थात् अन्तःक्रिया यदि सुघटित होती है-ठीक समाधि-पूर्वक मरण बनता है-तो किये हुए तप का फल भी सुघटित होता है; अन्यथा उसका फल नहीं भी मिलता । अन्त:क्रिया से पूर्व वह तप कौन-सा है जिसके फल की बात को यहाँ उठाया गया है ? वह तप श्रावकों का प्रणव्रत-और शिक्षावतात्मक चारित्र है और मुनियों का महाव्रत-गुप्ति-समित्यादि रूप चारि चारित्र के अनुष्ठान में जो कुछ उद्योग किया जाता है और उपयोग लगाया जाता है वह सब 'तप' कहलाता है।' इस तप का परलोक-सम्बन्धी यथेष्ट फल प्रायः तभी प्राप्त होता है जब समाधि-पूर्वक मरण होता है; क्योंकि मरण के समय यदि धर्मानुष्ठान रूप परिणाम न होकर धर्म की विरावना हो जाती है तो उससे दुर्गति में जाना पड़ता है और वहां पूर्वोपार्जित शुभ कर्मों के फल को भोगने का कोई अवसर ही नहीं मिलता-निमित्त के अभाव में वे शुभ कर्म बिना रस दिये ही बिखर जाते हैं। एक बार दुर्गति में पड़कर बहुधा दुर्गति की परम्परा बन जाती है और पुनः धर्म को प्राप्त करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। इसी से श्री शिवार्य जी अपनी भगवती आराधना में लिखते हैं कि 'दर्शन-ज्ञान-चारित्र रूप धर्म में चिरकाल तक निरतिचार प्रवृति करने वाला
१. जैसा कि भगवती आराधना की निम्न गाथा से प्रकट है :
चरणम्मि तीभ्म जो उज्जमो य पाउंजणो य जो होई। सो चेव जिणेहि तवो मरिणदो असदं चरंतस्स ।। १०॥
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org