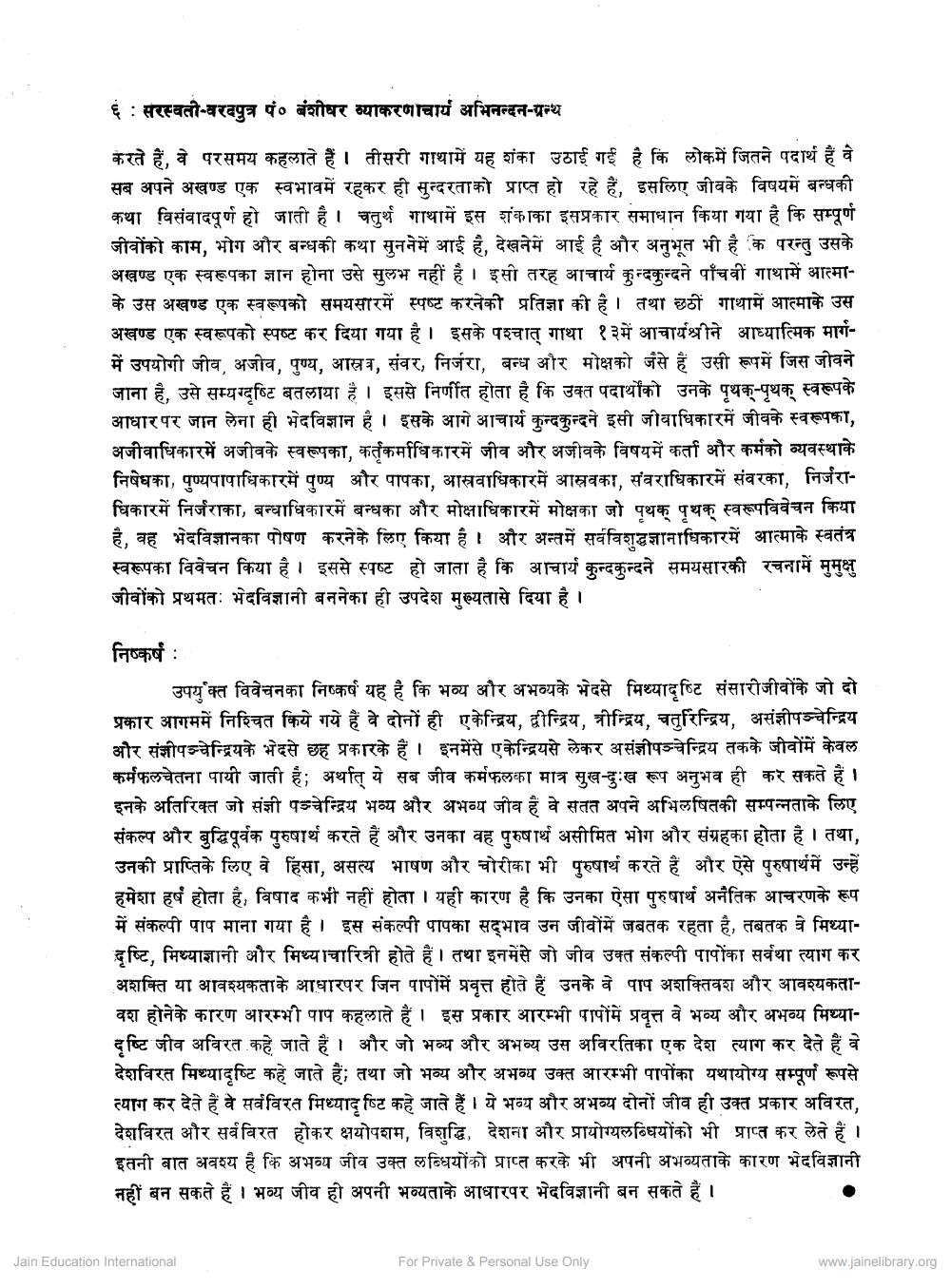________________ 6 : सरस्वती-वरदपुत्र पं० बंशीधर व्याकरणाचार्य अभिनन्दन-ग्रन्थ करते हैं, वे परसमय कहलाते हैं। तीसरी गाथामें यह शंका उठाई गई है कि लोकमें जितने पदार्थ हैं वे सब अपने अखण्ड एक स्वभावमें रहकर ही सुन्दरताको प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए जीवके विषयमें बन्धकी कथा विसंवादपूर्ण हो जाती है। चतुर्थ गाथामें इस शंकाका इसप्रकार समाधान किया गया है कि सम्पूर्ण जीवोंको काम, भोग और बन्धकी कथा सुनने में आई है, देखने में आई है और अनुभूत भी है क परन्तु उसके अखण्ड एक स्वरूपका ज्ञान होना उसे सुलभ नहीं है। इसी तरह आचार्य कुन्दकुन्दने पाँचवीं गाथामें आत्माके उस अखण्ड एक स्वरूपको समयसारमें स्पष्ट करनेकी प्रतिज्ञा की है। तथा छठीं गाथामें आत्माके उस अखण्ड एक स्वरूपको स्पष्ट कर दिया गया है। इसके पश्चात गाथा १३में आचार्यश्रीने आध्यात्मिक मार्गमें उपयोगी जीव, अजीव, पुण्य, आस्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्षको जैसे हैं उसी रूप में जिस जीवने जाना है, उसे सम्यग्दृष्टि बतलाया है। इससे निर्णीत होता है कि उक्त पदार्थोंको उनके पृथक्-पृथक् स्वरूपके आधार पर जान लेना ही भेदविज्ञान है / इसके आगे आचार्य कुन्दकुन्दने इसी जीवाधिकारमें जीवके स्वरूपका, अजीवाधिकारमें अजीवके स्वरूपका, कर्तकर्माधिकारमें जीव और अजीवके विषयमें कर्ता और कर्मको व्यवस्थाके निषेधका, पुण्यपापाधिकारमें पुण्य और पापका, आस्रवाधिकारमें आस्रवका, संवराधिकारमें संवरका, निर्जराधिकारमें निर्जराका, बन्धाधिकारमें बन्धका और मोक्षाधिकारमें मोक्षका जो पृथक् पृथक् स्वरूपविवेचन किया है, वह भेदविज्ञानका पोषण करने के लिए किया है। और अन्त में सर्वविशुद्धज्ञानाधिकारमें आत्माके स्वतंत्र स्वरूपका विवेचन किया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य कुन्दकुन्दने समयसारकी रचनामें मुमुक्षु जीवोंको प्रथमतः भेदविज्ञानी बननेका ही उपदेश मुख्यतासे दिया है। निष्कर्ष : उपयुक्त विवेचनका निष्कर्ष यह है कि भव्य और अभव्यके भेदसे मिथ्यादष्टि संसारीजीवोंके जो दो . प्रकार आगममें निश्चित किये गये हैं वे दोनों ही एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चरिन्द्रिय, असंज्ञीपञ्चेन्द्रिय और संज्ञीपञ्चेन्द्रियके भेदसे छह प्रकारके हैं। इनमेंसे एकेन्द्रियसे लेकर असंज्ञीपञ्चेन्द्रिय तकके जीवोंमें केवल कर्मफलचेतना पायी जाती है; अर्थात् ये सब जीव कर्मफलका मात्र सुख-दुःख रूप अनुभव ही कर सकते हैं / इनके अतिरिक्त जो संज्ञी पञ्चेन्द्रिय भव्य और अभव्य जीव है वे सतत अपने अभिलषितकी सम्पन्नताके लिए संकल्प और बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करते हैं और उनका वह पुरुषार्थ असीमित भोग और संग्रहका होता है / तथा, उनकी प्राप्तिके लिए वे हिंसा, असत्य भाषण और चोरीका भी पुरुषार्थ करते हैं और ऐसे पुरुषार्थमें उन्हें हमेशा हर्ष होता है, विषाद कभी नहीं होता / यही कारण है कि उनका ऐसा पुरुषार्थ अनैतिक आचरणके रूप में संकल्पी पाप माना गया है। इस संकल्पी पापका सद्भाव उन जीवोंमें जबतक रहता है, तबतक वे मिथ्यादृष्टि, मिथ्याज्ञानी और मिथ्याचारित्री होते हैं। तथा इनमेंसे जो जीव उक्त संकल्पी पापोंका सर्वथा त्याग कर अशक्ति या आवश्यकताके आधारपर जिन पापोंमें प्रवृत्त होते हैं उनके वे पाप अशक्तिवश और आवश्यकतावश होनेके कारण आरम्भी पाप कहलाते हैं। इस प्रकार आरम्भी पापोंमें प्रवृत्त वे भव्य और अभव्य मिथ्यादृष्टि जीव अविरत कहे जाते हैं। और जो भव्य और अभव्य उस अविरतिका एक देश त्याग कर देते हैं वे देशविरत मिथ्यादृष्टि कहे जाते हैं तथा जो भव्य और अभव्य उक्त आरम्भी पापोंका यथायोग्य सम्पूर्ण रूपसे त्याग कर देते हैं वे सर्वविरत मिथ्यादृष्टि कहे जाते हैं। ये भव्य और अभव्य दोनों जीव ही उक्त प्रकार अविरत, देशविरत और सर्व विरत होकर क्षयोपशम, विशद्धि, देशना और प्रायोग्यलब्धियोंको भी प्राप्त कर लेते हैं / इतनी बात अवश्य है कि अभव्य जीव उक्त लब्धियोंको प्राप्त करके भी अपनी अभव्यताके कारण भेदविज्ञानी नहीं बन सकते हैं। भव्य जीव ही अपनी भव्यताके आधारपर भेदविज्ञानी बन सकते हैं। Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org