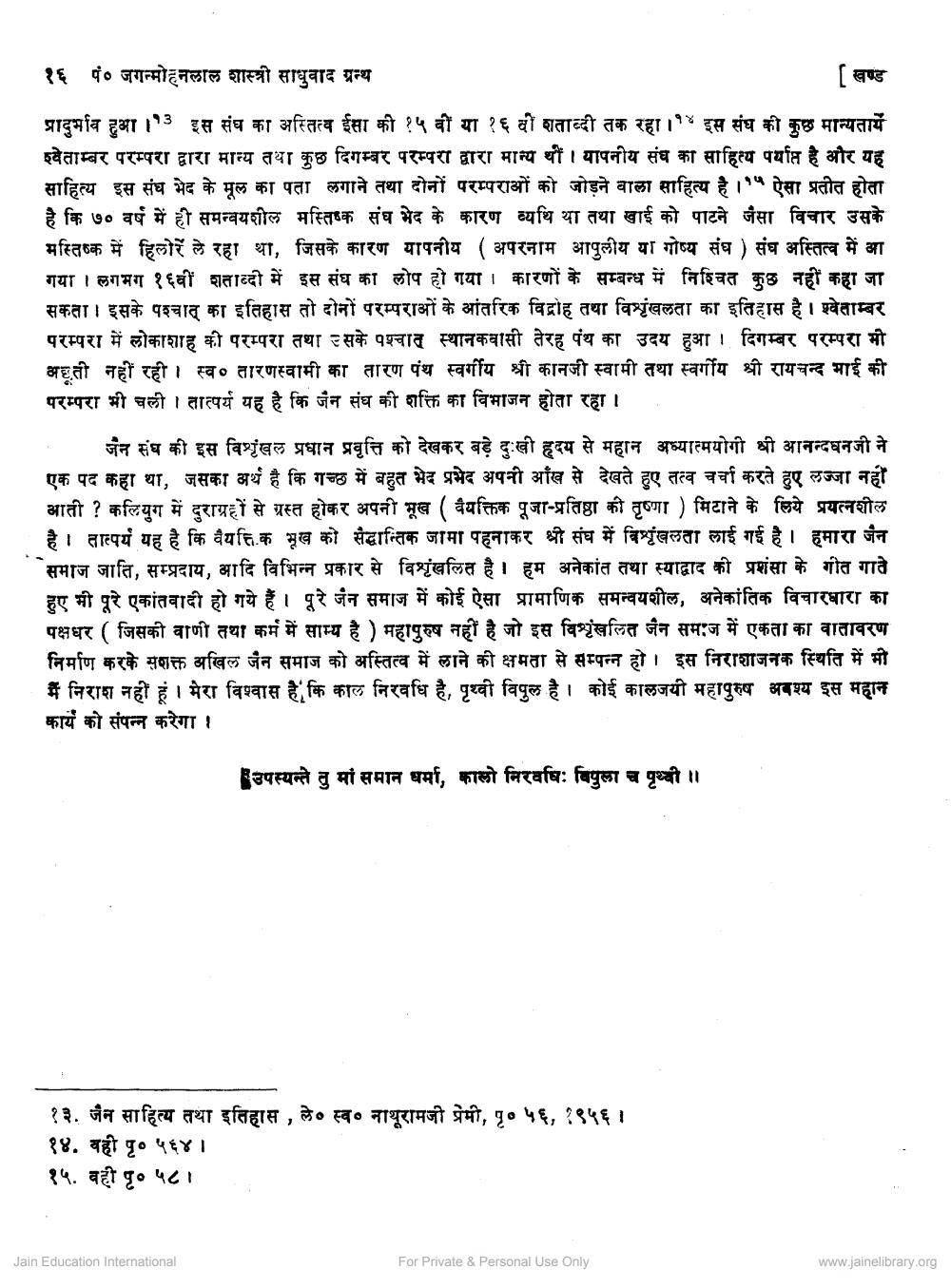________________ 16 पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [खण्ड प्रादुर्भाव हुआ।'3 इस संघ का अस्तित्व ईसा की 15 वी या 16 वीं शताब्दी तक रहा। इस संघ की कुछ मान्यतायें श्वेताम्बर परम्परा द्वारा मान्य तथा कुछ दिगम्बर परम्परा द्वारा मान्य थौं / यापनीय संघ का साहित्य पर्याप्त है और यह साहित्य इस संघ भेद के मूल का पता लगाने तथा दोनों परम्पराओं को जोड़ने वाला साहित्य है।५ऐसा प्रतीत होता है कि 70 वर्ष में ही समन्वयशील मस्तिष्क संघ भेद के कारण व्यथि था तथा खाई को पाटने जैसा विचार उसके मस्तिष्क में हिलोरें ले रहा था, जिसके कारण यापनीय ( अपरनाम आपुलीय या गोष्य संघ) संघ अस्तित्व में आ गया। लगभग १६वीं शताब्दी में इस संघ का लोप हो गया। कारणों के सम्बन्ध में निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके पश्चात् का इतिहास तो दोनों परम्पराओं के आंतरिक विद्रोह तथा विशृंखलता का इतिहास है। श्वेताम्बर परम्परा में लोकाशाह की परम्परा तथा उसके पश्चात् स्थानकवासी तेरह पंथ का उदय हआ। दिगम्बर परम्परा मी अहती नहीं रही। स्व० तारणस्वामी का तारण पंथ स्वर्गीय श्री कानजी स्वामी तथा स्वर्गीय श्री रायचन्द माई की परम्परा भी चली / तात्पर्य यह है कि जैन संघ की शक्ति का विभाजन होता रहा। जैन संघ की इस विशृंखल प्रधान प्रवृत्ति को देखकर बड़े दुःखी हृदय से महान अध्यात्मयोगी श्री आनन्दधनजी ने एक पद कहा था, जसका अर्थ है कि गच्छ में बहुत भेद प्रभेद अपनी आँख से देखते हुए तत्व चर्चा करते हुए लज्जा नहीं आती ? कलियग में दराग्रहों से ग्रस्त होकर अपनी भख ( वैयक्तिक पूजा-प्रतिष्ठा की तषणा ) मिटाने के लिये प्रयत्नशील है। तात्पर्य यह है कि वैयक्तिक भूख को सैद्धान्तिक जामा पहनाकर श्री संघ में विशृंखलता लाई गई है। हमारा जैन समाज जाति, सम्प्रदाय, आदि विभिन्न प्रकार से विशृंखलित है। हम अनेकांत तथा स्याद्वाद की प्रशंसा के गीत गाते हुए भी पूरे एकांतवादी हो गये हैं। पूरे जैन समाज में कोई ऐसा प्रामाणिक समन्वयशील, अनेकांतिक विचारधारा का पक्षधर ( जिसकी वाणी तथा कर्म में साम्य है ) महापुरुष नहीं है जो इस विशृंखलित जैन समाज में एकता का वातावरण निर्माण करके सशक्त अखिल जैन समाज को अस्तित्व में लाने की क्षमता से सम्पन्न हो। इस निराशाजनक स्थिति में भी मैं निराश नहीं हूं। मेरा विश्वास है कि काल निरवधि है, पृथ्वी विपुल है। कोई कालजयी महापुरुष अवश्य इस महान कार्य को संपन्न करेगा। उपस्यन्ते तु मां समान धर्मा, कालो निरवषिः विपुला च पृथ्वी // 13. जैन साहित्य तथा इतिहास , ले० स्व. नाथूरामजी प्रेमी, पृ० 56, 1956 / 14. वही पृ० 564 / 15. वही पृ०५८। Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org