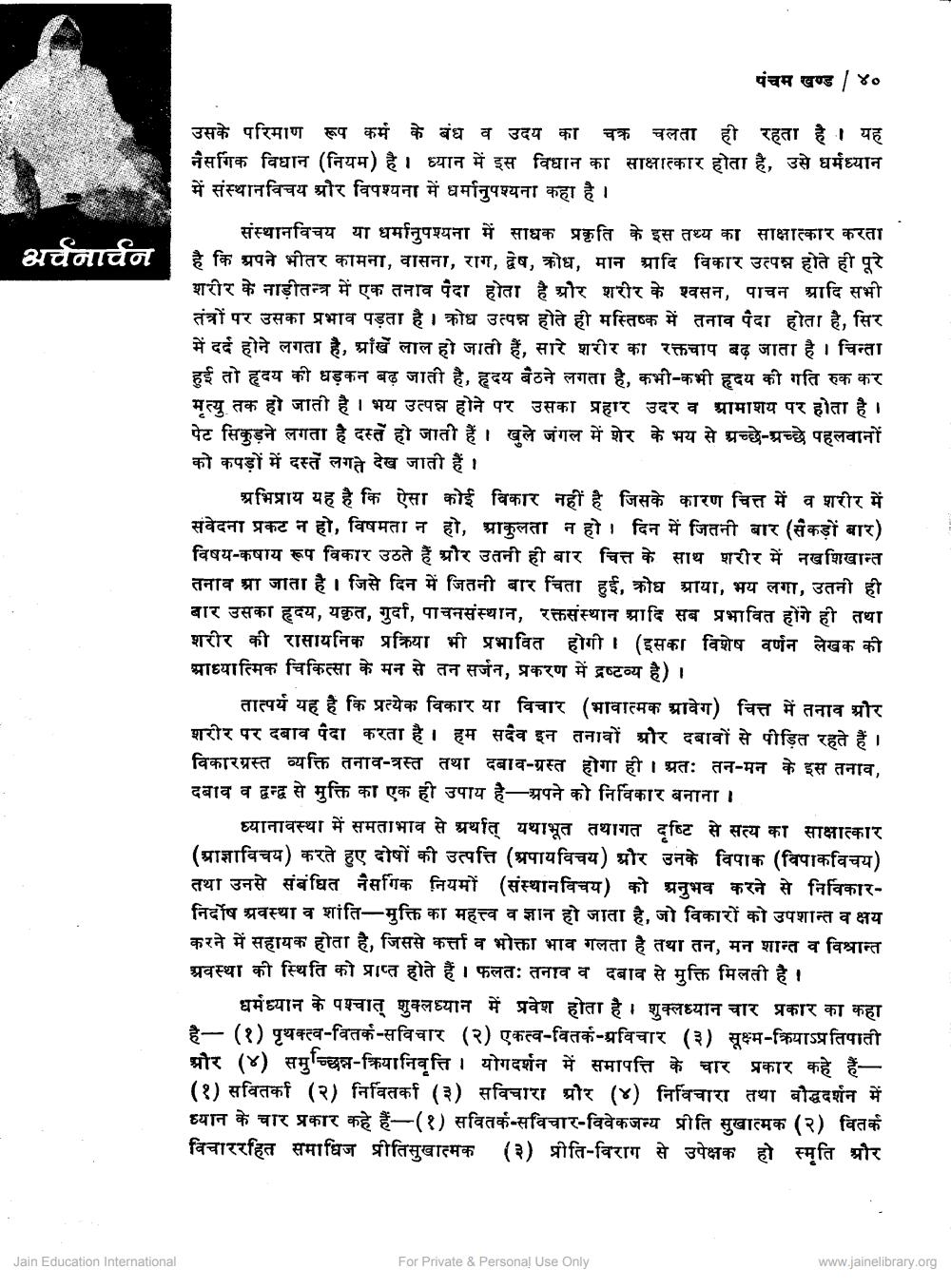________________
पंचम खण्ड / ४०
उसके परिमाण रूप कर्म के बंध व उदय का चक्र चलता ही रहता है । यह नैसर्गिक विधान (नियम) है। ध्यान में इस विधान का साक्षात्कार होता है, उसे धर्मध्यान में संस्थानविचय और विपश्यना में धर्मानुपश्यना कहा है।
अर्चनार्चन
संस्थानविचय या धर्मानुपश्यना में साधक प्रकृति के इस तथ्य का साक्षात्कार करता है कि अपने भीतर कामना, वासना, राग, द्वेष, क्रोध, मान आदि विकार उत्पन्न होते ही पूरे शरीर के नाड़ीतन्त्र में एक तनाव पैदा होता है और शरीर के श्वसन, पाचन आदि सभी तंत्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है। क्रोध उत्पन्न होते ही मस्तिष्क में तनाव पैदा होता है, सिर में दर्द होने लगता है, अाँखें लाल हो जाती हैं, सारे शरीर का रक्तचाप बढ़ जाता है । चिन्ता हुई तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, हृदय बैठने लगता है, कभी-कभी हृदय की गति रुक कर मत्यु तक हो जाती है । भय उत्पन्न होने पर उसका प्रहार उदर व प्रामाशय पर होता है। पेट सिकुड़ने लगता है दस्त हो जाती हैं। खुले जंगल में शेर के भय से अच्छे-अच्छे पहलवानों को कपड़ों में दस्त लगते देख जाती हैं।
अभिप्राय यह है कि ऐसा कोई विकार नहीं है जिसके कारण चित्त में व शरीर में संवेदना प्रकट न हो, विषमता न हो, आकुलता न हो। दिन में जितनी बार (सैकड़ों बार) विषय-कषाय रूप विकार उठते हैं और उतनी ही बार चित्त के साथ शरीर में नखशिखान्त तनाव पा जाता है। जिसे दिन में जितनी बार चिंता हुई, क्रोध आया, भय लगा, उतनी ही बार उसका हृदय, यकृत, गुर्दा, पाचनसंस्थान, रक्तसंस्थान प्रादि सब प्रभावित होंगे ही तथा शरीर की रासायनिक प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। (इसका विशेष वर्णन लेखक की आध्यात्मिक चिकित्सा के मन से तन सर्जन, प्रकरण में द्रष्टव्य है)।
तात्पर्य यह है कि प्रत्येक विकार या विचार (भावात्मक आवेग) चित्त में तनाव और शरीर पर दबाव पैदा करता है। हम सदैव इन तनावों और दबावों से पीड़ित रहते हैं । विकारग्रस्त व्यक्ति तनाव-त्रस्त तथा दबाव-ग्रस्त होगा ही। अतः तन-मन के इस तनाव, दबाव व द्वन्द्व से मुक्ति का एक ही उपाय है-अपने को निर्विकार बनाना।
ध्यानावस्था में समताभाव से अर्थात् यथाभूत तथागत दृष्टि से सत्य का साक्षात्कार (प्राज्ञाविचय) करते हुए दोषों की उत्पत्ति (अपायविचय) और उनके विपाक (विपाकविचय) तथा उनसे संबंधित नैसर्गिक नियमों (संस्थानविचय) को अनुभव करने से निर्विकारनिर्दोष अवस्था व शांति-मुक्ति का महत्त्व व ज्ञान हो जाता है, जो विकारों को उपशान्त व क्षय करने में सहायक होता है, जिससे कर्ता व भोक्ता भाव गलता है तथा तन, मन शान्त व विश्रान्त अवस्था की स्थिति को प्राप्त होते हैं । फलतः तनाव व दबाव से मुक्ति मिलती है।
धर्मध्यान के पश्चात् शुक्लध्यान में प्रवेश होता है। शुक्लध्यान चार प्रकार का कहा है- (१) पृथक्त्व-वितर्क-सविचार (२) एकत्व-वितर्क-विचार (३) सूक्ष्म-क्रियाऽप्रतिपाती और (४) समुच्छिन्न-क्रियानिवृत्ति । योगदर्शन में समापत्ति के चार प्रकार कहे हैं(१) सवितर्का (२) निर्वितर्का (३) सविचारा और (४) निर्विचारा तथा बौद्धदर्शन में ध्यान के चार प्रकार कहे हैं-(१) सवितर्क-सविचार-विवेकजन्य प्रीति सुखात्मक (२) वितर्क विचाररहित समाधिज प्रीतिसुखात्मक (३) प्रीति-विराग से उपेक्षक हो स्मृति और
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org