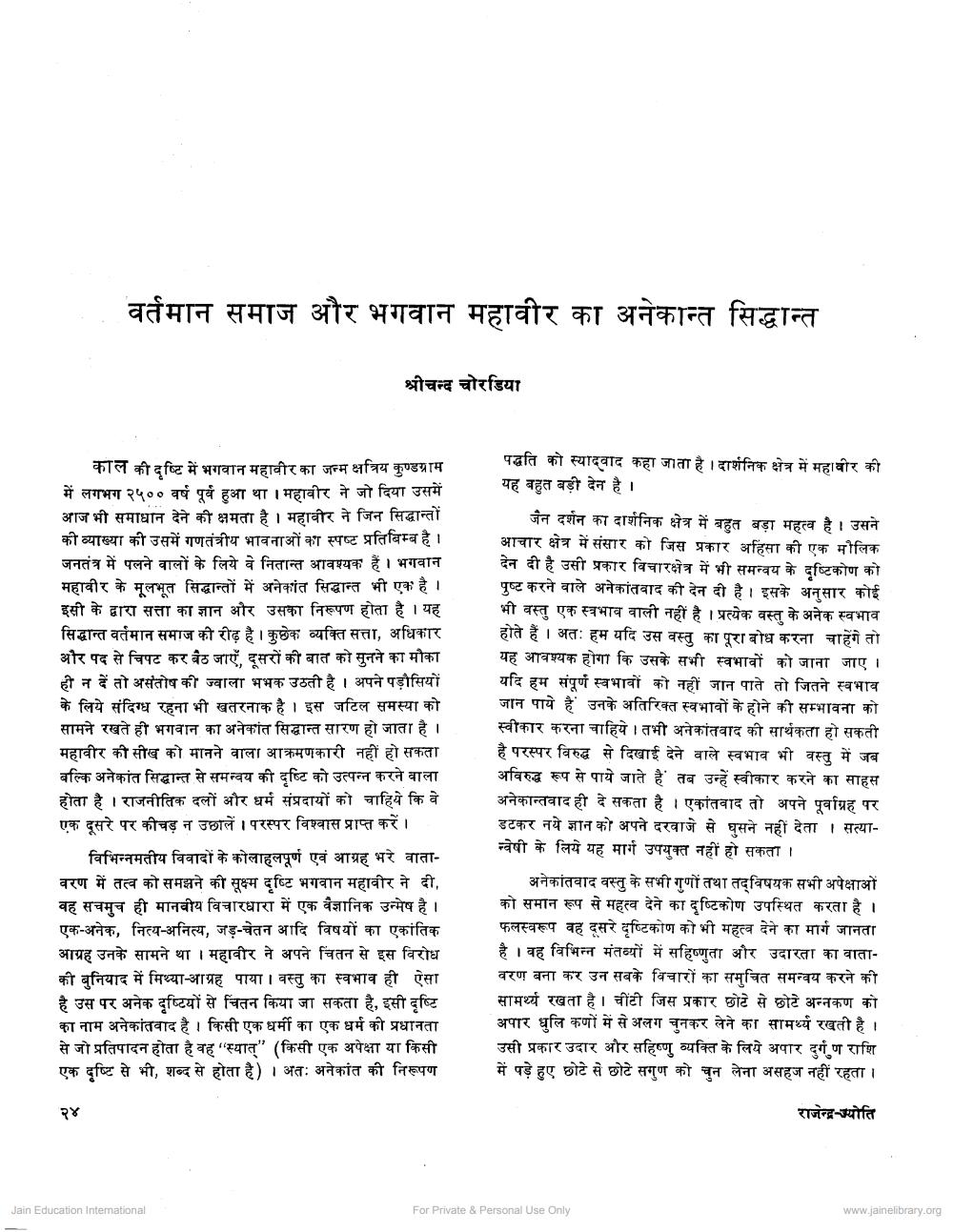________________
वर्तमान समाज और भगवान महावीर का अनेकान्त सिद्धान्त
श्रीचन्द चोरडिया
काल की दृष्टि में भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय कुण्डग्राम में लगभग २५०० वर्ष पूर्व हुआ था । महावीर ने जो दिया उसमें आज भी समाधान देने की क्षमता है। महावीर ने जिन सिद्धान्तों की व्याख्या की उसमें गणतंत्रीय भावनाओं का स्पष्ट प्रतिबिम्ब है। जनतंत्र में पलने वालों के लिये वे नितान्त आवश्यक हैं । भगवान महावीर के मूलभूत सिद्धान्तों में अनेकांत सिद्धान्त भी एक है । इसी के द्वारा सत्ता का ज्ञान और उसका निरूपण होता है । यह सिद्धान्त वर्तमान समाज की रीढ़ है । कुछेक व्यक्ति सत्ता, अधिकार
और पद से चिपट कर बैठ जाएँ, दूसरों की बात को सुनने का मौका ही न दें तो असंतोष की ज्वाला भभक उठती है । अपने पड़ोसियों के लिये संदिग्ध रहना भी खतरनाक है। इस जटिल समस्या को सामने रखते ही भगवान का अनेकांत सिद्धान्त सारण हो जाता है । महावीर की सीख को मानने वाला आक्रमणकारी नहीं हो सकता बल्कि अनेकांत सिद्धान्त से समन्वय की दृष्टि को उत्पन्न करने वाला होता है । राजनीतिक दलों और धर्म संप्रदायों को चाहिये कि वे एक दूसरे पर कीचड़ न उछालें । परस्पर विश्वास प्राप्त करें।
विभिन्नमतीय विवादों के कोलाहलपूर्ण एवं आग्रह भरे वातावरण में तत्व को समझने की सूक्ष्म दृष्टि भगवान महावीर ने दी, वह सचमुच ही मानवीय विचारधारा में एक वैज्ञानिक उन्मेष है । एक-अनेक, नित्य-अनित्य, जड़-चेतन आदि विषयों का एकांतिक आग्रह उनके सामने था । महावीर ने अपने चिंतन से इस विरोध की बुनियाद में मिथ्या-आग्रह पाया । वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है उस पर अनेक दृष्टियों से चिंतन किया जा सकता है, इसी दृष्टि का नाम अनेकांतवाद है। किसी एक धर्मी का एक धर्म को प्रधानता से जो प्रतिपादन होता है वह "स्यात्” (किसी एक अपेक्षा या किसी एक दृष्टि से भी, शब्द से होता है) । अतः अनेकांत की निरूपण
पद्धति को स्यादवाद कहा जाता है । दार्शनिक क्षेत्र में महावीर की यह बहुत बड़ी देन है।
जैन दर्शन का दार्शनिक क्षेत्र में बहुत बड़ा महत्व है। उसने आचार क्षेत्र में संसार को जिस प्रकार अहिंसा की एक मौलिक देन दी है उसी प्रकार विचारक्षेत्र में भी समन्वय के दृष्टिकोण को पुष्ट करने वाले अनेकांतवाद की देन दी है। इसके अनुसार कोई भी वस्तु एक स्वभाव वाली नहीं है । प्रत्येक वस्तु के अनेक स्वभाव होते हैं । अतः हम यदि उस वस्तु का पूरा बोध करना चाहेंगे तो यह आवश्यक होगा कि उसके सभी स्वभावों को जाना जाए । यदि हम संपूर्ण स्वभावों को नहीं जान पाते तो जितने स्वभाव जान पाये हैं उनके अतिरिक्त स्वभावों के होने की सम्भावना को स्वीकार करना चाहिये । तभी अनेकांतवाद की सार्थकता हो सकती है परस्पर विरुद्ध से दिखाई देने वाले स्वभाव भी वस्तु में जब अविरुद्ध रूप से पाये जाते हैं तब उन्हें स्वीकार करने का साहस अनेकान्तवाद ही दे सकता है । एकांतवाद तो अपने पूर्वाग्रह पर डटकर नये ज्ञान को अपने दरवाजे से घुसने नहीं देता । सत्यान्वेषी के लिये यह मार्ग उपयुक्त नहीं हो सकता ।
अनेकांतवाद वस्तु के सभी गुणों तथा तद्विषयक सभी अपेक्षाओं को समान रूप से महत्व देने का दृष्टिकोण उपस्थित करता है । फलस्वरूप वह दूसरे दृष्टिकोण को भी महत्व देने का मार्ग जानता है । वह विभिन्न मंतव्यों में सहिष्णुता और उदारता का वातावरण बना कर उन सबके विचारों का समुचित समन्वय करने की सामर्थ्य रखता है। चींटी जिस प्रकार छोटे से छोटे अन्नकण को अपार धुलि कणों में से अलग चुनकर लेने का सामर्थ्य रखती है । उसी प्रकार उदार और सहिष्णु व्यक्ति के लिये अपार दुर्ग ण राशि में पड़े हुए छोटे से छोटे सगुण को चुन लेना असहज नहीं रहता।
२४
राजेन्द्र-ज्योति
Jain Education Interational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org