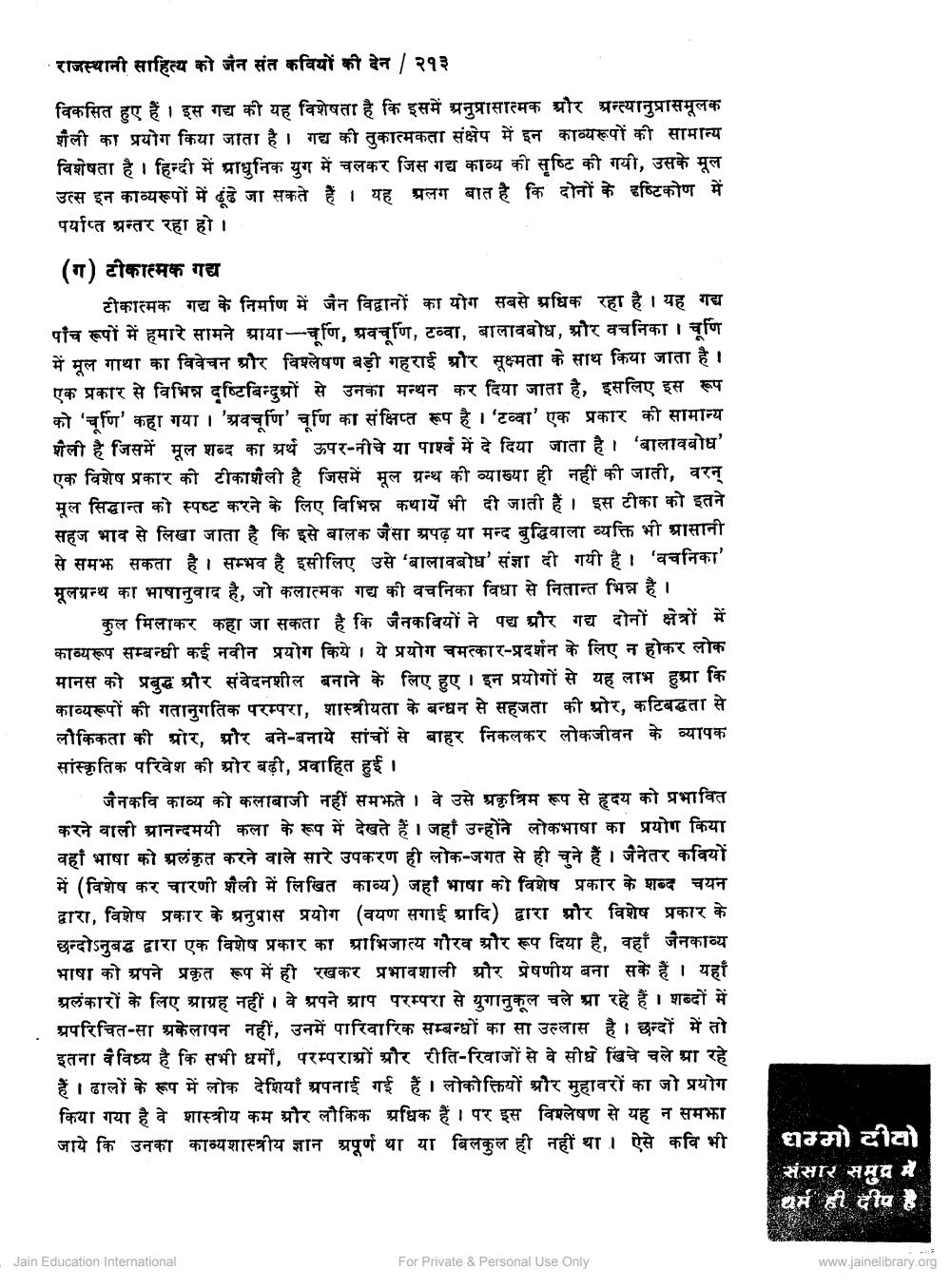________________
राजस्थानी साहित्य को जैन संत कवियों की देन / २१३
विकसित हुए हैं । इस गद्य की यह विशेषता है कि इसमें अनुप्रासात्मक और अन्त्यानुप्रासमूलक शैली का प्रयोग किया जाता है। गद्य की तुकात्मकता संक्षेप में इन काव्यरूपों की सामान्य विशेषता है। हिन्दी में प्राधुनिक युग में चलकर जिस गद्य काव्य की सृष्टि की गयी, उसके मूल उत्स इन काव्यरूपों में ढंढे जा सकते हैं । यह अलग बात है कि दोनों के दृष्टिकोण में पर्याप्त अन्तर रहा हो।
(ग) टीकात्मक गद्य
टीकात्मक गद्य के निर्माण में जैन विद्वानों का योग सबसे अधिक रहा है। यह गद्य पांच रूपों में हमारे सामने आया-चूणि, अवचूणि, टव्वा, बालावबोध, और वचनिका । चूणि में मूल गाथा का विवेचन और विश्लेषण बड़ी गहराई और सूक्ष्मता के साथ किया जाता है। एक प्रकार से विभिन्न दृष्टिबिन्दुओं से उनका मन्थन कर दिया जाता है, इसलिए इस रूप को 'चूणि' कहा गया। 'प्रवचूर्णि' चूणि का संक्षिप्त रूप है। 'टव्वा' एक प्रकार की सामान्य शैली है जिसमें मूल शब्द का अर्थ ऊपर-नीचे या पार्श्व में दे दिया जाता है। 'बालावबोध' एक विशेष प्रकार की टीकाशैली है जिसमें मूल ग्रन्थ की व्याख्या ही नहीं की जाती, वरन् मूल सिद्धान्त को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न कथायें भी दी जाती हैं। इस टीका को इतने सहज भाव से लिखा जाता है कि इसे बालक जैसा अपढ़ या मन्द बुद्धिवाला व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है। सम्भव है इसीलिए उसे 'बालावबोध' संज्ञा दी गयी है। 'वचनिका' मूलग्रन्थ का भाषानुवाद है, जो कलात्मक गद्य की वचनिका विधा से नितान्त भिन्न है।
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जैनकवियों ने पद्य और गद्य दोनों क्षेत्रों में काव्यरूप सम्बन्धी कई नवीन प्रयोग किये । ये प्रयोग चमत्कार-प्रदर्शन के लिए न होकर लोक मानस को प्रबुद्ध और संवेदनशील बनाने के लिए हुए । इन प्रयोगों से यह लाभ हुप्रा कि काव्यरूपों की गतानुगतिक परम्परा, शास्त्रीयता के बन्धन से सहजता की प्रोर, कटिबद्धता से लौकिकता की पोर, और बने-बनाये सांचों से बाहर निकलकर लोकजीवन के व्यापक सांस्कृतिक परिवेश की ओर बढ़ी, प्रवाहित हुई।
जैनकवि काव्य को कलाबाजी नहीं समझते। वे उसे अकृत्रिम रूप से हृदय को प्रभावित करने वाली प्रानन्दमयी कला के रूप में देखते हैं। जहां उन्होंने लोकभाषा का प्रयोग किया वहाँ भाषा को अलंकृत करने वाले सारे उपकरण ही लोक-जगत से ही चने हैं। जैनेतर कवियों में (विशेष कर चारणी शैली में लिखित काव्य) जहाँ भाषा को विशेष प्रकार के शब्द चयन द्वारा, विशेष प्रकार के अनुप्रास प्रयोग (वयण सगाई आदि) द्वारा और विशेष प्रकार के छन्दोऽनुबद्ध द्वारा एक विशेष प्रकार का प्राभिजात्य गौरव और रूप दिया है, वहाँ जैनकाव्य भाषा को अपने प्रकृत रूप में ही रखकर प्रभावशाली और प्रेषणीय बना सके हैं । यहाँ अलंकारों के लिए आग्रह नहीं। वे अपने आप परम्परा से युगानुकूल चले आ रहे हैं। शब्दों में अपरिचित-सा अकेलापन नहीं, उनमें पारिवारिक सम्बन्धों का सा उल्लास है। छन्दों में तो इतना वैविध्य है कि सभी धर्मों, परम्पराओं और रीति-रिवाजों से वे सीधे खिचे चले पा रहे हैं । ढालों के रूप में लोक देशियां अपनाई गई हैं। लोकोक्तियों और मुहावरों का जो प्रयोग किया गया है वे शास्त्रीय कम और लौकिक अधिक हैं। पर इस विश्लेषण से यह न समझा जाये कि उनका काव्यशास्त्रीय ज्ञान अपूर्ण था या बिलकुल ही नहीं था। ऐसे कवि भी
धम्मो दीवो संसार समुद्र में धर्म ही दीय है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org