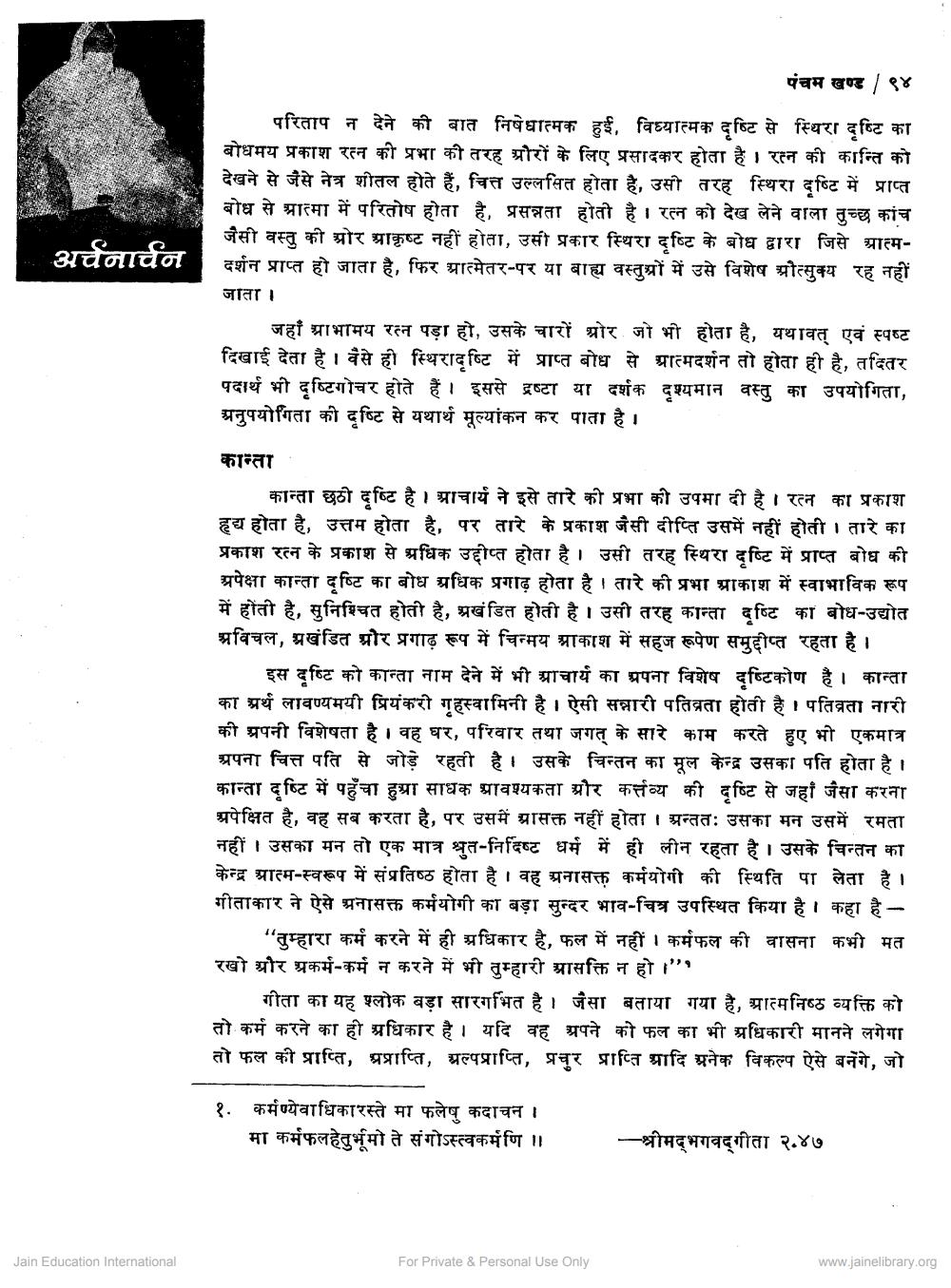________________
पंचम खण्ड / ९४
अर्चनार्चन
परिताप न देने की बात निषेधात्मक हुई, विध्यात्मक दृष्टि से स्थिरा दृष्टि का बोधमय प्रकाश रत्न की प्रभा की तरह औरों के लिए प्रसादकर होता है। रत्न की कान्ति को देखने से जैसे नेत्र शीतल होते हैं, चित्त उल्लसित होता है, उसी तरह स्थिरा दृष्टि में प्राप्त बोध से प्रात्मा में परितोष होता है, प्रसन्नता होती है। रत्न को देख लेने वाला तुच्छ कांच जैसी वस्तु की ओर आकृष्ट नहीं होता, उसी प्रकार स्थिरा दृष्टि के बोध द्वारा जिसे प्रात्मदर्शन प्राप्त हो जाता है, फिर आत्मेतर-पर या बाह्य वस्तुओं में उसे विशेष प्रौत्सुक्य रह नहीं जाता।
जहाँ आभामय रत्न पड़ा हो, उसके चारों ओर जो भी होता है, यथावत् एवं स्पष्ट दिखाई देता है। वैसे ही स्थिरादृष्टि में प्राप्त बोध से प्रात्मदर्शन तो होता ही है, तदितर पदार्थ भी दृष्टिगोचर होते हैं। इससे द्रष्टा या दर्शक दृश्यमान वस्तु का उपयोगिता, अनुपयोगिता की दृष्टि से यथार्थ मूल्यांकन कर पाता है।
कान्ता
__ कान्ता छठी दृष्टि है। प्राचार्य ने इसे तारे की प्रभा की उपमा दी है। रत्न का प्रकाश हृद्य होता है, उत्तम होता है, पर तारे के प्रकाश जैसी दीप्ति उसमें नहीं होती। तारे का प्रकाश रत्न के प्रकाश से अधिक उद्दीप्त होता है। उसी तरह स्थिरा दृष्टि में प्राप्त बोध की अपेक्षा कान्ता दष्टि का बोध अधिक प्रगाढ़ होता है। तारे की प्रभा पाकाश में स्वाभाविक रूप में होती है, सुनिश्चित होती है, अखंडित होती है। उसी तरह कान्ता दृष्टि का बोध-उद्योत अविचल, अखंडित और प्रगाढ़ रूप में चिन्मय आकाश में सहज रूपेण समुद्दीप्त रहता है।
इस दृष्टि को कान्ता नाम देने में भी प्राचार्य का अपना विशेष दृष्टिकोण है। कान्ता का अर्थ लावण्यमयी प्रियंकरी गहस्वामिनी है। ऐसी सन्नारी पतिव्रता होती है। पतिव्रता नारी की अपनी विशेषता है। वह घर, परिवार तथा जगत् के सारे काम करते हुए भी एकमात्र अपना चित्त पति से जोड़े रहती है। उसके चिन्तन का मूल केन्द्र उसका पति होता है। कान्ता दष्टि में पहँचा हुअा साधक आवश्यकता और कर्त्तव्य की दृष्टि से जहाँ जैसा करना अपेक्षित है, वह सब करता है, पर उसमें प्रासक्त नहीं होता । अन्तत: उसका मन उसमें रमता नहीं। उसका मन तो एक मात्र श्रुत-निर्दिष्ट धर्म में ही लीन रहता है। उसके चिन्तन का केन्द्र आत्म-स्वरूप में संप्रतिष्ठ होता है। वह अनासक्त कर्मयोगी की स्थिति पा लेता है। गीताकार ने ऐसे अनासक्त कर्मयोगी का बड़ा सुन्दर भाव-चित्र उपस्थित किया है। कहा है
"तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं । कर्मफल की वासना कभी मत रखो और अकर्म-कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति न हो।''
गीता का यह श्लोक बड़ा सारगभित है। जैसा बताया गया है, अात्मनिष्ठ व्यक्ति को तो कर्म करने का ही अधिकार है। यदि वह अपने को फल का भी अधिकारी मानने लगेगा तो फल की प्राप्ति, अप्राप्ति, अल्पप्राप्ति, प्रचुर प्राप्ति आदि अनेक विकल्प ऐसे बनेंगे, जो
१. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भमो ते संगोऽस्त्वकर्मणि ।।
-श्रीमद्भगवद्गीता २.४७
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org