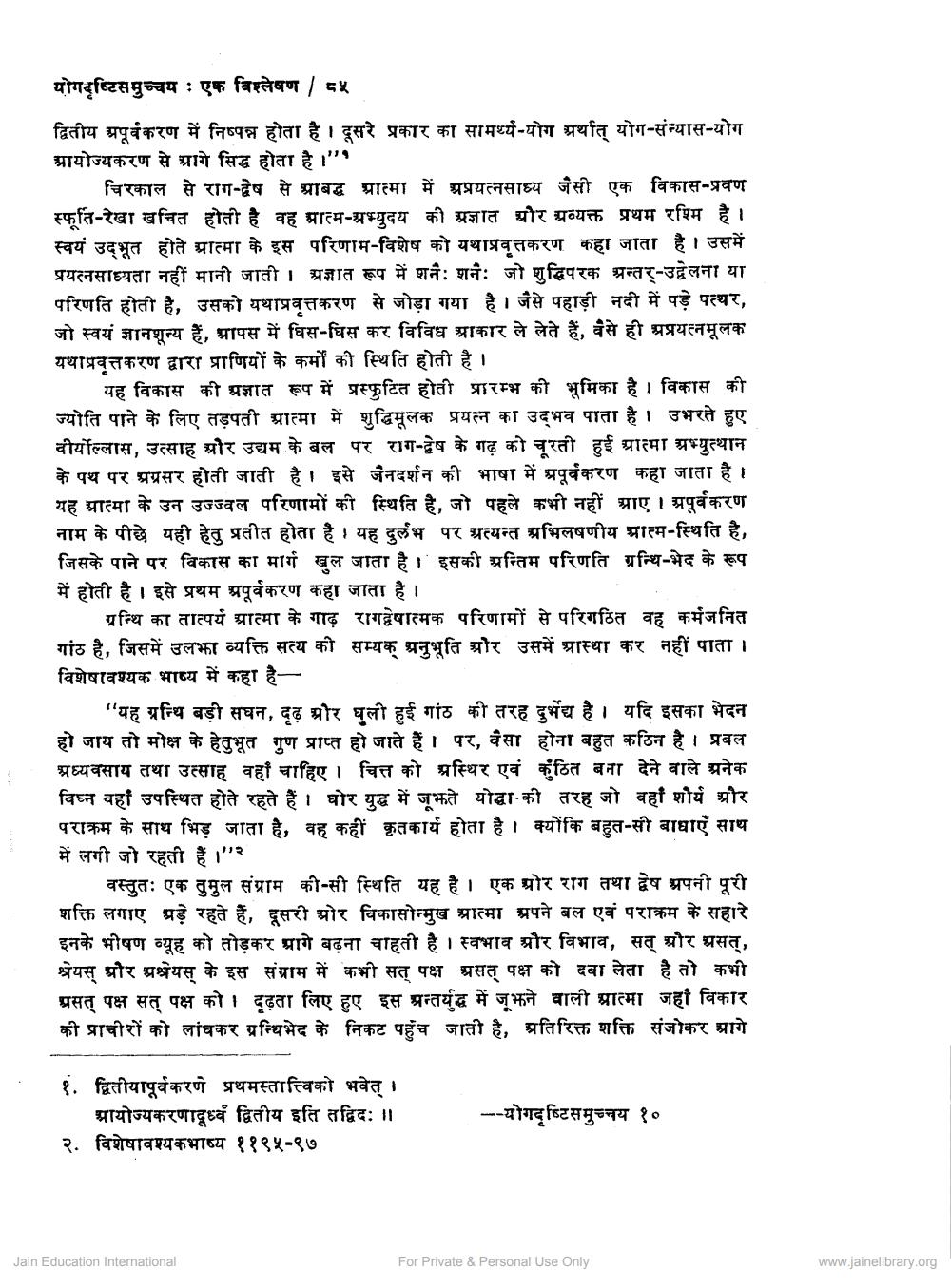________________
योगदृष्टिसमुच्चय : एक विश्लेषण / ८५ द्वितीय अपूर्वकरण में निष्पन्न होता है । दूसरे प्रकार का सामर्थ्य-योग अर्थात् योग-संन्यास-योग आयोज्यकरण से आगे सिद्ध होता है।''
चिरकाल से राग-द्वेष से प्राबद्ध प्रात्मा में अप्रयत्नसाध्य जैसी एक विकास-प्रवण स्फूर्ति-रेखा खचित होती है वह प्रात्म-अभ्युदय की अज्ञात और अव्यक्त प्रथम रश्मि है। स्वयं उद्भूत होते प्रात्मा के इस परिणाम-विशेष को यथाप्रवृत्तकरण कहा जाता है। उसमें प्रयत्नसाध्यता नहीं मानी जाती। अज्ञात रूप में शनैः शनैः जो शुद्धिपरक अन्तर्-उद्वेलना या परिणति होती है, उसको यथाप्रवृत्तकरण से जोड़ा गया है। जैसे पहाड़ी नदी में पड़े पत्थर, जो स्वयं ज्ञानशून्य हैं, आपस में घिस-घिस कर विविध आकार ले लेते हैं, वैसे ही अप्रयत्नमूलक यथाप्रवृत्तकरण द्वारा प्राणियों के कर्मों की स्थिति होती है।
यह विकास की अज्ञात रूप में प्रस्फुटित होती प्रारम्भ की भूमिका है। विकास की ज्योति पाने के लिए तडपती प्रात्मा में शुद्धिमुलक प्रयत्न का उदभव पाता है। उभरते हुए वीर्योल्लास, उत्साह और उद्यम के बल पर राग-द्वेष के गढ़ को चूरती हुई प्रात्मा अभ्युत्थान के पथ पर अग्रसर होती जाती है। इसे जैनदर्शन की भाषा में अपूर्वकरण कहा जाता है। यह आत्मा के उन उज्ज्वल परिणामों की स्थिति है, जो पहले कभी नहीं आए । अपूर्वकरण नाम के पीछे यही हेतु प्रतीत होता है। यह दुर्लभ पर अत्यन्त अभिलषणीय प्रात्म-स्थिति है, जिसके पाने पर विकास का मार्ग खुल जाता है। इसकी अन्तिम परिणति ग्रन्थि-भेद के रूप में होती है । इसे प्रथम अपूर्वकरण कहा जाता है ।
ग्रन्थि का तात्पर्य आत्मा के गाढ़ रागद्वेषात्मक परिणामों से परिगठित वह कर्मजनित गांठ है, जिसमें उलझा व्यक्ति सत्य की सम्यक् अनुभूति और उसमें आस्था कर नहीं पाता। विशेषावश्यक भाष्य में कहा है
"यह ग्रन्थि बड़ी सघन, दृढ़ और घुली हुई गांठ की तरह दुर्भेद्य है। यदि इसका भेदन हो जाय तो मोक्ष के हेतुभूत गुण प्राप्त हो जाते हैं। पर, वैसा होना बहुत कठिन है। प्रबल अध्यवसाय तथा उत्साह वहाँ चाहिए। चित्त को अस्थिर एवं कुंठित बना देने वाले अनेक विघ्न वहां उपस्थित होते रहते हैं। घोर यद्ध में जझते योद्धा की तरह जो वहाँ शौर्य और पराक्रम के साथ भिड़ जाता है, वह कहीं कृतकार्य होता है। क्योंकि बहुत-सी बाधाएँ साथ में लगी जो रहती हैं।"२
वस्तुतः एक तुमुल संग्राम की-सी स्थिति यह है। एक पोर राग तथा द्वेष अपनी पूरी शक्ति लगाए अड़े रहते हैं, दूसरी ओर विकासोन्मुख पात्मा अपने बल एवं पराक्रम के सहारे इनके भीषण व्यूह को तोड़कर भागे बढ़ना चाहती है । स्वभाव और विभाव, सत् और असत्, श्रेयस् और अश्रेयस् के इस संग्राम में कभी सत् पक्ष असत् पक्ष को दबा लेता है तो कभी प्रसत् पक्ष सत् पक्ष को। दृढ़ता लिए हुए इस अन्तर्युद्ध में जझने वाली प्रात्मा जहाँ विकार की प्राचीरों को लांघकर ग्रन्थिभेद के निकट पहंच जाती है, अतिरिक्त शक्ति संजोकर पागे
१. द्वितीयापूर्वकरणे प्रथमस्तात्त्विको भवेत् ।
प्रायोज्यकरणावं द्वितीय इति तद्विदः ।। २. विशेषावश्यकभाष्य ११९५-९७
-~-योगदृष्टिसमुच्चय १०
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org