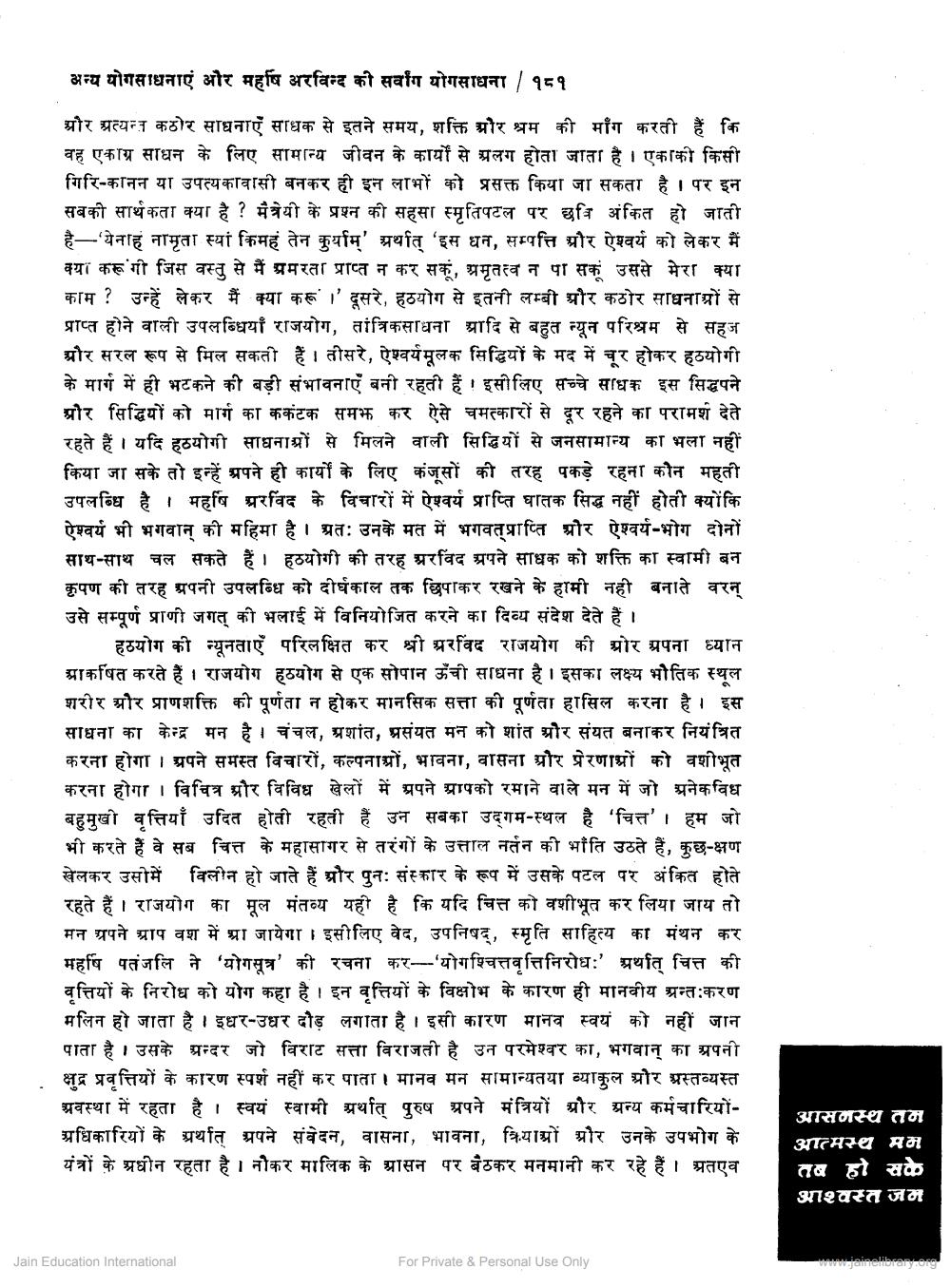________________
अन्य योगसाधनाएं और महर्षि अरविन्द की सर्वांग योगसाधना | १८१
और अत्यन्त कठोर साधनाएँ साधक से इतने समय, शक्ति और श्रम की माँग करती हैं कि वह एकाग्र साधन के लिए सामान्य जीवन के कार्यों से अलग होता जाता है । एकाकी किसी गिरि-कानन या उपत्यकावासी बनकर ही इन लाभों को प्रसक्त किया जा सकता है । पर इन सबकी सार्थकता क्या है ? मैत्रेयी के प्रश्न की सहसा स्मृतिपटल पर छवि अंकित हो जाती है—'येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्याम्' अर्थात् 'इस धन, सम्पत्ति और ऐश्वर्य को लेकर मैं क्या करूगी जिस वस्तु से मैं अमरता प्राप्त न कर सकू, अमृतत्व न पा सकू उससे मेरा क्या काम? उन्हें लेकर मैं क्या करू ।' दूसरे, हठयोग से इतनी लम्बी और कठोर साधनाओं से प्राप्त होने वाली उपलब्धियाँ राजयोग, तांत्रिकसाधना आदि से बहुत न्यून परिश्रम से सहज और सरल रूप से मिल सकती हैं। तीसरे, ऐश्वर्यमूलक सिद्धियों के मद में चूर होकर हठयोगी के मार्ग में ही भटकने की बड़ी संभावनाएँ बनी रहती हैं। इसीलिए सच्चे साधक इस सिद्धपने और सिद्धियों को मार्ग का ककंटक समझ कर ऐसे चमत्कारों से दूर रहने का परामर्श देते रहते हैं। यदि हठयोगी साधनाओं से मिलने वाली सिद्धियों से जनसामान्य का भला नहीं किया जा सके तो इन्हें अपने ही कार्यों के लिए कंजूसों की तरह पकड़े रहना कौन महती उपलब्धि है । महर्षि अरविंद के विचारों में ऐश्वर्य प्राप्ति घातक सिद्ध नहीं होती क्योंकि ऐश्वर्य भी भगवान् की महिमा है । अत: उनके मत में भगवत्प्राप्ति और ऐश्वर्य-भोग दोनों साथ-साथ चल सकते हैं। हठयोगी की तरह अरविंद अपने साधक को शक्ति का स्वामी बन कृपण की तरह अपनी उपलब्धि को दीर्घकाल तक छिपाकर रखने के हामी नही बनाते वरन् उसे सम्पूर्ण प्राणी जगत् की भलाई में विनियोजित करने का दिव्य संदेश देते हैं।
हठयोग की न्यूनताएँ परिलक्षित कर श्री अरविंद राजयोग की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं । राजयोग हठयोग से एक सोपान ऊँची साधना है। इसका लक्ष्य भौतिक स्थल शरीर और प्राणशक्ति की पूर्णता न होकर मानसिक सत्ता की पूर्णता हासिल करना है। इस साधना का केन्द्र मन है। चंचल, प्रशांत, प्रसंयत मन को शांत और संयत बनाकर नियंत्रित करना होगा। अपने समस्त विचारों, कल्पनाओं, भावना, वासना और प्रेरणाओं को वशीभूत करना होगा । विचित्र और विविध खेलों में अपने आपको रमाने वाले मन में जो अनेकविध बहुमुखी वृत्तियाँ उदित होती रहती हैं उन सबका उद्गम-स्थल है 'चित्त'। हम जो भी करते हैं वे सब चित्त के महासागर से तरंगों के उत्ताल नर्तन की भाँति उठते हैं, कुछ-क्षण खेलकर उसोमें विलीन हो जाते हैं और पुन: संस्कार के रूप में उसके पटल पर अंकित होते रहते हैं। राजयोग का मूल मंतव्य यही है कि यदि चित्त को वशीभूत कर लिया जाय तो मन अपने आप वश में पा जायेगा। इसीलिए वेद, उपनिषद्, स्मृति साहित्य का मंथन कर महर्षि पतंजलि ने 'योगसूत्र' की रचना कर-'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' अर्थात् चित्त की वत्तियों के निरोध को योग कहा है। इन वृत्तियों के विक्षोभ के कारण ही मानवीय अन्तःकरण मलिन हो जाता है। इधर-उधर दौड़ लगाता है। इसी कारण मानव स्वयं को नहीं जान पाता है । उसके अन्दर जो विराट सत्ता विराजती है उन परमेश्वर का, भगवान् का अपनी क्षुद्र प्रवृत्तियों के कारण स्पर्श नहीं कर पाता। मानव मन सामान्यतया व्याकुल और अस्तव्यस्त अवस्था में रहता है। स्वयं स्वामी अर्थात् पुरुष अपने मंत्रियों और अन्य कर्मचारियोंअधिकारियों के प्रति अपने संवेदन, वासना, भावना, क्रियाओं और उनके उपभोग के यंत्रों के अधीन रहता है। नौकर मालिक के आसन पर बैठकर मनमानी कर रहे हैं। अतएव
आसनस्थ तम आत्मस्व मम तब हो सके आश्वस्त जम
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org