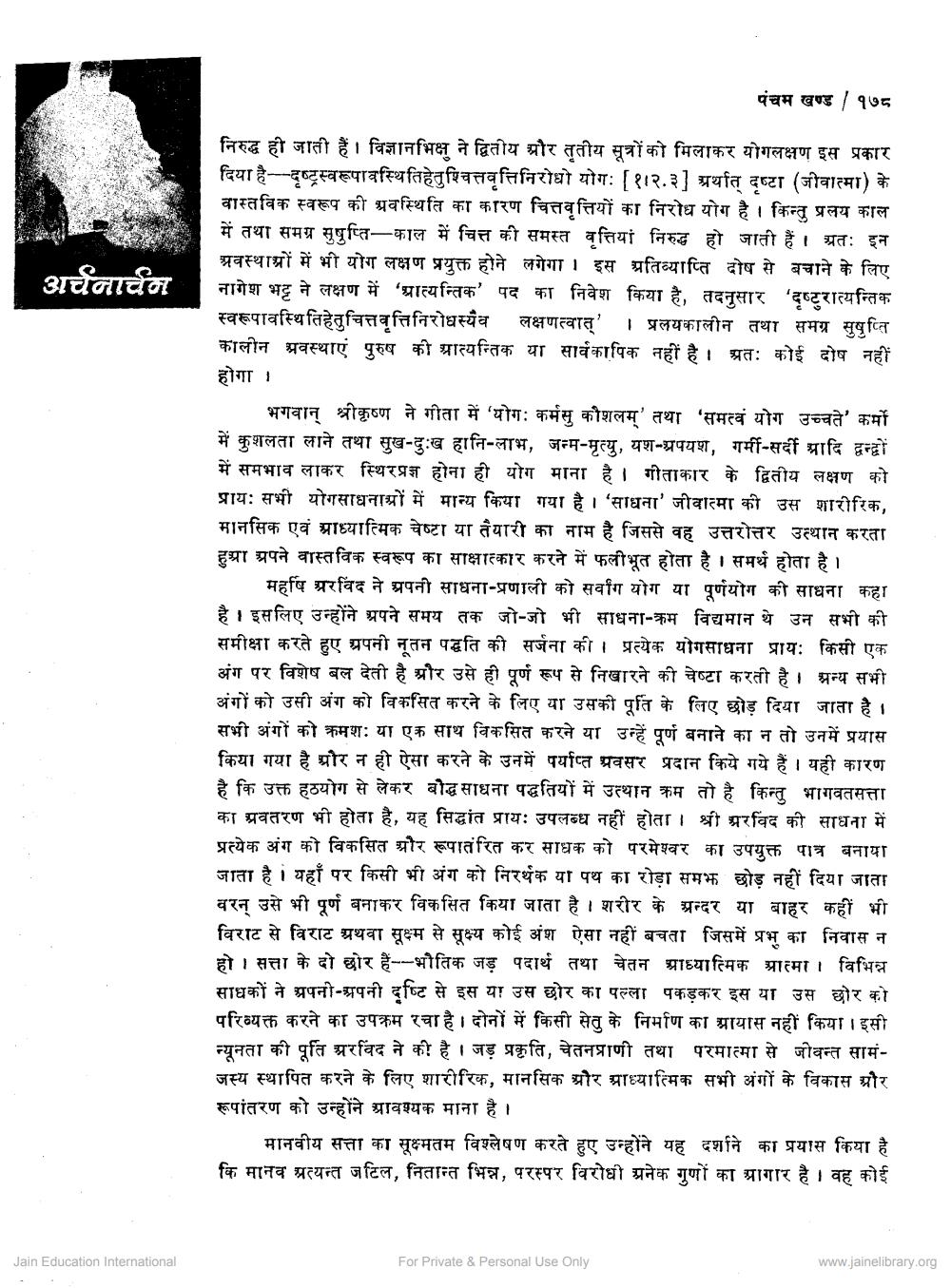________________
पंचम खण्ड / १७८
अर्चनार्चन
निरुद्ध ही जाती हैं। विज्ञानभिक्ष ने द्वितीय और तृतीय सूत्रों को मिलाकर योगलक्षण इस प्रकार दिया है--दृष्ट्रस्वरूपावस्थितिहेतुश्चित्तवृत्तिनिरोधो योगः [११२.३] अर्थात् दृष्टा (जीवात्मा) के वास्तविक स्वरूप की अवस्थिति का कारण चित्तवृत्तियों का निरोध योग है। किन्तु प्रलय काल में तथा समग्र सुषुप्ति-काल में चित्त की समस्त वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं। अत: इन अवस्थानों में भी योग लक्षण प्रयुक्त होने लगेगा। इस अतिव्याप्ति दोष से बचाने के लिए नागेश भट्ट ने लक्षण में 'प्रात्यन्तिक' पद का निवेश किया है, तदनुसार 'दष्ट्रात्यन्तिक स्वरूपावस्थितिहेतुचित्तवृत्तिनिरोधस्यैव लक्षणत्वात्' । प्रलयकालीन तथा समग्र सुषुप्ति कालीन अवस्थाएं पुरुष की प्रात्यन्तिक या सार्वकापिक नहीं है। अत: कोई दोष नहीं होगा ।
भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में 'योगः कर्मसु कौशलम्' तथा 'समत्वं योग उच्चते' कर्मों में कुशलता लाने तथा सुख-दुःख हानि-लाभ, जन्म-मृत्यु, यश-अपयश, गर्मी-सर्दी आदि द्वन्द्वों में समभाव लाकर स्थिरप्रज्ञ होना ही योग माना है। गीताकार के द्वितीय लक्षण को प्रायः सभी योगसाधनाओं में मान्य किया गया है। 'साधना' जीवात्मा की उस शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक चेष्टा या तैयारी का नाम है जिससे वह उत्तरोत्तर उत्थान करता हुया अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करने में फलीभूत होता है । समर्थ होता है।
महर्षि अरविंद ने अपनी साधना-प्रणाली को सर्वांग योग या पूर्णयोग की साधना कहा है। इसलिए उन्होंने अपने समय तक जो-जो भी साधना-क्रम विद्यमान थे उन सभी की समीक्षा करते हए अपनी नतन पद्धति की सर्जना की। प्रत्येक योगसाधना प्रायः किसी एक अंग पर विशेष बल देती है और उसे ही पूर्ण रूप से निखारने की चेष्टा करती है। अन्य सभी अंगों को उसी अंग को विकसित करने के लिए या उसकी पूर्ति के लिए छोड़ दिया जाता है । सभी अंगों को क्रमशः या एक साथ विकसित करने या उन्हें पूर्ण बनाने का न तो उनमें प्रयास किया गया है और न ही ऐसा करने के उनमें पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये हैं। यही कारण है कि उक्त हठयोग से लेकर बौद्ध साधना पद्धतियों में उत्थान क्रम तो है किन्तु भागवतसत्ता का अवतरण भी होता है, यह सिद्धांत प्रायः उपलब्ध नहीं होता। श्री अरविंद की साधना में प्रत्येक अंग को विकसित और रूपातंरित कर साधक को परमेश्वर का उपयुक्त पात्र बनाया जाता है। यहाँ पर किसी भी अंग को निरर्थक या पथ का रोड़ा समझ छोड़ नहीं दिया जाता वरन् उसे भी पूर्ण बनाकर विकसित किया जाता है। शरीर के अन्दर या बाहर कहीं भी विराट से विराट अथवा सूक्ष्म से सूक्ष्य कोई अंश ऐसा नहीं बचता जिसमें प्रभु का निवास न हो । सत्ता के दो छोर हैं--भौतिक जड़ पदार्थ तथा चेतन आध्यात्मिक प्रात्मा। विभिन्न साधकों ने अपनी-अपनी दृष्टि से इस या उस छोर का पल्ला पकड़कर इस या उस छोर को परिव्यक्त करने का उपक्रम रचा है। दोनों में किसी सेतु के निर्माण का प्रायास नहीं किया। इसी न्यूनता की पूर्ति अरविंद ने की है । जड़ प्रकृति, चेतनप्राणी तथा परमात्मा से जीवन्त सामंजस्य स्थापित करने के लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी अंगों के विकास और रूपांतरण को उन्होंने आवश्यक माना है।
मानवीय सत्ता का सूक्ष्मतम विश्लेषण करते हुए उन्होंने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि मानव अत्यन्त जटिल, नितान्त भिन्न, परस्पर विरोधी अनेक गुणों का आगार है। वह कोई
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org