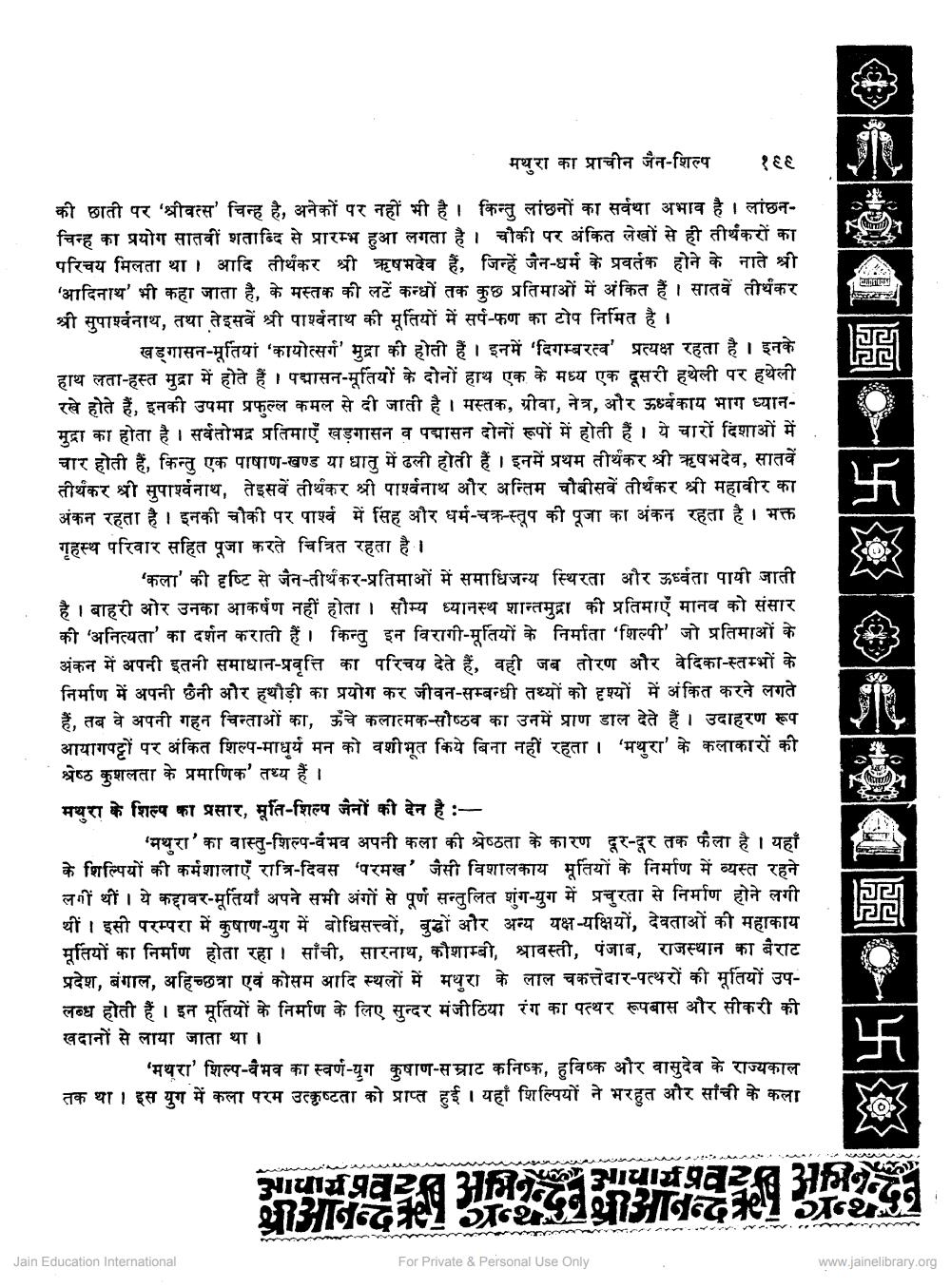________________
मथुरा का प्राचीन जैन-शिल्प
१६९
AIRAT
गातारा
की छाती पर 'श्रीवत्स' चिन्ह है, अनेकों पर नहीं भी है। किन्तु लांछनों का सर्वथा अभाव है । लांछनचिन्ह का प्रयोग सातवीं शताब्दि से प्रारम्भ हुआ लगता है। चौकी पर अंकित लेखों से ही तीर्थंकरों का परिचय मिलता था। आदि तीर्थंकर श्री ऋषभदेव हैं, जिन्हें जैन-धर्म के प्रवर्तक होने के नाते श्री 'आदिनाथ' भी कहा जाता है, के मस्तक की लौ कन्धों तक कुछ प्रतिमाओं में अंकित हैं । सातवें तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ, तथा तेइसवें श्री पार्श्वनाथ की मूर्तियों में सर्प-फण का टोप निर्मित है।
खड्गासन-मूर्तियां 'कायोत्सर्ग' मुद्रा की होती हैं। इनमें 'दिगम्बरत्व' प्रत्यक्ष रहता है। इनके हाथ लता-हस्त मुद्रा में होते हैं । पद्मासन-मूर्तियों के दोनों हाथ एक के मध्य एक दूसरी हथेली पर हथेली रखे होते हैं, इनकी उपमा प्रफुल्ल कमल से दी जाती है। मस्तक, ग्रीवा, नेत्र, और ऊर्ध्वकाय भाग ध्यानमुद्रा का होता है। सर्वतोभद्र प्रतिमाएँ खड़गासन व पद्मासन दोनों रूपों में होती हैं। ये चारों दिशाओं में चार होती हैं, किन्तु एक पाषाण-खण्ड या धातु में ढली होती हैं। इनमें प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव, सातवें तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ, तेइसवें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ और अन्तिम चौबीसवें तीर्थंकर श्री महावीर का अंकन रहता है। इनकी चौकी पर पार्श्व में सिंह और धर्म-चक्र-स्तूप की पूजा का अंकन रहता है। भक्त गृहस्थ परिवार सहित पूजा करते चित्रित रहता है।
'कला' की दृष्टि से जैन-तीर्थंकर-प्रतिमाओं में समाधिजन्य स्थिरता और ऊर्ध्वता पायी जाती है। बाहरी ओर उनका आकर्षण नहीं होता। सौम्य ध्यानस्थ शान्तमुद्रा की प्रतिमाएँ मानव को संसार की 'अनित्यता' का दर्शन कराती हैं। किन्तु इन विरागी-मूर्तियों के निर्माता 'शिल्पी' जो प्रतिमाओं के अंकन में अपनी इतनी समाधान-प्रवृत्ति का परिचय देते हैं, वही जब तोरण और वेदिका-स्तम्भों के निर्माण में अपनी छैनी और हथौड़ी का प्रयोग कर जीवन-सम्बन्धी तथ्यों को दृश्यों में अंकित करने लगते हैं, तब वे अपनी गहन चिन्ताओं का, ऊँचे कलात्मक-सौष्ठव का उनमें प्राण डाल देते हैं। उदाहरण रूप आयागपट्टों पर अंकित शिल्प-माधुर्य मन को वशीभूत किये बिना नहीं रहता। 'मथुरा' के कलाकारों की श्रेष्ठ कुशलता के प्रमाणिक' तथ्य हैं। मथुरा के शिल्प का प्रसार, मूति-शिल्प जैनों की देन है :
'मथरा' का वास्तु-शिल्प-वैभव अपनी कला की श्रेष्ठता के कारण दूर-दूर तक फैला है। यहाँ के शिल्पियों की कर्मशालाएँ रात्रि-दिवस 'परमख' जैसी विशालकाय मूर्तियों के निर्माण में व्यस्त रहने लगीं थीं। ये कहावर-मतियाँ अपने सभी अंगों से पूर्ण सन्तुलित शंग-युग में प्रचुरता से निर्माण होने लगी थीं। इसी परम्परा में कुषाण-युग में बोधिसत्त्वों, बुद्धों और अन्य यक्ष-यक्षियों, देवताओं की महाकाय मूर्तियों का निर्माण होता रहा। साँची, सारनाथ, कौशाम्बी, श्रावस्ती, पंजाब, राजस्थान का बैराट प्रदेश, बंगाल, अहिच्छत्रा एवं कोसम आदि स्थलों में मथरा के लाल चकत्तेदार-पत्थरों की मूर्तियों उपलब्ध होती हैं । इन मूर्तियों के निर्माण के लिए सुन्दर मंजीठिया रंग का पत्थर रूपबास और सीकरी की खदानों से लाया जाता था।
'मथरा' शिल्प-वैभव का स्वर्ण-युग कुषाण-सम्राट कनिष्क, हुविष्क और वासुदेव के राज्यकाल तक था। इस युग में कला परम उत्कृष्टता को प्राप्त हुई । यहाँ शिल्पियों ने भरहुत और सांची के कला
भाचाफारसाआचार्यasan
virynviryiwww
TVVVPw.rY
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org