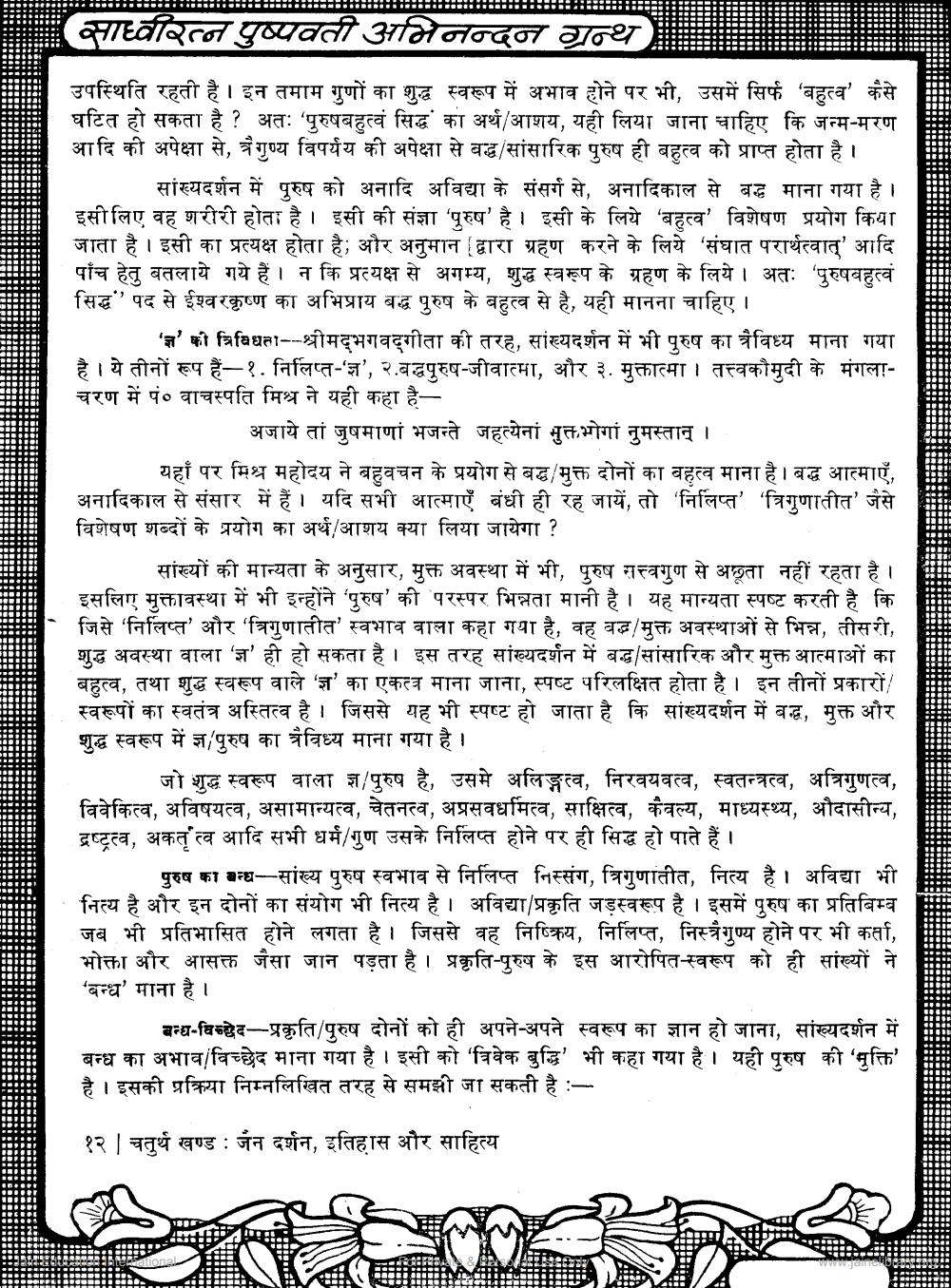________________
साध्वीरत्न पुष्पवती अभिनन्दन ग्रन्थ
उपस्थिति रहती है । इन तमाम गुणों का शुद्ध स्वरूप में अभाव होने पर भी, उसमें सिर्फ 'बहुत्व' कैसे घटित हो सकता है ? अतः 'पुरुषबहुत्वं सिद्ध का अर्थ / आशय, यही लिया जाना चाहिए कि जन्म-मरण आदि की अपेक्षा से त्रैगुण्य विपर्यय की अपेक्षा से बद्ध / सांसारिक पुरुष ही बहुत्व को प्राप्त होता है ।
सांख्यदर्शन में पुरुष को अनादि अविद्या के संसर्ग से, अनादिकाल से बद्ध माना गया है । इसीलिए वह शरीरी होता है। इसी की संज्ञा 'पुरुष' है । इसी के लिये 'बहुत्व' विशेषण प्रयोग किया जाता है । इसी का प्रत्यक्ष होता है; और अनुमान [ द्वारा ग्रहण करने के लिये 'संघात परार्थत्वात्' आदि पाँच हेतु बतलाये गये हैं । न कि प्रत्यक्ष से अगम्य, शुद्ध स्वरूप के ग्रहण के लिये । अतः 'पुरुषबहुत्वं सिद्ध" पद से ईश्वरकृष्ण का अभिप्राय बद्ध पुरुष के बहुत्व से है, यही मानना चाहिए ।
'ज्ञ' की त्रिविधता -- श्रीमद्भगवद्गीता की तरह, सांख्यदर्शन में भी पुरुष का त्रैविध्य माना गया है । ये तीनों रूप हैं—१. निर्लिप्त 'ज्ञ', २. बद्धपुरुष - जीवात्मा, और ३ मुक्तात्मा । तत्त्वकौमुदी के मंगलाचरण में पं० वाचस्पति मिश्र ने यही कहा है
अजाये तां जुषमाणां भजन्ते जहत्येनां मुक्तभोगां नुमस्तान् ।
यहाँ पर मिश्र महोदय ने बहुवचन के प्रयोग से बद्ध / मुक्त दोनों का बहुत्व माना है । बद्ध आत्माएँ, अनादिकाल से संसार में हैं । यदि सभी आत्माएँ बंधी ही रह जायें, तो 'निर्लिप्त' 'त्रिगुणातीत' जैसे विशेषण शब्दों के प्रयोग का अर्थ / आशय क्या लिया जायेगा ?
सांख्यों की मान्यता के अनुसार, मुक्त अवस्था में भी, पुरुष सत्त्वगुण से अछूता नहीं रहता है । इसलिए मुक्तावस्था में भी इन्होंने 'पुरुष' की परस्पर भिन्नता मानी है । यह मान्यता स्पष्ट करती है कि जिसे 'निर्लिप्त' और 'त्रिगुणातीत' स्वभाव वाला कहा गया है, वह बद्ध / मुक्त अवस्थाओं से भिन्न, तीसरी, शुद्ध अवस्था वाला 'ज्ञ' ही हो सकता है । इस तरह सांख्यदर्शन में बद्ध / सांसारिक और मुक्त आत्माओं का बहुत्व, तथा शुद्ध स्वरूप वाले 'ज्ञ' का एकत्व माना जाना, स्पष्ट परिलक्षित होता है। इन तीनों प्रकारों / स्वरूपों का स्वतंत्र अस्तित्व है । जिससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सांख्यदर्शन में बद्ध, मुक्त और शुद्ध स्वरूप में ज्ञ / पुरुष का त्रैविध्य माना गया है ।
जो शुद्ध स्वरूप वाला ज्ञ / पुरुष है, उसमे अलिङ्गत्व, निरवयवत्व, स्वतन्त्रत्व, अत्रिगुणत्व, विवेकित्व, अविषयत्व, असामान्यत्व, चेतनत्व, अप्रसवधर्मित्व, साक्षित्व, कैवल्य, माध्यस्थ्य, औदासीन्य, द्रष्टृत्व, कर्तृत्व आदि सभी धर्म / गुण उसके निर्लिप्त होने पर ही सिद्ध हो पाते हैं ।
पुरुष का बन्ध-सांख्य पुरुष स्वभाव से निर्लिप्त निस्संग, त्रिगुणातीत, नित्य है । अविद्या भी नित्य है और इन दोनों का संयोग भी नित्य है । अविद्या / प्रकृति जड़स्वरूप है । इसमें पुरुष का प्रतिबिम्ब जब भी प्रतिभासित होने लगता है । जिससे वह निष्क्रिय, निर्लिप्त, निस्त्रैगुण्य होने पर भी कर्ता, भोक्ता और आसक्त जैसा जान पड़ता है । प्रकृति-पुरुष के इस आरोपित स्वरूप को ही सांख्यों ने 'बन्ध' माना है ।
बन्ध-विच्छेद - प्रकृति / पुरुष दोनों को ही अपने-अपने बन्ध का अभाव / विच्छेद माना गया है । इसी को 'विवेक बुद्धि' है । इसकी प्रक्रिया निम्नलिखित तरह से समझी जा सकती है :
१२ | चतुर्थ खण्ड : जैन दर्शन, इतिहास और साहित्य
स्वरूप का ज्ञान हो जाना, सांख्यदर्शन में भी कहा गया है । यही पुरुष की 'मुक्ति'