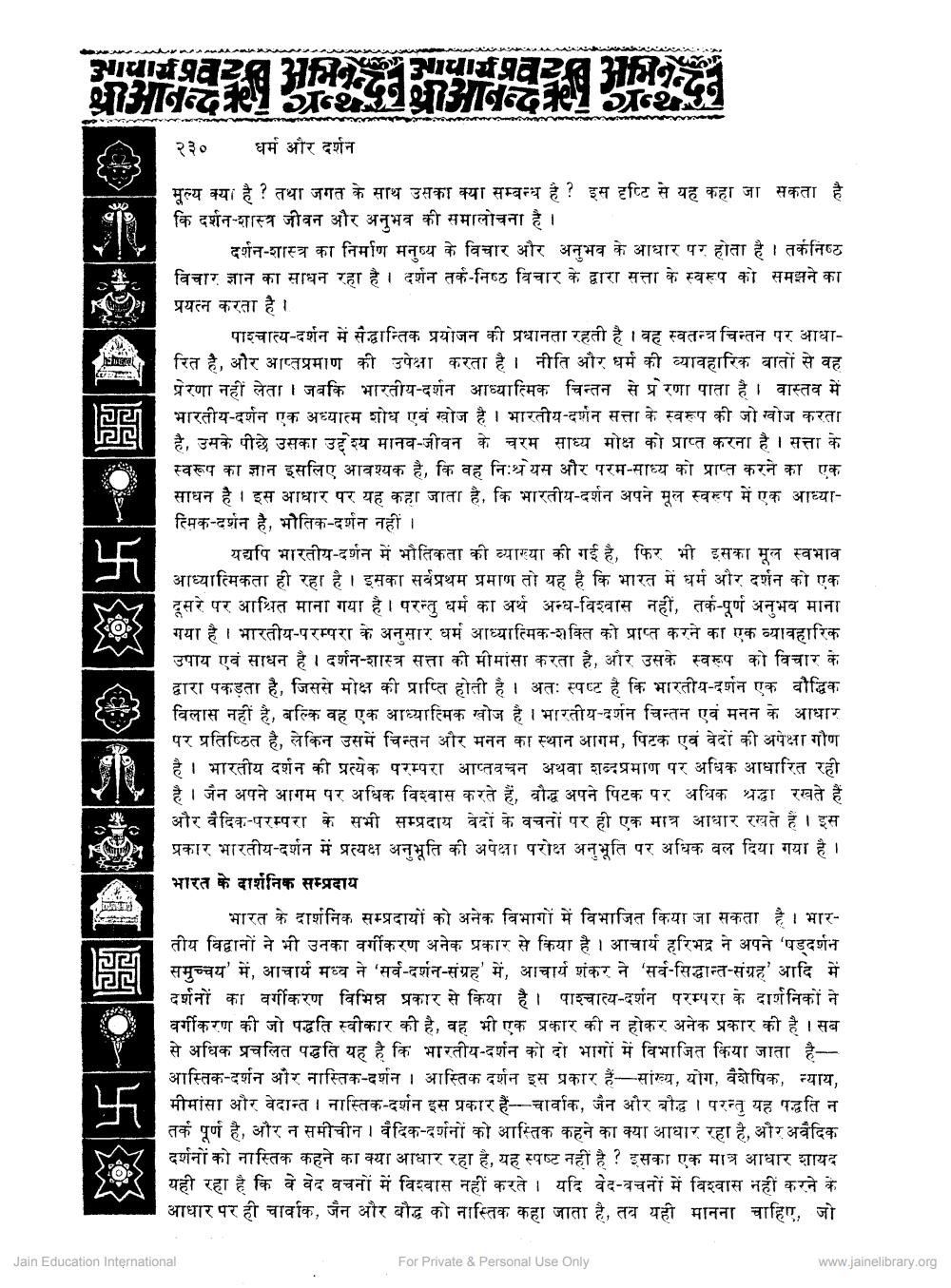________________
श्रीआनन्द अन्य श्रीआनन्द अन्य
२३०
धर्म और दर्शन
मुल्य क्या है ? तथा जगत के साथ उसका क्या सम्बन्ध है ? इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि दर्शन-शास्त्र जीवन और अनुभव की समालोचना है।
दर्शन-शास्त्र का निर्माण मनुष्य के विचार और अनुभव के आधार पर होता है। तर्कनिष्ठ विचार ज्ञान का साधन रहा है। दर्शन तर्क-निष्ठ विचार के द्वारा सत्ता के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करता है।
पाश्चात्य-दर्शन में सैद्धान्तिक प्रयोजन की प्रधानता रहती है । वह स्वतन्त्र चिन्तन पर आधारित है, और आप्तप्रमाण की उपेक्षा करता है। नीति और धर्म की व्यावहारिक बातों से वह प्रेरणा नहीं लेता । जबकि भारतीय-दर्शन आध्यात्मिक चिन्तन से प्रेरणा पाता है। वास्तव में भारतीय-दर्शन एक अध्यात्म शोध एवं खोज है। भारतीय-दर्शन सत्ता के स्वरूप की जो खोज करता है, उसके पीछे उसका उद्देश्य मानव-जीवन के चरम साध्य मोक्ष को प्राप्त करना है । सत्ता के स्वरूप का ज्ञान इसलिए आवश्यक है, कि वह निःश्रेयस और परम-साध्य को प्राप्त करने का एक साधन है । इस आधार पर यह कहा जाता है, कि भारतीय-दर्शन अपने मूल स्वरूप में एक आध्यात्मिक-दर्शन है, भौतिक-दर्शन नहीं।
यद्यपि भारतीय-दर्शन में भौतिकता की व्याख्या की गई है, फिर भी इसका मूल स्वभाव आध्यात्मिकता ही रहा है। इसका सर्वप्रथम प्रमाण तो यह है कि भारत में धर्म और दर्शन को एक दूसरे पर आश्रित माना गया है। परन्तु धर्म का अर्थ अन्ध-विश्वास नहीं, तर्क-पूर्ण अनुभव माना गया है। भारतीय-परम्परा के अनुसार धर्म आध्यात्मिक-शक्ति को प्राप्त करने का एक व्यावहारिक उपाय एवं साधन है । दर्शन-शास्त्र सत्ता की मीमांसा करता है, और उसके स्वरूप को विचार के द्वारा पकड़ता है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः स्पष्ट है कि भारतीय-दर्शन एक बौद्धिक विलास नहीं है, बल्कि वह एक आध्यात्मिक खोज है । भारतीय-दर्शन चिन्तन एवं मनन के आधार पर प्रतिष्ठित है, लेकिन उसमें चिन्तन और मनन का स्थान आगम, पिटक एवं वेदों की अपेक्षा गौण है । भारतीय दर्शन की प्रत्येक परम्परा आप्तवचन अथवा शब्दप्रमाण पर अधिक आधारित रही है । जैन अपने आगम पर अधिक विश्वास करते हैं, वौद्ध अपने पिटक पर अधिक श्रद्धा रखते हैं और वैदिक-परम्परा के सभी सम्प्रदाय वेदों के वचनों पर ही एक मात्र आधार रखते हैं । इस प्रकार भारतीय-दर्शन में प्रत्यक्ष अनभूति की अपेक्षा परोक्ष अनुभूति पर अधिक बल दिया गया है । भारत के दार्शनिक सम्प्रदाय
भारत के दार्शनिक सम्प्रदायों को अनेक विभागों में विभाजित किया जा सकता है। भारतीय विद्वानों ने भी उनका वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया है। आचार्य हरिभद्र ने अपने 'पड्दर्शन समुच्चय' में, आचार्य मध्व ने 'सर्व-दर्शन-संग्रह' में, आचार्य शंकर ने 'सर्व-सिद्धान्त-संग्रह' आदि में दर्शनों का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया है। पाश्चात्य-दर्शन परम्परा के दार्शनिकों ने वर्गीकरण की जो पद्धति स्वीकार की है, वह भी एक प्रकार की न होकर अनेक प्रकार की है । सब से अधिक प्रचलित पद्धति यह है कि भारतीय-दर्शन को दो भागों में विभाजित किया जाता हैआस्तिक-दर्शन और नास्तिक-दर्शन । आस्तिक दर्शन इस प्रकार हैं-सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा और वेदान्त । नास्तिक-दर्शन इस प्रकार हैं--चार्वाक, जैन और बौद्ध । परन्तु यह पद्धति न तर्क पूर्ण है, और न समीचीन । वैदिक-दर्शनों को आस्तिक कहने का क्या आधार रहा है, और अवैदिक दर्शनों को नास्तिक कहने का क्या आधार रहा है, यह स्पष्ट नहीं है ? इसका एक मात्र आधार शायद यही रहा है कि वे वेद वचनों में विश्वास नहीं करते। यदि वेद-वचनों में विश्वास नहीं करने के आधार पर ही चार्वाक, जैन और बौद्ध को नास्तिक कहा जाता है, तब यही मानना चाहिए, जो
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org