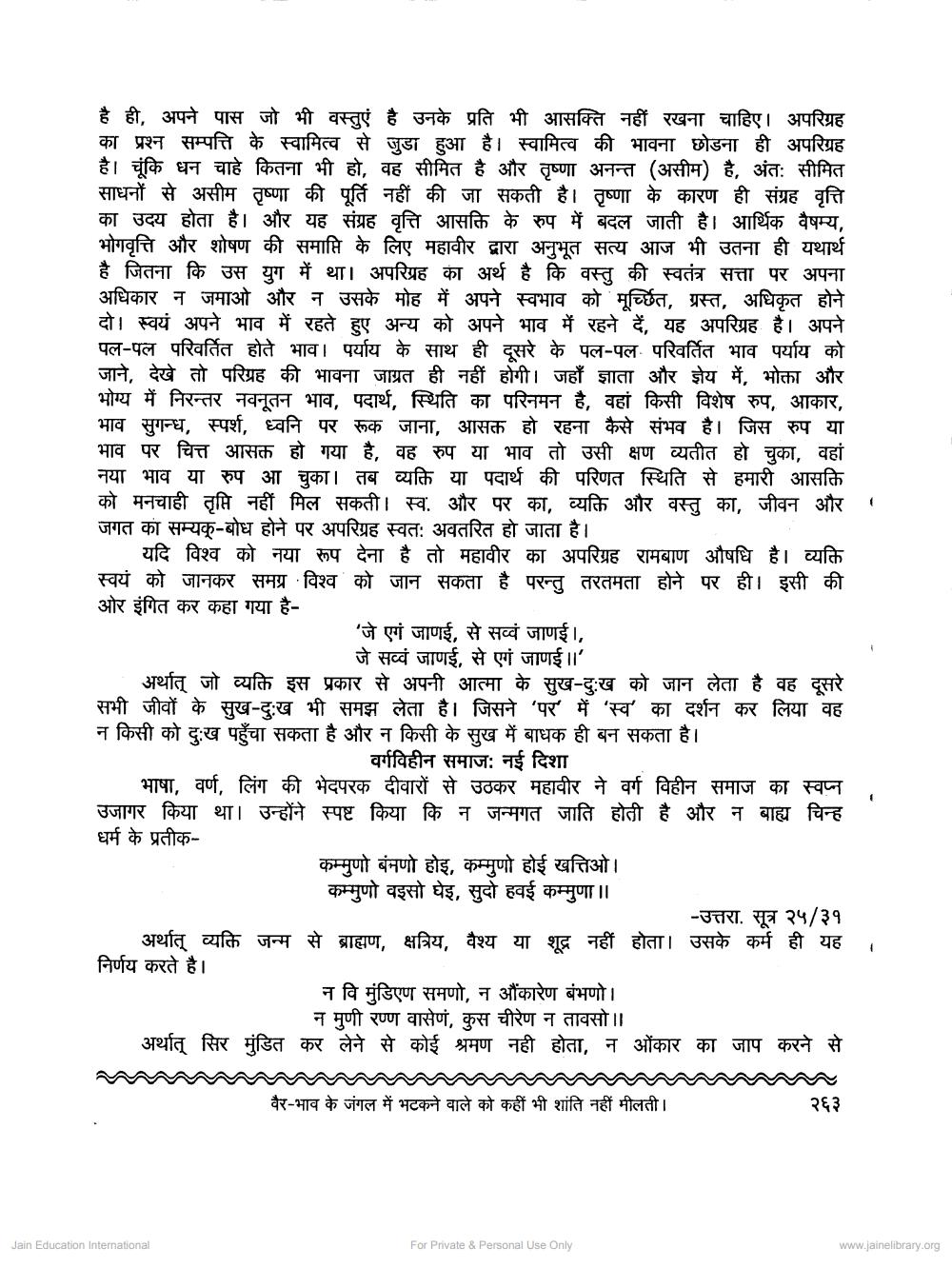________________
है ही, अपने पास जो भी वस्तुएं है उनके प्रति भी आसक्ति नहीं रखना चाहिए। अपरिग्रह का प्रश्न सम्पत्ति के स्वामित्व से जुड़ा हुआ है। स्वामित्व की भावना छोडना ही अपरिग्रह है। चूंकि धन चाहे कितना भी हो, वह सीमित है और तृष्णा अनन्त (असीम) है, अंत: सीमित साधनों से असीम तृष्णा की पूर्ति नहीं की जा सकती है। तृष्णा के कारण ही संग्रह वृत्ति का उदय होता है। और यह संग्रह वृत्ति आसक्ति के रुप में बदल जाती है। आर्थिक वैषम्य, भोगवृत्ति और शोषण की समाप्ति के लिए महावीर द्वारा अनुभूत सत्य आज भी उतना ही यथार्थ है जितना कि उस युग में था। अपरिग्रह का अर्थ है कि वस्तु की स्वतंत्र सत्ता पर अपना अधिकार न जमाओ और न उसके मोह में अपने स्वभाव को मूर्च्छित, ग्रस्त, अधिकृत होने दो। स्वयं अपने भाव में रहते हुए अन्य को अपने भाव में रहने दें, यह अपरिग्रह है। अपने पल-पल परिवर्तित होते भाव। पर्याय के साथ ही दूसरे के पल-पल परिवर्तित भाव पर्याय को जाने, देखे तो परिग्रह की भावना जाग्रत ही नहीं होगी। जहाँ ज्ञाता और ज्ञेय में, भोक्ता और भोग्य में निरन्तर नवनूतन भाव, पदार्थ, स्थिति का परिनमन है, वहां किसी विशेष रुप, आकार, भाव सुगन्ध, स्पर्श, ध्वनि पर रूक जाना, आसक्त हो रहना कैसे संभव है। जिस रुप या भाव पर चित्त आसक्त हो गया है, वह रुप या भाव तो उसी क्षण व्यतीत हो चुका, वहां नया भाव या रुप आ चुका। तब व्यक्ति या पदार्थ की परिणत स्थिति से हमारी आसक्ति को मनचाही तृप्ति नहीं मिल सकती। स्व. और पर का, व्यक्ति और वस्तु का, जीवन और । जगत का सम्यकू-बोध होने पर अपरिग्रह स्वत: अवतरित हो जाता है।
यदि विश्व को नया रूप देना है तो महावीर का अपरिग्रह रामबाण औषधि है। व्यक्ति स्वयं को जानकर समग्र विश्व को जान सकता है परन्तु तरतमता होने पर ही। इसी की ओर इंगित कर कहा गया है
'जे एगं जाणई, से सव्वं जाणई।,
जे सव्वं जाणई, से एणं जाणई।' अर्थात् जो व्यक्ति इस प्रकार से अपनी आत्मा के सुख-दु:ख को जान लेता है वह दूसरे सभी जीवों के सुख-दु:ख भी समझ लेता है। जिसने 'पर' में 'स्व' का दर्शन कर लिया वह न किसी को दु:ख पहुँचा सकता है और न किसी के सुख में बाधक ही बन सकता है।
वर्गविहीन समाज: नई दिशा भाषा, वर्ण, लिंग की भेदपरक दीवारों से उठकर महावीर ने वर्ग विहीन समाज का स्वप्न उजागर किया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि न जन्मगत जाति होती है और न बाह्य चिन्ह धर्म के प्रतीक
कम्मुणो बनणो होइ, कम्मुणो होई खत्तिओ। कम्मुणो वइसो घेइ, सुदो हवई कम्मुणा।।
-उत्तरा. सूत्र २५/३१ अर्थात् व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं होता। उसके कर्म ही यह । निर्णय करते है।
न वि मुंडिएण समणो, न औंकारेण बंभणो।
न मुणी रण वासेणं, कुस चीरेण न तावसो।। अर्थात् सिर मुंडित कर लेने से कोई श्रमण नही होता, न ओंकार का जाप करने से
वैर-भाव के जंगल में भटकने वाले को कहीं भी शांति नहीं मीलती।
२६३
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org