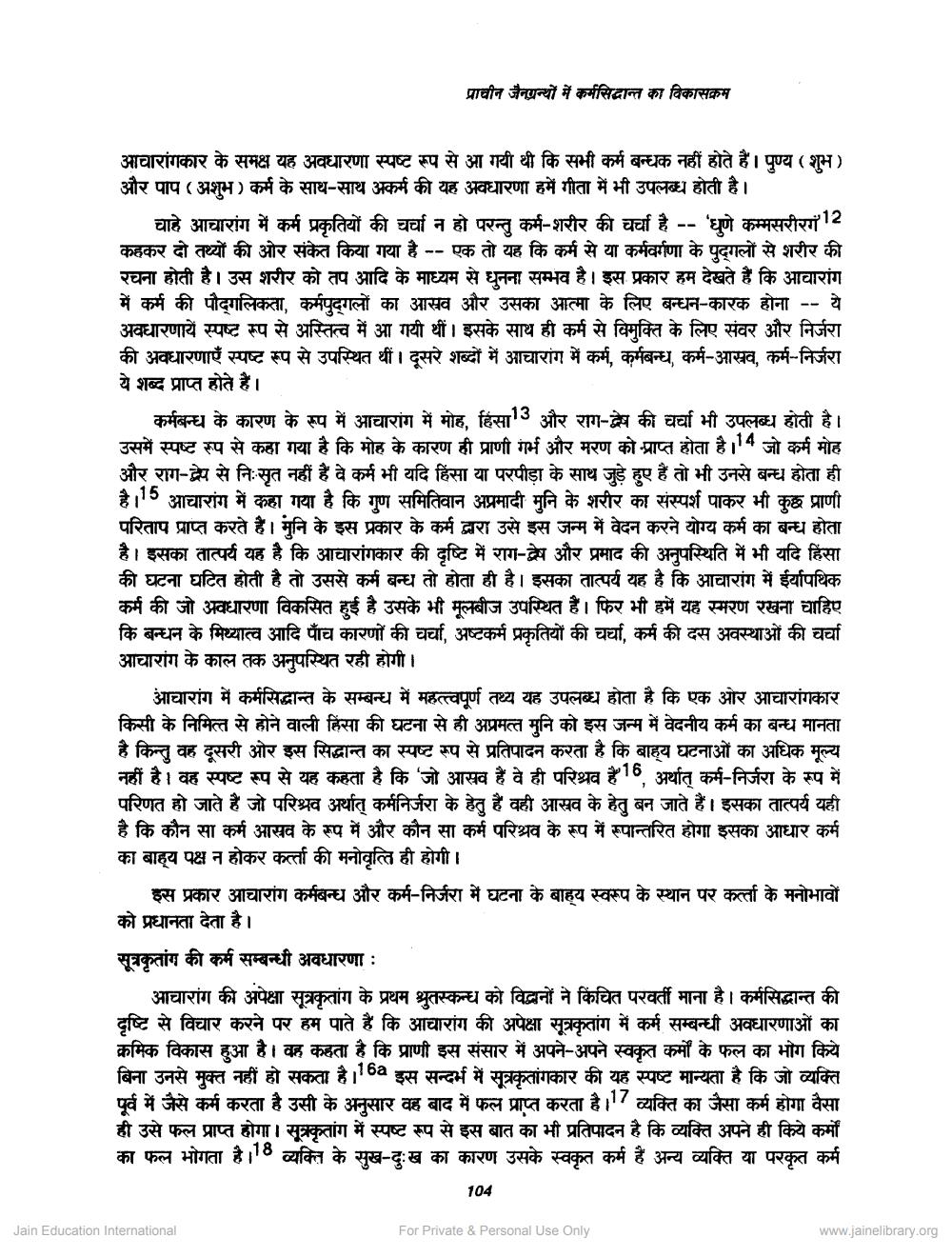________________
प्राचीन जैनग्रन्थों में कर्मसिद्धान्त का विकासक्रम
आचारांगकार के समक्ष यह अवधारणा स्पष्ट रूप से आ गयी थी कि सभी कर्म बन्धक नहीं होते हैं। पुण्य (शुभ) और पाप (अशुभ) कर्म के साथ-साथ अकर्म की यह अवधारणा हमें गीता में भी उपलब्ध होती है।
चाहे आचारांग में कर्म प्रकृतियों की चर्चा न हो परन्तु कर्म-शरीर की चर्चा है -- 'धुणे कम्मसरीरगं12 कहकर दो तथ्यों की ओर संकेत किया गया है -- एक तो यह कि कर्म से या कर्मवर्गणा के पुद्गलों से शरीर की रचना होती है। उस शरीर को तप आदि के माध्यम से धुनना सम्भव है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आवारांग में कर्म की पौद्गलिकता, कर्मपुद्गलों का आसव और उसका आत्मा के लिए बन्धन-कारक होना -- ये अवधारणायें स्पष्ट रूप से अस्तित्व में आ गयी थीं। इसके साथ ही कर्म से विमुक्ति के लिए संवर और निर्जरा की अवधारणाएँ स्पष्ट रूप से उपस्थित थीं। दूसरे शब्दों में आचारांग में कर्म, कर्मबन्ध कर्म-आसव, कर्म-निर्जरा ये शब्द प्राप्त होते हैं।
कर्मबन्ध के कारण के रूप में आचारांग में मोह, हिंसा और राग-द्वेष की चर्चा भी उपलब्ध होती है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मोह के कारण ही प्राणी गर्भ और मरण को प्राप्त होता है। जो कर्म मोह
और राग-द्वेष से निःसृत नहीं हैं वे कर्म भी यदि हिंसा या परपीड़ा के साथ जुड़े हुए हैं तो भी उनसे बन्ध होता ही है। आचारांग में कहा गया है कि गुण समितिवान अप्रमादी मुनि के शरीर का संस्पर्श पाकर भी कुछ प्राणी परिताप प्राप्त करते हैं। मुनि के इस प्रकार के कर्म द्वरा उसे इस जन्म में वेदन करने योग्य कर्म का बन्ध होता है। इसका तात्पर्य यह है कि आचारांगकार की दृष्टि में राग-द्वेष और प्रमाद की अनुपस्थिति में भी यदि हिंसा की घटना घटित होती है तो उससे कर्म बन्ध तो होता ही है। इसका तात्पर्य यह है कि आचारांग में ईर्यापथिक कर्म की जो अवधारणा विकसित हुई है उसके भी मूलबीज उपस्थित हैं। फिर भी हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि बन्धन के मिथ्यात्व आदि पाँच कारणों की चर्चा, अष्टकर्म प्रकृतियों की चर्चा, कर्म की दस अवस्थाओं की चर्चा आचारांग के काल तक अनुपस्थित रही होगी।
आचारांग में कर्मसिद्धान्त के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण तथ्य यह उपलब्ध होता है कि एक ओर आचारांगकार किसी के निमित्त से होने वाली हिंसा की घटना से ही अप्रमत्त मुनि को इस जन्म में वेदनीय कर्म का बन्ध मानता है किन्तु वह दूसरी ओर इस सिद्धान्त का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करता है कि बाह्य घटनाओं का अधिक मूल्य नहीं है। वह स्पष्ट रूप से यह कहता है कि 'जो आसव हैं वे ही परिश्रव हैं।०, अर्थात कर्म-निर्जरा के रूप में परिणत हो जाते हैं जो परिश्रव अर्थात् कर्मनिर्जरा के हेतु हैं वही आसव के हेतु बन जाते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि कौन सा कर्म आसव के रूप में और कौन सा कर्म परिश्रव के रूप में रूपान्तरित होगा इसका आधार कर्म का बाह्य पक्ष न होकर कर्ता की मनोवृत्ति ही होगी।
इस प्रकार आचारांग कर्मबन्ध और कर्म-निर्जरा में घटना के बाहय स्वरूप के स्थान पर कर्ता के मनोभावों को प्रधानता देता है। सूत्रकृतांग की कर्म सम्बन्धी अवधारणा :
आचारांग की अपेक्षा सूत्रकृतांग के प्रथम श्रुतस्कन्ध को विद्वानों ने किंचित परवर्ती माना है। कर्मसिद्धान्त की दृष्टि से विचार करने पर हम पाते हैं कि आचारांग की अपेक्षा सूत्रकृतांग में कर्म सम्बन्धी अवधारणाओं का क्रमिक विकास हुआ है। वह कहता है कि प्राणी इस संसार में अपने-अपने स्वकृत कर्मों के फल का भोग किये बिना उनसे मुक्त नहीं हो सकता है। इस सन्दर्भ में सूत्रकृतांगकार की यह स्पष्ट मान्यता है कि जो व्यक्ति पूर्व में जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार वह बाद में फल प्राप्त करता है।17 व्यक्ति का जैसा कर्म होगा वैसा ही उसे फल प्राप्त होगा। सूत्रकृतांग में स्पष्ट रूप से इस बात का भी प्रतिपादन है कि व्यक्ति अपने ही किये कर्मों का फल भोगता है। व्यक्ति के सुख-दुःख का कारण उसके स्वकृत कर्म हैं अन्य व्यक्ति या परकृत कर्म
104
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org