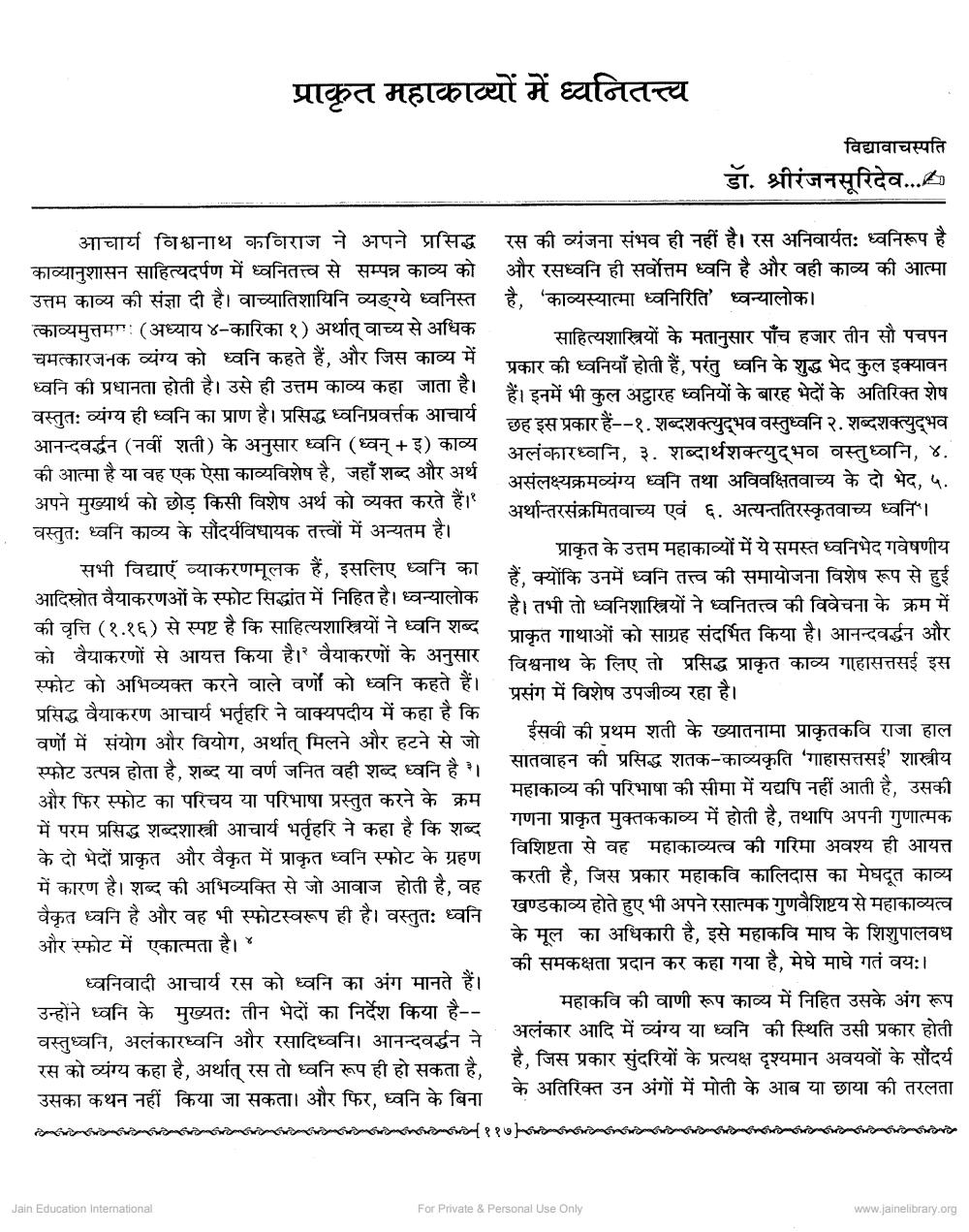________________
प्राकृत महाकाव्यों में ध्वनितत्त्व
आचार्य विश्वनाथ कविराज ने अपने प्रसिद्ध काव्यानुशासन साहित्यदर्पण में ध्वनितत्त्व से सम्पन्न काव्य को उत्तम काव्य की संज्ञा दी है। वाच्यातिशायिनि व्यङ्ग्ये ध्वनिस्त त्काव्यमुत्तम: (अध्याय ४ - कारिका १) अर्थात् वाच्य से अधिक चमत्कारजनक व्यंग्य को ध्वनि कहते हैं, और जिस काव्य में ध्वनि की प्रधानता होती है। उसे ही उत्तम काव्य कहा जाता है। वस्तुतः व्यंग्य ही ध्वनि का प्राण है। प्रसिद्ध ध्वनिप्रवर्त्तक आचार्य आनन्दवर्द्धन (नवीं शती) के अनुसार ध्वनि (ध्वन् + इ) काव्य की आत्मा है या वह एक ऐसा काव्यविशेष है, जहाँ शब्द और अर्थ अपने मुख्यार्थ को छोड़ किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं। " वस्तुतः ध्वनि काव्य के सौंदर्यविधायक तत्त्वों में अन्यतम है।
सभी विद्याएँ व्याकरणमूलक हैं, इसलिए ध्वनि का आदिस्रोत वैयाकरणओं के स्फोट सिद्धांत में निहित है। ध्वन्यालोक की वृत्ति (१.१६ ) से स्पष्ट है कि साहित्यशास्त्रियों ने ध्वनि शब्द को वैयाकरणों से आयत्त किया है। वैयाकरणों के अनुसार स्फोट को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों को ध्वनि कहते हैं । प्रसिद्ध वैयाकरण आचार्य भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में कहा है कि वर्णों में संयोग और वियोग, अर्थात् मिलने और हटने से जो स्फोट उत्पन्न होता है, शब्द या वर्ण जनित वही शब्द ध्वनि है । और फिर स्फोट का परिचय या परिभाषा प्रस्तुत करने के क्रम में परम प्रसिद्ध शब्दशास्त्री आचार्य भर्तृहरि ने कहा है कि शब्द के दो भेदों प्राकृत और वैकृत में प्राकृत ध्वनि स्फोट के ग्रहण में कारण है। शब्द की अभिव्यक्ति से जो आवाज होती है, वह कृत ध्वनि है और वह भी स्फोटस्वरूप ही है। वस्तुतः ध्वनि और स्फोट में एकात्मता है । ४
Jain Education International
रस की व्यंजना संभव ही नहीं है। रस अनिवार्यतः ध्वनिरूप है और रसध्वनि ही सर्वोत्तम ध्वनि है और वही काव्य की आत्मा है, 'काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति ध्वन्यालोक ।
विद्यावाचस्पति
डॉ. श्रीरंजनसूरिदेव.......
साहित्यशास्त्रियों के मतानुसार पाँच हजार तीन सौ पचपन प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, परंतु ध्वनि के शुद्ध भेद कुल इक्यावन हैं। इनमें भी कुल अट्ठारह ध्वनियों के बारह भेदों के अतिरिक्त शेष छह इस प्रकार हैं -- १. शब्दशक्त्युद्भव वस्तुध्वनि २. शब्दशक्त्युद्भव अलंकारध्वनि, ३. शब्दार्थशक्त्युद्भव वस्तुध्वनि, ४. असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि तथा अविवक्षितवाच्य के दो भेद, ५. अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य एवं ६. अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि ।
प्राकृत के उत्तम महाकाव्यों में ये समस्त ध्वनिभेद गवेषणीय हैं, क्योंकि उनमें ध्वनि तत्त्व की समायोजना विशेष रूप से हुई है। तभी तो ध्वनिशास्त्रियों ने ध्वनितत्त्व की विवेचना के क्रम में प्राकृत गाथाओं को साग्रह संदर्भित किया है। आनन्दवर्द्धन और विश्वनाथ के लिए तो प्रसिद्ध प्राकृत काव्य गाहासत्तसई इस प्रसंग में विशेष उपजीव्य रहा है।
ध्वनिवादी आचार्य रस को ध्वनि का अंग मानते हैं। उन्होंने ध्वनि के मुख्यतः तीन भेदों का निर्देश किया है-वस्तुध्वनि, अलंकारध्वनि और रसादिध्वनि । आनन्दवर्द्धन ने रस को व्यंग्य कहा है, अर्थात् रस तो ध्वनि रूप ही हो सकता है, उसका कथन नहीं किया जा सकता। और फिर, ध्वनि के बिना
[११]
ईसवी की प्रथम शती के ख्यातनामा प्राकृतकवि राजा हाल सातवाहन की प्रसिद्ध शतक - काव्यकृति 'गाहासत्तसई' शास्त्रीय महाकाव्य की परिभाषा की सीमा में यद्यपि नहीं आती है, उसकी गणना प्राकृत मुक्तककाव्य में होती है, तथापि अपनी गुणात्मक विशिष्टता से वह महाकाव्यत्व की गरिमा अवश्य ही आयत्त करती है, जिस प्रकार महाकवि कालिदास का मेघदूत काव्य खण्डकाव्य होते हुए भी अपने रसात्मक गुणवैशिष्टय से महाकाव्यत्व के मूल का अधिकारी है, इसे महाकवि माघ के शिशुपालवध की समकक्षता प्रदान कर कहा गया है, मेघे माघे गतं वयः ।
महाकवि की वाणी रूप काव्य में निहित उसके अंग रूप अलंकार आदि में व्यंग्य या ध्वनि की स्थिति उसी प्रकार होती है, जिस प्रकार सुंदरियों के प्रत्यक्ष दृश्यमान अवयवों के सौंदर्य के अतिरिक्त उन अंगों में मोती के आब या छाया की तरलता
For Private Personal Use Only
SHS
www.jainelibrary.org