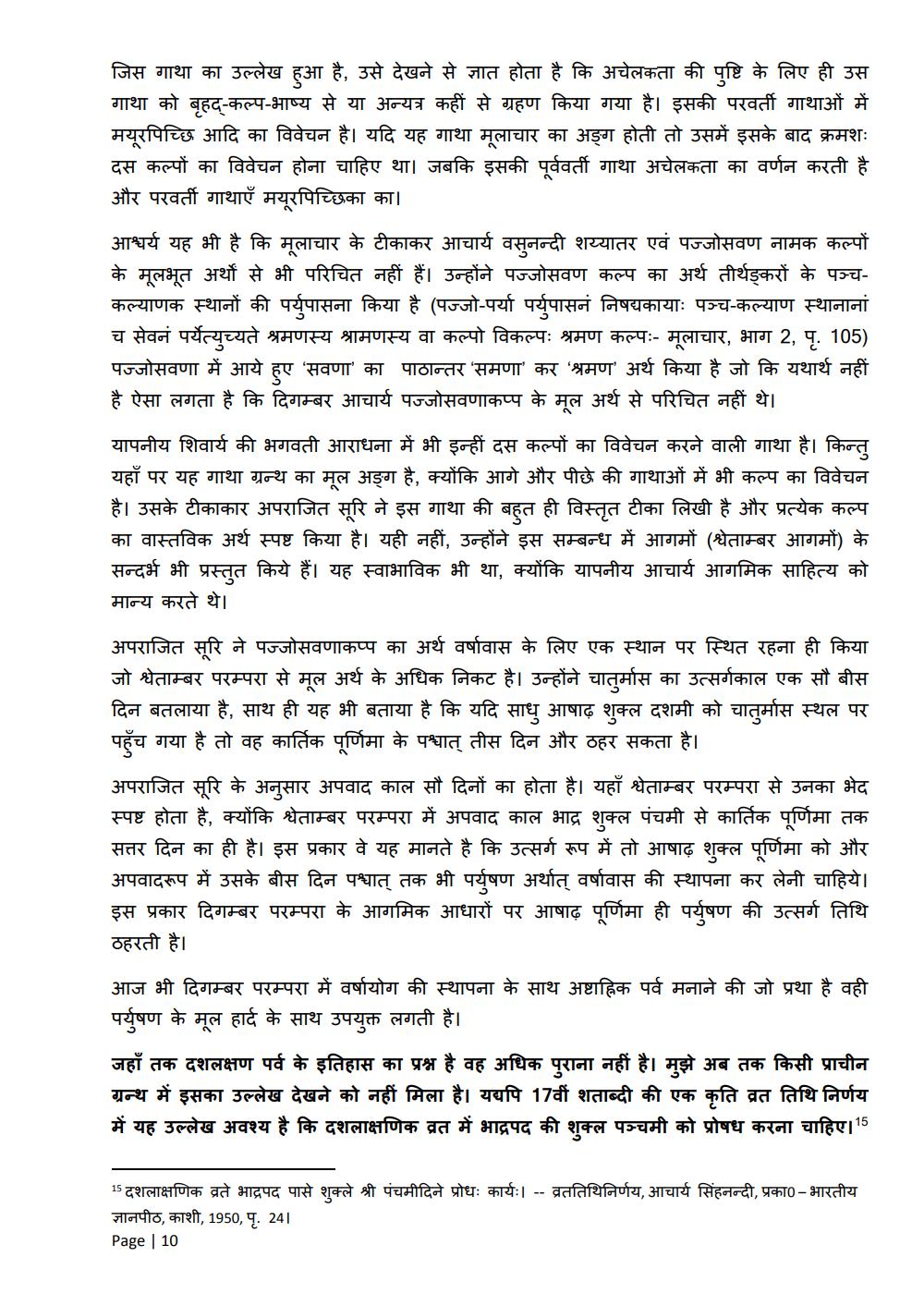________________ जिस गाथा का उल्लेख हुआ है, उसे देखने से ज्ञात होता है कि अचेलकता की पुष्टि के लिए ही उस गाथा को बृहद्-कल्प-भाष्य से या अन्यत्र कहीं से ग्रहण किया गया है। इसकी परवर्ती गाथाओं में मयूरपिच्छि आदि का विवेचन है। यदि यह गाथा मूलाचार का अङ्ग होती तो उसमें इसके बाद क्रमशः दस कल्पों का विवेचन होना चाहिए था। जबकि इसकी पूर्ववर्ती गाथा अचेलकता का वर्णन करती है और परवर्ती गाथाएँ मयूरपिच्छिका का। आश्चर्य यह भी है कि मूलाचार के टीकाकर आचार्य वसुनन्दी शय्यातर एवं पज्जोसवण नामक कल्पों के मूलभूत अर्थों से भी परिचित नहीं हैं। उन्होंने पज्जोसवण कल्प का अर्थ तीर्थङ्करों के पञ्चकल्याणक स्थानों की पर्युपासना किया है (पज्जो-पर्या पर्युपासनं निषद्यकायाः पञ्च-कल्याण स्थानानां च सेवनं पर्येत्युच्यते श्रमणस्य श्रामणस्य वा कल्पो विकल्पः श्रमण कल्पः- मूलाचार, भाग 2, पृ. 105) पज्जोसवणा में आये हुए ‘सवणा' का पाठान्तर 'समणा' कर 'श्रमण' अर्थ किया है जो कि यथार्थ नहीं है ऐसा लगता है कि दिगम्बर आचार्य पज्जोसवणाकप्प के मूल अर्थ से परिचित नहीं थे। यापनीय शिवार्य की भगवती आराधना में भी इन्हीं दस कल्पों का विवेचन करने वाली गाथा है। किन्तु यहाँ पर यह गाथा ग्रन्थ का मल अग है, क्योंकि आगे और पीछे की गाथाओं में भी कल्प का विवेचन है। उसके टीकाकार अपराजित सूरि ने इस गाथा की बहुत ही विस्तृत टीका लिखी है और प्रत्येक कल्प का वास्तविक अर्थ स्पष्ट किया है। यही नहीं, उन्होंने इस सम्बन्ध में आगमों (श्वेताम्बर आगमों) के सन्दर्भ भी प्रस्तुत किये हैं। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि यापनीय आचार्य आगमिक साहित्य को मान्य करते थे। अपराजित सूरि ने पज्जोसवणाकप्प का अर्थ वर्षावास के लिए एक स्थान पर स्थित रहना ही किया जो श्वेताम्बर परम्परा से मूल अर्थ के अधिक निकट है। उन्होंने चातुर्मास का उत्सर्गकाल एक सौ बीस दिन बतलाया है, साथ ही यह भी बताया है कि यदि साधु आषाढ़ शुक्ल दशमी को चातुर्मास स्थल पर पहुँच गया है तो वह कार्तिक पूर्णिमा के पश्चात् तीस दिन और ठहर सकता है। अपराजित सूरि के अनुसार अपवाद काल सौ दिनों का होता है। यहाँ श्वेताम्बर परम्परा से उनका भेद स्पष्ट होता है, क्योंकि श्वेताम्बर परम्परा में अपवाद काल भाद्र शक्ल पंचमी से कार्तिक पर्णिमा सत्तर दिन का ही है। इस प्रकार वे यह मानते है कि उत्सर्ग रूप में तो आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को और अपवादरूप में उसके बीस दिन पश्चात् तक भी पर्युषण अर्थात् वर्षावास की स्थापना कर लेनी चाहिये। इस प्रकार दिगम्बर परम्परा के आगमिक आधारों पर आषाढ़ पूर्णिमा ही पर्युषण की उत्सर्ग तिथि ठहरती है। आज भी दिगम्बर परम्परा में वर्षायोग की स्थापना के साथ अष्टाह्निक पर्व मनाने की जो प्रथा है वही पर्युषण के मूल हार्द के साथ उपयुक्त लगती है। जहाँ तक दशलक्षण पर्व के इतिहास का प्रश्न है वह अधिक पुराना नहीं है। मुझे अब तक किसी प्राचीन ग्रन्थ में इसका उल्लेख देखने को नहीं मिला है। यद्यपि 17वीं शताब्दी की एक कृति व्रत तिथि निर्णय में यह उल्लेख अवश्य है कि दशलाक्षणिक व्रत में भाद्रपद पञ्चमी को प्रोषध करना चाहिए।15 15 दशलाक्षणिक व्रते भाद्रपद पासे शुक्ले श्री पंचमीदिने प्रोधः कार्यः। -- व्रततिथिनिर्णय, आचार्य सिंहनन्दी, प्रका0- भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, 1950, पृ. 241 Page | 10