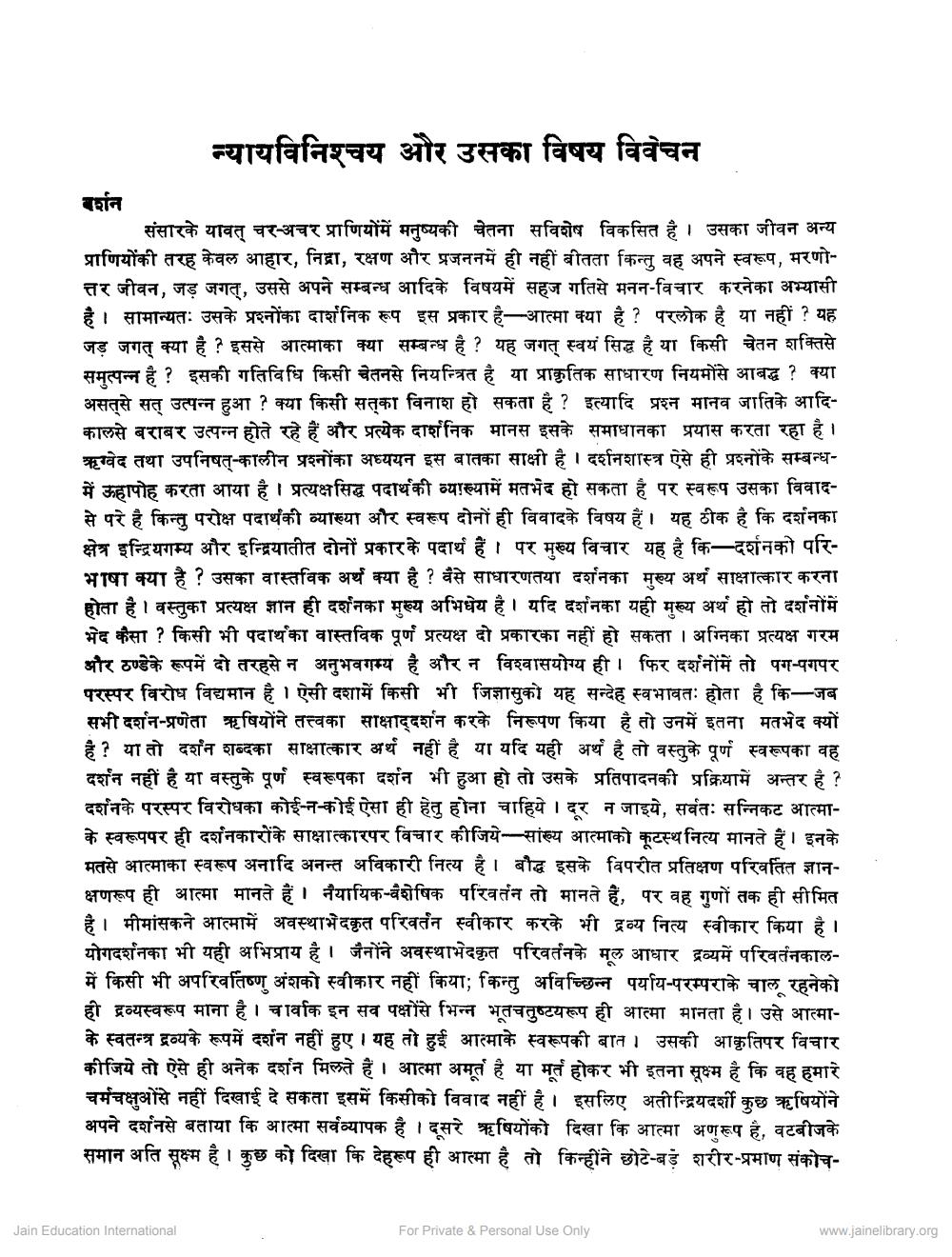________________
न्यायविनिश्चय और उसका विषय विवेचन
वर्शन
संसारके यावत चर-अचर प्राणियोंमें मनुष्यकी चेतना सविशेष विकसित है। उसका जीवन अन्य प्राणियोंकी तरह केवल आहार, निद्रा, रक्षण और प्रजननमें ही नहीं बीतता किन्तु वह अपने स्वरूप, मरणोत्तर जीवन, जड़ जगत, उससे अपने सम्बन्ध आदिके विषयमें सहज गतिसे मनन-विचार करनेका अभ्यासी है। सामान्यतः उसके प्रश्नोंका दार्शनिक रूप इस प्रकार है-आत्मा क्या है ? परलोक है या नहीं ? यह जड़ जगत् क्या है ? इससे आत्माका क्या सम्बन्ध है ? यह जगत् स्वयं सिद्ध है या किसी चेतन शक्तिसे समत्पन्न है ? इसकी गतिविधि किसी चेतनसे नियन्त्रित है या प्राकृतिक साधारण नियमोंसे आबद्ध ? क्या
सत उत्पन्न हआ ? क्या किसी सतका विनाश हो सकता है ? इत्यादि प्रश्न मानव जातिके आदिकालसे बराबर उत्पन्न होते रहे हैं और प्रत्येक दार्शनिक मानस इसके समाधानका प्रयास करता रहा है। ऋग्वेद तथा उपनिषत्-कालीन प्रश्नोंका अध्ययन इस बातका साक्षी है । दर्शनशास्त्र ऐसे ही प्रश्नोंके सम्बन्धमें ऊहापोह करता आया है। प्रत्यक्षसिद्ध पदार्थकी व्याख्या में मतभेद हो सकता है पर स्वरूप उसका विवादसे परे है किन्तु परोक्ष पदार्थकी व्याख्या और स्वरूप दोनों ही विवादके विषय हैं। यह ठीक है कि दर्शनका
इन्द्रियगम्य और इन्द्रियातीत दोनों प्रकार के पदार्थ हैं। पर मख्य विचार यह है कि दर्शनको परिभाषा क्या है ? उसका वास्तविक अर्थ क्या है ? वैसे साधारणतया दर्शनका मुख्य अर्थ साक्षात्कार करना होता है । वस्तुका प्रत्यक्ष ज्ञान ही दर्शनका मुख्य अभिधेय है। यदि दर्शनका यही मुख्य अर्थ हो तो दर्शनोंमें भेद कैसा ? किसी भी पदार्थका वास्तविक पूर्ण प्रत्यक्ष दो प्रकारका नहीं हो सकता । अग्निका प्रत्यक्ष गरम और ठण्डेके रूपमें दो तरहसे न अनुभवगम्य है और न विश्वासयोग्य ही। फिर दर्शनोंमें तो पग-पगपर परस्पर विरोध विद्यमान है। ऐसी दशामें किसी भी जिज्ञासुको यह सन्देह स्वभावतः होता है कि जब सभी दर्शन-प्रणेता ऋषियोंने तत्त्वका साक्षाद्दर्शन करके निरूपण किया है तो उनमें इतना मतभेद क्यों है? या तो दर्शन शब्दका साक्षात्कार अर्थ नहीं है या यदि यही अर्थ है तो वस्तुके पूर्ण स्वरूपका वह दर्शन नहीं है या वस्तुके पूर्ण स्वरूपका दर्शन भी हुआ हो तो उसके प्रतिपादनकी प्रक्रियामें अन्तर है ? दर्शनके परस्पर विरोधका कोई-न-कोई ऐसा ही हेतु होना चाहिये । दूर न जाइये, सर्वतः सन्निकट आत्माके स्वरूपपर ही दर्शनकारों के साक्षात्कारपर विचार कीजिये-सांख्य आत्माको कूटस्थ नित्य मानते हैं। इनके मतसे आत्माका स्वरूप अनादि अनन्त अविकारी नित्य है। बौद्ध इसके विपरीत प्रतिक्षण परिवर्तित ज्ञानक्षणरूप ही आत्मा मानते हैं। नैयायिक-वैशेषिक परिवर्तन तो मानते हैं, पर वह गणों तक ही सीमित है। मीमांसकने आत्मामें अवस्थाभेदकृत परिवर्तन स्वीकार करके भी द्रव्य नित्य स्वीकार किया है। योगदर्शनका भी यही अभिप्राय है। जैनोंने अवस्थाभेदकृत परिवर्तनके मूल आधार द्रव्यमें परिवर्तनकालमें किसी भी अपरिवर्तिष्णु अंशको स्वीकार नहीं किया; किन्तु अविच्छिन्न पर्याय-परम्पराके चाल रहनेको ही द्रव्यस्वरूप माना है। चार्वाक इन सव पक्षोंसे भिन्न भूतचतुष्टयरूप ही आत्मा मानता है। उसे आत्माके स्वतन्त्र द्रव्यके रूप में दर्शन नहीं हुए। यह तो हुई आत्माके स्वरूपकी बात। उसकी आकृतिपर विचार कीजिये तो ऐसे ही अनेक दर्शन मिलते है । आत्मा अमूर्त है या मर्त होकर भी इतना सूक्ष्म है कि वह हमारे चर्मचक्षओंसे नहीं दिखाई दे सकता इसमें किसीको विवाद नहीं है। इसलिए अतीन्द्रियदर्शी कुछ ऋषियोंने अपने दर्शनसे बताया कि आत्मा सर्वव्यापक है । दूसरे ऋषियोंको दिखा कि आत्मा अणरूप है, वटबीजके समान अति सूक्ष्म है । कुछ को दिखा कि देहरूप ही आत्मा है तो किन्हींने छोटे-बड़े शरीर-प्रमाण संकोच
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org