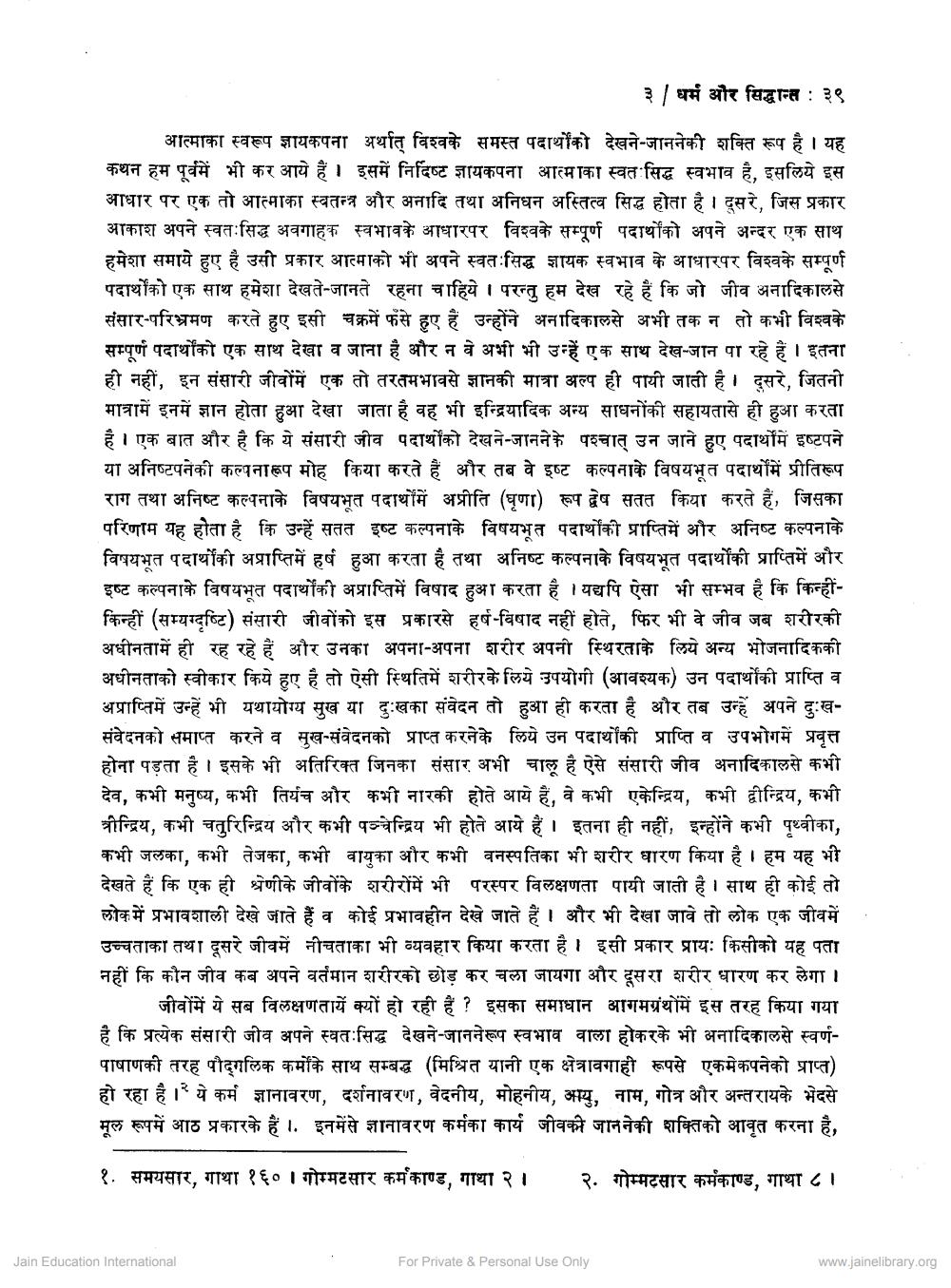________________
३ / धर्म और सिद्धान्त : ३९
आत्माका स्वरूप ज्ञायकपना अर्थात् विश्वके समस्त पदार्थोंको देखने-जाननेकी शक्ति रूप है । यह कथन हम पूर्वमें भी कर आये हैं। इसमें निर्दिष्ट ज्ञायकपना आत्माका स्वत सिद्ध स्वभाव है, इसलिये इस आधार पर एक तो आत्माका स्वतन्त्र और अनादि तथा अनिधन अस्तित्व सिद्ध होता है। दुसरे, जिस प्रकार आकाश अपने स्वतःसिद्ध अवगाहक स्वभावके आधारपर विश्वके सम्पूर्ण पदार्थों को अपने अन्दर एक साथ हमेशा समाये हुए है उसी प्रकार आत्माको भी अपने स्वतःसिद्ध ज्ञायक स्वभाव के आधारपर विश्वके सम्पूर्ण पदार्थों को एक साथ हमेशा देखते-जानते रहना चाहिये । परन्तु हम देख रहे हैं कि जो जीव अनादिकालसे संसार परिभ्रमण करते हुए इसी चक्रमें फंसे हुए हैं उन्होंने अनादिकालसे अभी तक न तो कभी विश्वके सम्पूर्ण पदार्थोंको एक साथ देखा व जाना है और न वे अभी भी उन्हें एक साथ देख-जान पा रहे हैं । इतना ही नहीं, इन संसारी जीवोंमें एक तो तरतमभावसे ज्ञानकी मात्रा अल्प ही पायी जाती है। दुसरे, जितनी मात्रामें इनमें ज्ञान होता हुआ देखा जाता है वह भी इन्द्रियादिक अन्य साधनोंकी सहायतासे ही हुआ करता है। एक बात और है कि ये संसारी जीव पदार्थोंको देखने-जानने के पश्चात् उन जाने हुए पदार्थोंमें इष्टपने या अनिष्टपनेकी कल्पनारूप मोह किया करते हैं और तब वे इष्ट कल्पनाके विषयभूत पदार्थोंमें प्रीतिरूप राग तथा अनिष्ट कल्पनाके विषयभूत पदार्थोंमें अप्रीति (घृणा) रूप द्वेष सतत किया करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि उन्हें सतत इष्ट कल्पनाके विषयभूत पदार्थों की प्राप्तिमें और अनिष्ट कल्पनाके विषयभूत पदार्थोकी अप्राप्तिमें हर्ष हुआ करता है तथा अनिष्ट कल्पनाके विषयभूत पदार्थोंकी प्राप्तिमें और इष्ट कल्पनाके विषयभूत पदार्थोंकी अप्राप्तिमें विषाद हुआ करता है । यद्यपि ऐसा भी सम्भव है कि किन्हींकिन्हीं (सम्यग्दृष्टि) संसारी जीवोंको इस प्रकारसे हर्ष-विषाद नहीं होते, फिर भी वे जीव जब शरीरकी अधीनतामें ही रह रहे हैं और उनका अपना-अपना शरीर अपनी स्थिरताके लिये अन्य भोजनादिककी अधीनताको स्वीकार किये हुए है तो ऐसी स्थितिमें शरीरके लिये उपयोगी (आवश्यक) उन पदार्थोकी प्राप्ति व अप्राप्तिमें उन्हें भी यथायोग्य सुख या दुःखका संवेदन तो हुआ ही करता है और तब उन्हें अपने दुःखसंवेदनको समाप्त करने व सुख-संवेदनको प्राप्त करने के लिये उन पदार्थों की प्राप्ति व उपभोगमें प्रवृत्त होना पड़ता है। इसके भी अतिरिक्त जिनका संसार अभी चाल है ऐसे संसारी जीव अनादिकालसे कभी देव, कभी मनुष्य, कभी तिर्यच और कभी नारकी होते आये हैं, वे कभी एकेन्द्रिय, कभी द्वीन्द्रिय, कभी त्रीन्द्रिय, कभी चतुरिन्द्रिय और कभी पञ्चेन्द्रिय भी होते आये हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने कभी पृथ्वीका, कभी जलका, कभी तेजका, कभी वायुका और कभी वनस्पतिका भी शरीर धारण किया है । हम यह भी देखते हैं कि एक ही श्रेणीके जीवोंके शरीरोंमें भी परस्पर विलक्षणता पायी जाती है । साथ ही कोई तो लोक में प्रभावशाली देखे जाते हैं व कोई प्रभावहीन देखे जाते हैं। और भी देखा जावे तो लोक एक जीवमें उच्चताका तथा दूसरे जीवमें नीचताका भी व्यवहार किया करता है। इसी प्रकार प्रायः किसीको यह पता नहीं कि कौन जीव कब अपने वर्तमान शरीरको छोड़ कर चला जायगा और दूसरा शरीर धारण कर लेगा।
जीवोंमें ये सब विलक्षणतायें क्यों हो रही हैं ? इसका समाधान आगमग्रंथोंमें इस तरह किया गया है कि प्रत्येक संसारी जीव अपने स्वतःसिद्ध देखने-जाननेरूप स्वभाव वाला होकरके भी अनादिकालसे स्वर्णपाषाणकी तरह पौद्गलिक कर्मोंके साथ सम्बद्ध (मिश्रित यानी एक क्षेत्रावगाही रूपसे एकमेकपनेको प्राप्त) हो रहा है। ये कर्म ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तरायके भेदसे मुल रूपमें आठ प्रकारके हैं। इनमें से ज्ञानावरण कर्मका कार्य जीवको जाननेकी शक्तिको आवत करना है,
१. समयसार, गाथा १६० । गोम्मटसार कर्मकाण्ड, गाथा २।
२. गोम्मटसार कर्मकाण्ड, गाथा ८ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org