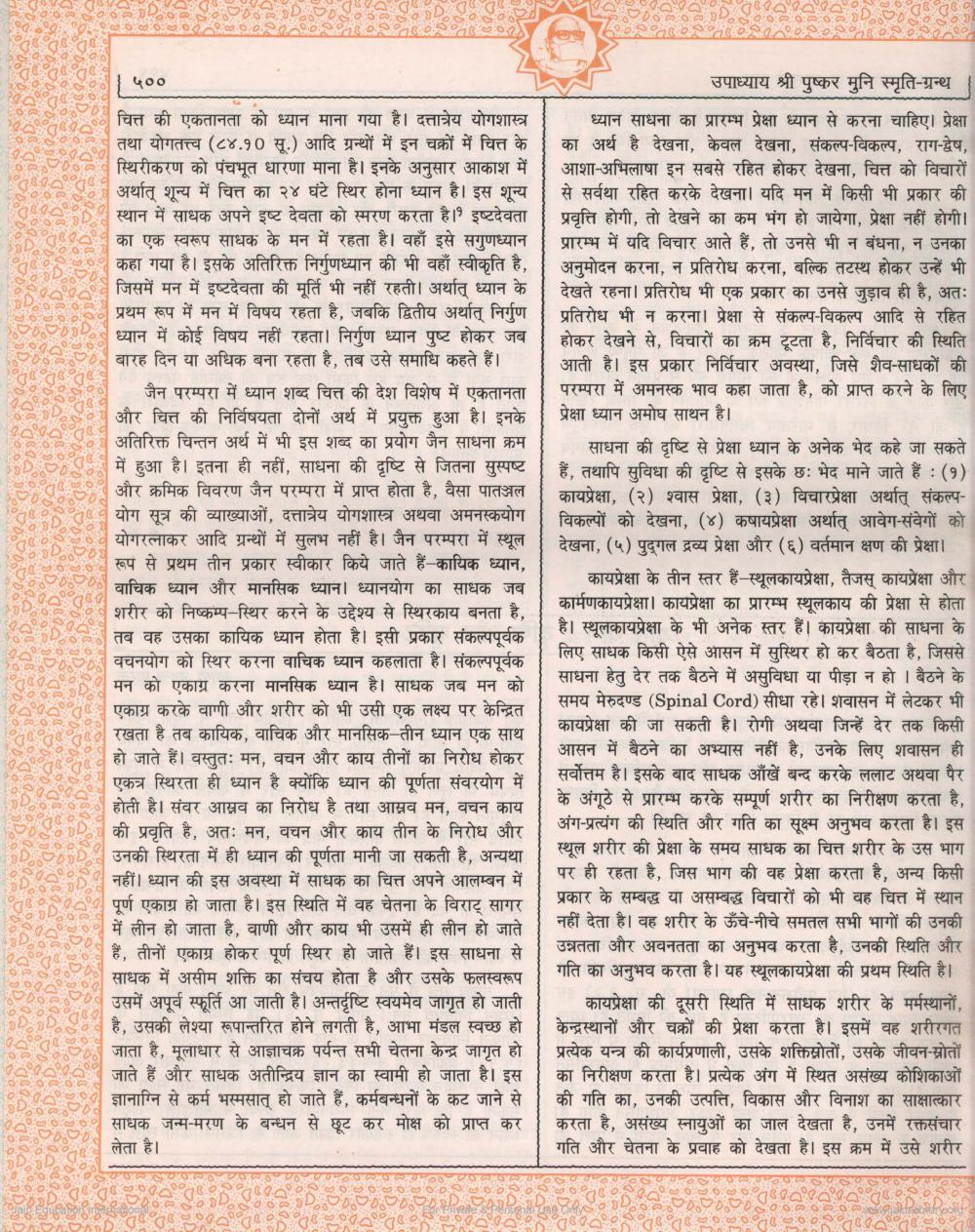________________
५००
चित्त की एकतानता को ध्यान माना गया है। दत्तात्रेय योगशास्त्र तथा योगतत्त्व (८४.१0 सू.) आदि ग्रन्थों में इन चक्रों में चित्त के स्थिरीकरण को पंचभूत धारणा माना है। इनके अनुसार आकाश में अर्थात् शून्य में चित्त का २४ घंटे स्थिर होना ध्यान है। इस शून्य स्थान में साधक अपने इष्ट देवता को स्मरण करता है।' इष्टदेवता का एक स्वरूप साधक के मन में रहता है। वहाँ इसे सगुणध्यान कहा गया है। इसके अतिरिक्त निर्गुणध्यान की भी वहाँ स्वीकृति है, जिसमें मन में इष्टदेवता की मूर्ति भी नहीं रहती। अर्थात् ध्यान के प्रथम रूप में मन में विषय रहता है, जबकि द्वितीय अर्थात् निर्गुण ध्यान में कोई विषय नहीं रहता। निर्गुण ध्यान पुष्ट होकर जब बारह दिन या अधिक बना रहता है, तब उसे समाधि कहते हैं।
जैन परम्परा में ध्यान शब्द चित्त की देश विशेष में एकतानता और चित्त की निर्विषयता दोनों अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इनके अतिरिक्त चिन्तन अर्थ में भी इस शब्द का प्रयोग जैन साधना क्रम में हुआ है। इतना ही नहीं, साधना की दृष्टि से जितना सुस्पष्ट और क्रमिक विवरण जैन परम्परा में प्राप्त होता है, वैसा पातञ्जल योग सूत्र की व्याख्याओं, दत्तात्रेय योगशास्त्र अथवा अमनस्कयोग योगरत्नाकर आदि ग्रन्थों में सुलभ नहीं है। जैन परम्परा में स्थूल रूप से प्रथम तीन प्रकार स्वीकार किये जाते हैं कायिक ध्यान, वाचिक ध्यान और मानसिक ध्यान। ध्यानयोग का साधक जब शरीर को निष्कम्प - स्थिर करने के उद्देश्य से स्थिरकाय बनता है, तब वह उसका कायिक ध्यान होता है। इसी प्रकार संकल्पपूर्वक वचनयोग को स्थिर करना वाचिक ध्यान कहलाता है। संकल्पपूर्वक मन को एकाग्र करना मानसिक ध्यान है। साधक जब मन को एकाग्र करके वाणी और शरीर को भी उसी एक लक्ष्य पर केन्द्रित रखता है तब कायिक, वाचिक और मानसिक-तीन ध्यान एक साथ हो जाते हैं। वस्तुतः मन, वचन और काय तीनों का निरोध होकर एकत्र स्थिरता ही ध्यान है क्योंकि ध्यान की पूर्णता संवरयोग में होती है। संवर आनव का निरोध है तथा आस्रव मन, वचन काय की प्रवृति है, अतः मन, वचन और काय तीन के निरोध और उनकी स्थिरता में ही ध्यान की पूर्णता मानी जा सकती है, अन्यथा नहीं। ध्यान की इस अवस्था में साधक का चित्त अपने आलम्बन में पूर्ण एकाग्र हो जाता है। इस स्थिति में वह चेतना के विराट् सागर में लीन हो जाता है, वाणी और काय भी उसमें ही लीन हो जाते हैं, तीनों एकाग्र होकर पूर्ण स्थिर हो जाते हैं। इस साधना से साधक में असीम शक्ति का संचय होता है और उसके फलस्वरूप उसमें अपूर्व स्फूर्ति आ जाती है। अन्तर्दृष्टि स्वयमेव जागृत हो जाती है. उसकी लेश्या रूपान्तरित होने लगती है, आभा मंडल स्वच्छ हो जाता है, मूलाधार से आज्ञाचक्र पर्यन्त सभी चेतना केन्द्र जागृत हो जाते हैं और साधक अतीन्द्रिय ज्ञान का स्वामी हो जाता है। इस ज्ञानाग्नि से कर्म भस्मसात् हो जाते हैं, कर्मबन्धनों के कट जाने से साधक जन्म-मरण के बन्धन से छूट कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।
Ge
उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि स्मृति ग्रन्थ
ध्यान साधना का प्रारम्भ प्रेक्षा ध्यान से करना चाहिए। प्रेक्षा का अर्थ है देखना, केवल देखना, संकल्प-विकल्प, राग-द्वेष, आशा - अभिलाषा इन सबसे रहित होकर देखना, वित्त को विचारों से सर्वथा रहित करके देखना। यदि मन में किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति होगी, तो देखने का कम भंग हो जायेगा, प्रेक्षा नहीं होगी। प्रारम्भ में यदि विचार आते हैं, तो उनसे भी न बंधना, न उनका अनुमोदन करना, न प्रतिरोध करना, बल्कि तटस्थ होकर उन्हें भी देखते रहना। प्रतिरोध भी एक प्रकार का उनसे जुड़ाव ही है, अतः प्रतिरोध भी न करना । प्रेक्षा से संकल्प-विकल्प आदि से रहित होकर देखने से विचारों का क्रम टूटता है, निर्विचार की स्थिति आती है। इस प्रकार निर्विचार अवस्था, जिसे शैव-साधकों की परम्परा में अमनस्क भाव कहा जाता है, को प्राप्त करने के लिए प्रेक्षा ध्यान अमोघ साथन है।
साधना की दृष्टि से प्रेक्षा ध्यान के अनेक भेद कहे जा सकते हैं, तथापि सुविधा की दृष्टि से इसके छः भेद माने जाते हैं : (१) कायप्रेक्षा, (२) श्वास प्रेक्षा, (३) विचारप्रेक्षा अर्थात् संकल्पविकल्पों को देखना, (४) कषायप्रेक्षा अर्थात् आवेग संवेगों को देखना, (५) पुद्गल द्रव्य प्रेक्षा और (६) वर्तमान क्षण की प्रेक्षा ।
कायप्रेक्षा के तीन स्तर हैं-स्थूलकायप्रेक्षा, तैजस् कायप्रेक्षा और कार्मणका प्रेक्षा । कायप्रेक्षा का प्रारम्भ स्थूलकाय की प्रेक्षा से होता है । स्थूलकायप्रेक्षा के भी अनेक स्तर हैं। कायप्रेक्षा की साधना के लिए साधक किसी ऐसे आसन में सुस्थिर हो कर बैठता है, जिससे साधना हेतु देर तक बैठने में असुविधा या पीड़ा न हो । बैठने के समय मेरुदण्ड (Spinal Cord) सीधा रहे। शवासन में लेटकर भी कायप्रेक्षा की जा सकती है। रोगी अथवा जिन्हें देर तक किसी आसन में बैठने का अभ्यास नहीं है, उनके लिए शवासन ही सर्वोत्तम है। इसके बाद साधक आँखें बन्द करके ललाट अथवा पैर के अंगूठे से प्रारम्भ करके सम्पूर्ण शरीर का निरीक्षण करता है, अंग-प्रत्यंग की स्थिति और गति का सूक्ष्म अनुभव करता है। इस स्थूल शरीर की प्रेक्षा के समय साधक का चित्त शरीर के उस भाग पर ही रहता है, जिस भाग की वह प्रेक्षा करता है, अन्य किसी प्रकार के सम्बद्ध या असम्बद्ध विचारों को भी वह चित्त में स्थान नहीं देता है। वह शरीर के ऊँचे-नीचे समतल सभी भागों की उनकी उन्नतता और अवनतता का अनुभव करता है, उनकी स्थिति और गति का अनुभव करता है। यह स्थूलकायप्रेक्षा की प्रथम स्थिति है।
कायप्रेक्षा की दूसरी स्थिति में साधक शरीर के मर्मस्थानों, केन्द्रस्थानों और चक्रों की प्रेक्षा करता है। इसमें वह शरीरगत प्रत्येक यन्त्र की कार्यप्रणाली, उसके शक्तिस्रोतों, उसके जीवन स्रोतों का निरीक्षण करता है। प्रत्येक अंग में स्थित असंख्य कोशिकाओं की गति का, उनकी उत्पत्ति, विकास और विनाश का साक्षात्कार करता है, असंख्य स्नायुओं का जाल देखता है, उनमें रक्तसंचार गति और चेतना के प्रवाह को देखता है। इस क्रम में उसे शरीर