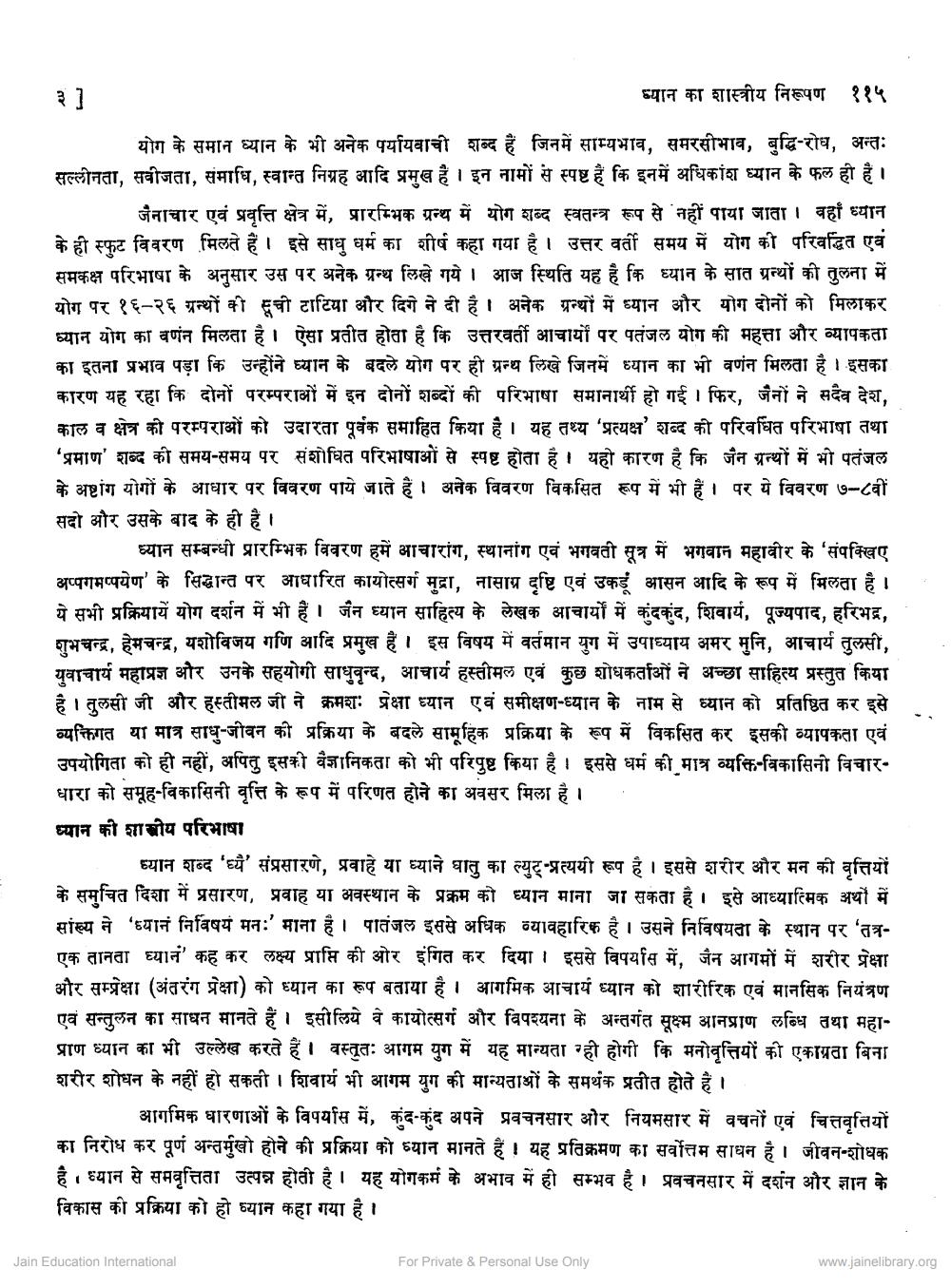________________
ध्यान का शास्त्रीय निरूपण ११५ योग के समान ध्यान के भी अनेक पर्यायवाची शब्द हैं जिनमें साम्यभाव, समरसीभाव, बुद्धि-रोध, अन्तः सल्लीनता, सवीजता, समाधि, स्वान्त निग्रह आदि प्रमुख हैं । इन नामों से स्पष्ट हैं कि इनमें अधिकांश ध्यान के फल ही है । जैनाचार एवं प्रवृत्ति क्षेत्र में, प्रारम्भिक ग्रन्थ में योग शब्द स्वतन्त्र रूप से नहीं पाया जाता । वहाँ ध्यान केही स्फुट विवरण मिलते हैं। इसे साधु धर्म का शीर्ष कहा गया है । उत्तरवर्ती समय में योग की परिवद्धित एवं समकक्ष परिभाषा के अनुसार उस पर अनेक ग्रन्थ लिखे गये । आज स्थिति यह है कि ध्यान के सात ग्रन्थों की तुलना में योग पर १६-२६ ग्रन्थों की सूची टाटिया और दिगे ने दी है। अनेक ग्रन्थों में ध्यान और योग दोनों को मिलाकर ध्यान योग का वर्णन मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरवर्ती आचार्यों पर पतंजल योग की महत्ता और व्यापकता का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने ध्यान के बदले योग पर ही ग्रन्थ लिखे जिनमें ध्यान का भी वर्णन मिलता है । इसका कारण यह रहा कि दोनों परम्पराओं में इन दोनों शब्दों की परिभाषा समानार्थी हो गई । फिर, जैनों ने सदैव देश, काल व क्षेत्र की परम्पराओं को उदारता पूर्वक समाहित किया है । यह तथ्य 'प्रत्यक्ष' शब्द की परिवर्धित परिभाषा तथा 'प्रमाण' शब्द की समय-समय पर संशोधित परिभाषाओं से स्पष्ट होता है । यही कारण है कि जैन ग्रन्थों में भी पतंजल के अष्टांग योगों के आधार पर विवरण पाये जाते हैं । अनेक विवरण विकसित रूप में भी हैं । सदों और उसके बाद के ही हैं ।
पर ये विवरण ७-८वीं
ध्यान सम्बन्धी प्रारम्भिक विवरण हमें आचारांग, स्थानांग एवं भगवती सूत्र में भगवान महावीर के 'संपक्खिए अप्पगमप्पयेण' के सिद्धान्त पर आधारित कायोत्सर्ग मुद्रा, नासाग्र दृष्टि एवं उकडूं आसन आदि के रूप में मिलता है । ये सभी प्रक्रियायें योग दर्शन में भी हैं । जैन ध्यान साहित्य के लेखक आचार्यों में कुंदकुंद, शिवार्य, पूज्यपाद, हरिभद्र, शुभचन्द्र, हेमचन्द्र, यशोविजय गणि आदि प्रमुख हैं । इस विषय में वर्तमान युग में उपाध्याय अमर मुनि, आचार्य तुलसी, युवाचार्य महाप्रज्ञ और उनके सहयोगी साधुवृन्द, आचार्य हस्तीमल एवं कुछ शोधकर्ताओं ने अच्छा साहित्य प्रस्तुत किया है । तुलसी जी और हस्तीमल जी ने क्रमशः प्रेक्षा ध्यान एवं समीक्षण-ध्यान के नाम से ध्यान को प्रतिष्ठित कर इसे व्यक्तिगत या मात्र साधु - जीवन की प्रक्रिया के बदले सामूहिक प्रक्रिया के रूप में विकसित कर इसकी व्यापकता एवं उपयोगिता को ही नहीं, अपितु इसकी वैज्ञानिकता को भी परिपुष्ट किया है। इससे धर्म की मात्र व्यक्ति विकासिनी विचारधारा को समूह विकासिनी वृत्ति के रूप में परिणत होने का अवसर मिला है ।
ध्यान की शास्त्रीय परिभाषा
३]
व्यावहारिक है। उसने निर्विषयता के स्थान पर 'तत्रदिया । इससे विपर्यास में, जैन आगमों में शरीर प्रेक्षा
ध्यान शब्द 'ध्यै' संप्रसारणे, प्रवाहे या ध्याने धातु का ल्युट् प्रत्ययी रूप है । इससे शरीर और मन की वृत्तियों के समुचित दिशा में प्रसारण प्रवाह या अवस्थान के प्रक्रम को ध्यान माना जा सकता है । इसे आध्यात्मिक अर्थों में सांख्य ने 'ध्यानं निर्विषयं मनः' माना है । पातंजल इससे अधिक एक तानता ध्यानं' कह कर लक्ष्य प्राप्ति की ओर इंगित कर और सम्प्रेक्षा (अंतरंग प्रेक्षा) को ध्यान का रूप बताया है । आगमिक आचार्य ध्यान को शारीरिक एवं मानसिक नियंत्रण एवं सन्तुलन का साधन मानते हैं । इसीलिये वे कायोत्सर्ग और विपश्यना के अन्तर्गत सूक्ष्म आनप्राण लब्धि तथा महाप्राण ध्यान का भी उल्लेख करते हैं । वस्तुतः आगम युग में यह मान्यता रही होगी कि मनोवृत्तियों की एकाग्रता बिना शरीर शोधन के नहीं हो सकती । शिवार्य भी आगम युग की मान्यताओं के समर्थक प्रतीत होते हैं ।
आगमिक धारणाओं के विपर्यास में, कुंद-कुंद अपने प्रवचनसार और नियमसार में वचनों एवं चित्तवृत्तियों का निरोध कर पूर्ण अन्तर्मुखो होने की प्रक्रिया को ध्यान मानते हैं । यह प्रतिक्रमण का सर्वोत्तम साधन है । जीवन-शोधक है। ध्यान से समवृत्तिता उत्पन्न होती है । यह योगकर्म के अभाव में ही सम्भव है । प्रवचनसार में दर्शन और ज्ञान के विकास की प्रक्रिया को हो ध्यान कहा गया है ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org