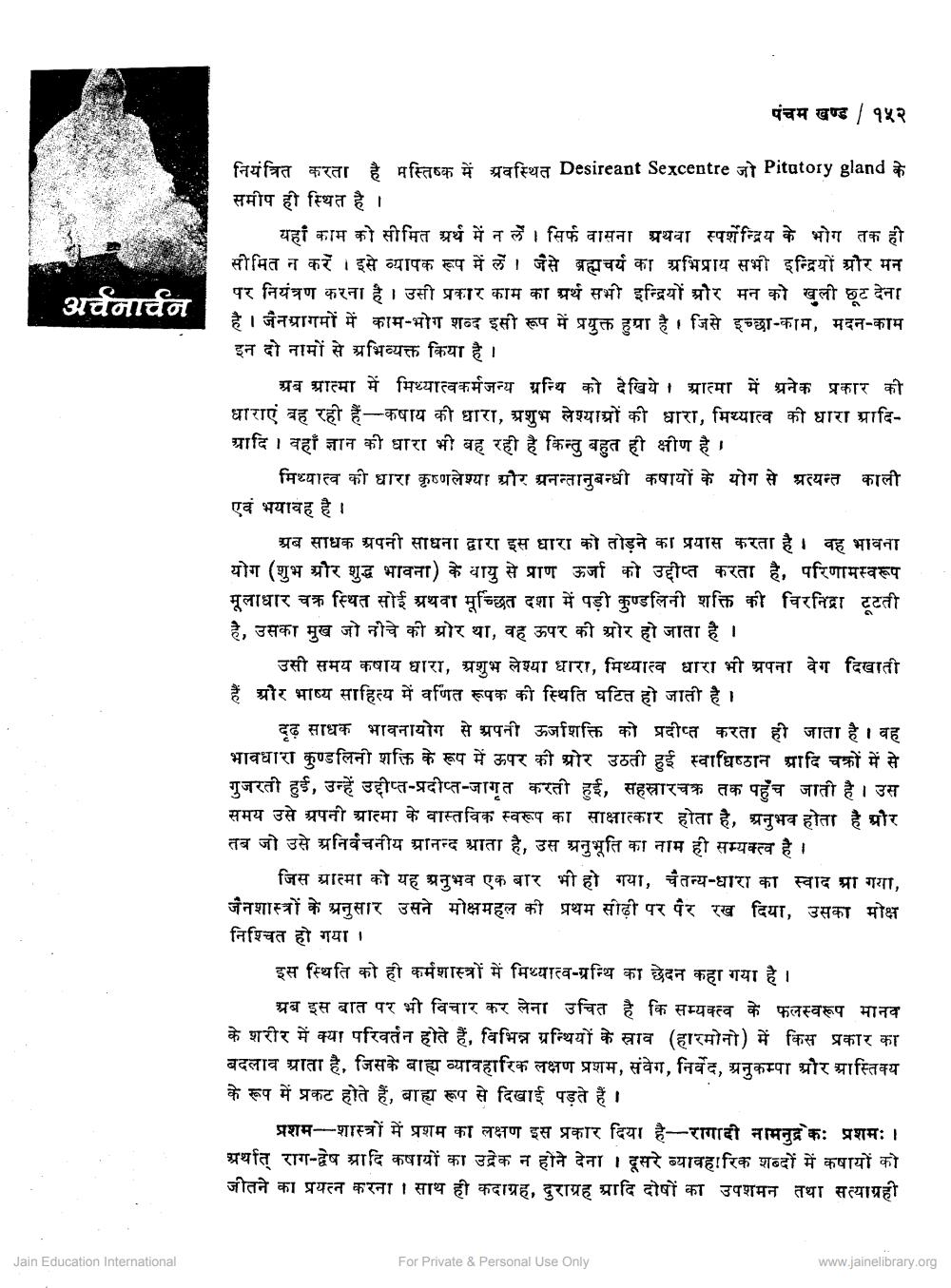________________
पंचम खण्ड | १५२
अर्चनार्चन
नियंत्रित करता है मस्तिष्क में अवस्थित Desireant Sexcentre जो Pitatory gland के समीप ही स्थित है ।
यहां काम को सीमित अर्थ में न लें। सिर्फ वासना अथवा स्पर्शेन्द्रिय के भोग तक ही सीमित न करें। इसे व्यापक रूप में लें। जैसे ब्रह्मचर्य का अभिप्राय सभी इन्द्रियों और मन पर नियंत्रण करना है। उसी प्रकार काम का अर्थ सभी इन्द्रियों और मन को खुली छूट देना है । जैनागमों में काम-भोग शब्द इसी रूप में प्रयुक्त हपा है। जिसे इच्छा-काम, मदन-काम इन दो नामों से अभिव्यक्त किया है।
अब प्रात्मा में मिथ्यात्वकर्मजन्य ग्रन्थि को देखिये। आत्मा में अनेक प्रकार की धाराएं बह रही हैं-कषाय की धारा, अशुभ लेश्यामों की धारा, मिथ्यात्व की धारा प्रादिग्रादि । वहाँ ज्ञान की धारा भी बह रही है किन्तु बहुत ही क्षीण है।
मिथ्यात्व की धारा कृष्णलेश्या और अनन्तानुबन्धी कषायों के योग से अत्यन्त काली एवं भयावह है।
अब साधक अपनी साधना द्वारा इस धारा को तोड़ने का प्रयास करता है। वह भावना योग (शुभ और शुद्ध भावना) के वायु से प्राण ऊर्जा को उद्दीप्त करता है, परिणामस्वरूप मूलाधार चक्र स्थित सोई अथवा मूच्छित दशा में पड़ी कुण्डलिनी शक्ति की चिरनिद्रा टूटती है, उसका मुख जो नीचे की ओर था, वह ऊपर की ओर हो जाता है ।
उसी समय कषाय धारा, अशुभ लेश्या धारा, मिथ्यात्व धारा भी अपना वेग दिखाती हैं और भाष्य साहित्य में वर्णित रूपक की स्थिति घटित हो जाती है।
दृढ़ साधक भावनायोग से अपनी ऊर्जाशक्ति को प्रदीप्त करता ही जाता है। वह भावधारा कुण्डलिनी शक्ति के रूप में ऊपर की ओर उठती हुई स्वाधिष्ठान आदि चक्रों में से गुजरती हुई, उन्हें उद्दीप्त-प्रदीप्त-जागृत करती हुई, सहस्रारचक्र तक पहुंच जाती है । उस समय उसे अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार होता है, अनुभव होता है और तब जो उसे अनिर्वचनीय आनन्द आता है, उस अनुभूति का नाम ही सम्यक्त्व है।
जिस प्रात्मा को यह अनुभव एक बार भी हो गया, चैतन्य-धारा का स्वाद पा गया, जैनशास्त्रों के अनुसार उसने मोक्षमहल की प्रथम सीढ़ी पर पैर रख दिया, उसका मोक्ष निश्चित हो गया।
इस स्थिति को ही कर्मशास्त्रों में मिथ्यात्व-ग्रन्थि का छेदन कहा गया है।
अब इस बात पर भी विचार कर लेना उचित है कि सम्यक्त्व के फलस्वरूप मानव के शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं, विभिन्न ग्रन्थियों के स्राव (हारमोनो) में किस प्रकार का बदलाव पाता है, जिसके बाह्य व्यावहारिक लक्षण प्रशम, संवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्तिक्य के रूप में प्रकट होते हैं, बाह्य रूप से दिखाई पड़ते हैं।
प्रशम-शास्त्रों में प्रशम का लक्षण इस प्रकार दिया है-रागादी नामनुद्र कः प्रशमः । अर्थात् राग-द्वेष आदि कषायों का उद्रेक न होने देना । दूसरे ब्यावहारिक शब्दों में कषायों को जीतने का प्रयत्न करना । साथ ही कदाग्रह, दुराग्रह आदि दोषों का उपशमन तथा सत्याग्रही
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org