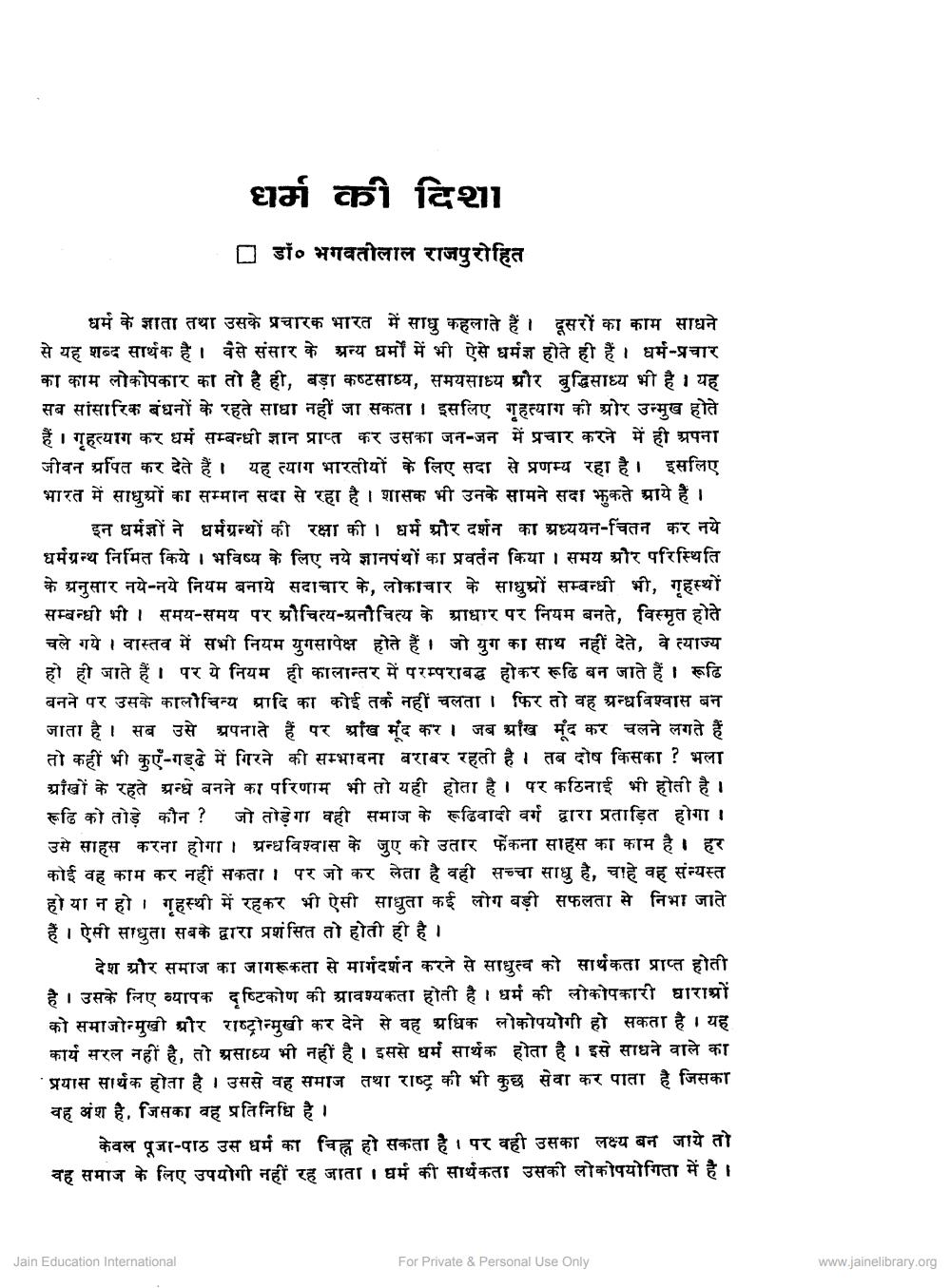________________
धर्म की दिशा
0 डॉ० भगवतीलाल राजपुरोहित
धर्म के ज्ञाता तथा उसके प्रचारक भारत में साधु कहलाते हैं। दूसरों का काम साधने से यह शब्द सार्थक है। वैसे संसार के अन्य धर्मों में भी ऐसे धर्मज्ञ होते ही हैं। धर्म-प्रचार का काम लोकोपकार का तो है ही, बड़ा कष्टसाध्य, समयसाध्य और बुद्धिसाध्य भी है। यह सब सांसारिक बंधनों के रहते साधा नहीं जा सकता। इसलिए गृहत्याग की ओर उन्मुख होते हैं । गृहत्याग कर धर्म सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त कर उसका जन-जन में प्रचार करने में ही अपना जीवन अपित कर देते हैं। यह त्याग भारतीयों के लिए सदा से प्रणम्य रहा है। इसलिए भारत में साधुओं का सम्मान सदा से रहा है। शासक भी उनके सामने सदा झुकते आये हैं।
इन धर्मज्ञों ने धर्मग्रन्थों की रक्षा की। धर्म और दर्शन का अध्ययन-चिंतन कर नये धर्मग्रन्थ निर्मित किये । भविष्य के लिए नये ज्ञानपंथों का प्रवर्तन किया। समय और परिस्थिति के अनुसार नये-नये नियम बनाये सदाचार के, लोकाचार के साधुनों सम्बन्धी भी, गृहस्थों सम्बन्धी भी। समय-समय पर औचित्य-अनौचित्य के आधार पर नियम बनते, विस्मृत होते चले गये । वास्तव में सभी नियम युगसापेक्ष होते हैं। जो युग का साथ नहीं देते, वे त्याज्य हो ही जाते हैं। पर ये नियम ही कालान्तर में परम्पराबद्ध होकर रूढि बन जाते हैं। रूढि बनने पर उसके कालौचिन्य प्रादि का कोई तर्क नहीं चलता। फिर तो वह अन्धविश्वास बन जाता है। सब उसे अपनाते हैं पर आंख मूंद कर । जब आँख मूंद कर चलने लगते हैं तो कहीं भी कुएँ-गड्ढे में गिरने की सम्भावना बराबर रहती है। तब दोष किसका ? भला आँखों के रहते अन्धे बनने का परिणाम भी तो यही होता है। पर कठिनाई भी होती है। रूढि को तोड़े कौन? जो तोड़ेगा वही समाज के रूढिवादी वर्ग द्वारा प्रताड़ित होगा। उसे साहस करना होगा। अन्धविश्वास के जुए को उतार फेंकना साहस का काम है। हर कोई वह काम कर नहीं सकता। पर जो कर लेता है वही सच्चा साधु है, चाहे वह संन्यस्त हो या न हो। गृहस्थी में रहकर भी ऐसी साधुता कई लोग बड़ी सफलता से निभा जाते हैं । ऐसी साधुता सबके द्वारा प्रशंसित तो होती ही है ।
देश और समाज का जागरूकता से मार्गदर्शन करने से साधुत्व को सार्थकता प्राप्त होती है । उसके लिए व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। धर्म की लोकोपकारी धाराओं को समाजोन्मुखी और राष्ट्रोन्मुखी कर देने से वह अधिक लोकोपयोगी हो सकता है । यह कार्य सरल नहीं है, तो असाध्य भी नहीं है। इससे धर्म सार्थक होता है। इसे साधने वाले का प्रयास सार्थक होता है। उससे वह समाज तथा राष्ट्र की भी कुछ सेवा कर पाता है जिसका वह अंश है, जिसका वह प्रतिनिधि है।
केवल पूजा-पाठ उस धर्म का चिह्न हो सकता है। पर वही उसका लक्ष्य बन जाये तो वह समाज के लिए उपयोगी नहीं रह जाता। धर्म की सार्थकता उसकी लोकोपयोगिता में है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org