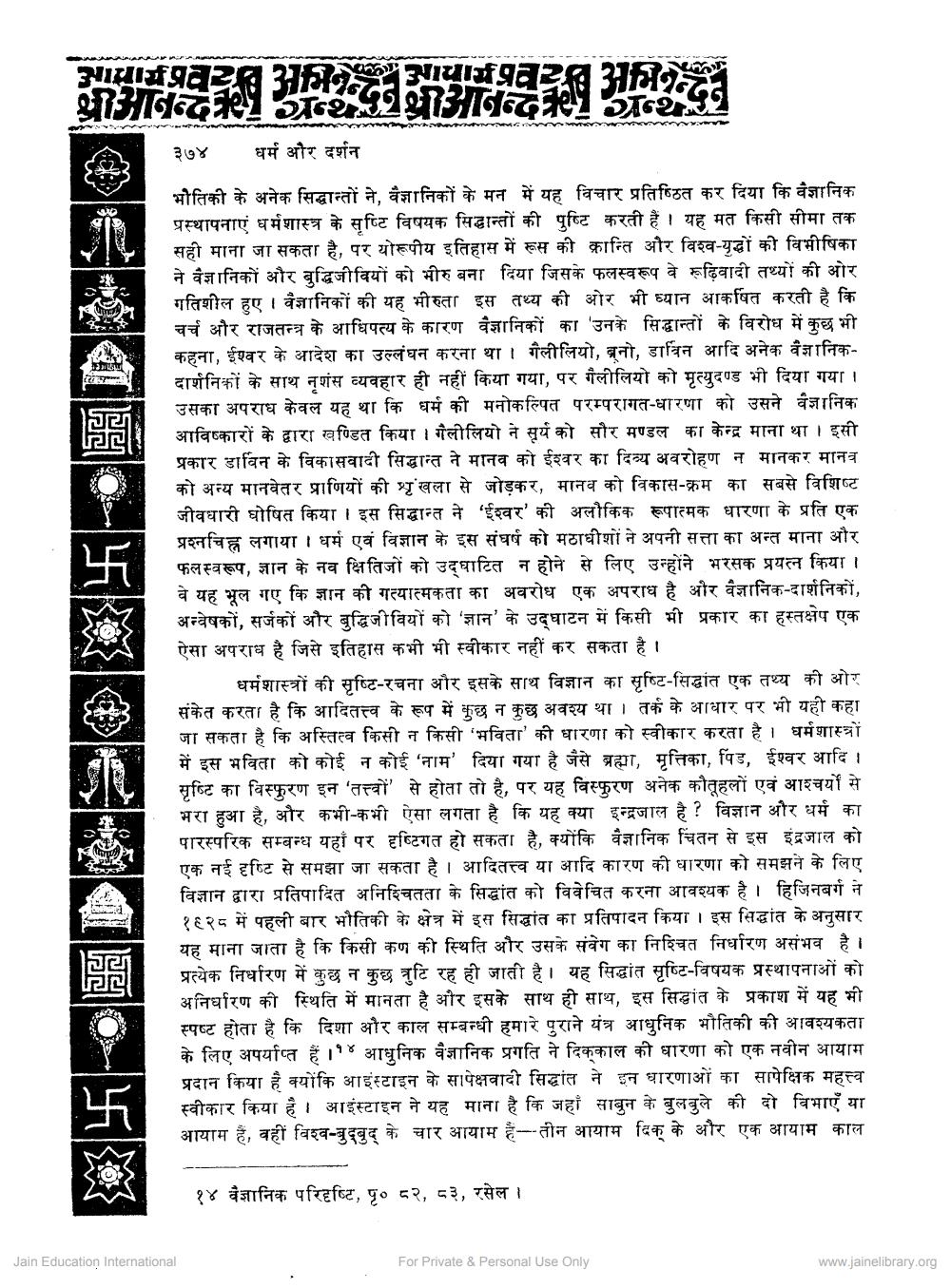________________
आर्य प्रव श्री आनन्दन ग्रन्थ
आमद आमद श्री आनन्दव
३७४
धर्म और दर्शन
भौतिकी के अनेक सिद्धान्तों ने वैज्ञानिकों के मन में यह विचार प्रतिष्ठित कर दिया कि वैज्ञानिक प्रस्थापनाएं धर्मशास्त्र के सृष्टि विषयक सिद्धान्तों की पुष्टि करती है यह मत किसी सीमा तक सही माना जा सकता है, पर योरुपीय इतिहास में रूस की क्रान्ति और विश्व युद्धों की विभीषिका ने वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों को भीरु बना दिया जिसके फलस्वरूप वे रूढ़िवादी तथ्यों की ओर गतिशील हुए। वैज्ञानिकों की यह भीरुता इस तथ्य की ओर भी ध्यान आकर्षित करती है कि चर्च और राजतन्त्र के आधिपत्य के कारण वैज्ञानिकों का उनके सिद्धान्तों के विरोध में कुछ भी ईश्वर के आदेश का उल्लंघन करना था। गैलीलियो बनो, डाबिन आदि अनेक वैज्ञानिकदार्शनिकों के साथ नृशंस व्यवहार ही नहीं किया गया, पर गैलीलियो को मृत्युदण्ड भी दिया गया। उसका अपराध केवल यह था कि धर्म की मनोकल्पित परम्परागत धारणा को उसने वैज्ञानिक आविष्कारों के द्वारा सहित किया। गैलीलियो ने सूर्य को सौर मण्डल का केन्द्र माना था। इसी प्रकार डार्विन के विकासवादी सिद्धान्त ने मानव को ईश्वर का दिव्य अवरोहण न मानकर मानव को अन्य मानवेतर प्राणियों की श्रृंखला से जोड़कर मानव को विकास क्रम का सबसे विशिष्ट जीवपारी घोषित किया। इस सिद्धान्त ने 'ईश्वर' की अलौकिक रूपात्मक धारणा के प्रति एक प्रश्नचिह्न लगाया। धर्म एवं विज्ञान के इस संघर्ष को मठाधीशों ने अपनी सत्ता का अन्त माना और फलस्वरूप, ज्ञान के नव क्षितिजों को उद्घाटित न होने से लिए उन्होंने भरसक प्रयत्न किया । वे यह भूल गए कि ज्ञान की गत्यात्मकता का अवरोध एक अपराध है और वैज्ञानिक - दार्शनिकों, अन्वेषकों, सर्जकों और बुद्धिजीवियों को 'शान' के उद्घाटन में किसी भी ऐसा अपराध है जिसे इतिहास कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता है ।
प्रकार का हस्तक्षेप एक
乖
Murp
धर्मशास्त्रों की सृष्टि रचना और इसके साथ विज्ञान का सृष्टि-सिद्धांत एक तथ्य की ओर
संकेत करता है कि आदितत्त्व के रूप में कुछ न कुछ अवश्य था । तर्क के आधार पर भी यही कहा जा सकता है कि अस्तित्व किसी न किसी 'भविता' की धारणा को स्वीकार करता है। धर्मशास्त्रों में इस भविता को कोई न कोई 'नाम' दिया गया है जैसे ब्रह्मा, मृत्तिका, पिंड, ईश्वर आदि । सृष्टि का विस्फुरण इन 'तत्वों' से होता तो है, पर यह विस्फुरण अनेक कौतुहलों एवं आश्चर्यों से भरा हुआ है, और कभी-कभी ऐसा लगता है कि यह क्या इन्द्रजाल है ? विज्ञान और धर्म का पारस्परिक सम्बन्ध यहाँ पर दृष्टिगत हो सकता है, क्योंकि वैज्ञानिक चिंतन से इस इंद्रजाल को एक नई दृष्टि से समझा जा सकता है। आदितत्त्व या आदि कारण की धारणा को समझने के लिए विज्ञान द्वारा प्रतिपादित अनिश्चितता के सिद्धांत को विवेचित करना आवश्यक है। हिजिनबर्ग ने १६२० में पहली बार भौतिकी के क्षेत्र में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि किसी कम की स्थिति और उसके संवेग का निश्चित निर्धारण असंभव है। प्रत्येक निर्धारण में कुछ न कुछ त्रुटि रह ही जाती है। यह सिद्धांत सृष्टि-विषयक प्रस्थापनाओं को अनिर्धारण की स्थिति में मानता है और इसके साथ ही साथ इस सिद्धांत के प्रकाश में यह भी स्पष्ट होता है कि दिशा और काल सम्बन्धी हमारे पुराने यंत्र आधुनिक भौतिकी की आवश्यकता के लिए अपर्याप्त है। आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति ने दिक्काल की धारणा को एक नवीन आयाम प्रदान किया है क्योंकि आइंस्टाइन के सापेक्षवादी सिद्धांत ने इन धारणाओं का सापेक्षिक महत्त्व स्वीकार किया है। आइंस्टाइन ने यह माना है कि जहाँ साबुन के बुलबुले की दो विमाएँ या आयाम हैं, वहीं विश्व बुबु के चार आयाम है- तीन आयाम दिक् के और एक आयाम काल
१४ वैज्ञानिक परिदृष्टि, पृ० ८२, ८३, रसेल ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org