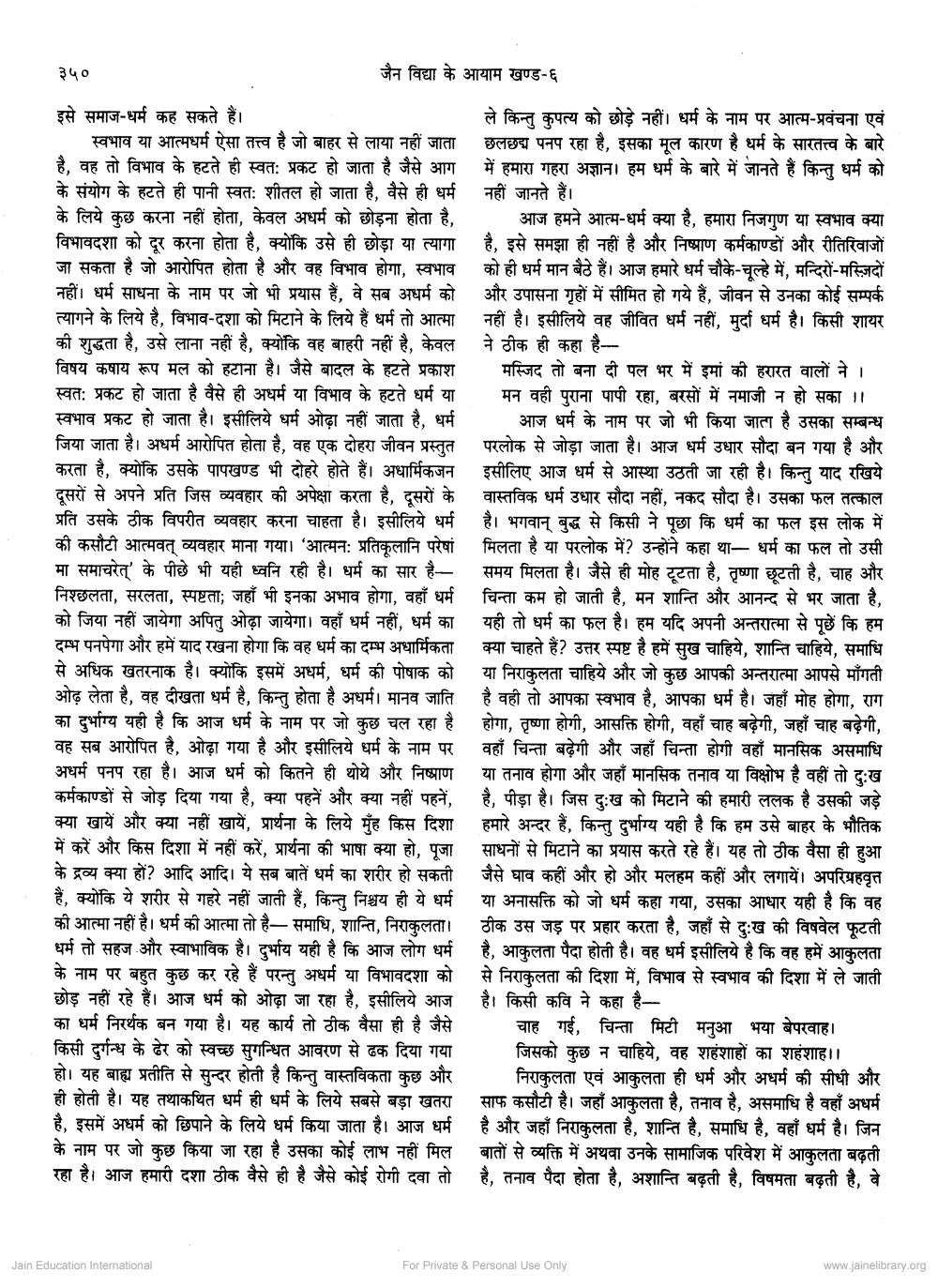________________
३५०
इसे समाज धर्म कह सकते हैं।
स्वभाव या आत्मधर्म ऐसा तत्त्व है जो बाहर से लाया नहीं जाता है, वह तो विभाव के हटते ही स्वतः प्रकट हो जाता है जैसे आग के संयोग के हटते ही पानी स्वतः शीतल हो जाता है, वैसे ही धर्म के लिये कुछ करना नहीं होता, केवल अधर्म को छोड़ना होता है, विभावदशा को दूर करना होता है, क्योंकि उसे ही छोड़ा या त्यागा जा सकता है जो आरोपित होता है और वह विभाव होगा, स्वभाव नहीं। धर्म साधना के नाम पर जो भी प्रयास हैं, वे सब अधर्म को त्यागने के लिये है, विभाव- दशा को मिटाने के लिये हैं धर्म तो आत्मा की शुद्धता है, उसे लाना नहीं है, क्योंकि वह बाहरी नहीं है, केवल विषय कषाय रूप मल को हटाना है। जैसे बादल के हटते प्रकाश स्वतः प्रकट हो जाता है वैसे ही अधर्म या विभाव के हटते धर्म या स्वभाव प्रकट हो जाता है। इसीलिये धर्म ओढ़ा नहीं जाता है, धर्म जिया जाता है। अधर्म आरोपित होता है, वह एक दोहरा जीवन प्रस्तुत करता है, क्योंकि उसके पापखण्ड भी दोहरे होते हैं। अधार्मिकजन दूसरों से अपने प्रति जिस व्यवहार की अपेक्षा करता है, दूसरों के प्रति उसके ठीक विपरीत व्यवहार करना चाहता है। इसीलिये धर्म की कसौटी आत्मवत् व्यवहार माना गया 'आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां मा समाचरेत्' के पीछे भी यही ध्वनि रही है। धर्म का सार हैनिश्छलता, सरलता, स्पष्टता; जहाँ भी इनका अभाव होगा, वहाँ धर्म को जिया नहीं जायेगा अपितु ओढ़ा जायेगा वहाँ धर्म नहीं, धर्म का दम्भ पनपेगा और हमें याद रखना होगा कि वह धर्म का दम्भ अधार्मिकता से अधिक खतरनाक है क्योंकि इसमें अधर्म, धर्म की पोषाक को ओढ़ लेता है, वह दीखता धर्म है, किन्तु होता है अधर्म । मानव जाति का दुर्भाग्य यही है कि आज धर्म के नाम पर जो कुछ चल रहा है वह सब आरोपित है, ओढ़ा गया है और इसीलिये धर्म के नाम पर अधर्म पनप रहा है। आज धर्म को कितने ही थोथे और निष्याण कर्मकाण्डों से जोड़ दिया गया है, क्या पहनें और क्या नहीं पहनें, क्या खायें और क्या नहीं खायें, प्रार्थना के लिये मुँह किस दिशा में करें और किस दिशा में नहीं करें, प्रार्थना की भाषा क्या हो, पूजा के द्रव्य क्या हो? आदि आदि। ये सब बातें धर्म का शरीर हो सकती हैं, क्योंकि ये शरीर से गहरे नहीं जाती हैं, किन्तु निश्चय ही ये धर्म की आत्मा नहीं है। धर्म की आत्मा तो है— समाधि, शान्ति, निराकुलता । धर्म तो सहज और स्वाभाविक है। दुर्भाय यही है कि आज लोग धर्म के नाम पर बहुत कुछ कर रहे हैं परन्तु अधर्म या विभावदशा को छोड़ नहीं रहे हैं। आज धर्म को ओढ़ा जा रहा है, इसीलिये आज का धर्म निरर्थक बन गया है। यह कार्य तो ठीक वैसा ही है जैसे किसी दुर्गन्ध के ढेर को स्वच्छ सुगन्धित आवरण से ढक दिया गया हो। यह बाह्य प्रतीति से सुन्दर होती है किन्तु वास्तविकता कुछ और ही होती है। यह तथाकथित धर्म ही धर्म के लिये सबसे बड़ा खतरा है, इसमें अधर्म को छिपाने के लिये धर्म किया जाता है। आज धर्म के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आज हमारी दशा ठीक वैसे ही है जैसे कोई रोगी दवा तो
जैन विद्या के आयाम खण्ड ६
Jain Education International
ले किन्तु कुपत्य को छोड़े नहीं। धर्म के नाम पर आत्म- प्रवंचना एवं छलछद्म पनप रहा है, इसका मूल कारण है धर्म के सारतत्त्व के बारे में हमारा गहरा अज्ञान। हम धर्म के बारे में जानते हैं किन्तु धर्म को नहीं जानते हैं।
आज हम आत्म-धर्म क्या है, हमारा निजगुण या स्वभाव क्या है, इसे समझा ही नहीं है और निष्माण कर्मकाण्डों और रीतिरिवाजों को ही धर्म मान बैठे हैं। आज हमारे धर्म चौके-चूल्हे में, मन्दिरों-मस्जिदों और उपासना गृहों में सीमित हो गये हैं, जीवन से उनका कोई सम्पर्क नहीं है। इसीलिये वह जीवित धर्म नहीं, मुर्दा धर्म है किसी शायर ने ठीक ही कहा है
मस्जिद तो बना दी पल भर में इमां की हरारत वालों ने । मन वही पुराना पापी रहा, वरसों में नमाजी न हो सका ।।
आज धर्म के नाम पर जो भी किया जाता है उसका सम्बन्ध परलोक से जोड़ा जाता है। आज धर्म उधार सौदा बन गया है और इसीलिए आज धर्म से आस्था उठती जा रही है। किन्तु याद रखिये वास्तविक धर्म उधार सौदा नहीं, नकद सौदा है। उसका फल तत्काल है। भगवान् बुद्ध से किसी ने पूछा कि धर्म का फल इस लोक में मिलता है या परलोक में? उन्होंने कहा था— धर्म का फल तो उसी समय मिलता है। जैसे ही मोह टूटता है, तृष्णा छूटती है, चाह और चिन्ता कम हो जाती है, मन शान्ति और आनन्द से भर जाता है, यही तो धर्म का फल है। हम यदि अपनी अन्तरात्मा से पूछें कि हम क्या चाहते हैं? उत्तर स्पष्ट है हमें सुख चाहिये, शान्ति चाहिये, समाधि या निराकुलता चाहिये और जो कुछ आपकी अन्तरात्मा आपसे माँगती है वही तो आपका स्वभाव है, आपका धर्म है। जहाँ मोह होगा, राग होगा, तृष्णा होगी, आसक्ति होगी, वहाँ चाह बढ़ेगी, जहाँ चाह बढ़ेगी, वहाँ चिन्ता बढ़ेगी और जहाँ चिन्ता होगी वहाँ मानसिक असमाधि या तनाव होगा और जहाँ मानसिक तनाव या विक्षोभ है वहीं तो 'दुःख है, पीड़ा है। जिस दुःख को मिटाने की हमारी ललक है उसकी जड़े हमारे अन्दर हैं, किन्तु दुर्भाग्य यही है कि हम उसे बाहर के भौतिक साधनों से मिटाने का प्रयास करते रहे हैं। यह तो ठीक वैसा ही हुआ जैसे घाव कहीं और हो और मलहम कहीं और लगायें अपरिग्रहवृत्त या अनासक्ति को जो धर्म कहा गया, उसका आधार यही है कि वह ठीक उस जड़ पर प्रहार करता है, जहाँ से दुःख की विषवेल फूटती है, आकुलता पैदा होती है। वह धर्म इसीलिये है कि वह हमें आकुलता से निराकुलता की दिशा में, विभाव से स्वभाव की दिशा में ले जाती है। किसी कवि ने कहा है
चाह गई, चिन्ता मिटी मनुआ भया बेपरवाह। जिसको कुछ न चाहिये, वह शहंशाहों का शहंशाह ।।
निराकुलता एवं आकुलता ही धर्म और अधर्म की सीधी और साफ कसौटी है। जहाँ आकुलता है, तनाव है, असमाधि है वहाँ अधर्म है और जहाँ निराकुलता है, शान्ति है, समाधि है, वहाँ धर्म है। जिन बातों से व्यक्ति में अथवा उनके सामाजिक परिवेश में आकुलता बढ़ती है, तनाव पैदा होता है, अशान्ति बढ़ती है, विषमता बढ़ती है, वे
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org.