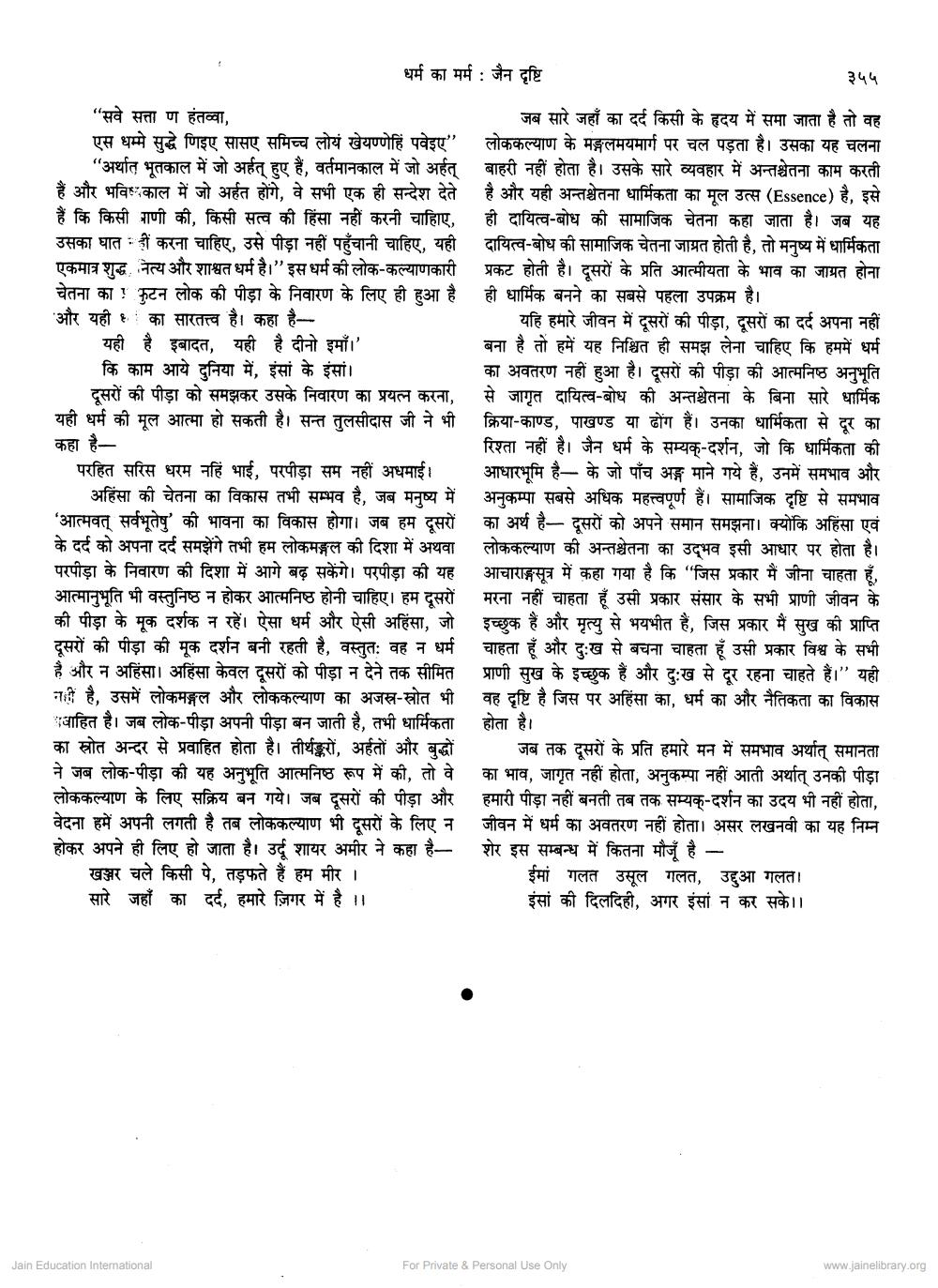________________
"सवे सत्ता ण हंतब्बा,
एस धम् सुद्धे णिइए सासए समिच्च लोयं खेयण्णेहिं पवेइए" "अर्थात भूतकाल में जो अर्हतु हुए हैं, वर्तमानकाल में जो अर्हत् और भविष्यकाल में जो अर्हत होंगे, वे सभी एक ही सन्देश देते हैं कि किसी वाणी की, किसी सत्व की हिंसा नहीं करनी चाहिए, उसका घात करना चाहिए, उसे पीड़ा नहीं पहुँचानी चाहिए. यही एकमात्र शुद्ध नित्य और शाश्वत धर्म है।" इस धर्म की लोक-कल्याणकारी चेतना का कुटन लोक की पीड़ा के निवारण के लिए ही हुआ है और यही का सारतत्त्व है। कहा है-
यही है इबादत, यही है दीनो इमाँ' कि काम आये दुनिया में, इंसां के इंसां ।
दूसरों की पीड़ा को समझकर उसके निवारण का प्रयत्न करना, यही धर्म की मूल आत्मा हो सकती है। सन्त तुलसीदास जी ने भी
कहा है
धर्म का मर्म जैन दृष्टि
:
परहित सरिस धरम नहिं भाई, परपीड़ा सम नहीं अधमाई।
अहिंसा की चेतना का विकास तभी सम्भव है, जब मनुष्य में 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की भावना का विकास होगा। जब हम दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझेंगे तभी हम लोकमङ्गल की दिशा में अथवा परपीड़ा के निवारण की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। परपीड़ा की यह आत्मानुभूति भी वस्तुनिष्ठ न होकर आत्मनिष्ठ होनी चाहिए। हम दूसरों की पीड़ा के मूक दर्शक न रहें। ऐसा धर्म और ऐसी अहिंसा, जो दूसरों की पीड़ा की मूक दर्शन बनी रहती है, वस्तुतः वह न धर्म है और न अहिंसा । अहिंसा केवल दूसरों को पीड़ा न देने तक सीमित नाई है, उसमें लोकमङ्गल और लोककल्याण का अजस्र स्रोत भी जाहित है जब लोक पीड़ा अपनी पीड़ा बन जाती है, तभी धार्मिकता का स्रोत अन्दर से प्रवाहित होता है। तीर्थङ्करों अहंतों और बुद्धों ने जब लोक पीड़ा की यह अनुभूति आत्मनिष्ठ रूप में की, तो वे लोककल्याण के लिए सक्रिय बन गये। जब दूसरों की पीड़ा और वेदना हमें अपनी लगती है तब लोककल्याण भी दूसरों के लिए न होकर अपने ही लिए हो जाता है। उर्दू शायर अमीर ने कहा हैखजर चले किसी पे, तड़फते हैं हम मीर । सारे जहाँ का दर्द, हमारे जिगर में है ।।
Jain Education International
जब सारे जहाँ का दर्द किसी के हृदय में समा जाता है तो वह लोककल्याण के मङ्गलमयमार्ग पर चल पड़ता है उसका यह चलना बाहरी नहीं होता है उसके सारे व्यवहार में अन्तक्षेतना काम करती है और यही अन्तश्चेतना धार्मिकता का मूल उत्स (Essence) है, इसे ही दायित्व बोध की सामाजिक चेतना कहा जाता है। जब यह दायित्व बोध की सामाजिक चेतना जाग्रत होती है, तो मनुष्य में धार्मिकता प्रकट होती है। दूसरों के प्रति आत्मीयता के भाव का जाग्रत होना ही धार्मिक बनने का सबसे पहला उपक्रम है।
यहि हमारे जीवन में दूसरों की पीड़ा, दूसरों का दर्द अपना नहीं बना है तो हमें यह निश्चित ही समझ लेना चाहिए कि हममें धर्म का अवतरण नहीं हुआ है। दूसरों की पीड़ा की आत्मनिष्ठ अनुभूति से जागृत दायित्व बोध की अन्तश्चेतना के बिना सारे धार्मिक क्रिया-काण्ड, पाखण्ड या ढोंग है उनका धार्मिकता से दूर का रिश्ता नहीं है। जैन धर्म के सम्यक् दर्शन, जो कि धार्मिकता की आधारभूमि है— के जो पाँच अङ्ग माने गये हैं, उनमें समभाव और अनुकम्पा सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। सामाजिक दृष्टि से समभाव का अर्थ है— दूसरों को अपने समान समझना। क्योंकि अहिंसा एवं लोककल्याण की अन्तश्चेतना का उदभव इसी आधार पर होता है। आचाराङ्गसूत्र में कहा गया है कि "जिस प्रकार में जीना चाहता हूँ, मरना नहीं चाहता हूँ उसी प्रकार संसार के सभी प्राणी जीवन के इच्छुक हैं और मृत्यु से भयभीत है, जिस प्रकार मैं सुख की प्राप्ति चाहता हूँ और दुःख से बचना चाहता हूँ उसी प्रकार विश्व के सभी प्राणी सुख के इच्छुक है और दुःख से दूर रहना चाहते हैं।" यही वह दृष्टि है जिस पर अहिंसा का धर्म का और नैतिकता का विकास होता है।
"
जब तक दूसरों के प्रति हमारे मन में समभाव अर्थात् समानता का भाव जागृत नहीं होता, अनुकम्पा नहीं आती अर्थात् उनकी पीड़ा हमारी पीड़ा नहीं बनती तब तक सम्यक् दर्शन का उदय भी नहीं होता, जीवन में धर्म का अवतरण नहीं होता। असर लखनवी का यह निम्न शेर इस सम्बन्ध में कितना मौजूं है
३५५
-
ईमां गलत उसूल गलत, उद्दुआ गलत। इंसां की दिलदिही, अगर इंसां न कर सके ।।
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org.