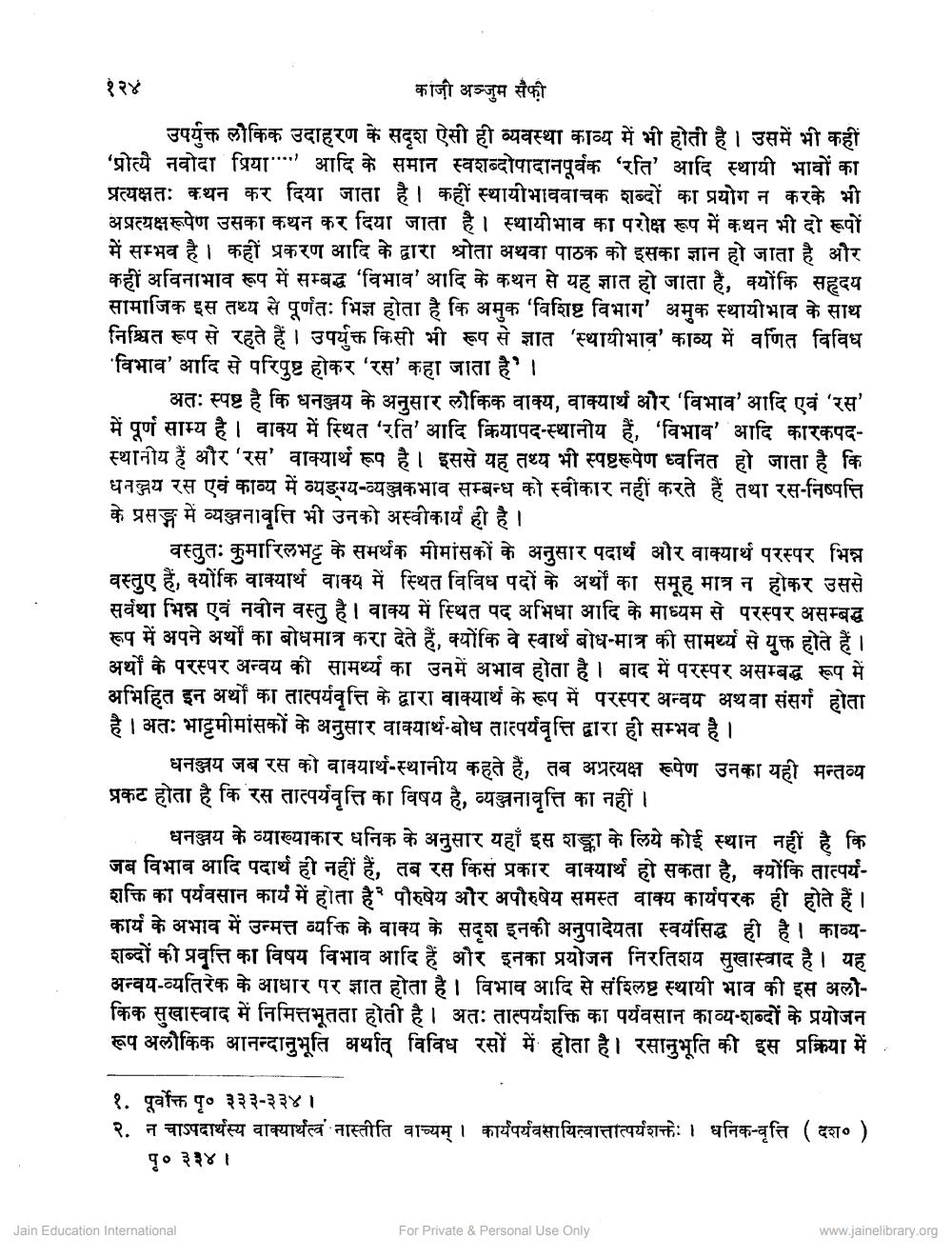________________ 124 काजी अजुम सैफी उपर्युक्त लौकिक उदाहरण के सदृश ऐसी ही व्यवस्था काव्य में भी होती है। उसमें भी कहीं 'प्रोत्यै नवोदा प्रिया...' आदि के समान स्वशब्दोपादानपूर्वक 'रति' आदि स्थायी भावों का प्रत्यक्षतः कथन कर दिया जाता है। कहीं स्थायीभाववाचक शब्दों का प्रयोग न करके भी अप्रत्यक्षरूपेण उसका कथन कर दिया जाता है। स्थायीभाव का परोक्ष रूप में कथन भी दो रूपों में सम्भव है। कहीं प्रकरण आदि के द्वारा श्रोता अथवा पाठक को इसका ज्ञान हो जाता है और कहीं अविनाभाव रूप में सम्बद्ध 'विभाव' आदि के कथन से यह ज्ञात हो जाता हैं, क्योंकि सहृदय सामाजिक इस तथ्य से पूर्णतः भिज्ञ होता है कि अमुक 'विशिष्ट विभाग' अमुक स्थायीभाव के साथ निश्चित रूप से रहते हैं। उपर्युक्त किसी भी रूप से ज्ञात 'स्थायीभाव' काव्य में वर्णित विविध 'विभाव' आदि से परिपुष्ट होकर 'रस' कहा जाता है। __ अतः स्पष्ट है कि धनञ्जय के अनुसार लौकिक वाक्य, वाक्यार्थ और 'विभाव' आदि एवं 'रस' में पूर्ण साम्य है। वाक्य में स्थित 'रति' आदि क्रियापद-स्थानीय हैं, "विभाव' आदि कारकपदस्थानीय हैं और 'रस' वाक्यार्थ रूप है। इससे यह तथ्य भी स्पष्टरूपेण ध्वनित हो जाता है कि धनन्जय रस एवं काव्य में व्यङ्ग्य-व्यञ्जकभाव सम्बन्ध को स्वीकार नहीं करते हैं तथा रस-निष्पत्ति के प्रसङ्ग में व्यञ्जनावृत्ति भी उनको अस्वीकार्य ही है। वस्तुतः कुमारिलभट्ट के समर्थक मीमांसकों के अनुसार पदार्थ और वाक्यार्थ परस्पर भिन्न वस्तुए हैं, क्योंकि वाक्यार्थ वाक्य में स्थित विविध पदों के अर्थों का समूह मात्र न होकर उससे सर्वथा भिन्न एवं नवीन वस्तु है। वाक्य में स्थित पद अभिधा आदि के माध्यम से परस्पर असम्बद्ध रूप में अपने अर्थों का बोधमात्र करा देते हैं, क्योंकि वे स्वार्थ बोध-मात्र की सामर्थ्य से युक्त होते हैं। अर्थों के परस्पर अन्वय की सामर्थ्य का उनमें अभाव होता है। बाद में परस्पर असम्बद्ध रूप में अभिहित इन अर्थों का तात्पर्यवृत्ति के द्वारा वाक्यार्थ के रूप में परस्पर अन्वय अथवा संसर्ग होता है / अतः भाट्टमीमांसकों के अनुसार वाक्यार्थ-बोध तात्पर्यवृत्ति द्वारा ही सम्भव है। धनञ्जय जब रस को वाक्यार्थ-स्थानीय कहते हैं, तब अप्रत्यक्ष रूपेण उनका यही मन्तव्य प्रकट होता है कि रस तात्पर्यवृत्ति का विषय है, व्यञ्जनावृत्ति का नहीं। .. धनञ्जय के व्याख्याकार धनिक के अनुसार यहाँ इस शङ्का के लिये कोई स्थान नहीं है कि जब विभाव आदि पदार्थ ही नहीं हैं, तब रस किस प्रकार वाक्यार्थ हो सकता है, क्योंकि तात्पर्यशक्ति का पर्यवसान कार्य में होता है। पौरुषेय और अपौरुषेय समस्त वाक्य कार्यपरक ही होते हैं / कार्य के अभाव में उन्मत्त व्यक्ति के वाक्य के सदृश इनकी अनुपादेयता स्वयंसिद्ध ही है। काव्यशब्दों की प्रवृत्ति का विषय विभाव आदि हैं और इनका प्रयोजन निरतिशय सुखास्वाद है। यह अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर ज्ञात होता है। विभाव आदि से संश्लिष्ट स्थायी भाव की इस अलोकिक सुखास्वाद में निमित्तभूतता होती है। अतः तात्पर्यशक्ति का पर्यवसान काव्य-शब्दों के प्रयोजन रूप अलौकिक आनन्दानुभूति अर्थात् विविध रसों में होता है। रसानुभूति की इस प्रक्रिया में . 1. पूर्वोक्त पृ० 333-334 / 2. न चापदार्थस्य वाक्यार्थत्वं नास्तीति वाच्यम् / कार्यपर्यवसायित्वात्तात्पर्यशक्तः। धनिक-वृत्ति (दश०) पृ० 334 / Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org