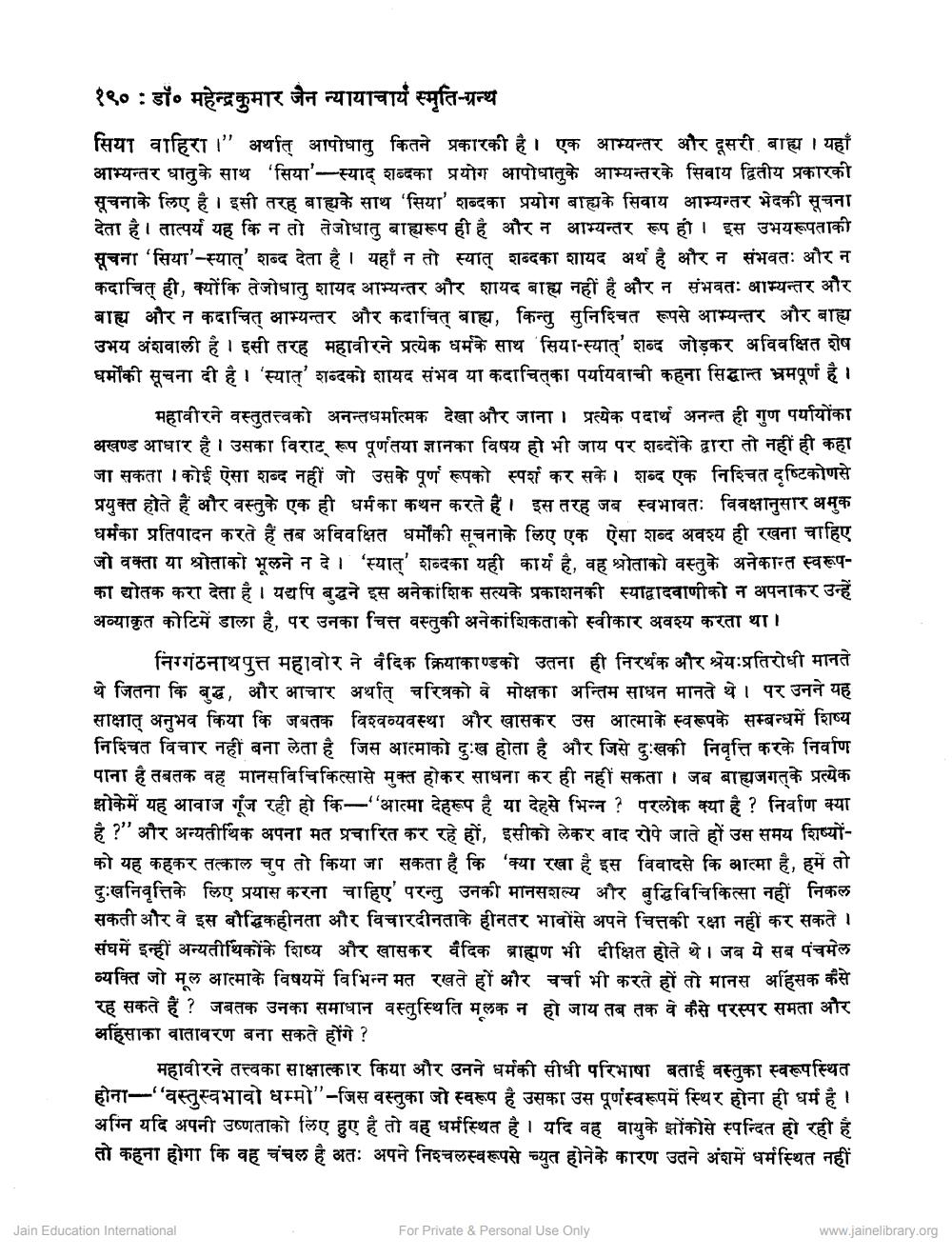________________
१९० : डॉ. महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ सिया वाहिरा।" अर्थात् आपोधातु कितने प्रकारकी है। एक आभ्यन्तर और दूसरी बाह्य । यहाँ आभ्यन्तर धातुके साथ 'सिया' स्याद् शब्दका प्रयोग आपोधातुके आभ्यन्तरके सिवाय द्वितीय प्रकारकी सूचनाके लिए है। इसी तरह बाह्यके साथ 'सिया' शब्दका प्रयोग बाह्यके सिवाय आभ्यन्तर भेदकी सूचना देता है । तात्पर्य यह कि न तो तेजोधातु बाह्यरूप ही है और न आभ्यन्तर रूप ही। इस उभयरूपताकी सूचना ‘सिया'-स्यात्' शब्द देता है। यहाँ न तो स्यात् शब्दका शायद अर्थ है और न संभवतः और न कदाचित ही, क्योंकि तेजोधातु शायद आभ्यन्तर और शायद बाह्य नहीं है और न संभवतः आभ्यन्तर और बाह्य और न कदाचित आभ्यन्तर और कदाचित् बाह्य, किन्तु सुनिश्चित रूपसे आभ्यन्तर और बाह्य उभय अंशवाली है । इसी तरह महावीरने प्रत्येक धर्मके साथ सिया-स्यात्' शब्द जोड़कर अविवक्षित शेष धर्मोकी सूचना दी है। 'स्यात्' शब्दको शायद संभव या कदाचितका पर्यायवाची कहना सिद्धान्त भ्रमपूर्ण है।
महावीरने वस्तुतत्त्वको अनन्तधर्मात्मक देखा और जाना। प्रत्येक पदार्थ अनन्त ही गुण पर्यायोंका अखण्ड आधार है । उसका विराट रूप पूर्णतया ज्ञानका विषय हो भी जाय पर शब्दोंके द्वारा तो नहीं ही कहा जा सकता । कोई ऐसा शब्द नहीं जो उसके पूर्ण रूपको स्पर्श कर सके। शब्द एक निश्चित दृष्टिकोणसे प्रयुक्त होते हैं और वस्तुके एक ही धर्मका कथन करते हैं। इस तरह जब स्वभावतः विवक्षानुसार अमुक धर्मका प्रतिपादन करते हैं तब अविवक्षित धर्मोंकी सूचनाके लिए एक ऐसा शब्द अवश्य ही रखना चाहिए जो वक्ता या श्रोताको भूलने न दे। 'स्यात्' शब्दका यही कार्य है, वह श्रोताको वस्तुके अनेकान्त स्वरूपका द्योतक करा देता है । यद्यपि बद्धने इस अनेकांशिक सत्यके प्रकाशनकी स्याद्वादवाणीको न अपनाकर उन्हें अव्याकृत कोटिमें डाला है, पर उनका चित्त वस्तुकी अनेकांशिकताको स्वीकार अवश्य करता था।
निग्गंठनाथपुत्त महावोर ने वैदिक क्रियाकाण्डको उतना ही निरर्थक और श्रेयःप्रतिरोधी मानते थे जितना कि बुद्ध, और आचार अर्थात् चरित्रको वे मोक्षका अन्तिम साधन मानते थे। पर उनने यह साक्षात् अनुभव किया कि जबतक विश्वव्यवस्था और खासकर उस आत्माके स्वरूपके सम्बन्धमें शिष्य निश्चित विचार नहीं बना लेता है जिस आत्माको दुःख होता है और जिसे दुःखकी निवृत्ति करके निर्वाण पाना है तबतक वह मानसविचिकित्सासे मुक्त होकर साधना कर ही नहीं सकता। जब बाह्यजगत्के प्रत्येक झोकेमें यह आवाज गूंज रही हो कि-"आत्मा देहरूप है या देहसे भिन्न? परलोक क्या है ? निर्वाण क्या है ?" और अन्यतीथिक अपना मत प्रचारित कर रहे हों, इसीको लेकर वाद रोपे जाते हों उस समय शिष्योंको यह कहकर तत्काल चुप तो किया जा सकता है कि 'क्या रखा है इस विवादसे कि आत्मा है, हमें तो दुःखनिवृत्तिके लिए प्रयास करना चाहिए' परन्तु उनकी मानसशल्य और बुद्धिविचिकित्सा नहीं निकल सकती और वे इस बौद्धिकहीनता और विचारदीनताके हीनतर भावोंसे अपने चित्तकी रक्षा नहीं कर सकते । संघमें इन्हीं अन्यतीथिकोंके शिष्य और खासकर वैदिक ब्राह्मण भी दीक्षित होते थे। जब ये सब पंचमेल व्यक्ति जो मूल आत्माके विषयमें विभिन्न मत रखते हों और चर्चा भी करते हों तो मानस अहिंसक कैसे रह सकते हैं ? जबतक उनका समाधान वस्तुस्थिति मलक न हो जाय तब तक वे कैसे परस्पर समता और अहिंसाका वातावरण बना सकते होंगे?
महावीरने तत्त्वका साक्षात्कार किया और उनने धर्मकी सीधी परिभाषा बताई वस्तुका स्वरूपस्थित होना-"वस्तुस्वभावो धम्मो"-जिस वस्तुका जो स्वरूप है उसका उस पूर्णस्वरूपमें स्थिर होना ही धर्म है। अग्नि यदि अपनी उष्णताको लिए हुए है तो वह धर्मस्थित है। यदि वह वायुके झोंकोसे स्पन्दित हो रही है तो कहना होगा कि वह चंचल है अतः अपने निश्चलस्वरूपसे च्यत होनेके कारण उतने अंशमें धर्मस्थित नहीं
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org