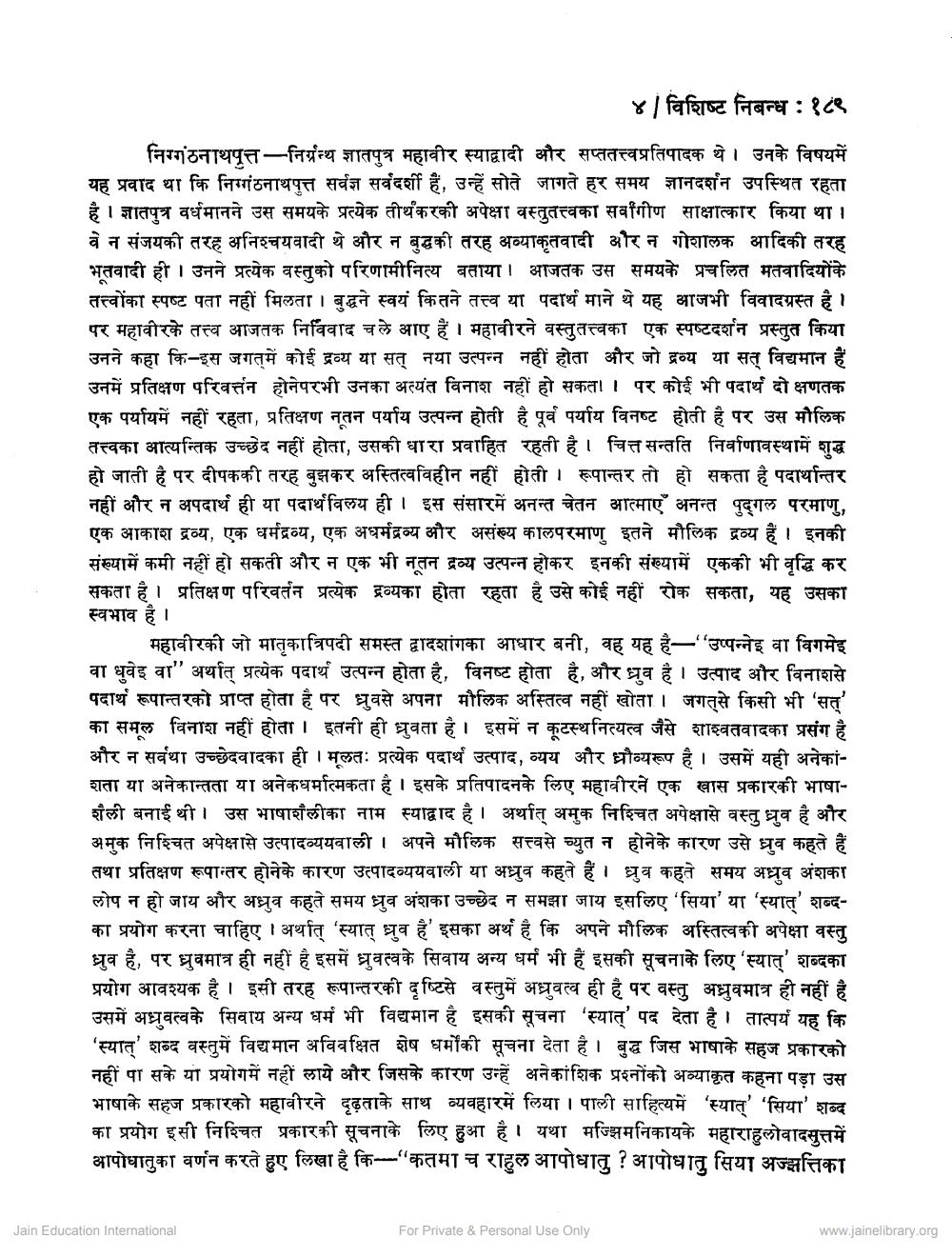________________
४/ विशिष्ट निबन्ध : १८९
निग्गंठनाथपूत्त-निर्ग्रन्थ ज्ञातपुत्र महावीर स्याद्वादी और सप्ततत्त्वप्रतिपादक थे। उनके विषयमें यह प्रवाद था कि निग्गंठनाथपुत्त सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, उन्हें सोते जागते हर समय ज्ञानदर्शन उपस्थित रहता है। ज्ञातपुत्र वर्धमानने उस समयके प्रत्येक तीर्थंकरकी अपेक्षा वस्तुतत्त्वका सर्वांगीण साक्षात्कार किया था। वे न संजयकी तरह अनिश्चयवादी थे और न बुद्धकी तरह अव्याकृतवादी और न गोशालक आदिकी तरह भतवादी ही। उनने प्रत्येक वस्तुको परिणामीनित्य बताया। आजतक उस समयके प्रचलित मतवादियोंके तत्त्वोंका स्पष्ट पता नहीं मिलता। बुद्धने स्वयं कितने तत्त्व या पदार्थ माने थे यह आजभी विवादग्रस्त है। पर महावीरके तत्त्व आजतक निर्विवाद चले आए हैं। महावीरने वस्तुतत्त्वका एक स्पष्टदर्शन प्रस्तुत किया उनने कहा कि-इस जगत्में कोई द्रव्य या सत् नया उत्पन्न नहीं होता और जो द्रव्य या सत् विद्यमान है उनमें प्रतिक्षण परिवर्तन होनेपरभी उनका अत्यंत विनाश नहीं हो सकत।। पर कोई भी पदार्थ दो क्षणतक एक पर्यायमें नहीं रहता, प्रतिक्षण नतन पर्याय उत्पन्न होती है पूर्व पर्याय विनष्ट होती है पर उस मौलिक तत्त्वका आत्यन्तिक उच्छेद नहीं होता, उसकी धारा प्रवाहित रहती है। चित्त सन्तति निर्वाणावस्थामें शुद्ध हो जाती है पर दीपककी तरह बुझकर अस्तित्वविहीन नहीं होती। रूपान्तर तो हो सकता है पदार्थान्तर नहीं और न अपदार्थ ही या पदार्थविलय ही। इस संसारमें अनन्त चेतन आत्माएँ अनन्त पुद्गल परमाणु, एक आकाश द्रव्य, एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य और असंख्य कालपरमाणु इतने मौलिक द्रव्य हैं। इनकी संख्यामें कमी नहीं हो सकती और न एक भी नतन द्रव्य उत्पन्न होकर इनकी संख्या एककी भी वृद्धि कर सकता है। प्रतिक्षण परिवर्तन प्रत्येक द्रव्यका होता रहता है उसे कोई नहीं रोक सकता, यह उसका स्वभाव है।
महावीरकी जो मातृकात्रिपदी समस्त द्वादशांगका आधार बनी, वह यह है-"उप्पन्नेइ वा विगमेइ वा धुवेइ वा" अर्थात् प्रत्येक पदार्थ उत्पन्न होता है, विनष्ट होता है, और ध्रुव है । उत्पाद और विनाशसे पदार्थ रूपान्तरको प्राप्त होता है पर ध्रुवसे अपना मौलिक अस्तित्व नहीं खोता। जगत्से किसी भी 'सत्' का समल विनाश नहीं होता। इतनी ही ध्रुवता है। इसमें न कूटस्थनित्यत्व जैसे शाश्वतवादका प्रसंग है और न सर्वथा उच्छेदवादका ही । मूलतः प्रत्येक पदार्थ उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यरूप है। उसमें यही अनेकांशता या अनेकान्तता या अनेकधर्मात्मकता है । इसके प्रतिपादनके लिए महावीरने एक खास प्रकारकी भाषाशैली बनाई थी। उस भाषाशैलीका नाम स्याद्वाद है। अर्थात् अमुक निश्चित अपेक्षासे वस्तु ध्रव है और अमुक निश्चित अपेक्षासे उत्पादव्ययवाली । अपने मौलिक सत्त्वसे च्युत न होनेके कारण उसे ध्रुव कहते हैं तथा प्रतिक्षण रूपान्तर होनेके कारण उत्पादव्ययवाली या अध्रुव कहते हैं। ध्रुव कहते समय अध्रुव अंशका लोप न हो जाय और अध्रुव कहते समय ध्रुव अंशका उच्छेद न समझा जाय इसलिए 'सिया' या 'स्यात्' शब्दका प्रयोग करना चाहिए । अर्थात् 'स्यात् ध्रुव है' इसका अर्थ है कि अपने मौलिक अस्तित्वकी अपेक्षा वस्तु ध्रुव है, पर ध्रुवमात्र ही नहीं है इसमें ध्रुवत्वके सिवाय अन्य धर्म भी हैं इसकी सूचनाके लिए 'स्यात्' शब्दका प्रयोग आवश्यक है। इसी तरह रूपान्तरकी दृष्टिसे वस्तुमें अध्रुवत्व ही है पर वस्तु अध्रुवमात्र ही नहीं है उसमें अध्रुवत्वके सिवाय अन्य धर्म भी विद्यमान है इसकी सूचना 'स्यात्' पद देता है। तात्पर्य यह कि 'स्यात्' शब्द वस्तुमें विद्यमान अविवक्षित शेष धर्मोंकी सूचना देता है। बुद्ध जिस भाषाके सहज प्रकारको नहीं पा सके या प्रयोगमें नहीं लाये और जिसके कारण उन्हें अनेकांशिक प्रश्नोंको अव्याकृत कहना पड़ा उस भाषाके सहज प्रकारको महावीरने दृढ़ताके साथ व्यवहारमें लिया । पाली साहित्यमें 'स्यात' 'सिया' शब्द का प्रयोग इसी निश्चित प्रकारकी सूचनाके लिए हुआ है। यथा मज्झिमनिकायके महाराहलोवादसूत्तमें आपोधातुका वर्णन करते हुए लिखा है कि-"कतमा च राहुल आपोधातु ? आपोधातु सिया अज्झत्तिका
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org