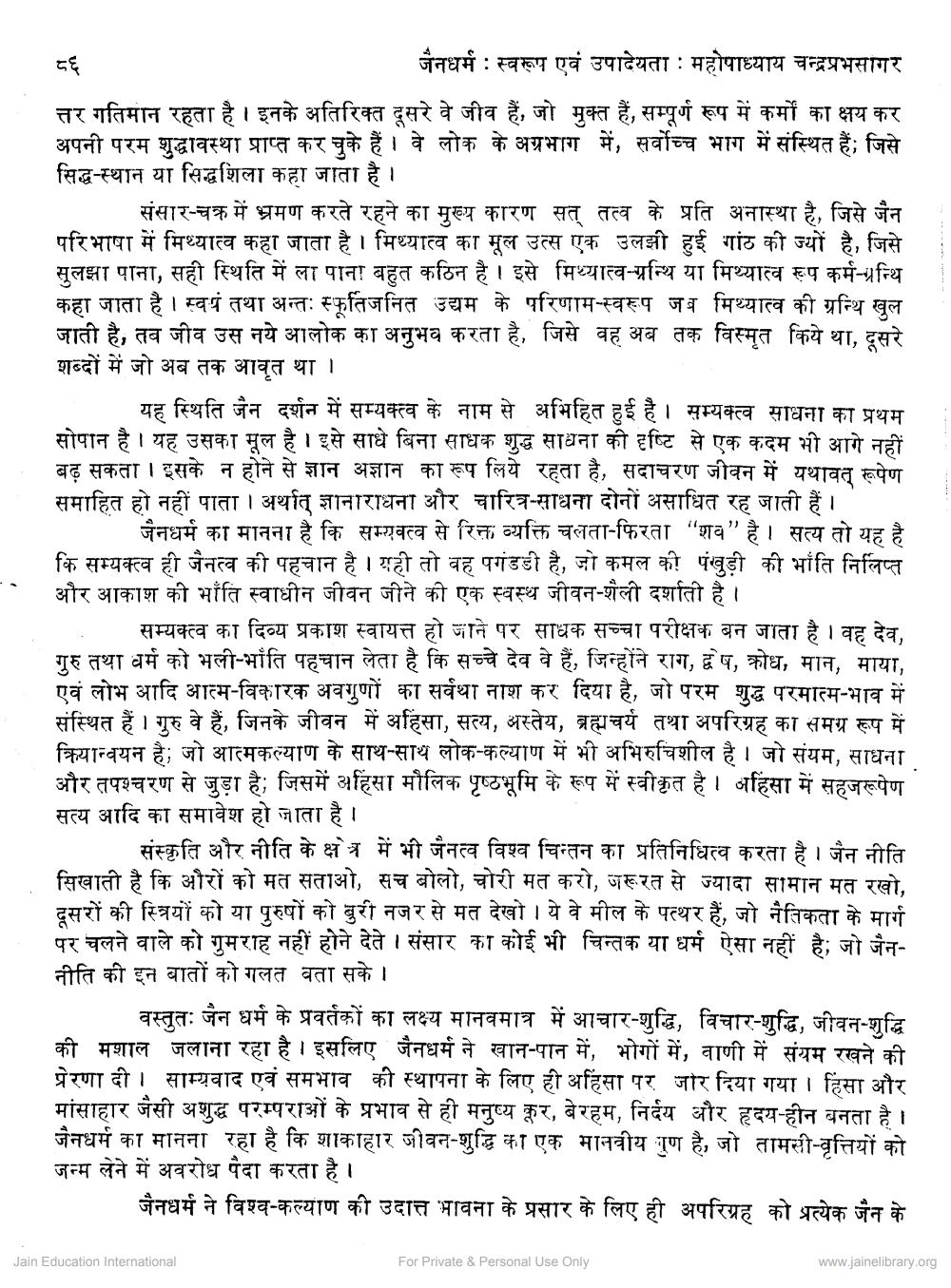________________
जैनधर्म : स्वरूप एवं उपादेयता : महोपाध्याय चन्द्रप्रभसागर तर गतिमान रहता है । इनके अतिरिक्त दूसरे वे जीव हैं, जो मुक्त हैं, सम्पूर्ण रूप में कर्मों का क्षय कर अपनी परम शुद्धावस्था प्राप्त कर चुके हैं। वे लोक के अग्रभाग में, सर्वोच्च भाग में संस्थित हैं; जिसे सिद्ध-स्थान या सिद्धशिला कहा जाता है।
संसार-चक्र में भ्रमण करते रहने का मुख्य कारण सत् तत्व के प्रति अनास्था है, जिसे जैन परिभाषा में मिथ्यात्व कहा जाता है । मिथ्यात्व का मूल उत्स एक उलझी हुई गांठ की ज्यों है, जिसे सुलझा पाना, सही स्थिति में ला पाना बहुत कठिन है। इसे मिथ्यात्व-ग्रन्थि या मिथ्यात्व रूप कर्म-ग्रन्थि कहा जाता है। स्वयं तथा अन्तः स्फूर्तिजनित उद्यम के परिणाम स्वरूप जब मिथ्यात्व की ग्रन्थि खुल जाती है, तब जीव उस नये आलोक का अनुभव करता है, जिसे वह अब तक विस्मत किये था. दसरे शब्दों में जो अब तक आवृत था ।
___ यह स्थिति जैन दर्शन में सम्यक्त्व के नाम से अभिहित हुई है। सम्यक्त्व साधना का प्रथम सोपान है । यह उसका मूल है । इसे साधे बिना साधक शुद्ध साधना की दृष्टि से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता । इसके न होने से ज्ञान अज्ञान का रूप लिये रहता है, सदाचरण जीवन में यथावत् रूपेण समाहित हो नहीं पाता । अर्थात् ज्ञानाराधना और चारित्र-साधना दोनों असाधित रह जाती हैं।
जैनधर्म का मानना है कि सम्यवत्व से रिक्त व्यक्ति चलता-फिरता "शव" है। सत्य तो यह है कि सम्यक्त्व ही जैनत्व की पहचान है । यही तो वह पगंडडी है, जो कमल की पंखुड़ी की भाँति निलिप्त और आकाश की भाँति स्वाधीन जीवन जीने की एक स्वस्थ जीवन-शैली दर्शाती है।
सम्यक्त्व का दिव्य प्रकाश स्वायत्त हो जाने पर साधक सच्चा परीक्षक बन जाता है । वह देव, गुरु तथा धर्म को भली-भाँति पहचान लेता है कि सच्चे देव वे हैं, जिन्होंने राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, एवं लोभ आदि आत्म-विकारक अवगुणों का सर्वथा नाश कर दिया है, जो परम शुद्ध परमात्म-भाव में संस्थित हैं । गुरु वे हैं, जिनके जीवन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह का समग्र रूप में क्रियान्वयन है; जो आत्मकल्याण के साथ-साथ लोक-कल्याण में भी अभिरुचिशील है। जो संयम, साधना
और तपश्चरण से जुड़ा है; जिसमें अहिंसा मौलिक पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकृत है। अहिंसा में सहजरूपेण सत्य आदि का समावेश हो जाता है ।
संस्कृति और नीति के क्षेत्र में भी जैनत्व विश्व चिन्तन का प्रतिनिधित्व करता है । जैन नीति सिखाती है कि औरों को मत सताओ, सच बोलो, चोरी मत करो, जरूरत से ज्यादा सामान मत रखो, दूसरों की स्त्रियों को या पुरुषों को बुरी नजर से मत देखो । ये वे मील के पत्थर हैं, जो नैतिकता के मार्ग पर चलने वाले को गुमराह नहीं होने देते । संसार का कोई भी चिन्तक या धर्म ऐसा नहीं है; जो जैननीति की इन बातों को गलत बता सके ।
वस्तुतः जैन धर्म के प्रवर्तकों का लक्ष्य मानवमात्र में आचार-शुद्धि, विचार-शुद्धि, जीवन-शुद्धि की मशाल जलाना रहा है। इसलिए जैनधर्म ने खान-पान में, भोगों में, वाणी में संयम रखने की प्रेरणा दी। साम्यवाद एवं समभाव की स्थापना के लिए ही अहिंसा पर जोर दिया गया। हिंसा और मांसाहार जैसी अशुद्ध परम्पराओं के प्रभाव से ही मनुष्य कूर, बेरहम, निर्दय और हृदय-हीन बनता है। जैनधर्म का मानना रहा है कि शाकाहार जीवन-शुद्धि का एक मानवीय गुण है, जो तामसी-वृत्तियों को जन्म लेने में अवरोध पैदा करता है।
जैनधर्म ने विश्व-कल्याण की उदात्त भावना के प्रसार के लिए ही अपरिग्रह को प्रत्येक जैन के
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org