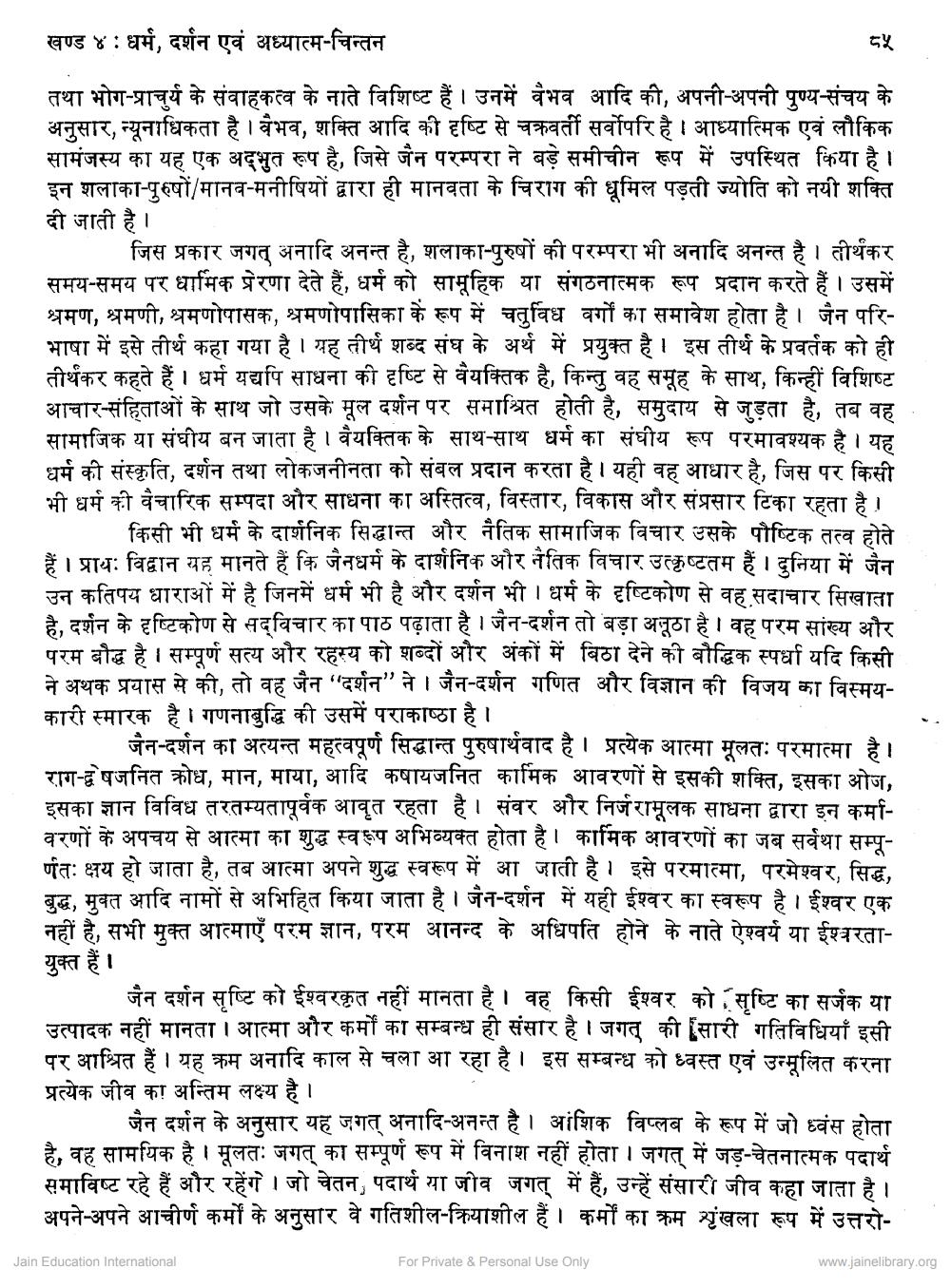________________
खण्ड ४ : धर्म, दर्शन एवं अध्यात्म-चिन्तन
तथा भोग-प्राचुर्य के संवाहकत्व के नाते विशिष्ट हैं। उनमें वैभव आदि की, अपनी-अपनी पुण्य-संचय के अनुसार, न्यूनाधिकता है । वैभव, शक्ति आदि की दृष्टि से चक्रवर्ती सर्वोपरि है । आध्यात्मिक एवं लौकिक सामंजस्य का यह एक अद्भुत रूप है, जिसे जैन परम्परा ने बड़े समीचीन रूप में उपस्थित किया है। इन शलाका-पुरुषों/मानव-मनीषियों द्वारा ही मानवता के चिराग की धूमिल पड़ती ज्योति को नयी शक्ति दी जाती है।
जिस प्रकार जगत् अनादि अनन्त है, शलाका-पुरुषों की परम्परा भी अनादि अनन्त है। तीर्थंकर समय-समय पर धार्मिक प्रेरणा देते हैं, धर्म को सामूहिक या संगठनात्मक रूप प्रदान करते हैं । उसमें श्रमण, श्रमणी, श्रमणोपासक, श्रमणोपासिका के रूप में चतुर्विध वर्गों का समावेश होता है। जैन परिभाषा में इसे तीर्थ कहा गया है । यह तीर्थ शब्द संघ के अर्थ में प्रयुक्त है। इस तीर्थ के प्रवर्तक को ही तीर्थंकर कहते हैं । धर्म यद्यपि साधना की दृष्टि से वैयक्तिक है, किन्तु वह समूह के साथ, किन्हीं विशिष्ट आचार-संहिताओं के साथ जो उसके मूल दर्शन पर समाश्रित होती है, समुदाय से जुड़ता है, तब वह सामाजिक या संघीय बन जाता है । वैयक्तिक के साथ-साथ धर्म का संघीय रूप परमावश्यक है। यह धर्म की संस्कृति, दर्शन तथा लोकजनीनता को संबल प्रदान करता है। यही वह आधार है, जिस पर किसी भी धर्म की वैचारिक सम्पदा और साधना का अस्तित्व, विस्तार, विकास और संप्रसार टिका रहता है।
किसी भी धर्म के दार्शनिक सिद्धान्त और नैतिक सामाजिक विचार उसके पौष्टिक तत्व होते हैं। प्रायः विद्वान यह मानते हैं कि जैनधर्म के दार्शनिक और नैतिक विचार उत्कृष्टतम हैं। दुनिया में जैन उन कतिपय धाराओं में है जिनमें धर्म भी है और दर्शन भी । धर्म के दृष्टिकोण से वह सदाचार सिखाता कै. दर्शन के दृष्टिकोण से सदविचार का पाठ पढ़ाता है । जैन-दर्शन तो बड़ा अनूठा है । वह परम सांख्य और परम बौद्ध है । सम्पूर्ण सत्य और रहस्य को शब्दों और अंकों में बिठा देने की बौद्धिक स्पर्धा यदि किसी ने अथक प्रयास से की, तो वह जैन "दर्शन" ने । जैन-दर्शन गणित और विज्ञान की विजय का विस्मयकारी स्मारक है । गणनाबुद्धि की उसमें पराकाष्ठा है।
जैन-दर्शन का अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्धान्त पुरुषार्थवाद है। प्रत्येक आत्मा मूलतः परमात्मा है। राग-द्वेषजनित क्रोध, मान, माया, आदि कषायजनित कार्मिक आवरणों से इसकी शक्ति, इसका ओज, इसका ज्ञान विविध तरतम्यतापूर्वक आवृत रहता है। संवर और निर्जरामूलक साधना द्वारा इन कर्मावरणों के अपचय से आत्मा का शुद्ध स्वरूप अभिव्यक्त होता है। कार्मिक आवरणों का जब सर्वथा सम्पर्णतः क्षय हो जाता है, तब आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाती है। इसे परमात्मा, परमेश्वर, सिद्ध, बुद्ध, मुक्त आदि नामों से अभिहित किया जाता है । जैन-दर्शन में यही ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर एक नहीं है, सभी मुक्त आत्माएँ परम ज्ञान, परम आनन्द के अधिपति होने के नाते ऐश्वर्य या ईश्वरतायुक्त हैं।
जैन दर्शन सष्टि को ईश्वरकृत नहीं मानता है। वह किसी ईश्वर को सृष्टि का सर्जक या उत्पादक नहीं मानता । आत्मा और कर्मों का सम्बन्ध ही संसार है । जगत् की सारी गतिविधियाँ इसी पर आश्रित हैं । यह क्रम अनादि काल से चला आ रहा है। इस सम्बन्ध को ध्वस्त एवं उन्मूलित करना प्रत्येक जीव का अन्तिम लक्ष्य है।
जैन दर्शन के अनुसार यह जगत् अनादि-अनन्त है । आंशिक विप्लब के रूप में जो ध्वंस होता है, वह सामयिक है । मूलतः जगत् का सम्पूर्ण रूप में विनाश नहीं होता । जगत् में जड़-चेतनात्मक पदार्थ समाविष्ट रहे हैं और रहेंगे । जो चेतन, पदार्थ या जीव जगत् में हैं, उन्हें संसारी जीव कहा जाता है। अपने-अपने आचीर्ण कर्मों के अनुसार वे गतिशील-क्रियाशील हैं। कर्मों का क्रम शृंखला रूप में उत्तरो
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org