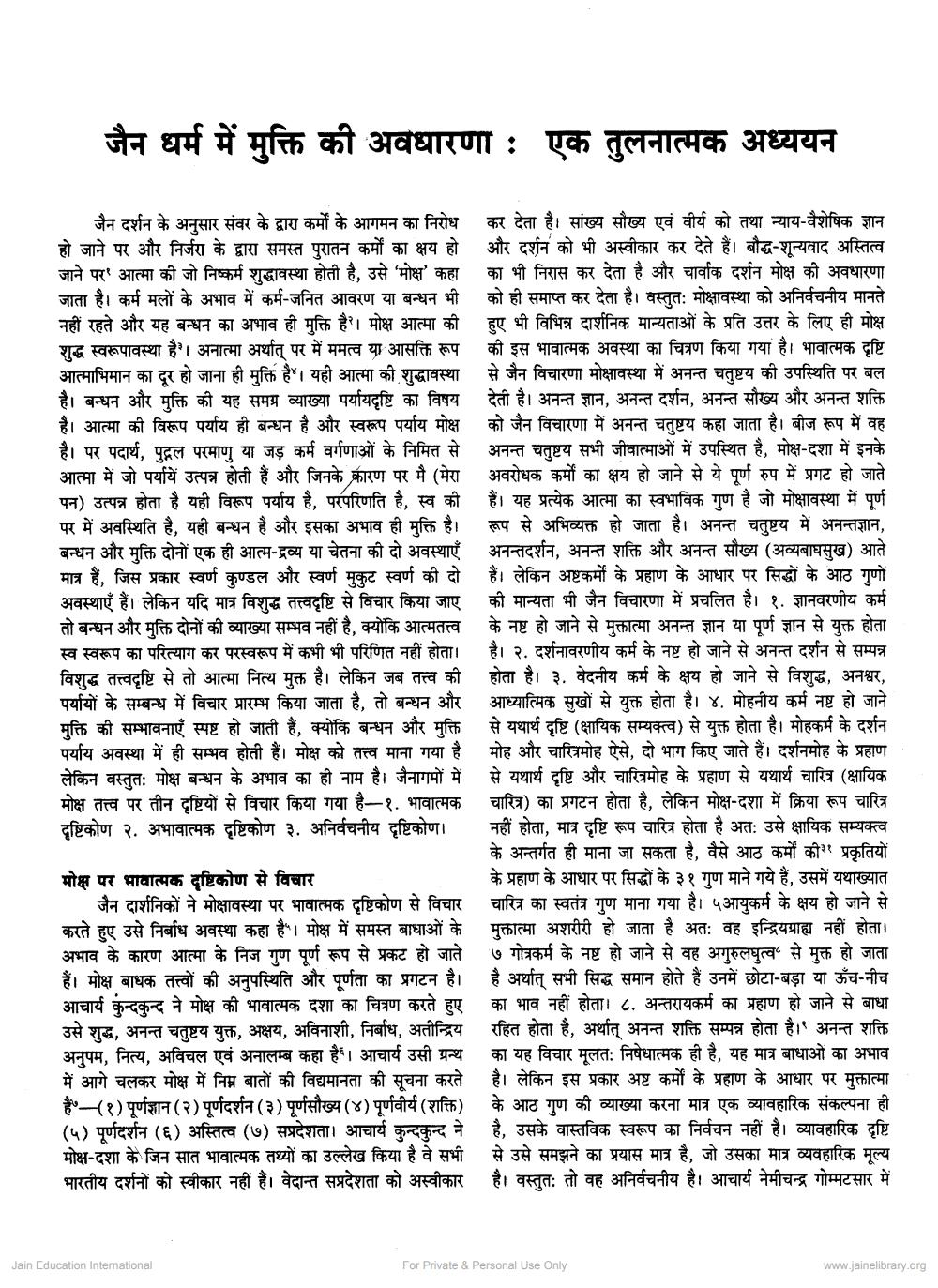________________
जैन धर्म में मुक्ति की अवधारणा एक तुलनात्मक अध्ययन
:
जैन दर्शन के अनुसार संवर के द्वारा कर्मों के आगमन का निरोध हो जाने पर और निर्जरा के द्वारा समस्त पुरातन कर्मों का क्षय हो जाने पर आत्मा की जो निष्कर्म शुद्धावस्था होती है, उसे 'मोक्ष' कहा जाता है। कर्म मलों के अभाव में कर्म-जनित आवरण या बन्धन भी नहीं रहते और यह बन्धन का अभाव ही मुक्ति है। मोक्ष आत्मा की शुद्ध स्वरूपावस्था है। अनात्मा अर्थात् पर में ममत्व या आसक्ति रूप आत्माभिमान का दूर हो जाना ही मुक्ति है । यही आत्मा की शुद्धावस्था है बन्धन और मुक्ति की यह समग्र व्याख्या पर्यायदृष्टि का विषय है। आत्मा की विरूप पर्याय ही बन्धन है और स्वरूप पर्याय मोक्ष है पर पदार्थ, पुगल परमाणु या जड़ कर्म वर्गणाओं के निमित्त से आत्मा में जो पर्याये उत्पन्न होती है और जिनके कारण पर मैं ( मेरा पन) उत्पन्न होता है यही विरूप पर्याय है, परपरिणति है, स्व की पर में अवस्थिति है, यही बन्धन है और इसका अभाव ही मुक्ति है। बन्धन और मुक्ति दोनों एक ही आत्म-द्रव्य या चेतना की दो अवस्थाएँ मात्र हैं, जिस प्रकार स्वर्ण कुण्डल और स्वर्ण मुकुट स्वर्ण की दो अवस्थाएँ हैं। लेकिन यदि मात्र विशुद्ध तत्त्वदृष्टि से विचार किया जाए तो बन्धन और मुक्ति दोनों की व्याख्या सम्भव नहीं है, क्योंकि आत्मतत्त्व स्व स्वरूप का परित्याग कर परस्वरूप में कभी भी परिणित नहीं होता। विशुद्ध तत्त्वदृष्टि से तो आत्मा नित्य मुक्त है। लेकिन जब तत्व की पर्यायों के सम्बन्ध में विचार प्रारम्भ किया जाता है, तो बन्धन और मुक्ति की सम्भावनाएँ स्पष्ट हो जाती हैं, क्योंकि बन्धन और मुक्ति पर्याय अवस्था में ही सम्भव होती हैं। मोक्ष को तत्त्व माना गया है लेकिन वस्तुतः मोक्ष बन्धन के अभाव का ही नाम है। जैनागमों में मोक्ष तत्त्व पर तीन दृष्टियों से विचार किया गया है - १. भावात्मक दृष्टिकोण २. अभावात्मक दृष्टिकोण ३. अनिर्वचनीय दृष्टिकोण |
मोक्ष पर भावात्मक दृष्टिकोण से विचार
जैन दार्शनिकों ने मोक्षावस्था पर भावात्मक दृष्टिकोण से विचार करते हुए उसे निर्बाध अवस्था कहा है। मोक्ष में समस्त बाधाओं के अभाव के कारण आत्मा के निज गुण पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं। मोक्ष बाधक तत्त्वों की अनुपस्थिति और पूर्णता का प्रगटन है। आचार्य कुन्दकुन्द ने मोक्ष की भावात्मक दशा का चित्रण करते हुए उसे शुद्ध, अनन्त चतुष्टय युक्त, अक्षय, अविनाशी, निर्बाध अतीन्द्रिय अनुपम, नित्य, अविचल एवं अनालम्ब कहा है। आचार्य उसी ग्रन्थ में आगे चलकर मोक्ष में निम्न बातों की विद्यमानता की सूचना करते हैं- (१) पूर्णज्ञान (२) पूर्णदर्शन (३) पूर्णसौख्य (४) पूर्णवीर्य (शक्ति) (५) पूर्णदर्शन (६) अस्तित्व (७) सप्रदेशता आचार्य कुन्दकुन्द ने । मोक्ष-दशा के जिन सात भावात्मक तथ्यों का उल्लेख किया है वे सभी भारतीय दर्शनों को स्वीकार नहीं हैं। वेदान्त सप्रदेशता को अस्वीकार
Jain Education International
कर देता है सांख्य सौख्य एवं वीर्य को तथा न्याय-वैशेषिक ज्ञान और दर्शन को भी अस्वीकार कर देते हैं। बौद्ध-शून्यवाद अस्तित्व का भी निरास कर देता है और चार्वाक दर्शन मोक्ष की अवधारणा को ही समाप्त कर देता है। वस्तुतः मोक्षावस्था को अनिर्वचनीय मानते हुए भी विभिन्न दार्शनिक मान्यताओं के प्रति उत्तर के लिए ही मोक्ष की इस भावात्मक अवस्था का चित्रण किया गया है। भावात्मक दृष्टि से जैन विचारणा मोक्षावस्था में अनन्त चतुष्टय की उपस्थिति पर बल देती है अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सौख्य और अनन्त शक्ति को जैन विचारणा में अनन्त चतुष्टय कहा जाता है। बीज रूप में वह अनन्त चतुष्टय सभी जीवात्माओं में उपस्थित है, मोक्ष- दशा में इनके अवरोधक कर्मों का क्षय हो जाने से ये पूर्ण रूप में प्रगट हो जाते हैं। यह प्रत्येक आत्मा का स्वभाविक गुण है जो मोक्षावस्था में पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हो जाता है। अनन्त चतुष्टय में अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्त शक्ति और अनन्त सौख्य (अव्यबाघसुख) आते है। लेकिन अष्टकर्मों के प्रहाण के आधार पर सिद्धों के आठ गुणों की मान्यता भी जैन विचारणा में प्रचलित है । १. ज्ञानवरणीय कर्म के नष्ट हो जाने से मुक्तात्मा अनन्त ज्ञान या पूर्ण ज्ञान से युक्त होता है। २. दर्शनावरणीय कर्म के नष्ट हो जाने से अनन्त दर्शन से सम्पन्न होता है। ३. वेदनीय कर्म के क्षय हो जाने से विशुद्ध, अनश्वर, आध्यात्मिक सुखों से युक्त होता है । ४. मोहनीय कर्म नष्ट हो जाने से यथार्थ दृष्टि ( क्षायिक सम्यक्त्व) से युक्त होता है। मोहकर्म के दर्शन मोह और चारित्रमोह ऐसे, दो भाग किए जाते हैं। दर्शनमोह के प्रहाण से यथार्थ दृष्टि और चारित्रमोह के प्राण से यथार्थ चारित्र ( क्षायिक चारित्र) का प्रगटन होता है, लेकिन मोक्ष-दशा में क्रिया रूप चारित्र नहीं होता, मात्र दृष्टि रूप चारित्र होता है अतः उसे क्षायिक सम्यक्त्व के अन्तर्गत ही माना जा सकता है, वैसे आठ कर्मों की प्रकृतियों के प्रहाण के आधार पर सिद्धों के ३१ गुण माने गये हैं, उसमें यथाख्या चारित्र का स्वतंत्र गुण माना गया है। ५ आयुकर्म के क्षय हो जाने से मुक्तात्मा अशरीरी हो जाता है अतः वह इन्द्रियग्राह्य नहीं होता। ७ गोत्रकर्म के नष्ट हो जाने से वह अगुरुलघुत्व से मुक्त हो जाता है अर्थात् सभी सिद्ध समान होते हैं उनमें छोटा-बड़ा या ऊँच-नीच का भाव नहीं होता। ८ अन्तरायकर्म का प्राण हो जाने से बाधा रहित होता है, अर्थात् अनन्त शक्ति सम्पन्न होता है।" अनन्त शक्ति का यह विचार मूलतः निषेधात्मक ही है, यह मात्र बाधाओं का अभाव है। लेकिन इस प्रकार अष्ट कर्मों के प्रहाण के आधार पर मुक्तात्मा के आठ गुण की व्याख्या करना मात्र एक व्यावहारिक संकल्पना ही है, उसके वास्तविक स्वरूप का निर्वाचन नहीं है। व्यावहारिक दृष्टि से उसे समझने का प्रयास मात्र है, जो उसका मात्र व्यवहारिक मूल्य है। वस्तुतः तो वह अनिर्वचनीय है। आचार्य नेमीचन्द्र गोम्मटसार में
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org.