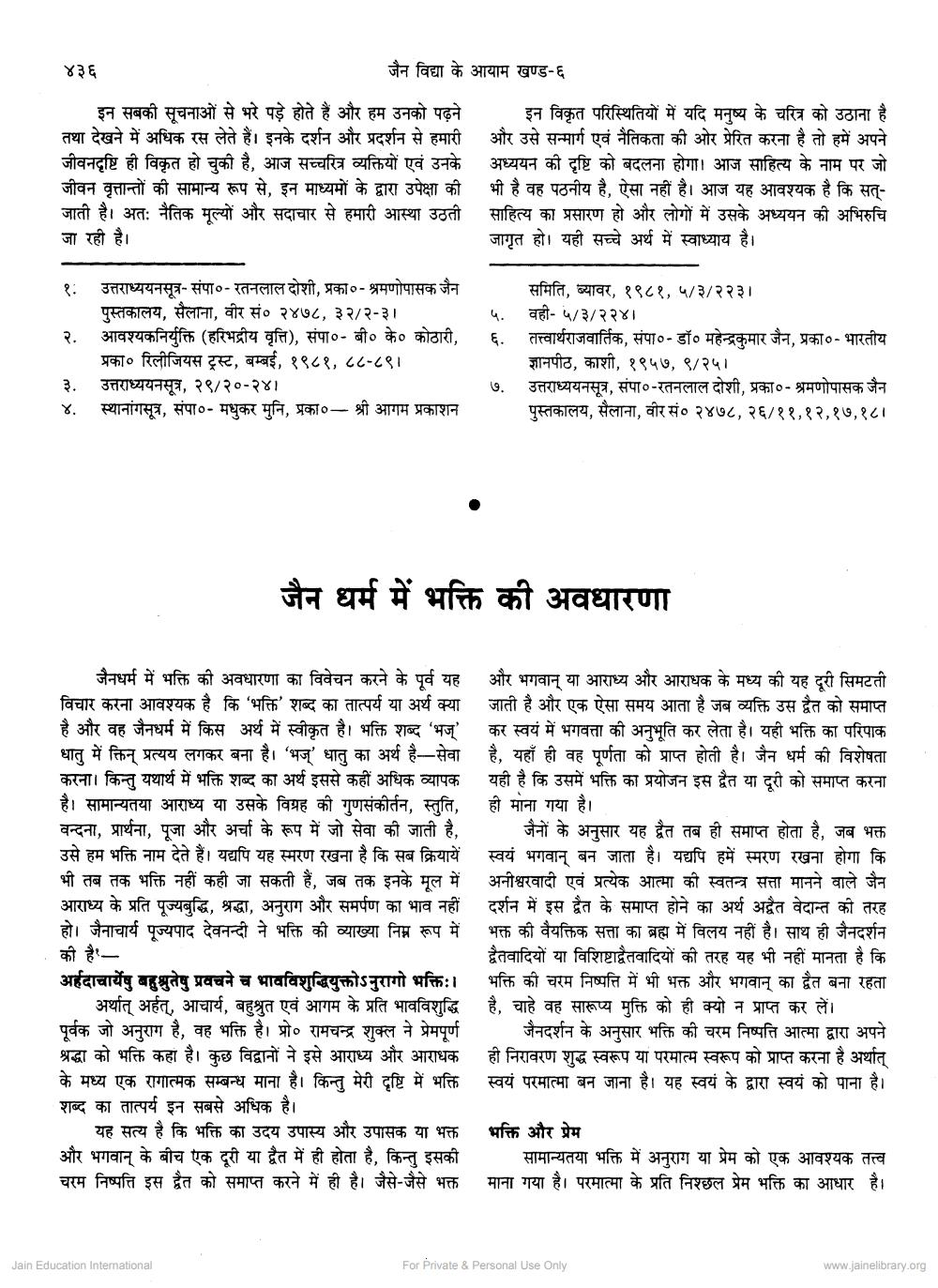________________
४३६
इन सबकी सूचनाओं से भरे पड़े होते हैं और हम उनको पढ़ने तथा देखने में अधिक रस लेते हैं। इनके दर्शन और प्रदर्शन से हमारी जीवनदृष्टि हो विकृत हो चुकी है, आज सच्चरित्र व्यक्तियों एवं उनके जीवन वृत्तान्तों की सामान्य रूप से, इन माध्यमों के द्वारा उपेक्षा की जाती है। अतः नैतिक मूल्यों और सदाचार से हमारी आस्था उठती जा रही है।
१.
२.
३.
४.
जैन विद्या के आयाम खण्ड ६
उत्तराध्ययनसूत्र- संपा० रतनलाल दोशी, प्रका०- श्रमणोपासक जैन पुस्तकालय, सैलाना, वीर सं० २४७८, ३२/२-३। आवश्यक नियुक्ति (हरिभद्रीय वृत्ति), संपा० बी० के० कोठारी, प्रका० रिलीजियस ट्रस्ट, बम्बई, १९८१, ८८-८९ । उत्तराध्ययनसूत्र २९ / २०-२४।
स्थानांगसूत्र, संपा०- मधुकर मुनि, प्रका०
श्री आगम प्रकाशन
जैनधर्म में भक्ति की अवधारणा का विवेचन करने के पूर्व यह विचार करना आवश्यक है कि 'भक्ति' शब्द का तात्पर्य या अर्थ क्या है और वह जैनधर्म में किस अर्थ में स्वीकृत है। भक्ति शब्द 'भज् धातु में क्तिन् प्रत्यय लगकर बना है। 'भज्' धातु का अर्थ है— सेवा करना । किन्तु यथार्थ में भक्ति शब्द का अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है। सामान्यतया आराध्य या उसके विग्रह की गुणसंकीर्तन, स्तुति, वन्दना, प्रार्थना, पूजा और अर्चा के रूप में जो सेवा की जाती है, उसे हम भक्ति नाम देते हैं। यद्यपि यह स्मरण रखना है कि सब क्रियायें भी तब तक भक्ति नहीं कही जा सकती हैं, जब तक इनके मूल में आराध्य के प्रति पूज्यबुद्धि, श्रद्धा, अनुराग और समर्पण का भाव नहीं हो जैनाचार्यं पूज्यपाद देवनन्दी ने भक्ति की व्याख्या निम्न रूप में की है—
अर्हदाचार्येषु बहुश्रुतेषु प्रवचने व भावविशुद्धियुक्तोऽनुरागो भक्तिः ।
अर्थात् अर्हत्, आचार्य, बहुश्रुत एवं आगम के प्रति भावविशुद्धि पूर्वक जो अनुराग है, वह भक्ति है। प्रो० रामचन्द्र शुक्ल ने प्रेमपूर्ण श्रद्धा को भक्ति कहा है। कुछ विद्वानों ने इसे आराध्य और आराधक के मध्य एक रागात्मक सम्बन्ध माना है। किन्तु मेरी दृष्टि में भक्ति शब्द का तात्पर्य इन सबसे अधिक है।
Jain Education International
यह सत्य है कि भक्ति का उदय उपास्य और उपासक या भक्त और भगवान् के बीच एक दूरी या द्वैत में ही होता है, किन्तु इसकी चरम निष्पत्ति इस द्वैत को समाप्त करने में ही है। जैसे-जैसे भक्त
इन विकृत परिस्थितियों में यदि मनुष्य के चरित्र को उठाना है और उसे सन्मार्ग एवं नैतिकता की ओर प्रेरित करना है तो हमें अपने अध्ययन की दृष्टि को बदलना होगा। आज साहित्य के नाम पर जो भी है वह पठनीय है, ऐसा नहीं है। आज यह आवश्यक है कि सत्साहित्य का प्रसारण हो और लोगों में उसके अध्ययन की अभिरुचि जागृत हो । यही सच्चे अर्थ में स्वाध्याय है।
५.
६.
७.
जैन धर्म में भक्ति की अवधारणा
समिति, ब्यावर, १९८१, ५/३/२२३। वही - ५/३/२२४।
तत्त्वार्थराजवार्तिक, संपा० डॉ० महेन्द्रकुमार जैन, प्रका०- भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९५७, ९/२५ ।
उत्तराध्ययनसूत्र, संपा० रतनलाल दोशी, प्रका०- श्रमणोपासक जैन पुस्तकालय, सैलाना, वीर सं० २४७८, २६ / ११, १२, १७, १८।
और भगवान् या आराध्य और आराधक के मध्य की यह दूरी सिमटती जाती है और एक ऐसा समय आता है जब व्यक्ति उस द्वैत को समाप्त कर स्वयं में भगवत्ता की अनुभूति कर लेता है। यही भक्ति का परिपाक है, यहाँ ही वह पूर्णता को प्राप्त होती है। जैन धर्म की विशेषता यही है कि उसमें भक्ति का प्रयोजन इस द्वैत या दूरी को समाप्त करना ही माना गया है।
जैनों के अनुसार यह द्वैत तब ही समाप्त होता है, जब भक्त स्वयं भगवान् बन जाता है। यद्यपि हमें स्मरण रखना होगा कि अनीश्वरवादी एवं प्रत्येक आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता मानने वाले जैन दर्शन में इस द्वैत के समाप्त होने का अर्थ अद्वैत वेदान्त की तरह भक्त की वैयक्तिक सत्ता का ब्रह्म में विलय नहीं है। साथ ही जैनदर्शन द्वैतवादियों या विशिष्टाद्वैतवादियों की तरह यह भी नहीं मानता है कि भक्ति की चरम निष्पत्ति में भी भक्त और भगवान् का द्वैत बना रहता है, चाहे वह सारूप्य मुक्ति को ही क्यो न प्राप्त कर लें।
जैनदर्शन के अनुसार भक्ति की चरम निष्पति आत्मा द्वारा अपने ही निरावरण शुद्ध स्वरूप या परमात्म स्वरूप को प्राप्त करना है अर्थात् स्वयं परमात्मा बन जाना है। यह स्वयं के द्वारा स्वयं को पाना है।
भक्ति और प्रेम
सामान्यतया भक्ति में अनुराग या प्रेम को एक आवश्यक तत्त्व माना गया है। परमात्मा के प्रति निश्छल प्रेम भक्ति का आधार है।
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org.